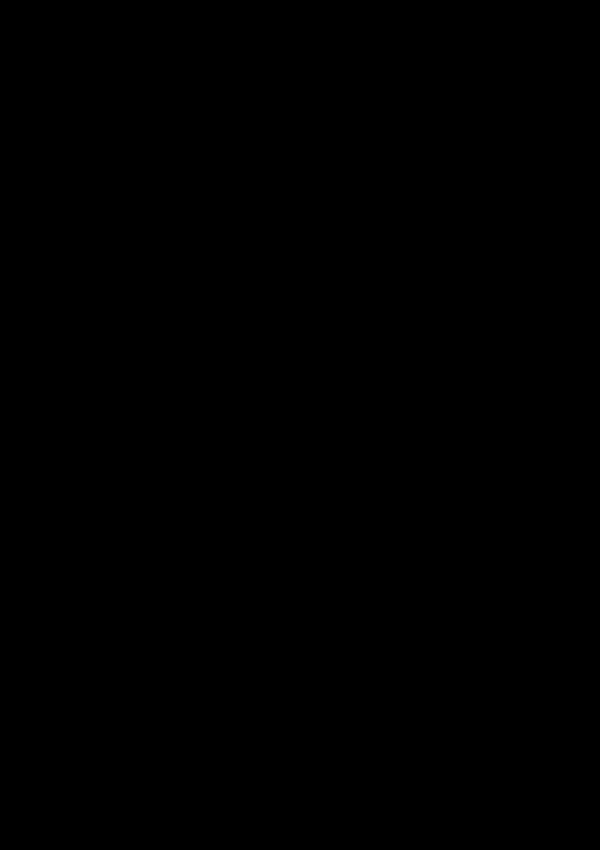मैं नदी मुखातिब हूँ
मैं नदी मुखातिब हूँ


आंखें खुली तो परबत की कोख पे
सूरज की उजाले,चंद की चांदनी में
पूछी परबत को अपनी नन्हीं तोतली में
क्या नीचे मैदान को जा सकती हूं मैं।
हंस कर बोला परबत-नहीं रख सकता तुझे
मंजिल तेरी सागर-उनपे जो तुझे सामना है
झर-झर, कल-कल संगीत की गूंज के साथ
उच्च-नीच राहों पर तुझे आगे जो चलना है।
परबत की कोखसे छलकी नीचे गिरी जमीन पर
धुआं धुआं से छह गयी, पेड़-पौधे घने जंगल में
आदमी हो या जानबर, चिड़िया हो या पतंग
पागल बन्दी सब को- अपनी ठंडक धारा की प्यार में।
फूलती गयी मेरी धार तो चलने लगी आहिस्ता
कितने अवाम,और सभ्यता,बसगये दोनों किनारे पे
अंदर ही अंदर झूम उठी, साथियां है मेटे कितने
अकेली नहीं हूँ में- ये सब जो मेरे अपने हैं।
पर पगली थी में जो इन लोगो और सभ्यता को
अपनी साथी मान गयी, झेल रही हूं हरदिन-हरपाल
पेड़ उजड़े, जंगल उजड़ा, बस कंक्रीटों की पडाब
रो रही हूँ अपने ही आप- ढाई कचरे की दल दल।
लूट रहे हैं भेड़ियों की तरह, सुख गयी तेज धार
कब तक झेलूंगी यह अत्यचार, इस सोच में पड़ी हूँ
सिमट गई हूँ किनारे पे, खींचते हैं खाल से फिरभी
कोई नहीं है अपनी, अपनों की हाय में लूट गयी हूँ।
किनारे पे सिमटी ईंतजार में, हूँ कि अछे दिन आएगी
हर वक़्त अंधेरा नहीं- उजाला भी होगा जरूर
तेजसे दौडूंगी कल कल फिर बसुंधरा पे
समझ जाओ तुम लोगो ने, बचना है तुम्हें अगर
बंद करो ये खिलबाड़े, फिरसे फूलना होगा जरूर।