शक़ की सुई
शक़ की सुई


यह सर्वविदित है कि शक़ वो 'बुरी बला' है, जो एक बसे-बसाए घर-संसार को नेस्तनाबूद कर देता है . ....और अजीब बात तो ये है कि जिस इंसान के दिमाग में 'शक़ की सुई' एक बार गलती से भी घूमना शुरू कर देती है, तो उसका 'सत्यानाश' होने से कोई नहीं बचा सकता -- चाहे वो कोई नारी अथवा पुरुष हो ।
शक़ एक ऐसी 'व्याधि' है, जो इंसानी दिल-ओ-दिमाग को दीमक की तरह चट जाता है और 'उस' शक्की इंसान को इस बात का इल्म ही नहीं होता ! और धीरे-धीरे उसका पूरा वजूद ही नष्ट हो जाता है ।
जो इंसान दीमागी तौर पर 'शक्की' होता है, वो हमेशा ही दुसरों में, दूसरों के काम करने के तरीकों में, भोजन करने के तरीकों में वगैरह वगैरह 'नुक्स' निकालकर ही दम लेता हैं ।
इसमें कोई दोराय नहीं कि 'शक्की' इंसान किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट हो ही नहीं पाता ! उसे इस बात का कभी तनिक भी एहसास नहीं होता कि उसके इस 'असहनीय-अशोभनीय' रवैये से दूसरों को कितनी तकलीफों और परेशानियों से गुज़रना पड़ता है...!
यही तो दु:खदायी मसला है, जो कि एक 'शक्की' इंसान की गलतफहमियों एवं भ्रांतियों की वजह से उसके घर में, समाज में, देश में और पूरे विश्व में एक 'त्रासदी-सा' परिवेश प्रस्तुत करता है, जिसका दुष्प्रभाव
उस विशेष घर में, उस समाज में, उस देश में और निस्संदेह अप्रत्यक्ष रूप में इस विश्व को भी प्रभावित करता है ।
इस परिपेक्ष्य में समाज के हर एक समान्य इंसान का ये परम 'दायित्व' बनता है कि वो एकजुटता एवं एकमत से विचार-विमर्श-मनन-चिंतन कर हमारे आस-पड़ोस की 'शक्की' इंसानों की शीघ्रातिशीघ्र पहचान कर, उनसे 'मानवीय संवेदनाओं एवं मानवीय मूल्यों' का सम्मान करते हुए उन्हें इस 'व्याधि' से सदा के लिए 'मुक्त' करने में अपना पूर्ण 'सहयोग' दें, अन्यथा, मसलन, न तो एक 'पति' सुख-चैन से जी सकता है और न ही एक 'पत्नी', क्योंकि 'शक़ की सुई' अक्सर उनकी आपसी तालमेल एवं "विश्वास की नींव" हिलाकर रख देती है।
निस्संदेह 'शक़ की सुई' तथाकथित 'प्रणय-सूत्र' में बंधे आज की ('जेट' युग की) आधुनिकता एवं अंधाधुंध भागमभाग भरी ज़िंदगी में अक्सर देखने को मिलता है, जो कि किसी के सुनहरे ख्वाबों-ख्वाहिशों की दुनिया में अनाकांशित दावानल उत्पन्न कर देती है ।
अपने 'तथाकथित' सुसंबंध के निरंतर कमज़ोर पड़ने के दौरान एक "सावधान-वाणी" हर एक युगल के दिल-ओ-दिमाग में बार-बार दस्तक ज़रूर दिया करता है, मगर 'मोहांध'-'अहंकारी'-'ज़िद्दी' पुरुष एवं नारी -- दोनों ही अपनी नासमझी व नाराज़गी में स्वयं ही अपने हाथों से अपना जीवनाधार अंधी गलियों की गुमनामी और गर्दिश में मोड़कर महज़ अपनी 'शक़ की सुई' इधर-से-उधर घूमाफिराकर
अंततः अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और इस विश्व की संरचना को ही असंयमित आचार-व्यवहार से दष्प्रभावित करते हैं, जो कि "सर्वजन हिताय : सर्वजन सुखाय" नीति की धज्जियां उड़ा देता है ।
क्या ऐसा करना उचित है ? क्या वक्त रहते 'शक़ की सुई' तोड़ा नहीं जा सकता ???





















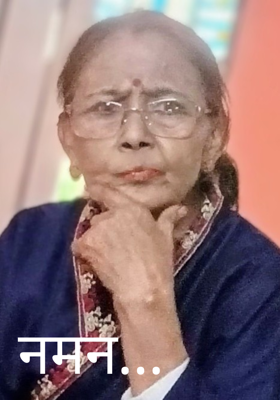




























![लॉक डाउन व्यंजन दोहे [ भाग- 1]](https://cdn.storymirror.com/cover/thumbnail/e50fcaac72d1fd157fc508e523af80e4.jpe)












![लॉक डाउन व्यंजन दोहे [ भाग-2 ]](https://cdn.storymirror.com/cover/thumbnail/eb5ac83a9ba6da72a96d770d1369d6b7.jpe)
