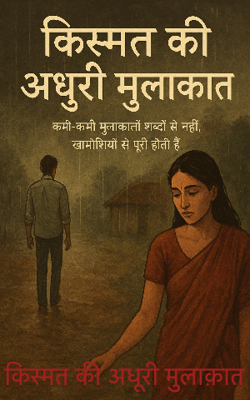"अंतिम साँसों में एक सुबह"
"अंतिम साँसों में एक सुबह"


अभी-अभी मैं शिमला एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर इस अनजानी राह पर चला हूँ। पहाड़ों की पतली, घुमावदार सड़कों पर टैक्सी जैसे-जैसे ऊपर चढ़ती जा रही थी, हवा में ठंडक घुलती जा रही थी। देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की सुनहरी किरणें मानो बादलों से आंख-मिचौली खेल रही थीं। आसमान धुंधलके से ढका था, और उस पर छिटकते बादलों की छाया, जैसे किसी पुराने ख्वाब की परछाईं हो।
जब टैक्सी होटल के गेट पर आकर रुकी, तो मेरी निगाह अचानक उस बोर्ड पर पड़ी—“The Heaven Hotel”
नाम पढ़ते ही दिल के भीतर कोई पुरानी आवाज गूंज उठी—एक रुकाव, एक थमाव, जैसे समय ने एक पल के लिए अपना प्रवाह रोक दिया हो।
"स्वर्ग का रास्ता..."
नाम में ही कुछ ऐसा था, जो आत्मा की तहों तक उतर गया। कोई अनकही दास्तान, कोई भूली हुई पुकार… जैसे ये जगह मुझे पहले से जानती हो।
अभी मैं इन भावनाओं से बाहर निकल ही रहा था कि होटल का एक युवा सहायक मेरे पास आया। वह शायद भारी-भरकम सामान की उम्मीद में दौड़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास बस एक छोटा-सा पिट्ठू बैग है, जिसे मैं खुद ही उठाकर चल पड़ा था, तो उसकी मुस्कान में एक हल्की सी मायूसी तैर गई।
मैंने उसे पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा,
“आपके होटल का नाम बहुत ख़ूबसूरत है—‘स्वर्ग का रास्ता’। कोई खास कहानी है इसके पीछे?”
वह कुछ पल चुप रहा। फिर मुस्कराया, जैसे किसी छुपे रहस्य को साझा करने से पहले सोच रहा हो।
“सर जी,” उसने धीरे से कहा,
“कहते हैं कि जब महाभारत समाप्त हुआ और पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े, तो अपनी आखिरी रात यहीं, इसी पहाड़ी पर गुजारी थी उन्होंने। तभी से इस जगह को ‘स्वर्ग का द्वार’ कहा जाने लगा।”
उसके शब्द हवा में तैरते हुए मेरे भीतर कहीं गहराई तक उतर गए।
सिहरन-सी दौड़ गई।
जैसे यह सब केवल एक संयोग न हो, बल्कि कोई अज्ञात संकेत हो। मैं खुद भी तो भागा था — उस बेमकसद शहरी ज़िंदगी से, भीतर की थकान और शोर से। शायद मैं भी किसी 'द्वार' की तलाश में यहाँ आया था—एक आंतरिक स्वर्ग की।
मैंने गहरी साँस ली और उससे पूछा,
“तो आपको क्या लगता है, पांडवों को अगली सुबह सच में स्वर्ग मिल गया था?”
वह हँसा नहीं, न चौंका। बस हल्की-सी मुस्कान के साथ बोला,
“सर जी, इसका जवाब तो वही दे सकते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं हैं।
हाँ, एक बात ज़रूर कहूँ—स्वर्ग शायद कोई मंज़िल नहीं, एक एहसास है… और वो यहीं मिल सकता है… अगर मन शांत हो।”
उसके शब्दों में शांति की एक अजीब सी चमक थी—जैसे पहाड़ों की धूप। मुझे लगा, मैंने किसी ऋषि से कुछ सुन लिया हो। मैं चुपचाप सिर हिलाकर भीतर की ओर बढ़ गया।
होटल के रिसेप्शन पर एक आत्मीय मुस्कान के साथ एक युवक बैठा था। जैसे ही मेरी नजरें उससे मिलीं, उसने पूछा:
“सर जी, कितने दिन रुकने का इरादा है?”
मैंने मुस्कराते हुए जवाब दिया,
“जब तक स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल जाता।”
उसने बिना चौंके कहा,
“फिक्र न करें सर। यहाँ रुकने वालों को वो मिल ही जाता है जिसकी तलाश में आते हैं। हर किसी को उसका ‘स्वर्ग’ अलग रूप में मिलता है।”
उसका आत्मविश्वास मेरे मन की बेचैनी को थोड़ा और शांत कर गया। जैसे इस जगह पर हर चेहरा किसी न किसी कारण से रखा गया हो—कोई रहस्य लिए हुए।
जब मैं अपने कमरे में पहुँचा और खिड़की खोली, तो सामने का दृश्य मेरे कल्पना से कहीं अधिक गहन था—सफेद धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियाँ, देवदार के हरे शिखर जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ हों, और नीचे गहराई में बादलों की रजाई ओढ़े शांत घाटियाँ।
एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दाख़िल हुआ, जैसे किसी ने मेरे चेहरे को हल्के से छू लिया हो—माँ के आँचल-सा सुकून।
मैं बिस्तर पर बैठ गया। बैग से सिर्फ एक डायरी और पेन निकाला—बस यही दो साथी लाया था मैं।
आँखें बंद कीं और पहली बार लगा जैसे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है। दिल की धड़कनें हल्की हो रही थीं, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो।
बाहर बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। नन्हीं-नन्हीं बर्फ़ की किरचें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं।
हर बूँद, हर किरन, हर हवा का झोंका, कुछ कह रहा था—
"स्वर्ग कहीं दूर नहीं… अगर तुमने सुनना सीख लिया है, तो यहीं है।"
दरवाज़ा खुला, और होटल का बेरा एक ट्रे में चाय और पहाड़ी स्नैक्स लिए मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा वही सौम्यता लिए था, जो केवल पहाड़ों में पाई जाती है।
“साहब जी, पहाड़ी चाय का आनंद लीजिए। यहां की हवा और चाय मन को भीतर से जगा देती है।”
मैंने मुस्कराकर उसे भीतर बुला लिया। चाय की भाप में लौंग और दालचीनी की महक थी — गर्म, गाढ़ी, और सुकून से भर देने वाली। जैसे हर घूंट बीते वर्षों की थकान को चुपचाप अपने साथ बहा ले जा रहा हो।
मैंने धीरे से पूछा,
“यहां के लोग इतने शांत कैसे होते हैं? शहरों में तो हर सांस एक रेस है, हर चेहरा किसी बोझ के नीचे दबा हुआ।”
वह मुस्कराया, फिर खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला —
“साहब, पहाड़ों में समय पिघलते बर्फ जैसा बहता है — धीरे, मौन और अपने ढंग से। हम यहां मौसम से सीखते हैं—सब्र, स्वीकृति और संतुलन। शायद इसी से शांति आती है।”
उसकी बातों ने जैसे मेरे भीतर की गर्म, उलझी साँसों को थाम लिया। शहरों में हम समय को मुट्ठी में पकड़ने की होड़ में खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यहां, समय खुद तुम्हारे पास बैठ जाता है — और कहता है,
“अब रुको… अब जी लो।”
उस रात मैं वर्षों बाद गहरी नींद में डूबा — बिना किसी बेचैनी, बिना किसी सपना। बस पहाड़ी हवा के स्पर्श में लिपटी एक लंबी, सांत्वनादायक नींद।
सुबह जब मेरी आँख खुली, तो बाहर की हवा में एक जादू था। खिड़की खोलते ही बर्फ की हल्की परत, धुंध से ढकी पहाड़ियों पर नाचती धूप, और पक्षियों की कोरस जैसी आवाज़ें — यह कोई सुबह नहीं थी, यह कोई अनुभव था।
मैं खामोशी से बैठा रहा।
चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन विचार बहते रहे।
और तभी अतीत के पन्ने खुलने लगे—
माँ की वो मुस्कान, उनका स्नेहिल हाथ मेरे माथे पर, और फिर वो अंतिम दृश्य... चिता की लपटें और मेरी आत्मा में उतरती सिसकी। उस दिन माँ के साथ, मेरी मासूमियत भी जली थी।
लेकिन आज... वह स्मृति केवल पीड़ा नहीं थी। वह अब मेरे जीवन की जड़ों का हिस्सा बन चुकी थी। माँ की यादें मुझे हर मोड़ पर थामे रहीं — और शायद आज इस शांत पहाड़ पर वह मेरे करीब थीं।
चाय की तासीर के साथ, और भी चेहरे सामने आने लगे — गाँव के बचपन के साथी, कॉलेज के वो पागल दिन, और शहर की भागदौड़ में खोए रिश्तेदार। उन सबकी छाया मेरे भीतर अब भी जिंदा थी। शायद यही वो "स्वर्ग" था — जहाँ अतीत से भागने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे स्वीकार कर, प्रेम से सहेज लिया जाता है।
शाम को मैं होटल के पीछे निकल पड़ा। एक पगडंडी मुझे बुला रही थी। जूते बर्फ में धँस रहे थे, साँसें बादलों में घुलती जा रही थीं, और हर कदम जैसे मुझे अपने भीतर ले जा रहा था। जब मैं एक ऊँची चट्टान पर पहुँचा, तो वहाँ बैठकर घाटी को देखा।
घाटी अब नीले धुंध से ढक गई थी। सामने तारे उगने लगे थे — धीरे-धीरे। जैसे आकाश खुद मुझे कहानी सुना रहा हो।
और फिर… एक पल आया —
पूरा मौन।
न कोई शोर, न कोई विचार, न कोई इच्छा।
बस मैं और पहाड़ — एक जैसे।
मौन, विशाल और अपने आप में पूर्ण।
मैं समझ गया—स्वर्ग कोई जगह नहीं, यह वही अनुभव है… जब तुम्हें खुद से मिल जाता है।
होटल लौटते समय अंधेरा था, लेकिन मेरे भीतर एक आलोक जल चुका था। रिसेप्शन पर पहुंचा तो वह युवक वही मुस्कान लिए खड़ा था।
मैंने उससे कहा,
“शायद मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिला, लेकिन मुझे वह मिल गया जिसकी मुझे सच्ची तलाश थी।”
उसने सिर हिलाया और बोला,
“स्वर्ग ढूँढने वालों को अक्सर खुद की खोई हुई आवाज़ मिल जाती है, सर।”
अगली सुबह होटल की बालकनी से जब सूरज की पहली किरणों ने मेरे चेहरे को छुआ, तो लगा — मैं नया हूँ। हवा में उस दिन पहाड़ की ठंडक नहीं, एक कोमल गर्माहट थी।
रेस्टोरेंट में वही बेरा मिला, वही सादगी, वही अपनापन।
“साहब जी, उम्मीद है चाय और पहाड़, दोनों पसंद आए होंगे।”
मैंने मुस्कराते हुए जवाब दिया,
“चाय तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ की ख़ामोशी उससे कहीं ज़्यादा गहराई तक उतर गई।”
वह बोला,
“यही तो असली स्वाद है, साहब जी। यहां हर चीज़ धीरे पकती है—चाय भी, और आत्मा भी।”
सुबह की हवा अब थोड़ी गरम होने लगी थी, लेकिन पहाड़ों की हल्की नमी अब भी दिल को सुकून दे रही थी। होटल की बालकनी से दूर तक फैले देवदारों के झुंड मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। उस शांत वातावरण में मन किसी नई दिशा की ओर बढ़ने को तैयार था। मैंने रिसेप्शन पर जाकर पूछा—
"क्या यहाँ आसपास कोई गाँव है? कुछ असली, कुछ सच्चा देखने का मन कर रहा है।"
रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा,
"सर, पास ही एक जगह है — 'शांति गाँव'। नाम ही बहुत कुछ कह देता है, है ना? वहाँ जाइए, शायद आपको वो शांति मिल जाए जिसे आप ढूँढ़ रहे हैं।"
मैंने पिट्ठू बैग उठाया और चल पड़ा। रास्ता घुमावदार था — हर मोड़ पर एक नई तस्वीर, जैसे प्रकृति कोई चित्रकार हो। कहीं पर धूप देवदार के बीच से झाँकती, कहीं बादल नीचे उतर आते। परिंदों की आवाज़ें हवा में घुली हुई थीं, और ज़मीन पर गिरती पत्तियाँ धीरे-धीरे हर साउंड को एक कोमल मौन में बदल रही थीं।
"शांति गाँव" अपने नाम के जैसे ही निकला — सादगी में लिपटा हुआ, आत्मा की गरमी से भरा हुआ। वहाँ कोई दौड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं — बस लोग थे, मुस्कुराहटें थीं, और जीवन का एक धीमा लेकिन सुंदर बहाव।
एक पुराने पीपल के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर समय की झुर्रियों में समाई हुई संतुष्टि थी। मैंने उनके पास बैठते हुए पूछा:
"बाबा जी, इस गाँव का नाम 'शांति गाँव' क्यों है?"
उन्होंने किताब बंद की, मेरी ओर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ बोले —
"क्योंकि यहाँ के लोग शांति में जीते हैं। प्रकृति को सुनते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं। यहाँ कोई कुछ बनना नहीं चाहता — यहाँ हर कोई 'होना' सीखता है। यही शांति है, यही स्वर्ग।"
उनके शब्दों में एक ऐसी स्थिरता थी, जो किताबों में नहीं, जीवन में मिलती है। मैं वहाँ कुछ देर रुका, फिर धीरे-धीरे होटल की ओर लौटने लगा।
अब शाम की परछाइयाँ पहाड़ों पर उतरने लगी थीं। सूरज नीचे सरक रहा था, और पगडंडी जो सुबह मुझे इतनी स्पष्ट दिखी थी, अब धुंध में लिपटने लगी थी। हवा में एक अजीब-सी ठंडक थी — ऐसी जो शरीर से ज़्यादा आत्मा को छूती है। हल्की-हल्की सिहरन — मानो रात कोई राज़ लेकर उतर रही हो।
जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, रास्ता अनजाना लगने लगा। पेड़ सघन हो गए थे, और धूप अब पूरी तरह छिप चुकी थी। जल्दबाज़ी में मैं दिशा भूल बैठा और अचानक एक पुराने, वीरान पार्क में जा पहुँचा।टूटी-फूटी बेंचें, उखड़ी हुई दीवारें, और पेड़ों पर झूलती बेलें — जैसे समय ने यहाँ आकर विश्राम लिया हो। झूलों की धीमी गति हवा में एक अजीब-सी खामोशी घोल रही थी। हर चीज़ शांत थी, लेकिन वह शांति सुकून देने वाली नहीं थी — उसमें एक किस्म की अनकही कहानी थी। जैसे कोई मुझे बुला रहा हो… या शायद मैं ही कुछ तलाश रहा था।
और तभी — मेरी नज़र झाड़ियों के पास कुछ हरकत पर पड़ी। एक छोटी बच्ची, करीब पाँच साल की, नीली ऊनी फ्रॉक में, बालों में दो प्यारी चोटी और हाथ में एक छोटी टॉर्च जो बार-बार बुझ रही थी। वह ज़मीन पर झुकी कुछ ढूँढ़ रही थी। उसकी मासूमता और अकेलापन दोनों मिलकर दिल को किसी अदृश्य चिंता से भर रहे थे।
मैं धीरे से आगे बढ़ा, बिना उसे चौंकाए। और शांत स्वर में पूछा:
“बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों हो?”
उसने सिर उठाया। बड़ी-बड़ी आँखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा अपनापन था।
वह मुस्कराई और बोली:
“मेरा नाम आशी है। आशी मतलब — मुस्कान, हँसी, आशीर्वाद।”
उसकी आवाज़ में ऐसी मासूम दृढ़ता थी, जैसे वह किसी परी कथा से निकली हो।
मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा,
“इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, आशी?”
वह गंभीर हो गई, और बोली:
“मैं अपनी गुड़िया ढूंढ़ रही हूँ। उसका नाम भी आशी है — मेरी तरह। खेलते-खेलते यहीं कहीं गिर गई।”
मैंने उसकी बात सुनी और भीतर कुछ पिघल गया।
गुड़िया को अपनी परछाई बनाना — शायद यही वह भाव है, जो हम बड़े खो देते हैं।
मैंने मुस्कराकर कहा:
“चलो, हम मिलकर ढूँढ़ते हैं — तुम्हारी आशी को।”
उसने मेरी तरफ देखा और आँखें चमक उठीं।
हम दोनों मिलकर पार्क की झाड़ियों में ढूँढ़ने लगे। हवा तेज़ हो रही थी, पत्तियाँ उड़कर आँखों तक आ रही थीं। लेकिन उस खोज में एक अजीब-सी गर्मी थी — जैसे मैं किसी मासूम दुनिया को फिर से छू रहा हूँ।
उसके चेहरे पर जैसे उम्मीद की धूप उतर आई थी। उसकी आँखें चमक रही थीं — नन्हीं मशालें जो अंधेरे से लड़ने को तैयार थीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे अब पूरी तरह विश्वास हो गया हो कि उसकी खोई हुई गुड़िया मिलकर ही रहेगी।
हम दोनों झाड़ियों और पेड़ों के बीच गुड़िया ढूँढ़ने लगे। आशी कभी किसी झाड़ी में झाँकती, कभी ज़मीन पर झुकती, और कभी पत्तों को उलट-पलट कर देखती। उसकी हल्की हँसी हर उस छाया को काटती जा रही थी जो रात के साथ उतर रही थी। उस गहराते अंधेरे में, उसकी मासूम मुस्कान किसी दीपक जैसी लग रही थी।
मैं भी उसके साथ चल रहा था — मिट्टी में हाथ डालता, पतझड़ की पत्तियाँ हटाता। धीरे-धीरे, उस मासूम रिश्ते में कुछ पवित्र-सा जुड़ गया था। यह कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं था, यह एक आत्मीय बंधन था — जहाँ एक मासूम की तलाश में एक वयस्क फिर से बच्चा बन गया था।
अंधेरा अब और गहराने लगा था। तारे अपनी जगह ले चुके थे और आकाश एक रहस्यमयी चादर बन गया था। सर्द हवा अब चेहरे को काटने लगी थी। पेड़ों की शाखाएँ एक-दूसरे से टकराकर सूखी फुसफुसाहटें कर रही थीं — मानो कोई पुरानी दास्तान दोहरा रही हों।
मैंने पास आकर आशी से पूछा,
“आशी, गुड़िया तो कहीं दिख नहीं रही… क्या याद है, कहाँ छूटी थी?”
वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आँखों में एक हल्की चिंता तैर गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
“नहीं पता, अंकल। शायद खेलते हुए गिर गई… लेकिन वो बहुत प्यारी है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है… मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती।”
उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। इतनी छोटी सी उम्र में, ऐसा समर्पण — ऐसा अपनापन। मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मैं बस उसकी आँखों में झाँकता रहा, और वहाँ एक अडिग विश्वास था — वैसा विश्वास जो हम उम्र के साथ खो देते हैं।
अब रात पूरी तरह छा चुकी थी। हवा ठंडी ही नहीं, नुकीली हो चुकी थी। हर सांस जैसे एक स्मृति को भीतर ले जा रही थी।
मैंने धीरे से कहा,
“आशी, अब बहुत रात हो गई है। चलो घर चलें… कल सूरज निकलेगा, तब हम फिर से गुड़िया ढूंढ़ेंगे। ठीक?”
उसके चेहरे पर एक क्षण को उदासी छा गई, जैसे कोई सपना बीच में टूट गया हो। लेकिन तुरंत उसने अपनी वही जानी-पहचानी मुस्कान के साथ कहा,
“ठीक है अंकल। लेकिन कल ज़रूर आइएगा। मैं यहीं रहूँगी… जब सूरज उगेगा।”
मैंने सिर हिलाया,
“पक्का बेटा… मैं ज़रूर आऊँगा।”
उसने फिर मेरी ओर देखा — उसकी नज़र में अब न कोई सवाल था, न कोई डर… बस विश्वास।
और फिर वह धीरे-धीरे झाड़ियों के पीछे मुड़ी — बिना किसी शोर, बिना किसी विदाई — जैसे वो आई ही नहीं थी, बस एक स्मृति की तरह उभरी और अब अपने घर लौट गई।
मैं कुछ देर उसी जगह खड़ा रहा। पार्क अब और भी चुप था — सिर्फ झूलों की धीमी आवाज़, कुछ पत्तियों की सरसराहट और मेरा धड़कता दिल।
लेकिन एक बात साफ थी — मैं अब अकेला नहीं था। आशी अपने साथ कुछ छोड़ गई थी — एक सीख, एक रोशनी, एक मासूम विश्वास।
अब रात अपने सबसे गहरे रंग में थी। पूरा आकाश किसी काले कैनवास की तरह फैला हुआ था — जहाँ तारे चुपचाप टिमटिमा रहे थे, और चाँद किसी बुद्धिजीवी की तरह सब देख रहा था।
हवा अब और भी तेज हो गई थी — पेड़ों की शाखाएँ एक-दूसरे से टकराकर ऐसी ध्वनि कर रही थीं, जैसे पुराने मंदिर की घंटियाँ बज रही हों। पार्क की पगडंडी अब घुल चुकी थी धुंध में — लेकिन मेरे भीतर… वहाँ कुछ और ही चल रहा था।
एक अजीब सी गर्माहट, एक भीनी सी लौ — जो भीतर कहीं धीमे-धीमे जल रही थी।
आशी की मुस्कान, उसकी आशा, और उसका यह विश्वास कि जो खो गया है, वह फिर मिलेगा — जैसे मेरे अंदर के जमे हुए हिस्सों को पिघला रहा था। उसकी बातों ने मुझे मेरे ही भीतर से जगा दिया था।
पार्क की पुरानी दीवारों को पार कर, जब मैं होटल की ओर लौटने लगा, तो रास्ता अब भी उतना ही सुनसान था… लेकिन अब डर नहीं था। वो डर, जो अकेलेपन से आता है, अब किसी भरेपन से बदल गया था।
हर कदम के साथ मेरे विचारों की गति धीमी होती जा रही थी — जैसे हर सवाल अब खुद ही सुलझता जा रहा था।
जैसे-जैसे मैं होटल के पास पहुँचा, आसमान एक चमकदार कालीन में बदल चुका था। चाँद अब पूरी तरह साफ था — और उसकी चाँदनी मेरी परछाईं को लम्बा करती जा रही थी।
मैं खिड़की से बाहर देख रहा था… और मेरे भीतर एक पुराना सवाल दस्तक दे रहा था —
"क्या हर खोई चीज़ सच में खो जाती है? या क्या हम ढूँढ़ना ही छोड़ देते हैं?"
आशी ने मुझे सिखाया था कि
खोई हुई चीज़ें तब तक नहीं मिलतीं, जब तक उन्हें ढूँढ़ने की मासूम जिद जिंदा न रहे।
और जब वह जिद किसी नन्हे हाथ से थमी होती है, तो वह सिर्फ वस्तु की तलाश नहीं होती — वह आत्मा की पुनर्प्राप्ति होती है।
होटल के कमरे में पहुँचते ही मैंने खिड़की खोली। बाहर की ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ नहीं, भीतर की धूल को छान दिया। हवा में देवदार की पत्तियों की गंध थी, और दूर से आती एक मंद सी बांसुरी की धुन-सी सरसराहट। यह हवा केवल मौसम नहीं, एक पुरानी आत्मा का संदेश लग रही थी — शांत, सम्मोहक, और भीतर तक पहुँचने वाली।
मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद… वह फिर से एक अधूरी कविता की तरह आँखों के पन्नों से फिसलती रही। और तभी, स्मृतियों के धागे बुनने लगे —
कांकरखेड़ा की गलियाँ, जहाँ धूल से भरी हवाओं में बचपन की साँसें अठखेलियाँ करती थीं,
माँ की झुकी कमर, जो हर दिन मेरी किताबों के बोझ से भारी हो जाती थी,
पिता की चुप्पी, जो हमेशा कुछ कहना चाहती थी, पर कभी शब्द नहीं बन सकी।
लकड़ी की पुरानी बेंचों पर बैठकर मैंने पाँचवीं पास की थी — वो बेंचें आज भी मेरे भीतर कहीं पड़ी हैं, दीमकों से नहीं, यादों से खोखली।
गाँव से निकलकर आठवीं सड़कड़ा के स्कूल में और फिर राजकीय इंटर कॉलेज, मुरादाबाद तक की यात्रा — एक ऐसा सफ़र जहाँ सपनों का बोझ किताबों से भारी था।
मेरे माता-पिता ने सब कुछ खोकर, मुझे थोड़ा-सा जीतने का अवसर दिया था।
लेकिन सपनों की राह कभी समतल नहीं होती।
पैसे की कमी, समय का अभाव — और इसी दरम्यान, ‘अमर उजाला’ की प्रेस में शुरू हुआ मेरा रात्रिकालीन संघर्ष। दिन में क्लास, रात में मशीनें — और उनके बीच एक ऐसी नींद, जो कभी पूरी नहीं होती थी।
मैं थकता नहीं था — क्योंकि भीतर एक जुनून था। लेकिन कभी-कभी जुनून भी साँस माँगता है — और तब वो शादी की साँस थी, जो मेरे जीवन में आ गई।
मैं तैयार नहीं था। लेकिन ज़िंदगी कभी पूछती नहीं।
शादी हुई, और कुछ ही समय में मेरी बेटी हुई — प्रिया।
वो मेरी दुनिया की पहली मुस्कान थी — उसकी पहली चीख, मेरे जीवन की पहली उम्मीद बन गई।
लेकिन उस उम्मीद को घर की दीवारों ने कैद नहीं किया।
मेरी पत्नी को चाहिए था रेशमी जीवन — उसकी आँखों में सपने थे, लेकिन वो मेरे जैसे नहीं थे।
उसे चाहिए था जगमगाहट, और मेरे पास था संघर्ष।
धीरे-धीरे रिश्तों की दीवारों में दरारें पड़ीं। और एक दिन…
वो सब छोड़कर चली गई — मेरी बेटी को साथ लेकर।
शुरुआत में मैं पत्थर हो गया।
सोचा — लौट आएगी।
लेकिन वक्त बीतता गया, और उसके साथ मेरी उम्मीदें भी दरकती गईं।
बंबई से लेकर कानपुर तक मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया।
फिर अफवाहें आईं —
वो किसी अमीर के साथ चली गई,
हीरोइन बनने का सपना था,
या शायद मुझसे तंग आ गई थी।
हर अफवाह, एक ज़ख्म थी — और हर ज़ख्म, एक शोर।
और जब शोर बहुत बढ़ गया…
मैं शराब की चुप्पी में उतर गया।
शुरुआत में वो राहत थी — फिर आदत बनी, फिर आदत से मजबूरी।
अब शराब मेरा साथी थी — जो मेरी बातें नहीं सुनता था, लेकिन मेरे सन्नाटे को गूंज से भर देता था।
आज जब आशी से मिला — उस नन्हीं बच्ची से, जो झाड़ियों में अपनी गुड़िया ढूँढ़ रही थी —
मुझे लगा जैसे मैं खुद को ढूँढ़ रहा हूँ।
उसका नाम ‘आशी’ था — मुस्कान, हँसी, आशीर्वाद।
और उसकी गुड़िया का नाम भी आशी ही था —
जैसे वो अपनी ही मासूमता को बचाने निकली हो।
जैसे मैं, अपने ही भीतर की किसी टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ना चाहता था।
गुड़िया की खोज कोई साधारण खोज नहीं थी —
वो एक यात्रा थी… मेरी आत्मा की,
जहाँ मैं एक पल के लिए फिर से वो बन गया था,
जो कभी प्रिया की मुस्कान में खो गया था।
आशी ने मुझे सिखाया —
मासूमियत उम्र से नहीं, दृष्टिकोण से आती है।
अगर हम फिर से बच्चों की तरह, बेझिझक भरोसा करना सीख जाएँ,
तो शायद टूटे सपने फिर से उड़ना सीख लें।
उसने मुझे यकीन दिलाया —
कि जो खो गया है, वह दोबारा पाया जा सकता है।
शर्त सिर्फ यह है कि
हम उसे ढूँढ़ना बंद न करें,
और उस पर विश्वास बनाए रखें।
उस रात, होटल के कमरे की खामोशी में
आशी की मासूम आवाज़ अब भी गूंज रही थी।
उसने मुझसे कहा था —
“जब सूरज उगेगा, हम फिर से गुड़िया ढूंढ़ेंगे।”
और मुझे लगता है…
मैं सूरज से पहले ही अपनी गुड़िया ढूँढ़ चुका हूँ —
अपना खोया हुआ विश्वास,
अपनी टूटी हुई मासूमियत,
और वह उम्मीद… जो फिर से सांस लेने लगी है।
कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। हवा बाहर से भीतर नहीं आ रही थी — वह जैसे आत्मा की किसी पगडंडी से होकर, सीधे मन के गहरे कुएँ में उतर रही थी। देवदार की पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं से आती किसी झींगुर की धीमी लय — सब कुछ एक पुराने गीत की तरह बज रहा था।
पर आज उस हवा में एक नई आवाज़ थी —
एक गुड़िया की तलाश में दौड़ती मासूम हँसी।
आशी की वो मुस्कान अब भी मेरे भीतर कहीं बज रही थी — एक ऐसी हँसी, जिसने मेरे टूटे हुए हिस्सों पर मरहम नहीं, बल्कि नई त्वचा चढ़ा दी थी।
मैंने आँखें बंद कीं और कल्पना की —
आशी कहीं पेड़ों के पीछे सो रही होगी, अपनी गुड़िया के सपनों में डूबी हुई।
और मैं… मैं भी अपने उन सपनों को फिर से खोजने के लिए तैयार हो गया था,
जिन्हें कभी ज़िम्मेदारियों की आँधियों में गुम कर आया था।
मैं जानता था — शराब मेरी समस्या का हल नहीं है।
परंतु वह एक छलावा था, एक आसान पलायन — अस्थायी राहत का रास्ता,
जहाँ कुछ देर के लिए आत्मा चुप हो जाती थी।
शराब ने मुझे गहराइयों में पहुँचाया —
इतनी गहराई में, जहाँ अब रोशनी लौटने से डरती थी।
शुरुआत एक बोतल से हुई —
फिर वो बोतल एक साथी बनी,
फिर आदत,
फिर ज़रूरत,
और फिर... एक नश्तर।
हर शाम ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लेना
अब केवल आदत नहीं, एक आत्म-निर्वासन था।
दीवारें गवाह थीं मेरी चुप चीखों की।
अमर उजाला प्रेस, जहाँ मेरी मेहनत की इबारतें छपती थीं, अब मेरे ढहते वजूद का मूक अखबार बन गई थी।
लोग अब मेरी ओर देखते नहीं थे — वे मुझे पढ़ते थे, एक चेतावनी की तरह।मित्र छूटते गए, और मैं…
मैं अपने ही भीतर एक अनाम अंधेरे का स्थायी निवासी बन गया।
एक रात, शराब ज़्यादा हो गई थी।
सीने में एक तेज़ दर्द उठा — जैसे किसी ने भीतर से कसकर पकड़ लिया हो।
साँस लेना दूभर हो गया। पसीना, धड़कनें, धरती घूमती हुई —
और फिर... एक क्षण, जब लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा।
उस क्षण में ज़िंदगी फिल्म की रील नहीं,
बल्कि टूटे हुए फ्रेमों का एक स्लाइड शो बन गई।
माँ की हथेली का आख़िरी स्पर्श,
बेटी की पहली हँसी,
बीवी की पीठ पलटती चुप्पी,
और एक गली... जहाँ कभी सपनों के बीज बोए थे।
डॉक्टर की आँखें किसी श्मशान की राख-सी ठंडी थीं।
उन्होंने जो कहा, वो शब्द नहीं थे — काल के दस्तावेज़ थे।
“लीवर सिरोसिस... और साथ ही लीवर कैंसर।
अंतिम अवस्था में है।
अब कोई इलाज नहीं... आपके पास साठ दिन हैं।”
साठ दिन?
वो शब्द कमरे में ठहर गए —
जैसे वक़्त ने अपनी घड़ी वहीं रोक दी हो।
मैं दीवार की तरफ़ देखने लगा —
सोचते हुए, क्या उस दीवार के पीछे कोई और जीवन है?
या बस यही दीवार मेरी आख़िरी साँसों की सीमा बन जाएगी?
ज़िंदगी की लंबी यात्रा में,
जहाँ लोग दशकों की योजनाएँ बनाते हैं,
मेरे पास अब सिर्फ दो महीने थे।
पर पहली बार लगा —
कि शायद यही साठ दिन मेरी वास्तविक ज़िंदगी हैं।
अब सवाल नहीं था कि कितने दिन हैं,
सवाल ये था — उनमें कितना जीवन है?
शायद ये आख़िरी साठ दिन
एक नई शुरुआत हैं —
जहाँ मैं फिर से उस ‘मैं’ से मिल सकूँ,
जो कभी संघर्ष, मोह, और उम्मीदों के बीच कहीं खो गया था।
मैंने खिड़की से बाहर देखा —
आकाश अब भी तारों से भरा था,
हवा अब भी वही थी,
पर आज उसमें मौत की ठंडक नहीं,
बल्कि एक ज़िंदा चुनौती की गर्माहट थी।
मैंने तय कर लिया —
अब ये साठ दिन सिर्फ मेरी नहीं,
उन सबकी यात्रा होंगे,
जिन्होंने कभी मुझसे प्यार किया था,
जिन्हें मैंने खो दिया,
और जिस ‘प्रिया’ की हँसी अब भी मेरी नींद में गूँजती है।
"सिर्फ साठ दिन..."
डॉक्टर के इन शब्दों की गूँज अब मेरे रगों में खून की तरह बह रही थी।
अस्पताल के दरवाज़े से बाहर निकलते ही, दुनिया बिलकुल वैसे ही चल रही थी —
रिक्शे वालों की पुकारें, पकोड़ों की चटपटी खुशबू, चाय के उबाल की भाप,
पर मेरे भीतर...
जैसे कोई टूट चुका था।
समय रुक गया था — पर सिर्फ मेरे लिए।
भीड़ में चलते-चलते अचानक मैं रुक गया।
एक कोना ढूँढा और एक पुरानी लोहे की बेंच पर बैठ गया।
दिल की धड़कनें ज़मीन पर गिरती बारिश की बूंदों जैसी थीं —
अनियमित, बेचैन, भयभीत।
"अब क्या करूँ?"
यह सवाल मेरे भीतर की हर दीवार से टकराने लगा।
हर गलती, हर पछतावा, हर छूटा हुआ रिश्ता —
मानो उस क्षण वापस लौट आए हों।
प्रिया...
मेरी वो नन्ही परी जिसकी ऊँगली थामकर मैंने खुद जीवन चलना सीखा था,
आज जाने किस शहर की भीड़ में गुम थी —
या शायद, मेरी यादों की गलियों में ही कहीं दब गई थी।
मैंने उसे ढूँढा — हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर डिजिटल कोना टटोल डाला।
लेकिन कुछ नहीं मिला,
सिवाय उस अधूरी तस्वीर के,
जो अब धुंधली हो चुकी थी… मेरी स्मृति की तरह।
और अब जब मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी के पन्ने गिने जा चुके हैं,
मुझे समझ नहीं आया कि मुझे मौत का डर सता रहा है
या इस बात का कि मैंने जीते हुए कुछ भी नहीं पाया।
घर की दीवारें — जो अब तक मेरी खामोशी की गवाह थीं —
आज मुझे घूर रही थीं,
जैसे कह रही हों,
"अब और बहाने नहीं, अब जीवन से आँख मिलाने का वक़्त है।"
मैं बिस्तर पर बैठा और पहली बार पूरे होश में अपनी ज़िंदगी देखी।
वो टूटी तस्वीर —
जिसमें रिश्तों की दरारें थीं,
सपनों की राख थी,
और मेरी आँखों में खोई हुई चमक का प्रतिबिंब।
खिड़की से बाहर देखा —
सूरज ढल रहा था।
आकाश में रक्तवर्णी रंग फैले थे,
मानो कोई चित्रकार अंतिम बार जीवन के रंगों से कुछ कहना चाहता हो।
और तभी…
मुझे याद आई मेरी बचपन की डायरी।
पुरानी अलमारी के कोने से मैंने उसे निकाला —
धूल भरी, पर भीतर अब भी वही ख्वाब संजोए हुए।
एक पन्ना खोला —
उस पर लिखा था:
"एक दिन मैं पहाड़ों पर जाऊँगा।
वहाँ दूर-दूर तक सिर्फ खामोशी होगी,
और मेरे दिल में भी शांति।
मैं पेड़ों से बातें करूँगा,
नदियों में अपनी परछाई देखूँगा,
और आकाश से पूछूँगा — क्या मैं अब भी कुछ महसूस कर सकता हूँ?"
पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखें भर आईं।
वो सपना,
जो कभी मेरी आत्मा का संगीत था,
जैसे आज फिर से धुन बनकर बजने लगा।
मैंने निर्णय लिया —
अब ये साठ दिन मेरा अंतिम निर्वासन नहीं,
बल्कि मेरे भीतर की खोई हुई भूमि की यात्रा होंगे।
मैंने सिर्फ एक बैग पैक किया:
कुछ कपड़े,
डायरी,
डॉक्टर की "60 दिन" वाली आवाज़ अब भी भीतर थी,
पर अब उसका असर अलग था।
पहले वो मुझे तोड़ रही थी,
अब वो मुझे पुकार रही थी।
जैसे ही मैं घाटी में पहुँचा,
पहाड़ों की ठंडी हवाओं ने मुझे गले से लगा लिया।
देवदारों के झुरमुट,
नीले आकाश पर बहते बादल,
नदियों की मृदुल लहरें —
जैसे सब मेरी प्रतीक्षा में थे।
हर सुबह मैं उस ऊँचे टीले पर जाकर बैठता —
जहाँ पूरी घाटी झाँकती थी।
वहाँ कोई शोर नहीं था,
केवल एक गूंजती हुई शांति —
जो मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरती जाती थी।
मैंने खुद से पूछा —
"क्या जीवन सिर्फ साँस लेने का नाम है?"
या…
"सच में जीने का मतलब कुछ और होता है?"
और पहाड़ों ने — बिना शब्दों के —
मुझे उत्तर दिया।
वह सुबह कुछ अलग थी।
सूरज की पहली किरणें जैसे मेरी खिड़की पर दस्तक दे रही थीं —
कह रही थीं,
"जागो — आज का दिन विशेष है।"
शायद अंतिम भी।
पर अब अंत मुझे डराता नहीं था।
अब अंत प्रार्थना जैसा था,
एक शुद्ध, निर्विकार विदाई —
जैसे सूरज शाम को डूबने से पहले आकाश को सुनहरी चादर ओढ़ा देता है।
फिर मुझे आशी की याद आई।
वो छोटी सी बच्ची, जिसकी मासूम उम्मीद ने मुझे फिर से जीना सिखाया था।
जिसने मुझसे कहा था, “आप सूरज निकलते ही आ जाना, हम मिलकर मेरी गुड़िया ढूंढेंगे।”मैंने जल्दी से कपड़े पहने, और बिना किसी देरी के होटल से निकल पड़ा।
पार्क दूर नहीं था, मगर उस दिन रास्ता लंबा लग रहा था। मेरे कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ एक सवाल मेरे भीतर उतरता चला जा रहा था—क्या आशी अब भी वहाँ होगी?
क्या वह अब तक इंतजार कर रही होगी?
या थक हार कर लौट गई होगी, यह मानकर कि मैं नहीं आऊँगा?
मन की हलचल के बीच मैं पार्क के पास पहुँचा। हवा में हल्की ठंडक थी, और आसमान में बादल अब धीरे-धीरे पीछे हटने लगे थे। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की किरणें झांक रही थीं। पार्क में अब भी कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मेरी आँखें उसी बेंच को खोज रही थीं—जहाँ कल मैंने आशी को पहली बार देखा था।
मैंने देखा—वो वही बेंच थी।
उस पर एक छोटी-सी लड़की बैठी थी।
उसकी टाँगें बेंच से झूल रही थीं, और उसकी नज़रें ज़मीन पर टिकी थीं। चेहरा गंभीर, और आँखों में एक हल्की-सी उदासी तैर रही थी।
वो आशी थी।
मैं धीरे-धीरे उसके पास गया, बिना कोई आवाज़ किए, और उसके बगल में बैठ गया।
कुछ पल खामोशी रही। वह मुझे देखे बिना टाँगें हिलाती रही, जैसे कोई सवाल उसके मन में चुपचाप साँस ले रहा हो।
फिर मैंने धीरे से उसके पास झुककर कहा,
"आई एम सॉरी... मैं देर से आया।"
उसने धीरे-धीरे मेरी ओर देखा।
एक क्षण को उसकी आँखों में ख़फ़गी की झलक थी — मासूमियत से सजी एक नाराज़गी, जैसे कह रही हो, "आपने मेरा भरोसा तोड़ा।"
लेकिन फिर… अचानक उसकी मुस्कान लौट आई।
"कोई बात नहीं," उसने हँसते हुए कहा, "चलो, अब गुड़िया को ढूंढते हैं।"
उसकी मुस्कान ने मेरे भीतर कोई पुराना दरवाज़ा खोल दिया।
जैसे मेरी अपनी स्मृतियों की कोई खोई हुई परत अब सामने आकर खड़ी हो गई हो।
हम दोनों गुड़िया ढूंढने में जुट गए।
इस बार, बहुत ध्यान से।
आशी ने हर कोना, हर गड्ढा, हर झाड़ी की तह तक खोज निकाली। कभी झूले के पीछे झाँकती, तो कभी क्यारियों में झुक-झुक कर देखती। उसकी आँखों में उम्मीद का समंदर था—न थकान, न हताशा।
मैं भी उसके साथ हर पत्ते, हर ज़मीन की दरार को खंगालता रहा।
लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली।
समय बीतता गया।
सूरज अब क्षितिज की ओर ढलने लगा था।
पार्क की चहल-पहल अब धीरे-धीरे शांत हो रही थी।
आशी की साँसें अब थोड़ी तेज़ थीं, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं। लेकिन उसकी आँखों में अब भी वह चमक थी—जिसे मैं शब्दों में बाँध नहीं पा रहा था।
मैंने उससे कहा,
"आशी, लगता है आज नहीं मिल पाएगी।"
उसने मेरी ओर देखा, और धीमे से मुस्कराई,
"कोई बात नहीं, अंकल। गुड़िया कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यह सिखा रही थी कि खोने का मतलब अंत नहीं होता।
उसने मेरी उंगली थामी, और हम दोनों धीरे-धीरे पार्क के गेट की ओर बढ़ने लगे।
सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था।
आकाश में लालिमा बिखर गई थी, और मंदिर की घंटियाँ हवा में गूंज रही थीं।
पार्क की बत्तियाँ जल चुकी थीं, और कुछ आख़िरी पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे।
हम दोनों चल रहे थे—एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची।
लेकिन उस शाम में, मैंने पहली बार जाना कि उम्र से नहीं, दृष्टिकोण से इंसान बड़ा होता है।
मेरे दिल में कई भावनाएँ थीं—पछतावा, पीड़ा, संतोष और कहीं न कहीं राहत।
आशी ने जो सिखाया, वह कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता था।
जैसे ही हम पार्क के गेट के पास पहुँचे, मैं थम सा गया।
आकाश अब और गहरा हो चुका था। सितारे धीरे-धीरे टिमटिमा रहे थे, और हवा में पहाड़ों की वह जानी-पहचानी ठंडक घुलने लगी थी—जैसे प्रकृति भी किसी पुरानी कहानी का धीमा अंत लिख रही हो।
पेड़ और झाड़ियाँ अब बस आकृतियाँ बनकर रह गए थे—काले साये जो दिन की रौशनी में जान डालते थे, अब रात की चुप्पी में विलीन हो रहे थे।
सारा माहौल शांत और गंभीर था—और भीतर भी, मेरे मन की सारी उथल-पुथल धीरे-धीरे शांत हो रही थी।
मैंने आशी की ओर देखा। वह अब भी मेरे साथ चल रही थी, पर उसकी चाल में हल्कापन था। जैसे कुछ पा लेने की संतुष्टि हो। जैसे वह अब समझ चुकी हो कि ज़िंदगी क्या होती है—या शायद वो पहले से ही जानती थी।
मैंने रुककर कहा,
"अब तुम्हें घर जाना चाहिए, आशी। मम्मी-पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देर हो गई है, और शायद वे परेशान भी हो रहे होंगे।"
उसने मेरी ओर देखा—गहरी, मासूम और भरोसे से भरी निगाहों से।
फिर मुस्कुराकर बोली,
"हाँ, मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन मैं कल फिर आऊँगी। आप भी आइएगा। हम फिर से गुड़िया ढूंढेंगे!"
उसने यह बात ऐसे कही, जैसे कल एक निश्चित घटना हो—जैसे उसमें कोई संदेह नहीं।
उसकी आँखों में जो चमक थी, वह किसी विश्वास की नहीं, बल्कि उम्मीद की थी—उस विश्वास की कि खोई हुई चीजें कभी-न-कभी मिल जाती हैं, और अगर नहीं मिलें, तो हम उन्हें फिर से बना सकते हैं।
मैंने सिर हिलाया और कहा,
"हाँ, आशी… मैं कल जरूर आऊँगा।"
वह तेज़ी से गेट की ओर भागी, फिर अचानक एक पल को मुड़ी।
उसने मुझे देखा और छोटी सी हथेली हिला दी।
उसकी मुस्कान, जैसे किसी दीपक की लौ, मेरे भीतर उजाला कर गई।
मैं वहीं खड़ा रहा…
वह जा चुकी थी।
उसका छोटा सा शरीर अंधेरे में खो गया, लेकिन उसकी बातें मेरे मन की दीवारों पर गूंजती रहीं।
मैंने गहरी सांस ली और पार्क से बाहर निकला।
मेरे मन में एक असामान्य शांति थी।
वो कुछ घंटे, जो मैंने आशी के साथ बिताए—वे मेरे लिए सिर्फ समय नहीं थे, बल्कि एक जीवन दर्शन थे।
उसकी खोई हुई गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी,
वह एक प्रतीक थी—हमारी ज़िंदगी में उन लोगों, उन संबंधों, उन सपनों की, जिन्हें हम खो चुके होते हैं, लेकिन जिनका दुःख हम अपने भीतर बसा लेते हैं।
मैं अब होटल की ओर बढ़ चला था।
रास्ता वही था, लेकिन कुछ बदल गया था—मुझमें।
पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये पहाड़, ये हवा, ये खामोशी — सब मुझसे कुछ कह रहे हैं।
वे मुझे विदा की भाषा में बोल रहे थे — एक ऐसी भाषा जिसमें कोई डर नहीं होता, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ स्वीकार।
मैंने एक मोड़ पर रुककर ऊपर देखा।
आसमान में अब चाँद निकल आया था—धीरे-धीरे अपनी शीतलता को फैला रहा था।
सूरज की अंतिम लालिमा पहाड़ों की चोटियों से धीरे-धीरे उतर रही थी—जैसे किसी ने पेंट ब्रश से उसे मिटा दिया हो।
चाँद की रौशनी हर पत्ते को एक रूप दे रही थी, हर पत्थर को एक अर्थ।
मुझे लगा, जीवन भी कुछ वैसा ही है।
दिन की तरह गर्म और तेज़,
रात की तरह शांत और स्वीकार्य।
और जब मृत्यु आती है,
वह चाँद की तरह आती है—
धीरे, शांत, पर पूर्ण।
मेरे पास अब भी वो कैंसर था,
वो गिनती के दिन थे,
वो थकावट और टूटन थी—
लेकिन अब उनके साथ थी एक नई दृष्टि।
अब जब मैं होटल की लॉबी में पहुँचा,
वहाँ कुछ लोग थे—पर मैं अकेला नहीं था।
मेरे साथ अब यादें थीं,
एक बच्ची की मासूम आँखें थीं,
और एक सीख थी—
"ज़िंदगी को अगर सहेजकर नहीं जिया,
तो वह रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है।
और अगर सहेज लिया,
तो वो एक मुस्कान की तरह अंत तक साथ चलती है।"
सूरज अब पूरी तरह से पहाड़ों के पीछे छिप चुका था।
आसमान की लालिमा धीरे-धीरे फीकी पड़ रही थी, और क्षितिज पर एक शांत चाँद अपना मुकुट पहन चुका था। उसकी रोशनी, न तेज़ थी और न ही धुंधली—बस इतनी कि एक टूटे हुए मन को सहला सके। मैं वहीं खड़ा था, पार्क से कुछ दूरी पर, पहाड़ियों के किनारे, और ऊपर आकाश की उस शांति को देख रहा था, जिसे शब्दों में बयाँ करना कठिन था।
सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का उदय होना, यह दोनों एक ही प्रक्रिया के दो छोर थे—एक अंत, तो दूसरा आरंभ। जैसे किसी पुराने मित्र का विदा लेना और किसी नए का स्वागत करना।
मैंने उसी क्षण सोचा—"क्या जीवन और मृत्यु भी ऐसा ही नहीं है?"
शरीर का झुक जाना, आत्मा का उठ जाना। एक समय का समाप्त होना, दूसरे काल की शुरुआत। मृत्यु अब मुझे डराने वाली नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे एक मूक संवाद की तैयारी में थी।
मेरे भीतर एक स्मृति जागी—कुरुक्षेत्र का वह क्षण, जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की इच्छा जताई थी। और तब श्रीकृष्ण ने कहा था,
“न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥”
(मैं कभी नहीं था, ऐसा मत सोचो। न तुम नहीं थे, न ये राजा। हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे।)
उन शब्दों की गूंज अब मेरे भीतर थी।
आत्मा अमर है, शरीर केवल एक यंत्र है—विनाशशील, लेकिन आत्मा तो सतत गति में है।
मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है, एक नया अध्याय शुरू होने से पहले।
रात अब पूरी तरह से ढल चुकी थी।
होटल तक पहुँचते-पहुँचते चाँद पूरे आकाश पर छा चुका था।
उसकी चाँदनी सड़क पर बिछी थी, जैसे किसी ने मेरी वापसी के लिए चुपचाप एक राह रच दी हो।
मैंने चलते-चलते रुककर हवा में एक लंबी साँस ली।
पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, और ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा को सहला रही हो—कह रही हो,
"अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम तैयार हो।"
अब मेरे कदम थमे हुए नहीं थे,
बल्कि किसी गहन शांति की ओर बढ़ रहे थे।
मैं जानता था कि मेरे जीवन के दिन गिने-चुने रह गए हैं।
पर अब, उन्हें मैं गिन नहीं रहा था।
मैं उन्हें जी रहा था।
हर सांस, हर क्षण, अब मेरे लिए एक प्रार्थना बन चुका था।
अब पछतावे का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि पछतावा अतीत से चिपकी आत्मा का रोना है, और आत्मा को उड़ना होता है।
अब जब मैं होटल की लॉबी में पहुँचा, वहाँ कुछ पर्यटक थे, कुछ हँसी की आवाज़ें थीं।
लेकिन मेरे भीतर अब एक स्थिर चुप्पी थी—एक पूर्ण शांति।
सूरज अपनी अंतिम किरणें धरती पर गिरा रहा था —
मानो किसी विदाई से पहले का आलिंगन दे रहा हो।
मैंने अपनी जैकेट की जेब से वो छोटी सी गुड़िया निकाली,
जिसे मैं कल ही कस्बे के बाज़ार से लाया था।
नीली फ्रॉक पहने, दो चोटियाँ, और हल्की मुस्कान लिए —
वो हूबहू आशी जैसी ही थी।
आज मैं फिर उसी पुराने पार्क में आया था —
जहाँ पहली बार उस मासूम बच्ची से मिला था,
जो अंधेरे से नहीं डरती थी,
बल्कि उसकी गोद में बैठकर अपनी गुड़िया को ढूँढती थी।
पेड़ों के झुरमुटों के बीच आशी दौड़ती हुई आई।
वही चमकती आँखें, वही मुस्कान।
"अंकल! आप आ गए!"
उसने कहा और मेरी ओर दौड़कर आ गई।
मैंने गुड़िया आगे बढ़ाई।
"ये लो आशी… तुम्हारी गुड़िया।"
वो चौंकी, फिर मुस्कराई, फिर थोड़ी उदास भी हुई।
"पर मेरी तो कहीं खो गई थी… ये नई है?"
मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा —
"हाँ बेटा… पुरानी चीज़ें कभी-कभी खो जाती हैं।
और जब वो नहीं मिलतीं, तो हम उन्हें ढूँढने के बजाय,
नई चीज़ें लाते हैं — ताकि हमारे दिल फिर से मुस्करा सकें।
यही ज़िंदगी है…
हर खोई हुई चीज़ के बाद एक नई सुबह आती है।"
वो चुप रही। शायद समझ रही थी… या शायद महसूस कर रही थी।
मैंने उसकी नन्हीं उँगली अपने हाथ में ली।
"आशी… अब मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ।
मेरा शरीर थोड़ा थक गया है।
मुझे अब आराम चाहिए…
शायद… बहुत लंबा आराम।"
वो मेरी आँखों में देखने लगी।
"आप मरने वाले हैं?"
मैं कुछ पल चुप रहा। हवा के झोंके में उसके बाल बिखर रहे थे।
"हाँ बेटा… अब मेरा समय पूरा हो रहा है।
लेकिन डरना नहीं।
मृत्यु अंत नहीं होती, ये तो सिर्फ एक दूसरी यात्रा है।
जैसे तुम रात को सोती हो, और फिर एक नई सुबह के लिए जागती हो।"
उसकी आँखों में नमी थी, पर डर नहीं था।
उसने मेरी हथेली में अपनी गुड़िया रख दी और बोली —
"जब आप वहाँ जाओगे ना… तो मेरी गुड़िया को साथ ले जाना।
ताकि आप अकेले ना हों।"
मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी।
बस आँखों में उतर आया वो प्यार… और चुप्पी में गूंजता वो अपनापन।
मैंने उसे गले से लगाया।
धीरे से उसके कान में कहा —
"तुम्हारी ये मुस्कान… मेरे साथ हमेशा रहेगी।
और जब तुम कभी अकेली महसूस करो,
तो आसमान की तरफ देखना।
वहाँ एक तारा तुम्हारी मुस्कान में शामिल होकर झिलमिलाएगा।"
उसने सिर हिलाया।
"आप फिर से मिलेंगे ना?"
मैं मुस्कराया।
"हाँ… कहानियाँ कभी पूरी तरह खत्म नहीं होतीं।
वो किसी बच्चे की याद, किसी पेड़ की छाँव,
या किसी गुड़िया की हँसी में ज़िंदा रहती हैं।
और मैं भी… वहीं कहीं रहूँगा — तुम्हारे पास।"
जब मैं होटल लौटा,
तो कमरे की खिड़की अब भी खुली थी।
हवा में अब वो पहचान थी —
आशी की हँसी, गुड़िया की मासूमियत,
और उस एक अंतिम अलविदा की गरमाहट।
मैंने गुड़िया को अपने तकिए के पास रखा।
और उस रात…
बहुत वक़्त बाद मुझे नींद आ गई।
वो सुबह कुछ अलग थी।
पहाड़ों की हवा में आज एक अलौकिक शांति थी —
जैसे सारी प्रकृति किसी विशेष पल के लिए थम गई हो।
मैंने धीरे-से अपनी शॉल ओढ़ी,
गुड़िया को जेब में रखा,
और पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी की ओर चल पड़ा —
जहाँ हर दिन की शुरुआत मैंने सूरज को देख कर की थी।
कदम अब भी उठते थे, लेकिन धीरे… थके हुए…
हर सांस, एक कहानी की तरह भारी थी।
लेकिन मन में हल्कापन था —
क्योंकि अब कोई बोझ नहीं था।
ना कोई शिकायत, ना कोई प्रतीक्षा,
बस — स्वीकार।
चोटी पर पहुँचकर मैंने चारों ओर देखा।
घाटियाँ बादलों से ढकी थीं।
सूरज की किरणें बादलों की ओट से झाँक रही थीं,
जैसे वो खुद देखना चाहता हो कि
आज कौन उसका स्वागत करने आया है।
मैं चट्टान पर बैठ गया — वही जगह,
जहाँ मैं हर सुबह आशी की बातें सोचता था,
अपनी डायरी में लिखता था,
और अपने जीवन को धीरे-धीरे समझने लगा था।
मैंने जेब से वो गुड़िया निकाली —
आशी की नई गुड़िया।
उसे अपनी गोद में रखा और कहा —
"अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, नन्ही दोस्त।
अब मुझे अकेले जाना होगा। लेकिन तुम रहोगी —
एक निशानी बनकर, एक मासूम विश्वास बनकर।"
मैंने उसे पास के देवदार के पेड़ की जड़ों में रख दिया —
जैसे कोई बीज जो कभी फिर से जीवन बनेगा।
सामने आकाश खुला था —
सूरज अब पूरी तरह बाहर आ चुका था।
मैंने अपनी आँखें बंद कीं।
हर साँस अब धीमी हो रही थी —
लेकिन हर साँस में अब शांति थी।
माँ की थपकी, बेटी की हँसी, आशी की मासूमियत,
और उस अनदेखे तारे की रोशनी… सब मेरे साथ थे।
आखिरी पल में मैंने सिर्फ एक बात कही —
मन ही मन —
"शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं…
वो एक क्षण होता है — जब तुम पूरी तरह खुद से मिल जाते हो।
और अब... मैं मिला हूँ।"
और फिर...
हवा एकदम शांत हो गई।
पेड़ों की सरसराहट थम गई।
और सूरज की एक किरण सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी —
जैसे आकाश ने मेरा अंतिम आलिंगन किया हो।
एक बच्ची — शायद अब बड़ी हो चुकी आशी —
एक दिन पहाड़ों की उसी चोटी पर आई।
उसने देवदार के पेड़ के नीचे
एक छोटी-सी गुड़िया देखी…
जो अब भी वहीं थी — धूल में सजीव।
वो मुस्कराई और धीरे से बोली —
"आपने कहा था… कहानियाँ खत्म नहीं होतीं।
सचमुच — आप अब भी यहीं हैं।"
उसने वह गुड़िया उठाई,
आकाश की ओर देखा,
और चल दी — एक नई कहानी के साथ।