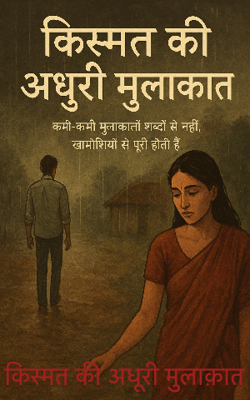एक रुपये की चुभन
एक रुपये की चुभन


लोगों की नज़रों में वह बस एक साधारण औरत थी — न धनी घराने की, न रूपवती। उसके नाक-नक्श आम से भी कम थे, उसके वस्त्र इतने घिसे हुए थे कि दोनों साड़ियों में अंतर कर पाना कठिन था। पर उसके बेटे की नज़रों में वह औरत साक्षात देवी थी — दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली और सबसे अनमोल।
उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज़ था, एक ऐसी मुस्कान जो जीवन की कठिनाइयों को ठहरने नहीं देती थी, और एक आत्मबल, जो हर दर्द को ओढ़ कर भी अडिग खड़ा रहता था।
वह औरत किसी नगर की ऊँची अट्टालिकाओं की नहीं, एक छोटे से गाँव काँकर खेड़ा की माटी में पली-बढ़ी थी। उसका जीवन किसी कविता-सा कोमल नहीं, बल्कि संघर्षों से पका एक अध्याय था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी — बस दो-तीन मिट्टी के बर्तन, दो साड़ियाँ और एक अटूट विश्वास।
गरीबी, लाचारी और जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उसके शरीर को तो झुका दिया था, पर उसकी आत्मा अब भी सीधी खड़ी थी। मात्र 35 वर्ष की आयु में वह साठ की दिखने लगी थी, लेकिन उसके भीतर की माँ अब भी युवती थी — संकल्पों से भरी, उम्मीदों से रची-बसी।
उसका सपना था — अपने बेटे को पढ़ा-लिखाकर एक दिन सम्मान की ऊँचाइयों तक पहुँचाना। लेकिन जब वह समय आया, जब बेटे को शहर पढ़ने भेजना ज़रूरी हो गया, तो एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी थी — किराया सिर्फ़ एक रुपया था, और वह एक रुपया भी उसके पास नहीं था।
लेकिन वह टूटी नहीं। उसने अपनी पुरानी बोरी में कुछ अनाज भर लिया और पूरे गाँव में घूमने लगी। कभी उसे बेचने की कोशिश करती, कभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती — “बस एक रुपया दे दो, मेरा बेटा पढ़ने जाएगा…”
गाँव जानता था उसकी मजबूरी। लोग कभी-कभी मदद भी कर देते, लेकिन यह रोज़ की याचना आसान नहीं थी। वह हर दिन उस बोरी को उठाकर निकलती — आँखों में आत्मसम्मान की लौ, लेकिन सिर पर समाज की जलील निगाहों का बोझ।
चार साल तक यह सिलसिला चला — एक रुपया रोज़, एक सपना हर रोज़। बेटे ने यह सब देखा, भीतर तक महसूस किया। माँ के कंधों पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन हौसला लहराता था। और जब उसका भविष्य आकार लेने लगा, जब उसकी मेहनत फल देने वाली थी । काल ने उसकी माँ को छीन लिया। उसी क्षण, माँ बिना कुछ कहे, चुपचाप इस दुनिया से विदा ले गई।
वह चली गई — जैसे अपना कर्तव्य निभा चुकी हो, जैसे सृष्टि ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली हो।
आज वह बेटा एक बड़ा अधिकारी है — उसके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर हैं, पैसा है, समाज में मान-सम्मान है। लेकिन अब भी एक चीज़ है, जो हर रोज़ उसकी आत्मा को चीर जाती है — माँ और वह “एक रुपया”।
वह एक रुपया जो कभी माँ ने माँगा था — सिर झुकाकर, बोरी उठाकर, लाचारी ओढ़कर।
वह एक रुपया जो तब कुछ नहीं था, लेकिन आज उसकी आत्मा की सबसे भारी कीमत बन चुका है।
अब जब वह बेटा स्वयं 60 का हो चुका है, माँ की चुभन उसके भीतर अब भी ताज़ा है।
जब वह अकेला होता है, जब शाम की खामोशी उसे घेरती है । जब रात का अन्धकार उसे डराता हैं ।जब उसे अपने गावं और अपने संघर्षो की याद आती हैं । तो कहीं भीतर से माँ की आवाज़ फिर गूंजती है —
“कोई एक रुपया दे दो… मेरा बेटा पढ़ने जाना चाहता है…”
उस माँ के लिए मेरी श्रृंदाजली
तपती धूप में जो छांव बन गई,
मुट्ठी भर साँसों में ही जीवन रच गई।
जिसने आँचल से ही स्वप्न बुने,
वही माँ, मौन रहकर भी इतिहास कह गई।