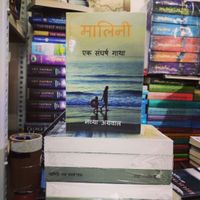कर्फ्यू
कर्फ्यू


अचानक ही स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गईं थी. मगर ऐसा पहली दफा हुआ था कि इसकी वजह स्कूल बंद होना नहीं, शहर बंद होना था. हर कोई कह रहा था की कर्फ्यू लगा है, पर मुझे ये वजह ख़ास समझ में नहीं आयी, इसलिए मैंने अपना मतलब छुटियों और उन्हें खर्च करने तक सीमित रक्खा। बीच-बीच जैसे माँ ने सिखाया, ठीक उसी ढंग से आँख बंद करके छुट्टियां बढ़ जाने की दुआ मांग लिया करता था. वैसे उस वक़्त मुझे 'दुआ' का मतलब पता नहीं था. घर बिलकुल वैसा था, जैसा छोटे शहरों में किराये के घर होते हैं, पर जिस कैंपस में था वो काफी बड़ा था, इसलिए बाहर की हवा मेरी आवारागर्दी को छू भी न सकी. बस मनाही थी तो इस बात कि कैंपस जितना बड़ा गेट, जो कार और स्कूटर के लिए अलग-अलग ढंग से खुलता था, उससे बाहर या किसी को अंदर लाने लिए एक से तीन का वक़्त मुक़र्रर था। अंदर लाने की बात का ज़िक्र मैंने अपने दोस्त ज़ीशान के लिए किया, जिसका नाम ज़ीशान नहीं था यह मुझे अच्छे से याद है, पर इस वक़्त ना जाने क्यूं यही नाम उसके असल नाम के करीब लग रहा है।
ज़ीशान शहर बंद होने से पहला मेरा दोस्त नहीं था. या यूँ कहूँ कि, इससे पहले इस शकल-ओ-सूरत का ज़ीशान नाम लड़का है, मै ये भी नहीं जानता था. हालांकि मैं यासीन अंकल, जो की ज़ीशान के पापा और कैंपस के ठीक सामने वाली छोटी सी दुकान, यासीन जनरल स्टोर के मालिक थे, उन्हें अच्छे से जानता था. घर का सारा सामान वहीँ से आता था. और अब मेरा एक दोस्त भी. दिन में एक से तीन के बीच. क्यूंकि शहर के साथ-साथ दरवाज़े, खिड़कियां और दुकाने भी बंद थी और सिर्फ एक से तीन के बीच ही खुला करती थी. क्यूं और किसके कहने से, पता नहीं। मैंने तो धर्म की तरह बस मान लिया था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर बच्चों का अकाल पड़ा था, बिलकुल भी नहीं। कोई 4-5 बच्चे तो किसी भी पहर पाये जा सकते थे, होमवर्क और घरवालों की गिरफ्त से आज़ाद। खेलने के लिए अपने निजी साधन और सोच के अलावा एक मैदान, जो उस उम्र के हिसाब से काफी बड़ा था, और एक झूला मौजूद थे. मैदान की लगभग पूरी चौड़ाई में फैले करौंदे के पेड़ के बगल में एक हर श्रृंगार का पेड़ था, जो ठीक उस तरह से हर सुबह अपने फूल झाड़ दिया करता था जैसे हमने अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं. और मैं उन्हें उठा लिया करता। सूंघने या सजाने के लिए नहीं, खेलने के लिए. उन्हें सींक-झाड़ू से चुराई सींकों पर रख कर, ज़ीशान और मैं तलवारबाज़ी किया करते, जिसका फैसला फूल के फ़ना हो जाने से होता। मैंने अपने इस खेल में चाइनीज़ मूवी की आवाज़ें भी शामिल कर ली थी, जिसे ज़ीशान भी बाद में दोहराने लगा था, बेहद ही अजीब से अंदाज़ में. जब तक फूल रहते, हमारा ये खेल चलता रहता। ना जीतने वाले को कुछ मिलता न हारने वाला का कुछ जाता। कुछ ही दिनों में इस खेल को पुराने संदूक की तरह हमने एक कोने फ़ेंक दिया, और नयी बातें करने लगे. क्यूंकि हम दोनों पूरी तरह से एक दुसरे के लिए नए थे.
"पापा को अब्बू कहते हैं."
"मम्मी को अम्मी"
उनके यहाँ नॉन-वेज खाने के लिए मना नहीं करते। बाकी दाल चावल वो भी खाते हैं.
थोड़ी देर बाद, मैंने भी भारी-भारी बातें करनी शुरू कर दी, और उन चीज़ों का भी सीना चौड़ा करके बखान करने लगा जिसने वैसे मुझे कुछ ख़ास लगाव नहीं था.
हमारे यहाँ, बहुत ताकतवर मंत्र होते हैं - ॐ नमोः नमः, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली.
और उधर से गूंजता हुआ या अल्लाह आया!
फिर हम दोनों ने भगवान और अल्लाह की ताकत का एक कॉम्पिटीशन किया। दोनों ने एक दुसरे को हारा हुआ माना और खुद को जीता हुआ.
दोनों अपने में खुश थे.
घर लौट के मैंने ज़ीशान के घर और मज़हब से जुड़े कई सवाल अपनी माँ से किये। बदले में कुछ नए सवाल मिले।
अगर उस समय मैँ किसी बड़ी क्लास में होता तो इस दिमागी उथल-पुथल को मैँ सवालों का न्यूक्लीयर रिएक्शन जैसा कुछ बोल देता, पर अगर मेरी उम्र उतनी होती तो सवालों का नक़्शा काफी अलग ही होता। हर सवाल के इर्द-गिर्द एक अजीब का घेरा था, डर का. ऐसा डर जो मुझे, रोक रहा था, इन सवालों को घर वालों के सामने रखने से. जैसे सवाल ना होकर वो गलतियां हो. प्लास्टिक की कुर्सी में आग लगा देने जैसी। चुप्पी बनाये रखने जैसी। असल में डर उन घेरों के बाहर निकल जाने का होता है, जैसे की हम आज हैं, डरे हुए. हम चाहते हैं कि कहीं से कोई घेरा आ जाए और हम उसके अंदर सांस लेने लगें, गहरी, शांत साँसे। ऐसी साँसे, जिन पर रंगो की पर्ते न चढ़ी हो, जिन्हे फूंक-फूंक कर न अपनाना पड़े. पर अब घेरा मिट चुका है.
ज़ाहिर है, मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले। पर ज़ीशान ज़रूर मिला। अगले दिन, वहीँ कैंपस के गेट पर, एक से तीन के बीच.
उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले राम, सीता, कृष्णा और लौकी की दही वाली सब्ज़ी के बारे में जानते हैं. ये सुनकर, मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा, इसलिए मैंने भी लौकी की सब्ज़ी की तरह जल्दी-जल्दी कुछ बाते बना दी. फिर हमने अपने दो चार पुराने खेल खेले, और बाय कहा. पर मैँ वापस ना आ सका. घर के अंदर होने के बावजूद भी, मैं ठीक वहीँ खड़ा था जहाँ मैंने ज़ीशान को झूठ बोला था. क्यूंकि उस दिन मैंने एक बात सीखी थी - कि झूठ का एक अजीब सा कड़वापन होता है, जो आपकी ज़बान से चिपका रहता, उसपे आप लाख चीनी रख लो या थूक लो, वो आसानी से जाता नहीं है, और आपके ख्यालों को डसता रहता है. मैंने तय कर लिया की मैं अगले दिन ज़ीशान को सच बोल दूंगा, और अगला दिन होते-होते मैंने अपने ज़मीर को मना लिया कि इस बार जाने दे, आगे से नहीं होगा। और आज तक वैसा ही है - हर दफा मना लेता हूँ.
ख़ैर, अब तक शहर के इस बंद में, दो सन्डे बीत गए थे और तीसरा कतार में था। जितने दिन बीतते जाते थे, मेरी और ज़ीशान की ख़ुशी बढ़ती जाती थी। अब हम दोनों साथ ही में दुआ करने लगे थे। उसने मुझे दुआ का मतलब भी समझा दिया था। एक बार तो हमने सोचा ऊपर वाले को कंफ्यूज़ करते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मैं हाथ फैला के। हम दोनों ने तय किया कि ये बात हम अपने घर वालों को तब बताएंगे जब दुआ कबूल हो जॉएगी। फिर हम भूल गए। बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी ना।
अभी तक हम दोनों एक बार भी एक-दूसरे के घर नहीं गए थे, पर शायद ही घर का ऐसा कोई कोना या शख्स था जिसे हम नहीं जानते थे. शायद यही वजह दोनों एक दूसरे के घर जाना चाहते भी थे, और नहीं भी. पर हमने इतना सोचा नहीं, क्यूंकि हम छोटे थे. हम एक दूसरे के खेलों और खेलने के ढंग को काफी अच्छी तरह समझ चुके थे, और जितना हम सोच रहे थे, शायद उतने अलग थे भी नहीं। जैसे की उसके यहाँ भी सीवाइंया बनती थी, जो मैंने उसके टिफ़िन से खायी थीं. थोड़ी अलग भले ही थी, पर थीं सीवाइंया ही. एक-आध बार माँ को घुमा-फिरा के बताने की कोशिश की थी की मुझे वैसी वाली खानी हैं, पर सब कुछ बोल कर भी ज़ीशान के टिफ़िन का नाम नहीं ले सका. क्यूंकि मैं ज़ीशान को जानता हूँ, ये बात उन्हें नहीं पता थी. बता सकता था मैं, कि हाँ ज़ीशान मेरा नया और एक बहुत अच्छा दोस्त है. कैंपस के बाकी बच्चों से अच्छा। वो आपको भी जानता है, और आपकी दही वाली लौकी की सब्ज़ी को भी. पर पता नहीं, क्यूँ नहीं बताया मैंने।
छुट्टियां ठीक तीसरे सन्डे पर खत्म हो रही थी। ज़ीशान के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने चाइनीज़ फाइट सीन वाली आवाज़ें निकलना बंद कर दी। और एक बुनियादी सवाल पूछ डाला - क्यूँ?
"मामला शांत जो हो गया है" ज़ीशान ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया. और अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ में घर का कोई बड़ा आकर बैठ गया हो.
कैसा मामला? मेरा अगला सवाल किसी कुतूहली बच्चे की तरह अपने पंजो के बल उछल पड़ा.
"कुछ हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था, यार"
ऐसा उसने अपना दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखते हुए बोला।