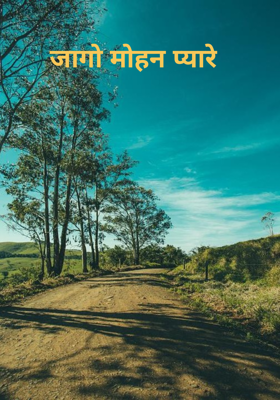02 - जागो मोहन प्यारे
02 - जागो मोहन प्यारे


यह कहानी आज से पच्चीस–तीस वर्ष पीछे जाती है, उस समय जब पढ़ाई समाप्त हुई ही थी और जीवन ने एक नई दिशा माँगी थी। उस मोड़ पर खड़े होकर मुझे एक बात बिल्कुल साफ़ दिखी—अगर जीवन में उड़ान भरनी है तो घोंसले से बाहर निकलना ही होगा। घर पर रहकर मैं रोज़ की जरूरतें तो पूरी कर लूंगा, पर सोच का आकाश सीमित ही रह जाएगा। दायरे छोटा करेंगे, सपने और छोटे हो जाएंगे।
यही समझ मुझे चंडीगढ़ ले गई। फिर अहमदाबाद, फिर मुंबई, बैंगलोर और न जाने कितने शहर मेरे जीवन के पन्नों पर दर्ज होते चले गए। कितनी किराये की जगहें, कितनी बस-ट्रेन की यात्राएँ, कितने अनजाने चेहरे—इन सबके बीच आखिरकार पच्चीस साल पहले एक ठिकाना मिल ही गया, जहां मैंने खुद को बसाया, और कह सका—हाँ, अब यह मेरा है।
इसी बीच पिता की मृत्यु हो गई। जीवन ने फिर से एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया—अब दोनों दुनिया कैसे संभाली जाएँ? एक ओर होमटाउन की जड़ें, दूसरी ओर वह शहर जहाँ मेरी मेहनत का गुंबद खड़ा था। शुरुआत में यह संतुलन पत्थर के पुल पर चलने जैसा कठिन था। कभी इधर, कभी उधर—दो-दो शहरों के बीच भागदौड़। लेकिन समय शिक्षक भी है और मरहम भी। दो सालों में सब कुछ पटरी पर आ गया। माँ के लिए भी एक रूटीन बन गया—सर्दियाँ मेरे पास और गर्मियाँ होमटाउन में। खर्च की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे कंधों पर थी, इसलिए उनके खाते में पैसे डालना और मिलने पर अतिरिक्त कैश देना एक रिवाज बन चुका था।
ऊपर से सब कुछ सलीके में दिखता था। पर भीतर कहीं एक अदृश्य चीड़ का बीज अंकुरित हो रहा था, जिसका मुझे आभास नहीं था।
एक शाम सारा पर्दा हट गया। माँ ने फोन पर बड़े सम्मान के साथ बताया कि उन्होंने चौकीदार को पैसे देने से इनकार कर दिया। मोहल्ले में एक चौकीदार था, सबकी सुरक्षा के लिए। हर घर से एक तय रकम वह लेता था। यह व्यवस्था वर्षों पुरानी थी। फिर एक स्थानीय नेता उभरा, जिसने यह सब अपने हाथों में ले लिया। चौकीदार की तनख्वाह भी वही देता और साल में एक बार लोगों से पैसे भी वही वसूल करता। मुझे यह तरीका कभी पसंद नहीं आया, पर दुनिया हर बात हमारी पसंद पूछकर थोड़े चलती है।
उस दिन जब नेता जी पैसे लेने आए, माँ ने छह महीने का पैसा दे दिया और बाकी छह महीने का रोक लिया। रकम बहुत मामूली थी। पर जो कारण उन्होंने नेता जी को दिया—वह तीर की तरह मेरे भीतर धँस गया।
“बुढ़िया को कौन पैसे देता है!”
छह सौ रुपए के लिए मेरी इज्ज़त को ऐसे सड़क पर पटक देना—मेरी समझ से परे था।
कुछ दिन बाद केबल वाला आया। उसने बताया कि फीस 100 से बढ़कर 150 हो गई है। माँ ने फिर वही बात दोहरा दी—
“बुढ़िया को कौन पैसे देता है!”
पचास रुपए के लिए एक और बदनामी। और यह सब उन्होंने शाम को मुझे बड़े गौरव के साथ सुनाया—मानो युद्ध में कोई किला जीतकर लौटी हों।
ये दो किस्से ही नहीं, बल्कि एक पूरी श्रृंखला की शुरुआत थे। आज पचास का, कल सौ का, परसों किसी और कारण का—यह सिलसिला रुका नहीं, फैला ही जाता रहा। किस-किस को जाकर समझाऊँ कि बुढ़िया उन चंद रुपयों के लिए मुझे दुनिया के सामने कंगाल घोषित कर रही है? कितना समझाऊँ? किसको समझाऊँ?
धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है। यह तो समाज का एक गुप्त अध्याय है। कई घरों में यही होता है—माँएँ अपने बेटों को बेवजह बदनाम कर देती हैं, बस एक छोटी-सी सुविधा पाने के लिए। कहीं छूट, कहीं फायदा, कहीं अपनी बात मनवाने के लिए—मानो यह कोई स्वाभाविक चाल हो, जो पीढ़ियों से चली आ रही हो।
और यह बात मैंने अकेले नहीं देखी। आसपास झाँको, तो हर दूसरे घर में यही नाटक चलता मिलता है। बेटे को कठघरे में खड़ा कर देना अक्सर सबसे आसान रास्ता बन जाता है—और दुख की बात यह है कि वह रास्ता चुना भी खूब जाता है।
इसलिए अगली बार जब कोई माँ, बहन या कोई भी औरत अपने ही लड़के के बारे में बुराई करते हुए नज़र आए, तो यह मत समझ लेना कि कहानी सिर्फ उतनी है जितनी सुनी। असल कहानी अक्सर उसके पीछे छिपी होती है—और वह कहानी कुछ और ही कहती है।
वैसे इस कहानी का अंजाम भी है पर वह अलग किस्सा है इसीलिए फिर कभी ।
जागो मोहन प्यारे… बहुत सो गए, अब जागने की घड़ी है ।
आजाद परिंदा