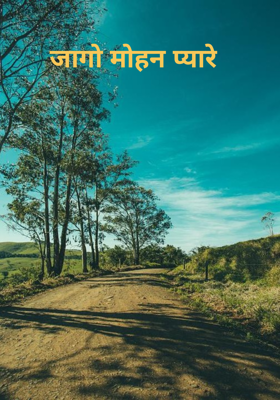शराफत का सफर
शराफत का सफर


रेलवे का नॉन-एसी डिब्बा, भीड़ से भरा हुआ, लोगों की आवाज़ों से गूंजता हुआ। गर्मी, धूल और पसीने की मिली-जुली गंध में मैं अपनी सीट खोज रहा था। दिन की यात्रा थी, आठ घंटे लंबी। आम तौर पर मैं ऊपरी सीट लेता हूँ—शांति मिलती है, भीड़ से थोड़ा बचाव भी रहता है। मगर इस बार जाने क्यों, नीचे की सीट बुक कर डाली थी। शायद किसी पुराने अनुभव की याद में, या बस यूँ ही। ट्रेन चली ही थी कि एक युवक मेरे पास आया—बीस-पच्चीस साल का, पर आँखों में चमक थी। "भाईसाहब, सीट बदल लीजिए ना... मेरी ऊपर वाली है।" उसकी आवाज़ में विनती थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया—"माफ़ करना भाई, इस बार नहीं।" असल में ऊपर की सीट तो मेरी पसंदीदा ही थी, लेकिन उसकी उम्र देखकर मना कर दिया। आखिर एक पचास साल का आदमी ऊपर बैठे और जवान लड़का नीचे चढ़े— उम्र का लिहाज़ भी कुछ होता है। वो चुपचाप लौट गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ‘ना’ कहूँगा। सामने की सीट पर एक जवान लड़की बैठी थी—स्मार्टफोन में खोई हुई, कानों में ईयरफोन, और एकदुनिया से बेख़बर। शायद उसी से सीट बदलने को कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो मुझसे कोशिश की थी। फिर जो हुआ, वो उम्मीद नहीं थी। अगले सात घंटे उस लड़के ने जैसे मेरा इम्तिहान ले लिया। कभी पैर हिलाता, कभी सीट पर उछलता, कभी जानबूझकर मेरे सामने खड़ा हो जाता। हर दो मिनट में मोबाइल की तेज़ रिंगटोन, ऊँची आवाज़ में बातें, और बीच-बीच में एक व्यंग्य भरी हँसी। एक बार जब वॉशरूम की तरफ गया तो पीछे से बीच वाली सीट खोल कर लेट भी गया । दुबारा सीट खोलने को राजी नहीं हुआ यहां तक कि टीटी भी कुछ नहीं कर पाया । त्यौहार का सीज़न था और वैसे भी इस ट्रेन में टीटी ज्यादा कुछ करता नहीं । मैंने शुरू में नज़रअंदाज़ किया, फिर एक-आध बार कहा भी—"भाई, ज़रा धीरे बात करो।" उसने मुस्कुराकर कहा, "जी अंकल, बिल्कुल।" और अगले ही पल, पहले से भी ज़्यादा शोर। सीट बंद करने की रिक्वेस्ट भी पूरी तरह इग्नोर कर दी । ट्रेन सरकती रही, बाहर खेत और धूल उड़ते रहे, पर मेरे भीतर एक झुँझलाहट उबलती रही। कभी-कभी मन हुआ कि मैं भी कुछ कह दूँ, कुछ सख़्त बोल दूँ। पर फिर वही पुरानी आदत—"चलो, कुछ नहीं कहते।" सात घंटे बाद ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुँची। मैं उतरा, बैग उठाया, और मन में एक भारीपन लिए प्लेटफ़ॉर्म पर कदम रखा। वो लड़का पीछे से हँसते हुए निकल गया—शायद उसे लगा, उसने जीत ली। मैं मुस्कुराया—क्योंकि असल में मैं हार गया था। अपनी शराफ़त से। उस दिन एक बात समझ आई—हर जगह शराफ़त दिखाना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी ज़रूरी होता है अपने लिए सख़्त होना। वरना ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लोग आपकी विनम्रता को आपकी कमज़ोरी समझ बैठते हैं। अगली बार ट्रेन में चढ़ा तब अपनी शराफत भी बेग में पैक करके एक तरफ रख दी और वही 8 घंटे की वापसी यात्रा बिना शराफत के ही की । संभव है वापसी यात्रा में मेरी वजह से कुछ लोगों को परेशानी हुई हो लेकिन शायद यह एक जरूरी कदम था । वापसी यात्रा कुछ अधिक दिलचस्प रही पर वह अगली बार ।