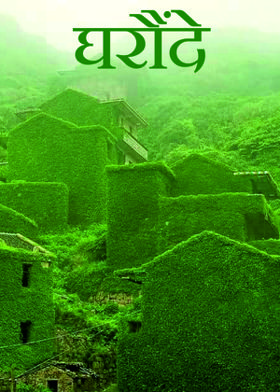लम्हे
लम्हे


दिन की गठरी खोल
समेट रही हूँ
होले होले गिरते लम्हे
बूँदों-से छलककर टपकते लम्हे।
पत्तों-से गिरते, उठते लम्हे
फूलों-से खिलते, मुरझाते लम्हे
हवाओं-से बहते,
हाथ में न आते लम्हे।
रेत-से फिसलते, सरकते लम्हे
पलकों से भागे सपनों से
नीम पके फल से लम्हे !
कभी सहरा सी धूप में
ओढ़े हुए बादल लम्हे
तो कभी सर्दियों में
हथेली पे पिघलते
धूप के टुकड़े लम्हे।
सिरों को खिंच कर जब तक
बाँधू दिन की गठरी
रात की टोकरी
खूल जाती है।
तारों से जड़े ढक्कन पर
चमकते लम्हे
पलकों पर सपनों की
सेज सजाते लम्हे।
अपने कंधे पर उठाये
नींदों के पैगाम;
झूकते, थक कर चूर लम्हे।
सुबहो-शाम की
गठरी और टोकरी
बाँधने-खोलने में
बीत रही है ज़िंदगी।
क्यूँ बाँधू इनको ?
क्यूँ सजाऊँ इनसे
अपने मन की अटारी ?
छोड दूँ गठरी के सिरों को खुला ही
बना लूँ रात के आसमाँ को
टोकरी का ढक्कन।
जीया जो पल उसे
बहा दूँ समय की नदी में
दीया बनाकर !
या हवा के परों पर रख दूँ
डेन्डिलायन्स जैसे…