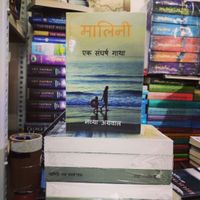हम कहां जा रहे हैं
हम कहां जा रहे हैं


एक राजा के सात बेटे थे। बिलकुल ठीक समझीं। आज फिर एक कहानी। कितना कुछ छिपा है इनमें, बचपन में सोचने की समझ नहीं थी अब समझने की इच्छा और ज़रूरत नहीं। ख़ैर छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। राजा के सात बेटे थे। एक दिन शिकार पर गए। सात मछलियां लेकर आए, सुखाने के लिए धूप में फ़ैला कर रख दीं। कूछ समय पश्चात देखने आए तो पाया मछलियां सूखी नहीं थीं। राजकुमारों ने पूछा तुम सूखीं क्यों नहीं? मछलियों ने कहा घास की ढ़ेरी आड़े आ गई। एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहे बात आगे बढ़ती रही।
राजकुमार आगे बढ़े, घास की ढ़ेरी से कारण पूछा। उत्तर मिला गाय चरने नहीं आई। गाय से न चरने का कारण जानना चाहा। गाय बोली आज ग्वाले ने दूध नहीं दुहा इसीलिए अभी तक मैंने चारा नहीं खाया। होते- होते राजकुमार ग्वाले तक पहुंचे। जानना चाहा कि उसने दूध क्यों नहीं दुहा। ग्वाला बोला मेरी बिटिया रो रही थी उसी को बहलाने में लगा था। राजकुमार भी धुन के पक्के थे। समस्या की जड़ तक पहुंचने का पाठ पढ़ चुके थे। सो ग्वाले की बेटी के पास गए- बोलो बिटिया रानी तुम क्यों रोईं? वह बोली मुझे चींटी ने काटा था। अब तक बिचारे राजकुमार भी थक चुके थे। ख़ैर, चींटी के पास पहुंचे। चींटी बोली कोई मेरे प्यारे से घर पर हाथ रखेगा तो मैं काटूंगी नहीं?
कहानी यहां समाप्त होती है। आजके सुपर हीरो की मारकाट वाली कहानियों पर पले बच्चों को बड़ी बचकानी ही बात लगेगी कि राजकुमार मछली पकड़ें, हर एक के पास जाकर बात करें, और तो और मछली चींटी जैसे प्राणी ही नहीं घास भी बात करे! ख़ैर यह उनकी सोच है जिसे हमने पोसा है। पर हमें इस कहानी से क्या मिला सोचें। यहां दो बातें मुख्य हैं- एक तो दोषारोपण की प्रवृत्ति और दूसरी स्व की, स्वायत्तता की, स्वामित्व की भावना। कैसे? देखते हैं-
अलग- अलग स्तर पर हुए वार्तालापों को देखें। हर कोई अगले पर दोष मढ़ रहा है – मछली से लेकर चींटी तक। छोटी सी बात है, बच्ची को तुरंत चुप कराता और दूध दुह डालता बो बात आगे ही नहीं बढ़ती। सुखाते समय ही यदि राजकुमार घास हटा देते तो बात शुरू ही न होती। कितना सरल परिष्कार है! दूसरी ओर चींटी सह न सकी कि उसके घर पर अनधिकार अतिक्रमण हो- घर आख़िर घर है, प्यार और परिश्रम से बनाया हुआ। उसमें कोई भी घुस आए सहा नहीं जा सकता। घर के स्वामी को प्रतिरोध का अधिकार है। एक तरफ सहनशीलता और धैर्य के संस्कार हैं, अभिजात्य है, मूल बात तक पहुंचने का विवेक है तो दूसरी तरफ असनशीलता, अधैर्य और आक्रामकता।
हमारे दैनंदिन जीवन में दोनों ही प्रवृत्तियों से हमारा सामना होता रहता है। पतला दूध देने पर दूधवाले को या पेपर देर से डालने पर पेपर वाले को हम उलाहना देते हैं और वह शांत भाव से अगले दिन का भरोसा दे कर चला जाता है। कई बार अपनी खीझ, भड़ास भी उस पर उतारते हैं, अपशब्द भी कहते हैं। पर वह शांति, संयम बनाए रखता है। सामने वाले को हर हाल में सुनना है और हम बात- बेबात, जो मन में आए बोलते जाने को अपना अधिकार समझने लगे हैं। बच्चे की अगर स्कूल से शिकायत आती है तो बिना सोचे, कई बार बच्चे के सामने ही हम स्कूल को, शिक्षकों को दोष देने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। बच्चे पर इसका कितना ओर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वह कितने गलत संस्कार पालेगा इसकी हमें किंचित भी परवाह नहीं। हमारा अहं संतुष्ट होना चाहिए बस। हमारी गाड़ी की जगह ग़लती से भी किसी और ने गाड़ी तो क्या साइकिल भी खड़ी कर दी तो हम गाली गलौज तो क्या हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। हमारे मरीज़ के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारा पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। तोड़- फोड़, मारा- मारी तो एक ओर ख़ून ख़राबे से भी पीछे नहीं हटते।
हमारे अविवेक के, असहनशीलता के, या आक्रामकता के कितने ही उदाहरण हम रोज़ देखते हैं। बड़े तो बड़े आज देश- विदेश में बच्चों में असहनशीलता और आक्रामकता के बढ़ते हुए आंकड़े चिंताजनक हैं। छोटे- छोटे बच्चे अपने ही भाई- बहनों पर, परिवार वालों पर घातक हमले कर रहे हैं। स्कूल- कॉलेज में आए दिन चाकू छुरियां और बंदूकें चलने लगी हैं। एकाधिक उदाहरण हैं असहनशीलता और आक्रामकता के हमारे चारों ओर। य़े संस्कार हमें दिए नहीं गए, हमने पाले हैं अपना अहं पोसने के लिए, अपनी वरीयता (?) बनाए रखने के लिए। समय आ गया है कि हम ठहरें और सोचें “आख़िर हम कहां जा रहे हैं!”