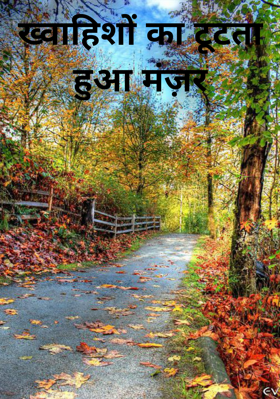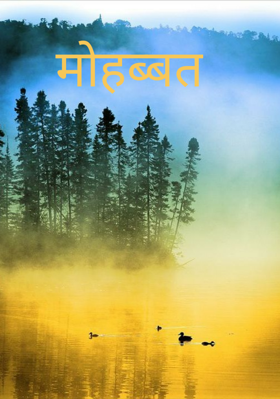जख़म-ए-तमन्ना
जख़म-ए-तमन्ना


ना जाने कब हमारे ज़ख़्म-ए-तमन्ना पुराने हो गए?
नासूर बनके धडकते थे सीनें में गुज़रे अब जमाने हो गए।
रिसतें जख़्म खत्म़ होते अवशेषों के बंद आशियाने हो गए।
दुवा-बद्दुवाओं से परे इन्स़ानियत के सारे फसाने खो गए।
रहमतों की कश्तीयों से गुल़ज़ार कहीं वो किनारे खो गए।
तन्हाईयों में इतरातें पलकों के सारे सपने यूँ ही सो गए।
इंत़ज़ार की घड़ियों के सारे सित़म सुहाने हो गए।
वादा ख़िलाफ़ी ना कर सके इतने हम दिवाने हो गए।
हसरत-ए-नाद़ान की दिलजोई के बहाने हो गए।
खुद के ही ज़ख़्मों से ना जाने कब हम अनजाने हो गए।