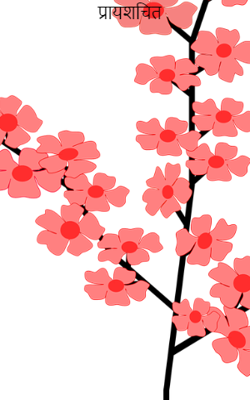"साँझ का दीया"
"साँझ का दीया"


किशन मल्लाह जब बाँसुरी की तान छेड़ता तो सारा गाँव सम्मोहित होकर बरबस घाट की ओर खींचा चला आता। यह उसका प्रतिदिन का नियम था । साँझ के समय वह नाव को किनारे से लगाता, मां नर्मदा में स्नान करने के बाद दीपदान करता और फिर घाट पर अपने गमछे का आसन लगाकर बांसुरी बजाने बैठ जाता। सर्दी , गर्मी हो या बारिश उसका यह नियम कभी ना टूटता। मानो उसने बारहमास का व्रत ले रखा हो।
एक दिन एक गुणी सज्जन जो कला के पारखी थे , किशन की सुमधुर स्वर लहरियो को सुनकर वही ठिठक गए। वह किशन से बोले- बेटा तुमने यह कला कहां से सीखी। किशन ने कहा मुझे अपने माता- पिता से विरासत में मिली। गुणी व्यक्ति ने कहा - अरे वाह!तुम्हारी यह कला इस गाँव और घाट के लिए नही बनी। तुम्हे तो एक ऐसा मंच चाहिए जहां तुम्हारी कला को नाम मिल सके। तुम मेरे साथ शहर चलो , वहां तुम्हें शोहरत और दौलत दोनों मिलेगी।
किशन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा- आप ठीक कह रहे हैं मगर मैं आपके साथ नही जा सकता।
यह बाँसुरी मेरे पिता की है, बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया था, माँ साँझ के समय मुझे इस घाट पर लेकर आती थी और दीपदान करती थी । वह हर दिन मुझे बाँसुरी बजाने के लिए कहती । मैं जब कहता मुझे बजानी नही आती तो कहती बाँसुरी ह्रदय से बजती है।जैसे आये वैसे बजाओ , डूबते सूरज की ओट से तुम्हारे पिता तुम्हें देख रहे है। सोचो बाँसुरी के स्वर इस दीपक के प्रकाश के साथ तुम्हारे पिता तक पहुँच रहे हैं । कुछ दिनों बाद ही मां भी पिताजी के पास चली गई। तब से आज तक मैं हर साँझ नियमित दीपदान करता हूँ और बाँसुरी बजाता हूँ। क्योंकि इस साँझ के समय में मेरे माता-पिता मेरे साथ होते है। अब आप ही बताइए मैं इस घाट और गाँव को कैसे छोड़ सकता हूँ। सज्जन व्यक्ति की आंखे आंसुओं से सराबोर हो गई। किशन के सर पर हाथ रखकर वह बिना कुछ कहे चल पड़े, मानो इस सुरमई सांझ को अपनी आंखों और दिल मे समेटकर ले जा रहे हो।