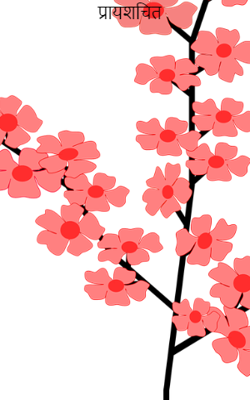अपनी देहरी ?
अपनी देहरी ?


उस दिन किसी ऑफीशियल कार्य से अपने गांव के पास के कस्बे में जाना हुआ तो अचानक मेरा मन किया कि एक चक्कर गांव का भी लगा लें। यूं तो करीब तीस पैंतीस साल का समय बीत चुका था मुझे गांव छोड़े, बहुत कुछ बदल गया था आसपास, जीवन भी किसी और दिशा में बह निकला था, पर पता नहीं क्या था कि उस दिन गांव बहुत खींच रहा था। सरसों फूलने के दिन थे तो मैं पैदल ही खेतों के बीच की पगडंडी पर चली जा रही थी बीते हुए बचपन और किशोरावस्था को मन ही मन जीती। न जाने कहां-कहां से स्मृतियां बंद किवाड़े खोल भागी चली आ रही थीं। अब यूं तो गांव से कोई भी रिश्ता नहीं रहा था हम लोगों का, न घर दुआर, जमीन, न बाग बगीचे लेकिन फिर भी माटी का जुड़ाव शायद इतनी आसानी से नहीं जाता।
गांव की शुरुआत पर ही पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी, मटमैली धोती में लिपटी एक आकृति दिखाई पड़ी। पास पहुंच कर देखा तो पहचान लिया, ये बृजरानी बुआ थीं। उनकी धुंधलाती आंखें मुझे नहीं पहचान सकी थीं पर हमारी यादों में उनकी सुनाई कहानियों के साथ साथ वो भी संपूर्ण रूप से जीवित थी। परिचय देने पर उनके चेहरे पर अजीब सी ललक और खुशी पसर गई। मैंने पूछा, "बुआ यहां अकेले गांव बाहर क्यों बैठी हो !"
पेड़ के नीचे सिंदूर में लिपटे भगवान की ओर इशारा करते हुए बोलीं, "बिटिया, अब यहीं ठिया है और यही आसरा।"
बृजरानी बुआ अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत छोटी अवस्था में ही अपने मायके वापस आ गई थीं। और चार भाइयों की इकलौती बहन को भाभियों समेत पूरे परिवार ने, परिवार क्या पूरे गांव ने पूरे लाड़ से संभाला था। बुआ थीं भी ऐसी कि जरूरत किसी की भी हो, कैसी भी हो, एक पांव से पूरे गांव में चकरघिन्नी की तरह घूमती रहती थी। सब के काम आने वाली, सबके दुख दर्द साझा करने वाली बुआ ने घरों में ही नहीं लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी।
लेकिन समय कब एक सा रहता है, पुराने गए, नए आए, बुआ भी शारीरिक रूप से अशक्त हो गई थीं। यूं जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे न उन्होंने कभी अपनी देहरी की कमी महसूस की न जमीन की। पर आज जीवन के इस पड़ाव पर वे कितनी निस्सहाय बैठी थीं। ऊंचा बड़ा फाटक और उसके भीतर खुला खुला आंगन जिसमें सांझ सबेरे आकाश भी टिक कर आ बैठता था अपने सूरज, चंदा तारों के संग, हर नए बंटवारे के संग कुछ और सिकुड़ता सिकुड़ता ज्यूं अंधरी कुइंया हो गया था. जमीन, देहरी से ले बरतन भाड़े तक सबका हिस्सा-बांट तो हो गया पर समूचे गांव की बुआ...!!! बुआ का बंटवारा कैसे होता और फिर बुआ के पास बेपनाह प्यार से भरपूर दिल के और कोई सम्पत्ति तो थी ही नहीं।
बुआ से बातें ही कर रहे थे कि करीब उन्नीस बीस साल की एक लड़की साइकिल चलाते हुए आई और रुक गई। उसने मेरी तरफ एक प्रश्नवाचक निगाह डाली और बुआ से बोली, "कुछ मिला है खाने को सवेरे से?" उनके कुछ कहने से पहले ही दो मिठाई के टुकड़े अपने झोले से निकाल उनके सामने बढ़ा दिए। बुआ के झुर्रियाये चेहरे पर ढलती धूप सी मुस्कान डोल गयी, कंपकपाते हाथों से उसका सिर सहलाती हुई बोली "काहे सारी दुनिया से बैर लिए डोला करती है रे, करेजा फुंक जई।"
"हां तो, तुम तो सारी दुनिया को पियार बांटे रहौ न, तुम्हरे करेजा में कौन चंदन लेप लाग गा, चंदन छोड़ो, एक कुठरिया और दुई रोटी न ढंग से नसीब होत है, सारी जिंदगी खप गई तुम्हार।"
ये सरोज थी, गांव की ही एक लड़की जो पास के डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाती थी। बचपन में ही मां गुजर गई थी उसकी। किसी भी गलत बात पर उसका आक्रोश, हमेशा ही एक सजग आक्रमकता से भरे रहना पता नहीं उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था या अपने भीतर की निरीहता को छुपाये रखने का तरीका। इस समय भी बुआ की दशा पर बतियाते-बतियाते उसका चेहरा आक्रोश से तमतमा गया था।
वो बोली, "अभी अगर दादी के नाम घर जमीन या बाग बगीचा होता तो सब इनको पूछते।"
तब तक आसपास और भी गांव की दो चार महिलाएं आ जुटी थीं। उनमें से एक बोली, "धत् पगलिया, लड़किन के नाम कहीं जमीन-जायदाद होत है। बियाव कई के उनका दूसर गांव घरै जाय का होत है तो मइके मा उनकेर हिस्सा कइस।"
तमक कर बोली सरोज, "अच्छा तो ई जो दूसर घर होत है, हुंआ होत है का हिस्सा...नहीं न....बिदा करैं के समय तो ढेर टेसुआ बहा के सब्बे कोई कही....बिटिया हो, बछिया हो दूनो देहरी की लाज राखयो....लाज राखन की जिम्मेदारी दूनौ देहरी की और हक एकऔ मां नाहीं। वाह भई वाह...."
सरोज की बात में दम लगने पर भी वे लोग उससे सहमत नहीं हो पा रहीं थीं। एक अजीब सी कशमकश झलक रही थी उनके चेहरों पर। बरसों से एक पगडंडी पर चलते रहो तो नयी राह पर अचानक थोड़ी मुड़ जाया करते हैं पैर।
पर इन सब से परे थी बुआ के मन की पीड़ा, उन्होंने तो ताउम्र घर दहलीज की कमी महसूस ही नहीं की थी। उनका कहना था कि घर जमीन होने से अगर चार लोग दरवाजे पर जुटे भी रहते तो क्या उससे मन का सुख मिल जाता ? सरोज की सोच इसके बिलकुल इतर थी, उसका कहना था, जरूरतें तो पूरी होतीं और गांठ मजबूत हो तो सम्मान मिल ही जाता है। और मैं सोच रही थी कि दो पीढ़ियों के बीच के इस वैचारिक और भावनात्मक अंतर पर कैसे एक पुल रचा जाए। कुछ तो ऐसा करना होगा कि न किसी बृजरानी बुआ का ठिया गांव बाहर के पीपल का चबूतरा हो, न किसी सरोज के भीतर की असुरक्षा आक्रोश बन फूटे। बुआ के कंपकंपाते सुर के साथ जब सरोज की सपनों से लबरेज आवाज बासन्ती खेतों पर लहरायेगी, धरती की छाती तो तभी जुड़ायेगी।