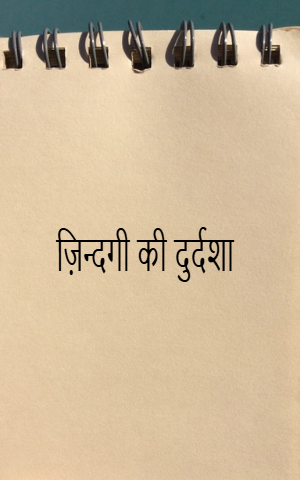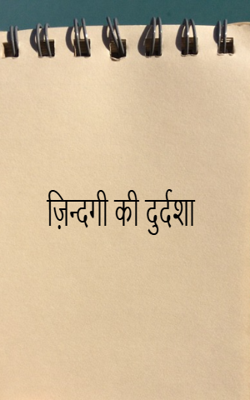ज़िन्दगी की दुर्दशा
ज़िन्दगी की दुर्दशा


क्या कोयल, क्या कौवा
शहर के शोर ने सबको शांत कर दिया।
केवल बड़ी-बड़ी इमारतें
आसमान से बात करती हैं।
ज़मीं पर अब मानस के चिथड़े और लोथड़े मिलते हैं
और ज़िन्दगी की इतनी दुर्दशा भी आम-सी लगती है।
सपनों को चाहे उड़ान न मिले,
मगर हर चीज़ के दामों पर पंख ज़रूर लगे हैं,
देखिये ज़रा, छूते ही बढ़ जाते हैं।
सरकार टैक्स मिशन के अन्तर्गत
आधा पैसा हमसे लेकर जाने कहाँ लगाती है
न सड़कें भली, न शिक्षा के केंद्र भले,
मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं होती
तो फिर हेरफेर किसने और क्यों की ?
न पेड़, न हवा,
हर गली में नाली गंगा सी बहती है,
खिड़की खोले तो मिले ये नज़ारा
और न खोले तो घुटन से भर जाये कमरा सारा!
कहो! क्या ये सब उचित है ?
तब भी किया क्या हमने?
सड़कों पर चलते वक़्त,
कचड़ा वहीं फेंक जाते हैं
और संविधान का नारा लगाते हैं।
हमसे बड़ा असभ्य और पाखंडी देखा है आपने ?
न खुद कुछ करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं।
अरे भई ! समस्या क्या है ?
भारत की नागरिकता तो सबके पास है
मगर भारत किसी के पास नहीं।