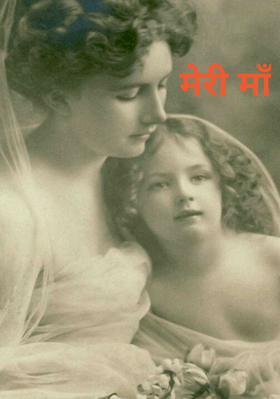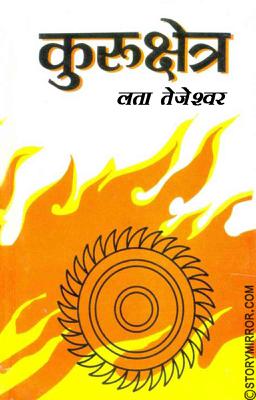पिता
पिता


लुटा देता है अपना,
जीवन, रुप, संपदा, यौवन
यानि 'सब कुछ'
तब कहीं गढ़ पाता है,
खुद में एक मुकम्मल किरदार
पिता का।
जो तपती दुपहरी में होता है
एक सघन छायादार वृक्ष -सा,
वहीं पूस की सघन ठिठुरन में
होता है एक बंद घर - सा,
सावन के मेह में होता है स्मित पवन- सा
उसकी डांट, मानो ऐसे हो जैसे,
ऊंचे स्वर का एक वस्त्र ,
बुना हो जिसका हर धागा असीमित नेह में,
वो नहीं होता कोई भगवान,
होता है उसका दर्जा
अव्वल कहीं ईश से भी ज्यादा,
वो होता है एक ऐसा दरख़्त,
होता है जिसकी हर शाख़ पर
संतानों का अधिकार रूपी बसर।
फिर जब निकल आते हैं संतानों के पर,
क्यूँ हो जाता है वही पिता
पतझड़ में खड़ा एक दरख़्त - सा।