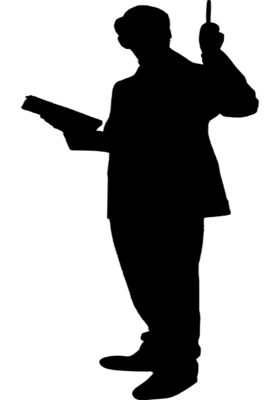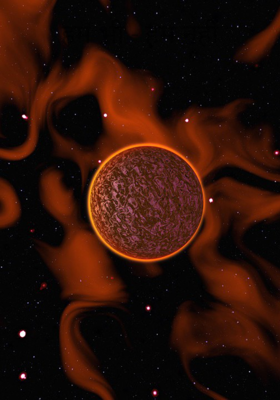सच की दृष्टि में उगते धुँधलके
सच की दृष्टि में उगते धुँधलके


सच को झूठ की चादर में लपेटना,
या झूठ को सच का मुखौटा पहनाना—
यह कोई कला नहीं,
बस एक सभ्यता का घाव है,
जिसे हम हर दिन ढोते हैं।
अरावली की दरारों में,
जहाँ पत्थर भी अब
सरकारी ‘रिसोर्स’ कहे जाते हैं।
अफ़ीम बीनती लड़की
अब बाघ से नहीं,
खनन कंपनी के ट्रकों से डरती है—
जो उदयपुर से प्रतापगढ़ तक
ज़मीन को छीलते हुए
उसके बचपन की लोरियों को कुचल जाते हैं।
और, टकराती है मार्बल की खदानों के बुलडोजरों से।
उसकी आँखों में एक ही सवाल—
“कहाँ है वो जंगल
जहाँ मेरी माँ
देव-डूँगर पर दीप रखती थी?”
अब तो वहाँ लगी है
“बायो-डायवर्सिटी पार्क” की पट्टी,
और सुरक्षा-कर्मी गिनते हैं
हर फूल, हर पत्थर,
लेकिन नहीं देखते उसकी आस्था।
अब जंगल
न हाथी के हैं, न भालू के,
न भील-मीणा के,
बल्कि बंद कमरों में तय होते
परियोजना प्रस्तावों के हैं—
जहाँ कागज़ पर बसे गाँव
हकीकत में उजड़ जाते हैं।
अरावली की छाँव
अब EIA रिपोर्ट की परिभाषा बन चुकी है,
जहाँ पेड़ों की गिनती तो होती है,
पर बच्चों की हँसी दर्ज नहीं की जाती।
अफ़ीम के खेत
अब केवल नशा नहीं,
एक अनकही अर्थव्यवस्था हैं,
जहाँ लड़की की हथेलियों की लकीरों में
शामिल है उसकी ज़मीन से जुदाई की तक़दीर।
उसकी माँ
अब गीत नहीं गाती,
बल्कि मेलों में “लोक-संगीत कलाकार” बन
अपने ही विरासत को किराए पर देती है,
और हर तालियों की गूँज में
उसकी आत्मा सिकुड़ती जाती है।
यह कविता नहीं,
एक चेतावनी है—
कि जब पंचतंत्र की कहानियों में
भीलों को बहादुर बताया जाता है,
तो हकीकत में उनके गाँव
'वन्यजीव गलियारा' घोषित कर दिए जाते हैं,
और उनकी आज़ादी
कानून की धाराओं में खो जाती है।
सच यह है—
कि बांसवाड़ा की पहाड़ियों में
अभी भी लड़कियाँ अफ़ीम चुनती हैं,
लेकिन अब वे
ड्रोन की गूँज से डरती हैं,
सरकारी कैमरों से छिपती हैं,
जिन्हें ‘विकास’ की निगरानी कहा जाता है।
झूठ यह है—
कि हमने मान लिया है
कि "विकास" की रोशनी
हर चेहरे पर बराबर पड़ती है।