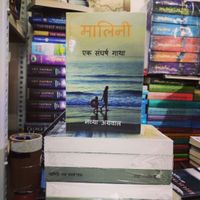स्वयं की निजता
स्वयं की निजता


प्रत्येक आत्मा की नैसर्गिकता की समझ अनिवार्य होती है। प्रत्येक जीवात्मा के आदि अनादि स्वभाव संस्कार नैसर्गिक होते हैं। लेकिन जिन्हें यह समझ नहीं होती है वे प्रायः दूसरों के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी ही समझ को थोपने का निरर्थक और अस्वाभाविक प्रयास करते हैं। पुरातन काल से परंपरागत तौर पर अधिकांशतः ऐसा होता आया है। पेश है एक व्यक्ति के जीवन का वाकया जो आपको इस विषय को ज्यादा अच्छी तरह से स्पस्ट करने में सहयोगी होगा।
एक बार हुआ यूं कि एक व्यक्ति के कंधे पर अनायास ही एक पक्षी आकर बैठ गया। उस पक्षी के पंख बड़े थे। कलंगी और चोंच भी बड़ी थी। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जिसके कंधे पर वह पक्षी आकर बैठा था, उसने केवल कबूतर पक्षी ही देखे होंगे। कहीं ऐसी जगह रहा होगा जहां केवल कबूतर ही कबूतर रहे होंगे। बाकी इस प्रकार के अन्य प्रजातियों के पक्षी उसने कभी देखे ही नहीं होंगे। ना ही कभी ऐसे किसी अन्य पक्षियों की प्रजातियों की उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति मन्द बुद्धि रहा होगा। उस व्यक्ति ने उस पक्षी को देखा तो उसे उस पक्षी के प्रति बहुत स्नेह उमड़ा और उसने अपने मन में सोचा कि इस बेचारे कबूतर की किसी ने चिन्ता ही नहीं की। किसी ने इसकी देखभाल की परवाह ही नहीं की। इसलिए ही इसके पंख बहुत बड़े हो गए हैं। चोंच और कलंगी भी बड़ी हो गई हैं। उसने उस पक्षी को बड़े प्यार से पकड़ा और कहा कि मैं तेरी हुलिया ठीक कर देता हूं। फिर तू ठीक हो जायेगा। फिर तू ठीक कबूतर जैसा लगने लगेगा। उसने कैंची लाकर उसके पंख छोटे कर दिए। चोंच भी छोटी कर दी। कलंगी भी छोटी कर दी। तब कहा कि अब तू बिल्कुल ठीक कबूतर जैसा लगता है। अब तू ठीक कबूतर जैसा हल्का हो गया है। अब तू आसानी से सहजता से उड़ सकता है। अब तेरी चोंच भी छोटी कर दी है। अब तू अपना भोजन भी आसानी से निगल सकता है। तब उसने उसे उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन अब वह पक्षी उड़ता ही नहीं था। उसे बहुत उड़ाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उड़ सका। उसके सामने भोजन डाला गया। लेकिन उसे छोटी चोंच से खाना खाने में भी कठिनाई होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह असलियत में नैसर्गिक रूप से कबूतर था ही नहीं। वह एक दूसरी ही प्रजाति का पक्षी था जो शक्ल से थोड़ा कबूतर जैसा लगता रहा होगा। पर नैसर्गिक स्वभाव से वह कबूतर नहीं था। उसके पास प्रकृति प्रदत्त पंख, चोंच और कलंगी थी। जैसी उसकी प्रकृति थी वैसा ही उसका उपयोग करना भी उसका स्वभाव था। लेकिन उसकी स्वाभाविक चोंच (मुखमंडल) जो जैसी थी वह वैसी नहीं रही। उसे भोजन को पकड़ने में कठिनाई होने लगी। उसके स्वाभाविक पंख जो जैसे थे, जिनसे वह उन्मुक्त आकाश में उड़ता था (उड़ सकता था); काट कर छोटे कर दिए गए थे। वे वैसे स्वाभाविक नहीं रहे। वह उड़े भी तो कैसे उड़े? वह नहीं उड़ सका।
अधिकांश मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ही तो करते हैं? मनुष्य यह जरा भी परवाह नहीं करते कि कम से कम यह तो जानें समझें कि उनके बच्चों के स्वाभाविक संस्कार कैसे हैं? उनका स्वाभाविक रुझान क्या है? परिणाम जब अवांछित होते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं। अधिकांश मनुष्यों की यह वृत्ति ही बन चुकी है। जितना उन्हें उनके अतीत के अनुभवों का ज्ञान होता है उसी को अपने बच्चों पर थोपने का उनका स्वभाव बन चुका होता है। कालांतर में यही जीवन की एक परंपरागत शैली बन जाती है। अधिकांश मामलों में इस प्रक्रिया में बच्चों के आंतरिक नैसर्गिक व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। वे अविकसित ही रह जाते है। उनके जीवन भर का स्वाभाविक विकास और सुखद एहसास थम जाता है। प्रकृति का नियम तो स्वाभाविक और सकारात्मक गुणों और संस्कारों के अनुकरण की बात करता है। लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इसे विश्व ड्रामा में उनके साथ ड्रामा अनुसार हैपनिंग ही कह सकते हैं।
इसलिए ही वैश्विक आंकड़ों के हिसाब से समझें तो गुणों और कलाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में अधिकांश के जीवन में अन्तिम परिणाम यह होता है कि वे समझौतावादी हो जाते हैं। यही सोच कर चलते रहते हैं कि अब तो असफलता और असंतुष्टता ही हमारी नियति है। स्वाभाविक नैसर्गिक निजता का विकास नहीं होने के परिणाम का एक दूसरा भी पहलू होता है। वह दूसरा पहलू है - उनकी मानसिक ऊर्जा कोई अन्य अनिश्चित अवधारणा की ओर उन्मुख हो जाती है जहां उसके स्वाभाविक गुणों और संस्कारों की ऊर्जा को गति मिलती है। उसके परिणाम अनिश्चित रूप वाले होते हैं। किसके जीवन के परिणाम कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक होते हैं यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि की अधिकांश नकारात्मकताओं और विरोधाभासों के पीछे मात्र यही एक कारण होता है कि मनुष्य या तो संयोगवश या अन्यान्य कारणों से, ना चाहते हुए भी अपनी स्वाभाविक गुण स्वभाव की प्रकृति से विमुख हो जाता है।
प्रत्येक आत्मा की नैसर्गिक निजता का आकाश ही उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्वयं की निजता के अंतराकाश में ही सृजन के सुमन खिलते हैं। स्वयं की निजता का अंतराकाश एक ऐसा आकाश होता है जिसमें प्रवेश करते ही आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां सक्रिय हो उठती हैं। जब ये दोनों शक्तियां जागृत हो सक्रिय होती हैं तो सृजन का कार्य स्वाभाविक रूप से घटता है। यह अंतर के आकाश में दीर्घकालीन प्रवेशता ही सम्पूर्ण संतुष्टता अर्थात संपूर्णता के प्रादुर्भाव के लिए अत्यंत अनिवार्य चीज है। इस प्रक्रिया में चलते चलते धीरे धीरे संपूर्ण संतुष्टता जीवन के आस पास नाचने लगती है। इसलिए स्वयं की और अन्यों की नैसर्गिक निजता की व्यापक समझ होनी चाहिए। तब ही नृत्य और नर्तक की एकता की आत्मसंबद्धता होना संभव होता है। जहां इन दोनों की आंतरिक एकता होती है वहां परिपूर्णता भी है। वहां संतुष्टता भी है। वहां समूर्णता भी है। इसलिए स्वयं की नैसर्गिकता की निजता में ही चलते चलना अपना स्वभाव बना लीजिए। दुनिया की सभी कृत्रिमताओं (आर्टिफिशियल) के बनाए हुए स्वभाव को तिलांजलि देते जाइए।