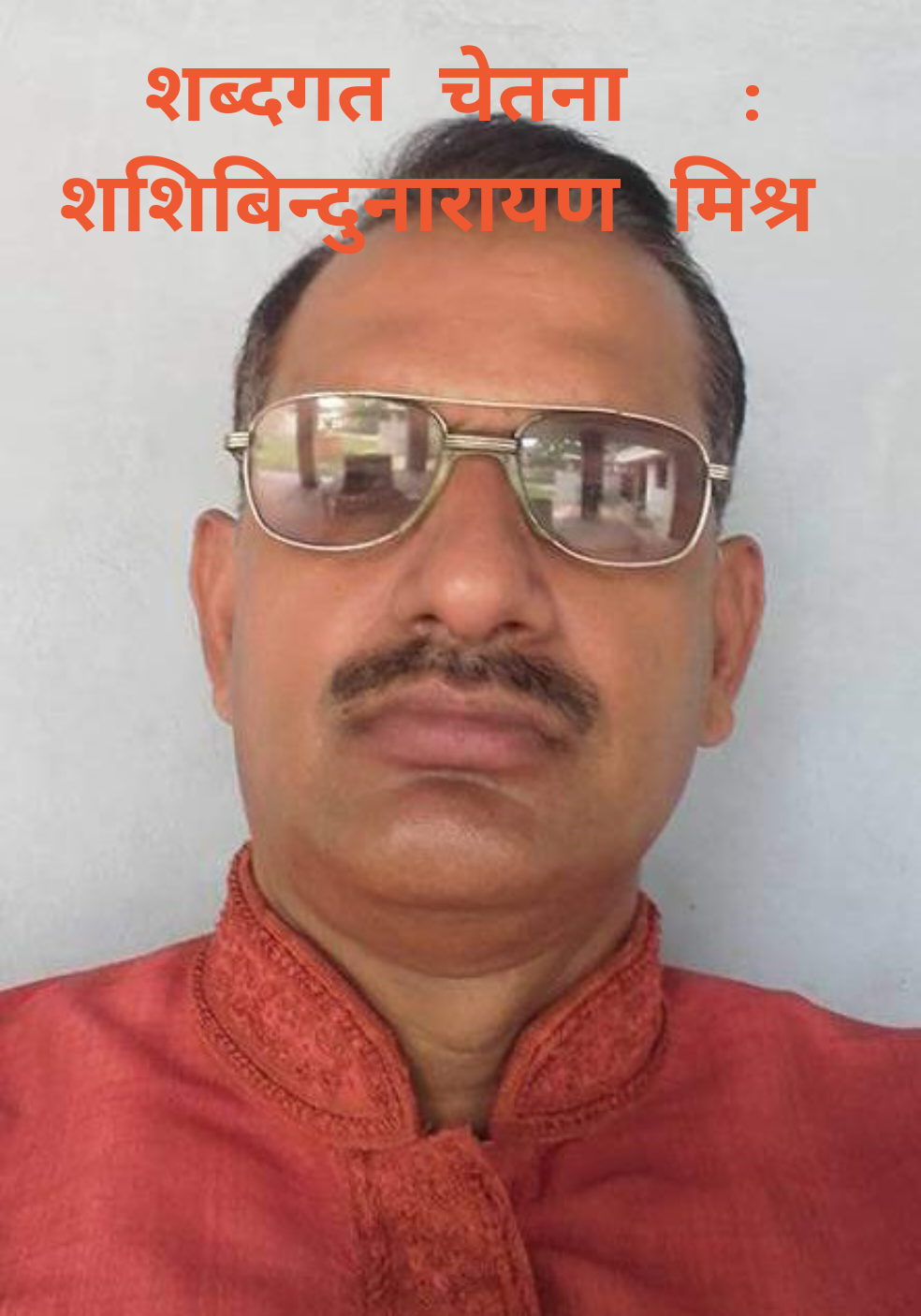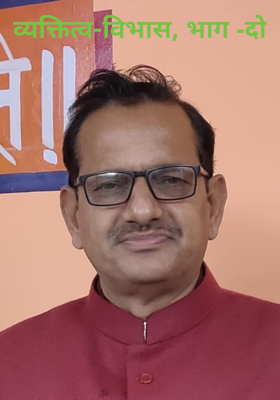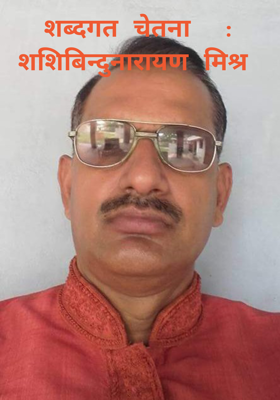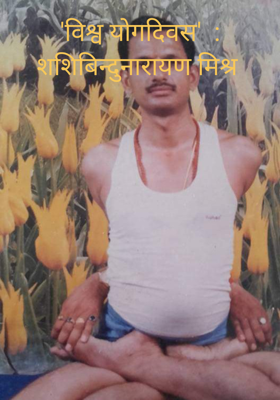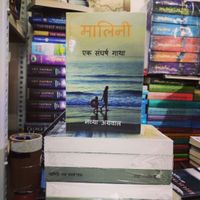शब्दगत चेतना
शब्दगत चेतना


भोजपुरी- संस्था 'यायावरी' द्वारा गोकुल भवन गोरखपुर में दिनांक - 09.06.2024 रविवार को आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। मेरे साथ भोजपुरी कवि कुमार अभिनीत जी, ग़ज़लकार सृजन गोरखपुरी जी, कवि प्रेमनाथ मिश्र जी, कवि चंद्रेश्वर परवाना जी , वरिष्ठ कवि नर्वदेश्वर सिंह 'मास्टर साहब' और गीतकार रामसमुझ 'साँवरा' जी भी थे। अतिशय प्रचण्ड गर्मी मे आयोजित इस कार्यक्रम मे जाने से मन घबराता रहा । 4 बजे सायं कार्यक्रम मे पहुँचा, वातानुकूलित हाल मे आयोजन को देखकर, काफी सुकून मिला। समारोह मे जलपान के लिए शुद्ध जल, काफ़ी , समोसा, कटलेट वगैरह की उत्तम व्यवस्था रही । हाल के दाईं ओर द्वार पर लगे बुक स्टॉल पर 'संस्मृति-सुधा' के प्रकाशक- सम्पादक रवीन्द्र मोहन त्रिपाठी जी अपना बुक स्टॉल छोड़ गर्मजोशी से मिले और ले जाकर जलपान कराया। कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण मुझे रवीन्द्र मोहन त्रिपाठी जी और भोजपुरी संगम के संयोजक कुमार अभिनीत जी ने ही दिया था।
सायंकालीन सत्र मे मंच पर भोजपुरी के किसी बड़े कलाकार से साक्षात्कार के क्रम मे भोजपुरी मे ही भाषा पर विचार किया जा रहा था। जब हम कार्यक्रम मे पहुँचे तो फिल्म इंडस्ट्री मे जाने पर श , ष और स के उच्चारण को लेकर जो समस्याएँ आती हैं, बातचीत मे उसी पर साक्षात्कार- कर्त्ता का ध्यान केंद्रित था। कार्यक्रम मे बीच-बीच मे प्रेमनाथ मिश्र जी मुझसे इस विषय पर चर्चा भी करते रहे।
आइए उक्त बिंदु पर हम अपने ढंग से भी विचार करते हैं। हिन्दी भाषा मुझे सर्वाधिक दुरूह लगती है, क्योंकि इसमें संसार की अनेक भाषाओं की ध्वनियाँ / शब्द आगत हैं, उनके प्रयोग को लेकर तरह-तरह की धारणाएँ हैं, ख़ासकर अरबी-फ़ारसी की ध्वनियाँ (क़, ख़ , ग़, ज़ , फ़ ) जहाँ नुक्ते का प्रयोग होता है , इनका उच्चारण संस्कृत -हिन्दी के क, ख, ग, ज, फ के उच्चारण से भिन्न होता है।
जैसे -जंग -ज़ंग (दोनों शब्द फ़ारसी भाषा से हिन्दी मे आगत हैं, पर दोनों का उच्चारण भिन्न है और अर्थ भी। 'जंग' स्त्रीलिंग मे प्रयुक्त होता है, इसका अर्थ रण, युद्ध, समर है। ज़ंग पुल्लिंगवत् व्यवहृत होता है जिसका अर्थ तरावट से धातुओं मे लगने वाली मैल है। आप देख सकते हैं कि जंग और ज़ंग दोनों शब्द फ़ारसी भाषा के हैं, एक जैसे लग भी रहे हैं, पर
एक स्त्रीलिंग मे प्रयुक्त हो रहा है और दूसरा पुल्लिंगवत् और दोनों का उच्चारण भी एकदम भिन्न है। अख़बार शुद्ध है , अखबार अशुद्ध शब्द है। इनका हम लोग दैनंदिन जीवन मे अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब जानबूझकर ग़लत उच्चारण करते हैं। हिन्दी पट्टी वाले अभ्यास के अभाव या न जानकारी मे ऐसा करते हैं। मै जब पीछे देखता हूँ, पढ़ाई के दिनों की यादें। जो हमारे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे, उनमें अधिकतर मिडिल पास थे, पर उनमें भाषा की अद्भुत व्यवहारगत समझ थी, उनमें अभ्यास भी था और जानकारी भी ।
भाषा के प्रति सावधानी व्यक्ति को अनुशासनप्रिय बनाती है,ऐसा कहा जाता है। सोशल मीडिया पर भी अपने को सफल और बड़ा कवि-आलोचक मानने वाले अनेक रचनाकार भी ह्रस्व-दीर्घ वर्तनी की आये दिन त्रुटियाँ करते देखे जाते हैं। मैने अनेक व्हाट्सअप 'ग्रुप्स' मे जिम्मेदार लोगों को संकेत भी किया, पर लोग ईमानदारी और दृढ़ता से सुधार की कोशिश नहीं करते है। हिन्दी के लोगों को हड़बड़ी में गड़बड़ी से हर सम्भव बचने की कोशिश करनी चाहिए।
सर्वप्रथम हम दो उदाहरण लेते हैं -- "कच्छा और कक्षा" में ज़रा अन्तर देखिए।
उदाहरण-01--"च्छ" और "क्ष" में अन्तर । "च्छ" से "कच्छा" जैसा शब्द अर्थात् Underwear -अण्डरवियर" होता है और "क्ष" से "कक्षा" अर्थात् विद्यार्थियों की श्रेणी, दर्जा या परिधि ,अंग्रेजी में इसे आप Class room - "क्लास-रूम_ या "Circle" "सर्किल" कहते हैं।
उदाहरण--02---च्छ - "शुभेच्छा" = शुभ की इच्छा, अंग्रेजी में यह "Well wish / well desire" है।
और क्ष- 'शुभेक्षा' (शुभ ईक्षा) अंग्रेजी में यह working of the senses, sight है। इसे और भी स्पष्ट करते हैं । शुभेक्षा (शुभ ईक्षा) मूल शब्द 'ईक्षा' , ईक्ष् धातु से बना है , जिसका अर्थ है -शुभ दृष्टि से देखना या ताकना । उसी से ईक्षक, ईक्षण, ईक्षा और ईक्षित जैसे शब्द बनते हैं।
उदाहरण -03---ऐसे ही "दीपोत्सव" में अपने को बड़ा कवि मानने वाले अनेक दम्भी लोगों ने "दीया" (दीपक) की जगह "दिया" लिखा, एक-दो बार नहीं, वर्षों से मै सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर यह देख रहा हूँ।
इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अन्तर है, "दीया" अंग्रेजी में "Lamplight" अर्थात् "दीपक" है और "दिया" भूतकालिक क्रिया है तथा अंग्रेजी में यही शब्द "Gave away" है।
उस लिखने का क्या लाभ जहाँ पढ़ने / बोलने / लिखने के दौरान अर्थ की जगह अनर्थ निकलता हो ? हमारे यहाँ "उपनिषद्" शब्द इसीलिए आया था , क्योंकि शिष्य अपने गुरु के पास निरन्तर बैठकर सीखता था, जब तक कि उसका गुरु जीवित रहता था। अब तो अधिकतर लोग पढ़ाई के बाद नौकरी मिलने पर "अहं ब्रह्मास्मि" वाली स्थिति के शिकार हो जाते हैं। अब नौकरी मिलने के बाद सीखने और पढ़ने की ललक लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि आज का छात्र भी केवल नौकरी के लिए ही पढ़ता है, शिक्षालयों से जुड़ता है, ज्ञानार्जन के लिए नहीं। बहुत सारी चीज़ें गूगल, इंटरनेट और सहायक पुस्तकों के ज़रिए उपलब्ध हैं, तो छात्र किसी शिक्षक को गुरु मानकर तपस्या / साधना क्यों करे ? आठ-दस प्रतिशत छात्र ही साधना मे लगे दिखते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए कि शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित होने से शैक्षिक और सामाजिक जीवन में जो उच्छृंखलता आयी है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है , सरकारें चाहे जितना नित-नव प्रयोग करती रहें। ज्ञान के लिए योग्य गुरु का सानिध्य आज भी उतना ही आवश्यक है, जितना पहले था।
नयी पीढ़ी मे बहुत ही कम लोग हैं जो ज्ञान-पिपासु हैं और गुरु का सानिध्य पाना चाहते हैं।
एक बात और है कि यदि आपने छोटे या बड़े किसी को ज़रा-सा भी सुझाव देना चाहा, तो सामने वाला ताल ठोककर दो-दो हाथ करने के लिए तैयार बैठा है। भोजपुरी मे कहावत है--"भल चाहें जेठानी, तs रखावें आपन पानी।"
ऊपर श, ष, स की चर्चा आयी है। तीनों ऊष्म व्यञ्जन वर्ण हैं। भाषाविज्ञानियों द्वारा इन्हें ऊष्म व्यञ्जन कहने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि है।
श , ष , स तीनों का उच्चारण तीन तरह से होता है और इनके उच्चारण के समय श्रोता को लगना चाहिए कि वक्ता तीनों वर्णों का अलग-अलग ढंग से उच्चारण कर रहा है।
श का उच्चारण आप तालु की सहायता से, ष का उच्चारण मूर्द्धा से और स का उच्चारण मुँह मे आगे के ऊपरी दाँतों की सहायता से करते हैं। इसीलिए इन्हें क्रमशः तालव्य श, मूर्द्धन्य ष और दन्त्य स कहा जाता है। चूँकि हम-सब इसके अभ्यस्त नहीं है, अतः शुरू-शुरू मे उच्चारण मे असहजता महसूस होती है। इसका कठोर अभ्यास बचपन मे ही गुरुजन द्वारा कराया जाना चाहिए।
'श' और 'स' मे व्यावहारिक अंतर को ऐसे भी समझें। उदाहरण के लिए -- गौर करें --
(1)
लास' संस्कृत का शब्द है, पुल्लिंगवत् व्यवहृत होता है, अर्थ है -नाचरंग, उछल-कूद, प्रेमालिंगन आदि Dancing, Dalliance .
'लास' फ़ारसी भाषा मे भी एक शब्द है, पर हिन्दी मे उसका चलन नहीं के बराबर है।
'लाश' मूल रूप मे तुर्की भाषा का शब्द है, स्त्रीलिंग मे प्रयुक्त होता है , यह भी हिन्दी मे आगत है, अर्थ है -मृत देह, मृत प्राणी का शरीर, संस्कृत मे यह शव कहा जाता है (अंग्रेजी मे यह Dead body है) । हिन्दी अञ्चल मे मृत देह या Dead body के लिए 'लाश' शब्द ही अधिक चलन मे है।
आप सकते हैं कि मात्र तालव्य 'श' और दन्त्य 'स' के अंतर से शब्द कैसे भिन्न अर्थ दे रहे हैं और हिन्दी अञ्चल मे इस दृष्टि से असावधान रहना बहुत ख़तरनाक स्थिति है, भाषा और साहित्य दोनों के लिए । शिक्षकों को तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए,पर उनकी असावधानी बहुत कचोटती है।
(2)
'निशा' शब्द मूल रूप मे संस्कृत भाषा का है , स्त्रीलिंग मे प्रयुक्त होता है और इसका हिन्दी अर्थ रात्रि / रात है। 'निशा' शब्द संस्कृत से हिन्दी मे आया है।- 'निशाँ' फ़ारसी का है, यह पुल्लिंगवत् प्रयुक्त होता है। 'निशान', 'निशानी' 'निशानची' आदि शब्द भी फ़ारसी भाषा के हैं, लेकिन 'निशाना' शब्द हिन्दी का अपना है, इस पर आप तर्क कर सकते हैं। अरबी-फ़ारसी मे निशाँ को निशान का लघु रूप माना जाता है। 'निशाँ' अधिकतर उर्दू शायरी या ग़ज़लों मे प्रयोग किया जाता है, 'निशान' नहीं।
-'निसा' शब्द मूल रूप मे अरबी भाषा का शब्द है, यह भी स्त्रीलिंग मे ही प्रयुक्त होता है और इसका हिन्दी मे अर्थ 'स्त्रियाँ या औरतें है। 'निसा' शब्द अरबी से उर्दू मे और फिर हिन्दी मे आया है।
'निशा', 'निशाँ' और 'निसा' तीनों शब्द अब हिन्दी भाषा और साहित्य मे ख़ूब चलन मे हैं।
यहाँ भी आप केवल श और स का भेद देख रहे हैं। अतः श और स को लेकर सतर्कता की बहुत अपेक्षा है। उपर्युक्त तीनों शब्दों के प्रयोग मे बोलने / लिखने मे सावधानियाँ अपेक्षित हैं। हमारी हिन्दी पट्टी मे लड़कियों का नाम लोग 'निशा' रखते रहे हैं और यही सही भी है, इसलिए भी कि अरबी भाषा के भारत मे आगमन से पहले भी भारत मे लड़कियों का नाम 'निशा' रखा जाता रहा है। लेकिन किसी लड़की का नाम यदि 'खुशबूनिसा' है तो उसमें निसा (दन्त्य स) सही है। 'खुशबू' मे खुश और बू मिलाकर 'खुशबू' बना है , दोनों फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। यहाँ श और स को लेकर प्रयोग की दृष्टि से अन्तर पर विशेष ध्यान अपेक्षित है। खुशबू फ़ारसी भाषा का शब्द है और निसा अरबी भाषा का। जैसे भारत मे बहुत-सी भाषाएँ / बोलियाँ आपस मे एकरस हैं, वैसे ही अरबी-फ़ारसी भी आपस मे एकरस हैं। खुशबूनिसा का अर्थ है - 'अच्छी-औरतें'।
उदाहरण-04--अब 'कुल' की जगह आप बार-बार 'कूल' लिखेंगे तो मूर्खता के अलावा और क्या कहा जायेगा ? 'कुल' अर्थात् खानदान अथवा पूरा / सम्पूर्ण , अंग्रेजी में इसे आप Clan या Total कहते हैं तथा "कूल" अर्थात् किनारा / तट है" और अंग्रेजी में यही Brink या Shore" है। उक्त दोनों शब्द संस्कृत से हिन्दी मे आगत हैं। यहाँ कुल और कूल मे केवल ह्रस्व (छोटी इ) और दीर्घ वर्तनी (बड़ी ई) का भेद है, पर दोनों के अर्थ मे बड़ा भारी अन्तर आप देख रहे हैं।
भाषा की हत्या करने का किसी को अधिकार तो नहीं है। यह गैरजिम्मेदारी अक्षम्य है। मार्क्सवादी
हिन्दी समालोचक आचार्य नामवर सिंह के यू. पी. कालेज वाराणसी में शैक्षिक गुरु इस तरह की त्रुटियों को भाषा की हत्या मानते थे, भाषा के साथ यह अत्याचार वाकई में अक्षम्य है, यह बात डॉ नामवर सिंह जी बार-बार कहते थे। निरन्तर मेहनत और अभ्यास के द्वारा सुधार का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
संस्कृत मे एक शब्द है- 'माला', इसी से ' ' 'मालाकार:' (पु.) जिसका हिन्दी अर्थ है माला बनाने वाला, माली। 'मालिन्' शब्द विशेषण है, अर्थ है -माला पहनने वाला, मालाधारी, मालाओं से सम्मानित । मालिक 'Gardener' शब्द माली का ही द्योतक है, जो हिन्दी मे किसी भी वस्तु के स्वामी अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। संस्कृत का 'मालिन्' शब्द जो विशेषण है, वह हलन्त रहित होकर 'मालिन' स्त्रीलिंग मे-माली की स्त्री का अर्थ देता है। माली का स्त्रीलिंग 'मालिनि' है, माली जाति की स्त्री के लिए मालन , मालिन या मालिनी भी प्रयुक्त किया जाता है। 'मालिनी' तो मूल रूप मे एक छन्द का नाम है , जो हिन्दी मे सवैया के अन्तर्गत आता है।
यदि कोई "कक्षा-विश्राम" की जगह "कच्छा- विश्राम" बोले, तो उसका अर्थ तो यही होगा -"चड्ढी को आराम", कच्छा अण्डरवियर को कहते हैं। उच्चारण पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, ख़ासकर अध्यापकों का छात्रों के सामने।
कई बार बहुतेरे नवनियुक्त शिक्षक "प्रिंसिपल" और "मैनेजर" को अपनी "ज्वाइनिंग" के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में चार पंक्तियों का प्रार्थना-पत्र नहीं लिख पाते हैं और पूछते हैं कि पत्र कैसे लिखा जायेगा ? ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनकी शिक्षा सूचना आधारित है और केवल नौकरी के लिए सीमित है। वर्तमान मे प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक 70-75 % शिक्षक नौकरी पा जाने के बाद स्वाध्याय से विरत हो जाते हैं। वे या तो व्यवसायी हो जाते हैं या तो प्रापर्टी डीलर हो जाते हैं या तो राजनीति मे कूदकर नेता बन जाते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर खोलकर कोचिंग सञ्चालक बन जाते हैं और शिक्षण कार्य अन्ततोगत्वा उनके लिए पार्टटाइम का कार्य हो जाता है। श्रेष्ठ गुरुजन कहते हैं कि अध्यापक को छात्र जीवन से अधिक पढ़ना चाहिए और सदैव विद्यार्थी भाव मे रहना चाहिए।
धर्मक्षेत्र- कुरुक्षेत्र में वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से अक्षर की महत्ता भी बतायी थी--" अक्षराणामकारोsस्मि........।" इससे भी लगता है कि हमें वर्ण / अक्षर के प्रति किस तरह से सावधान रहना चाहिए । उपनिषदों ने कहा कि- "अक्षर ही ब्रह्म है।" बहरहाल, इस लेख से लोगों को मुझसे चिढ़ हो सकती है, यदा-कदा त्रुटियाँ मुझसे आज भी हो जाती है, लेकिन दोबारा-तिबारा अपने ही लिखे को सम्पादित / संशोधित करता रहता हूंँ।
सोशल मीडिया पर और कागज पर लिखते वक्त भी काफी पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा भी ये त्रुटियांँ होती हैं, पर लोग कभी सुधार का प्रयास नहीं करते। हिन्दी में ऐसे लोग ही अर्थ का अनर्थ करते हैं और भाव का कुभाव । ऐसे लोग ही आने वाली पीढ़ियों में सुधार करने की बजाय अशुद्ध लिखने, समझने और बोलने का संस्कार डालते हैं।
मुक्तिबोध अपने पिता जी को याद करते हुए एक जगह लिखते हैं -"पिता जी ने मुझसे कहा था -कि आखिरी साँस छूटने तक नया सीखना पड़ता है, अपने आप मे संशोधन करते रहना पड़ता है, लगातार सीखते जाना और नये-नये पाठ पढ़ना, ऐसा। ........जो अपने हृदय को निरन्तर निरन्तर संशोधित और सम्पादित नहीं करता है, उसका विकास रुक जाता है।"
एक अध्यापक को या एक अधिवक्ता को या अपने को पढ़ा-लिखा मानने वाले किसी को भी लिखते - बोलते हुए "स्टाप-Stop" और "स्टाफ-Staff" में कम से कम अन्तर तो समझना ही चाहिए।
"स्टाप-Stop" और "स्टाफ- Staff" में यदि अन्तर नहीं पता है, तो शिक्षा के लिए यह एकदम ख़तरनाक स्थिति है। सम्भव है किसी का चयन या पढ़ाई ईमानदारी और सच्चाई से हुई हो, तो इसका मतलब यह कि यह ज्ञान / शिक्षा केवल सूचना आधारित है, इस परीक्षा प्रणाली का या इस शिक्षा पद्धति का ज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास से कोई सरोकार नहीं है। मुझसे कुछ मित्रों ने एक बार शिकायत के लहजे में कहा, कि - आप "सोशल-मीडिया" पर बहुत कम लोगों के लिए लिखते हैं, बहुतों के सिर के ऊपर से आपकी बातें निकल जाती हैं, अतः कोई पढ़ना नहीं चाहता है। लोग इसे जहमत समझते हैं, मुझे उनकी बातें इसलिए बुरी नहीं लगी, क्योंकि यह उनकी शैक्षिक परवरिश और परिवेश का दोष हो सकता है। मैंने जवाब दिया कि "मेरे लिखे को केवल एक ही व्यक्ति यदि रुचि से पढ़ता है, अपने दिल और दिमाग में उसे सहेजता है, तब भी मेरा लिखना सार्थक है, अनेक की बात ही छोड़ दीजिए। मेरा यह उद्देश्य स्वान्त: सुखाय है।
10-20 अच्छे , विचारशील और संवेदनशील पाठक ही हजार- पांँच सौ अत्यन्त हल्की समझ रखने वाले , संकीर्ण सोच के केवल लाइक ढकेलने वालों से हजार गुना बेहतर और प्रणम्य हैं। पुनः कह रहा हूँ , सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप सारी उम्र सीख सकते हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है ।
लेखन के समय तनिक भी संदेह की स्थिति में आज भी मैं अपने जीवन-दृष्टि को केंद्र मे रखकर गुरुजन से सम्पर्क करता हूंँ या तो प्रामाणिक पुस्तकों का बेहिचक तुरन्त आश्रय लेता हूंँ, यदि ऐसा न हो तो मुक्तिबोध के शब्दों मे विकास अवरूद्ध हो जायेगा।
मुझे आज भी अपना विषय एक विद्यार्थी की मानिंद नियमित एक घण्टे-दो घण्टे अध्ययन करना अच्छा लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूंँ कि जब तक शरीर की क्रियाशीलता में आंँखें सहयोगिनी रहें, तब तक अध्ययनशीलता भी बनी रहे। यह प्रवृत्ति ही मुझे Covid-19 के अत्यन्त बुरे दौर से उबारने में बहुत कारगार साबित हुई।
यह लेख उन्हें समर्पित है, जिन्होंने मुझमें भाषा का संस्कार दिया / जिनसे मैंने भाषा और साहित्य की थोड़ी - बहुत समझ पायी है।