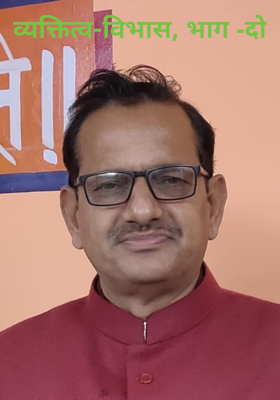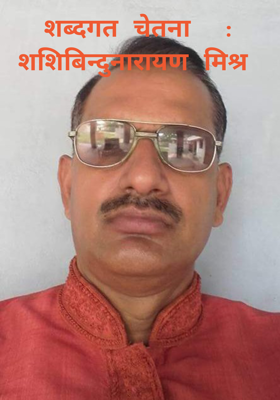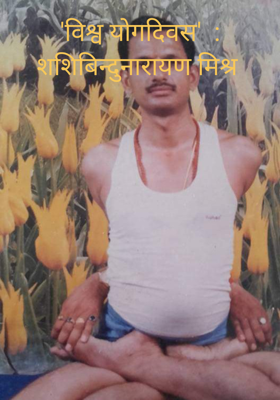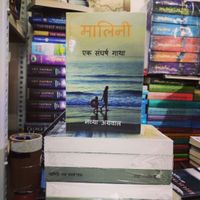'साधारणता में सुख' (संस्मरण)शशिबिन्दुनारायण मिश्र
'साधारणता में सुख' (संस्मरण)शशिबिन्दुनारायण मिश्र


आज बड़ी तेज़ लगन थी। आज की तारीख़ 21 नवम्बर को गाँव रानापार और गाँव के आस-पास के गाँवोँ का चार न्यौता निपटा कर सायं लगभग साढ़े चार बजे घर लौटा ही था कि गाँव के ब्रह्मानन्द कहार मिल गये। उम्र क़रीब 70 वर्ष । मध्यम कद-काठी, चेहरे पर घनी, सफ़ेद सजी हुई मूंँछों का ताव। रंग साँवला । राम-रहारी के बाद वे रुक गये, परस्पर हालचाल हुआ। ब्रह्मानन्द के बाबा के सहोदर जीऊत कहार जनता विद्या विकास समिति, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र विशुनपुरा द्वारा सञ्चालित विद्यालय में प्रथम परिचारक नियुक्त हुए थे, जिन्हें गाँव और स्कूल के लोग "जण्ठ" कहते थे। उनकी पत्नी को लोग 'जण्ठाइन' ईया कहते थे।
मेरे गाँव में कहार बिरादरी का पहले एक ही परिवार था। सुमेर और जीऊत कहार एक बाप की संतान थे। सुमेर के चचेरे भाई के लड़के जगन्नाथ (जगरनाथ) थे। सुमेर के दो लड़के हुए, बड़े पुत्र रामसमुझ कहार और छोटे पुत्र थे रामकिशुन कहार। रामसमुझ के दो बेटे हैं,एक ब्रह्मानन्द और दूसरे सदानंद। जगरनाथ के भी दो बेटे हुए पहले दयानन्द और दूसरे सेतुबंध। वंशवृद्धि होने पर उन्हीं में से तीन परिवार हुए। अब तो कई परिवार और भी बढ़ गये हैं।
कहारों का यह परिवार मेरे परिवार से अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। मेरे परिवार में किसी भी मांगलिक या अन्य अवसरों पर कहारों का यह परिवार जी-जान से सेवा में जुटा रहता था। उसी को देखते हुए जनता विद्या विकास समिति कार्यकारिणी विशुनपुरा के प्रथम अध्यक्ष रहे मनीषी रचनाकार पं. गणेश दत्त मिश्र 'मदनेश' ने जीऊत कहार को विद्यालय में प्रथम परिचारक नियुक्त करवाया था। जीऊत कहार की आकस्मिक मृत्यु के बाद विद्यालय से सूचना गयी थी कि उनके परिवार में कोई और जीऊत के निकट का लड़का हो, जिसे जीऊत की जगह पर रखा जाय। जब सूचना गयी तो रामकिशुन और ब्रह्मानन्द दोनों घर पर नहीं थे, डोली लेकर कहीं गये हुए थे। पट्टीदारी के दयानन्द घर पर ही थे, दयानन्द को ही विद्यालय पर बुलवाया गया। दयानन्द आठवीं तक पढ़े भी थे, शरीर से बलिष्ठ थे, लम्बे-चौड़े थे , कुश्ती वगैरह भी लड़ते थे और गाँव के ही अपने गायन-वादन के गुरु स्वर्गीय तारकेश्वर मिश्र के सहारे गाँव की राजनीति में अपनी सार्थक उपस्थिति
देने लगे थे। कुलमिला-जुलाकर दयानन्द होनहार थे, अतः तत्कालीन प्रधानाचार्य राजनारायण सिंह ने जीऊत कहार की जगह विद्यालय में सबको पानी पिलाने के लिए दयानन्द को ही परिचारक पद पर चुनाव किया और इनकी नियुक्ति हो गयी। रामकिशुन और ब्रह्मानन्द दोनों ही बाद में कहते थे कि -"जेकरे भागि में रहल, ते नोकरी पवलस।" कहा भी तो गया है, -"भाग्यं फलति सर्वदा .......।" इसका मतलब अकर्मण्य होना कदापि नहीं है। रामकिशुन और ब्रह्मानन्द अपनी डोली की दुनिया और खेती-बाड़ी में ही सदैव मस्त रहे।
इन सबके पारिवारिक विवरण की जरूरत इसलिए पड़ गयी कि आगे के प्रसंगों में उक्त में से रामकिशुन और ब्रह्मानन्द के सहारे ही बात आगे बढ़ेगी।
दरअस्ल आज से लगभग 37 वर्ष पहले अर्थात् 30 जून 1988 को जब मैं दूल्हा बन कर पहली बार डोली में बैठा था, तो उस डोली के पाँच कहारों की टोली में से आज केवल ब्रह्मानन्द कहार ही जीवित हैं, शेष चार कहार पांँचू (विशुनपुरा), रामकिशुन (रानापार), शिवजतन (गोबरौर) , रामू (गोबरौर) दिवंगत हो चुके हैं। रामकिशुन और ब्रह्मानन्द मेरे गाँव रानापार के ही थे। रामकिशुन मेरे पिता जी के हम उम्र थे और साथ ही थे उनके परम विश्वस्त और स्वभावत: निष्कपट। यदि कोई मुझसे कहे कि आप पिछले 50-60
वर्षों में अपने गाँव के एक दर्जन नितान्त सज्जन, मेहनतकश और विचारशील लोगों का चुनाव कीजिए, तो मैं उसमें एक नाम रामकिशुन का प्रमुखता से अवश्य रखूँगा। रामकिशुन केवल मेरे पिता के ही स्नेह भाजन नहीं रहे, मेरे प्रपितामह के भी रहे और गाँव में भी बहुतों के।
डोली में आगे की ओर ब्रह्मा और रामू कन्धा देते थे, पीछे की ओर पाँचू और रामकिशुन , शिवजतन बारी- बारी से कन्धा बदलकर एक-एक को बीच में थकने पर आराम देते थे। वैसे सभी कहारों में अद्भुत जिन्दादिली और सज्जनता थी, लेकिन पाँचू और रामकिशुन में जो विचारशीलता और सज्जनता थी , उस पर आज भी मन नमित होता है। वे दूसरे के पहाड़ बराबर धन को तिनके समान समझते थे। ईशावास्योपनिषद का निम्न मन्त्र
-- "ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।।"
उन कहारों ने जीवन में आत्मसात कर लिया था, बगैर पढ़े-लिखे होकर भी, हो सकता है यह उनका पूर्व जन्म-विपाक रहा हो। इसीलिए वे अत्यन्त ग़रीबी में भी सदैव खुशहाल रहे।
मैली-कुचैली बण्डी और जाँघ से ऊपर धोती को खुटिया कर कमर में खोंसी गयी धोती, पसीने से लथपथ कहार श्रम से उत्पन्न थकान के परिहार के लिए लाक्षणिक पर एकदम रसिक गद्य-गायन करते हुए चलते थे, जिससे उनकी डोली की रफ़्तार तीव्रतर होती रहती थी । कहारों के रसिक गद्य-गायन से डोली में प्रथम बार ससुराल पिया के घर को जाती दुलहन को कहार अपने रसिक उद्बोधनों से गुदगुदाते चलते थे, जिससे मायके के विछोह के दुःख से सुबकती दुलहन के विछोह का दुःख बूँद-बूँद कर पिघलता जाता था । डोली में बैठी दुलहन कहारों के रसीले गायन पर एक बार रीझ ही जाती और उसका सुबकना एक बार ठप्प हो जाता। यदि डोली किसी ऊँचाई या बंधे
पर चढ़ रही होती तो आगे के कहार बोल पड़ते --"ऊप्पर चढ़तिया (ऊप्पर चढ़ति बाs) , तो पीछे के कहार समझ जाते कि आगे कोई चढ़ाई है, अतः सम्हल कर आगे बढ़ना है। लेकिन डोली के भीतर बैठी दुलहन -"चढ़तिया" जैसे शब्दों को सुनती तो उसे लगता कि कहार चिलचिलाती धूप में अपने श्रम परिहार के लिए ये शब्द बोलते होंगे या ये हास-परिहास के शब्द हैं और भीतर ही भीतर खिलखिला पड़ती, ऐसे में डोली की रफ़्तार संग उसका सुबकना, रोना-धोना धीरे-धीरे बंद हो जाता। कहार पगडंडी रास्ते पर चलती हुई डोली के आगे यदि झूँटा देखते तो आगे के दोनों कहार समवेत स्वर में बोल पड़ते --"दहिने दाढ़ीवाल है।" तो पीछे के कहार समझ जाते और उस हिसाब से कदम आगे बढ़ाते।
यह सुनकर डोली के भीतर का दूल्हा हो या दुलहन (नवविवाहिता) , एक बार तो वे हँस ही पड़ते। कहार रास्ते में मौका देखकर दुलहन की आवश्यकता को समझते और पानी इत्यादि की जरूरत को पूरा भी कर देते। कहार बिना माँगे ही एक लोटा पानी दुलहन की ओर बढ़ा देते। जरूरत होने पर दुलहन पानी लेती अन्यथा हाथ हिलाकर मना कर देती। सभी कहार अपना-अपना लोटा साथ रखते थे। यह कहारों की गजब की नैतिकता और सूझ-बूझ थी।
कविवर धरीक्षण मिश्र जी ने अपनी एक कविता में डोली में विदा होती हुई दुलहन का बड़ा ही सजीव, मार्मिक और रोचक चित्रण किया है। इस भोजपुरी कविता का मुखड़ा है -"कौना दुखे डोली में रोवति जाति कनियाँ"
उसकी कुछ और पंक्तियाँ देखें --
"आजु जात बानी बन्द होखे एक जेल बीच,
जेलर जहाँ के सासु ननद आ जेठनियाँ।
दुइ चारि साल के न बाटे जेल के ई सजा,
जेले में बीती अब सउँसी जिन्दगनियाँ।"
(धरीक्षण मिश्र जी की भोजपुरी कुछ बिहारी प्रभाव समेटे हुए है। हमारे यहाँ 'सउँसी' को 'सगरो' या सज्जी (सब) कहा जाता है।)
यह कभी समाज का यथार्थ रहा है। इसे हम लोगों ने भी प्रत्यक्ष देखा है। तमाम नवविवाहिताएँ वर्षों तक सचमुच में ससुराल में एक तरह से यातना या जेलखाने जैसे जीवन में रहती थी। हमेशा घूँघट में रहना, कभी खुल न हँस पाना, यह सब होता था।
वह दुलहनों के लिए सासु , ननद और जेठानी द्वारा अनुशासन की पराकाष्ठा थी, लेकिन कभी-कभी उसका रूप बहुत विद्रूप भी हो जाता था। अब तो अति आधुनिकता के इस दौर में दुलहनें, दुलहने रह ही नहीं गयी हैं। पढ़े-लिखे और आधुनिक होने का मतलब यह तो नहीं है कि बहूपन को खोखला कर दिया जाये , दुलहनपन और बहूपन का सौन्दर्य खत्म हो जाये। इसीलिए अजीब तरह की नीरसता दिखाई देती है। अत्याधुनिकता या आजकल की विलासिता का अभिप्राय केवल परम्पराओं का निषेध तो नहीं है । अत्याधुनिकता और बड़े-बड़े शहरों में पढ़ाई-लिखाई का मतलब नंगा हो जाना तो नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अत्याधुनिक होकर भी संस्कारों और परम्पराओं की बखूबी रक्षा की जा सकती है। ऐसे लोग आज भी हैं, पर बहुत कम, गिने-चुने।
आज बहुत दिनों के बाद मिलने पर ब्रह्मानन्द भी आतुरता से मिले। परिवार में सबका हालचाल पूछा, पत्नी का भी। मैंने जब फोटो लेने के लिए तैयारी की, तो ब्रह्मानन्द हतप्रभ दिखे । " काs होई हमार फोटो ? आजु ले केहू हमार फोटो मोबाइल से नाहीं लिहलस।" कहते हुए ब्रह्मानन्द रोम-रोम से पुलकित भी हो रहे थे। "कार-मोटर" आदि की प्रगति ने कहारों की रोजी-रोटी छीन ली, तो वे दूसरे व्यवसायों की ओर मुड़ गये। ब्रह्मा अब जम्मू-कश्मीर में पेंट- पालिश का काम करते हैं। साल-छ: महीने पर घर आते हैं, पर हमेशा मस्ती में रहते हैं। गाँव की या देश-दुनिया की राजनीति से कोई ख़ास सरोकार नहीं। उन कहारों में बनावटीपन नहीं के बराबर था, वे वास्तविक जिंदगी जीते थे, अतः उनसे बात करने में मजा आता था। व्यक्ति बड़ा है या छोटा, इससे मतलब नहीं है, वह कितना जिन्दादिल और सहज है, इससे मतलब जरूर है। व्यक्ति जितना ही प्रकृति के निकट है, वह उतना ही वास्तविक है, अच्छा है। लोकतन्त्र और लेखन दोनों की भी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह ऊँच-नीच और अमीरी-गरीबी से लेशमात्र भी प्रभावित न हो। अब कोई यदि मुझसे यह कहता है कि ब्रह्मानन्द में कौन सी विशिष्टता है, कि उनके साथ फोटो खींचा- खिंचवाया जाय ? तो मेरा उत्तर यही होगा कि क्या किसी धनपशु- शोषक- अहंकारी के साथ फोटो लेकर अपनी आत्मा को सदैव धिक्कारा जाय ? क्या ऐसे लोगों के साथ फोटो लिया जाय, जिनकी बुद्धि दिन-रात तिकड़मबाजी में रहती है या जिन्होंने जीवन भर अनीतिपूर्वक सफलता पायी है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाई है और अनीति से सम्पत्ति कमाई है या जो तलवाचाटू भाव में थोड़ी बहुत महत्ता या लाभ पा जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचना-खिंचवाना और उस पर कुछ लिखना, मेरे लिए हरगिज सम्भव नहीं है।
बहरहाल ! विवाह के दो वर्ष बाद तीसरा वर्ष लग जाने पर प्रति रविवार और बुधवार को घर पर आकर हजामत बनाने वाले विशुनपुरा के प्रयाग (पराग) नाई की अस्वस्थता के कारण पण्डित जी के साथ मेरे गवना का शुभ मूहूर्त (लगन ) लेकर ब्रह्मानन्द कहार ही मेरी ससुराल गये थे। लगन निश्चित कराकर ब्रह्मानन्द ने माता-पिता जी को पत्र दिया और सूचित कर मुझे अलग से एक गोपनीय "पैक्ड" लिफाफा दिया। लिफाफा के भीतर भी लिफाफा वह भी पैक, मेरी तो कई गुना धड़कन बढ़ गयी थी । पत्र सरहज (जो उम्र में कुछ बड़ी हैं) ने लिखा था, सलीकेदार सम्बोधन और हालचाल के बाद उनकी पंक्तियाँ थीं कि "बाबू ! आप पहली बार ससुराल डोली में आये थे, तो ये बहिनी भी पहली बार ससुराल डोली में ही जायेंगी, इनकी हार्दिक इच्छा है।" अब समस्या यह हो गयी कि एक नयी-नयी "अम्बेसडर" कार तय हो चुकी थी, गवना के लिए । लेकिन यह चीज़ मेरे हिस्से की नहीं थी, इसका समाधान भी मेरे पास नहीं था, मैं इसके लिए पिता जी से पहल नहीं कर सकता था । चूँकि मेरे गाँव से चारों दिशाओं में समान दूरी पर नदियाँ हैं, दक्षिण-पश्चिम में राप्ती नदी और उत्तर-पूरब में गोर्रा नदी। किसी भी दिशा में जाने पर नाव से नदी को उस समय पार करना ही होता था । अतः हमारे कछार में नाव से नदी को पार कर बहुत मुश्किल से कार या जीप का आना हो पाता था। उस दौर के हमारे कछार की दशा और दिशा को ठीक से समझना और पढ़ना हो तो डॉ रामदरश मिश्र के पहले उपन्यास 'पानी के प्राचीर' को पढ़ा जा सकता है।
बहरहाल मैंने ब्रह्मानन्द से पत्र की बात ईमानदारी से बताई, तो ब्रह्मानन्द ने मेरी सास के हवाले से मेरी माता जी से काफ़ी बुद्धिमत्ता से डोली के लिए आग्रह किया। बात बन गयी। माता जी भी काफ़ी खुश हुई थीं। खैर, ब्रह्मानन्द ने ही इसका समाधान निकाला था। मुझे कदम-कदम पर ईमानदारी और स्वाभिमान की रक्षा करने का जीवन पर्यन्त पाठ पढ़ाने वाली माता जी आज संसार में नहीं हैं और बेहद दृढ़ निश्चयी सास भी अब संसार में नहीं है। आज ब्रह्मा जी का 10-15 मिनट का प्रीतिकर सानिध्य मुझे अतिशय भावुक कर गया और दोनों दिवंगत माताओं की याद में देर तक मैं डूबा रहा। साथ ही उन चारों दिवंगत कहारों की याद में भी आँखें नम हुईं, उन कहारों के हाथ का बरातों में 2-3 बार स्वादिष्ट भोजन करने का भी सुख मिला है। सभी दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि ।
अभावों की जिंदगी में भी उन कहारों का उन्नत सुभाव जीवन को उत्कर्षता प्रदान करता था।
ऊपर कह आया हूँ, वे लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, क्षण- प्रतिक्षण वे प्रकृति से रू-ब-रू होते थे। साहित्यकार निर्मल वर्मा ने अपने एक निबन्ध में लिखा है --"प्रकृति सत् की ओर प्रयत्नशील रहती है।"
अब आने वाली पीढ़ी डोली का सुख , डोली का महत्त्व और डोली की मर्यादा क्या समझेगी ? गाँव के बाहर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में बरात के पहुँचने पर पूरे गाँव द्वारा अगवानी करना और बरात का टिकना , लगता था कि सचमुच में प्रकृति भावविभोर हो रही है और बरात को प्रसन्नता में गुनगुना रही है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में शहरों में बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों और मैरेज हाउसों में आयोजित विवाह समारोहों तथा कारों के काफिले में विवाह का मूल आनन्द विरस हो गया है। बरातियों - घरातियों दोनों के लिए । गाँव और बहुतेरे सगे- सम्बन्धियों के यहाँ से डोली में बैठे दूल्हे-राजा के पीछे-पीछे जाने वाली बरात का पैदल भी और साइकिल से भी अनेक बार हिस्सा बना हूँ और जिनके घर डोली संग बरात आयी,उस घर के पक्ष का भी हिस्सा बनने का अनेक अवसर मिला है। ऐसे विवाह समारोहों का जो मौलिक सुख होता,वह आज वर्णनातीत है। कारों के काफिले संग बरातियों का सारा भाव हैसियत देखने-समझने में ही सिमट जाता है। ऐसे आयोजनों में मेरे जैसे लोग जल्दी भोजन करना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसे समारोहों में जाने से भरसक बचने का मन करता है , जहाँ केवल अपनी भुथरी हैसियत के प्रदर्शन का निर्लज्ज भाव हो । ऐसी जगहों पर भला कैसे जाया जा सकता है, जिनकी हैसियत कभी साफ - सुथरी रही ही नहीं । आज की अत्याधुनिक जीवन शैली और अपार सुख-सुविधाओं में जीवन जीने वाली पीढ़ी वास्तविक और मौलिक सुख से वंचित है। वह सौन्दर्य से भी अपरिचित हैं। आज कल सौन्दर्य को जो रोमैन्टिक बोध से जोड़ा जाता है, उसे यदि विचारक रिल्के के शब्दों में कहें तो जीवन में 'आतंक की शुरूआत' है।
आज ब्रह्मानन्द से उनकी कमाई आदि के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि --"बाबू ! अब पइसा कs जुग आ गइल बाs , सबके पइसवे चाहीं, ओह समय कुछु अवर रहल, रउरे अतरवलियाँ वाले खेते में हम आ राम किशुन काका डेढ़-डेढ़ बीगहा रहरि बोईं, खूब बढ़िया होखे। लदोरे दालि, भरुआ मरचा आ जाड़ा में हीक्क भरि कचरस पी के सभन सोझ हो जाईं, न कौनो रोग,न कौनो बेमारी।"
कुछ लोग मुझे अन्तर्मुखी भी कहते हैं, क्या करें? क्योंकि मैं कम लोगों से बातें करता हूँ, कम लोगों से रिश्ते रख पाता हूँ, बहुत ही कम लोगों के यहाँ जा पाता हूँ और बहुत ही कम लोगों को अपने यहाँ बुला पाता हूँ।
मेरे लिए आदर्श व्यक्तित्व मनीषी रचनाकार पं. गणेश दत्त मिश्र 'मदनेश' अक्सर कहा करते थे, कि - "हीत ओतने रखीं, जवनs अँगुरी पर गिना जाs । एतना हीत न रखीं, कि न्योतवेs भुला जाs।"
बहुधा साधारण लोगों का आत्मीय सानिध्य जीवन में असाधारण और आत्मिक सुख दे जाता है। आज कुछ ऐसा ही लगा।