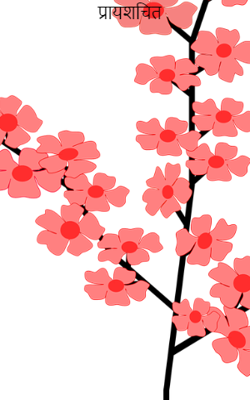पेंटर
पेंटर


शाम ढल रही थी। सड़क पर धूल उड़ रही थी और सूरज आख़िरी रोशनी समेट रहा था। एक शायर अपने कंधे पर झोला टाँगे, यूँ ही बिना किसी मंज़िल के चल रहा था। उसके पास न कोई बड़ी गाड़ी थी, न पहचान का शोर—बस कुछ अधूरी ग़ज़लें और ज़िंदगी को देखने की आदत।
चलते-चलते उसे एक पुराना सा ढाबा दिखा। टीन की छत, लकड़ी की बेंचें और चूल्हे से उठती दाल की खुशबू। भूख ने क़दम रोक लिए। शायर अंदर गया और एक कोने में बैठ गया।
उसी ढाबे के दूसरे सिरे पर एक पेंटर बैठा था। कपड़े रंगों से सने थे, उँगलियों पर पेंट सूखा हुआ, और आँखों में थकान। वो बार-बार चाय का खाली कप घुमा रहा था, जैसे किसी सोच में उलझा हो।
शायर की नज़र उस पर पड़ी, मगर उसने न गरीबी देखी, न हालात—बस एक इंसान देखा।
खाना आने में देर थी। बात यूँ ही शुरू हो गई—मौसम से, रास्तों से, और फिर ज़िंदगी से। पेंटर ने बताया कि आज काम नहीं मिला, दीवारें बहुत हैं पर रंग कम पड़ गए हैं।
शायर मुस्कुराया और बोला,
“दीवारें तो सबके पास होती हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें रंग देता है, कोई अल्फ़ाज़।”
खाना आया। शायर ने दो रोटियाँ उठाईं और पेंटर की थाली में रख दीं।
“भूख जात नहीं पूछती,” उसने सादा सा कहा।
पेंटर की आँखें कुछ पल के लिए झुक गईं। शायद वो शुक्रिया नहीं, सम्मान महसूस कर रहा था।
सीन बदलता है।
कई महीने बीत जाते हैं।
शायर एक नए शहर में है। किराए का कमरा, सफ़ेद दीवारें और जेब में गिने-चुने सिक्के। एक शाम मकान-मालिक आकर कहता है,
“कमरा खाली करना पड़ेगा, या दीवारें ठीक करवा दो।”
शायर परेशान है। पैसे नहीं, जान-पहचान नहीं। वो उसी सफ़ेद दीवार को देख रहा है, जो अब उसे अपनी तरह खाली लगती है।
अगले दिन दरवाज़े पर दस्तक होती है।
बाहर वही पेंटर खड़ा है। उम्र थोड़ी बढ़ गई है, मगर आँखों में वही सादगी।
“याद है ढाबा?” वो मुस्कुराकर पूछता है।
शायर कुछ कह नहीं पाता।
पेंटर बिना देर किए दीवारों पर रंग चढ़ाने लगता है। फूल, रास्ते, एक उड़ता हुआ पंछी। कमरा जैसे साँस लेने लगता है।
काम ख़त्म होने पर शायर पैसे की बात करता है।
पेंटर हाथ रोक देता है—
“उस दिन आपने खाना नहीं खिलाया था साहब, आपने बराबरी खिलाई थी।”
वो चला जाता है।
शायर दीवारों को देखता रह जाता है और सोचता है—
जो इंसान अमीर-गरीब, जात-पात नहीं देखता,
उसे ज़िंदगी कभी अकेला नहीं छोड़ती।
कभी ढाबे में,
तो कभी दीवारों पर रंग बनकर।
Tanha Shayar Hu Yash