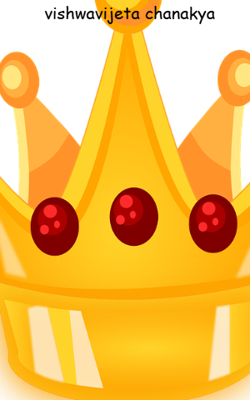khoobsurat sukrat
khoobsurat sukrat


सुकरात
अपनी बनाई इस नई मूर्ति के चेहरे को बहुत ही बारीकी के साथ तराश रहा था । शरीर का ढ़ाँचा लगभग तैयार ही था, बस चेहरे की भाव-भंगिमा व उसमें थोड़ी सजीवता लानी बाकी थी ।
रात का न जाने कौन-सा प्रहर था, काम में डूबा हुआ समय का कुछ होश ही नहीं रहा । घर से लगे इस मध्यम आकार के कमरे में अनेक मूर्तियाँ रखी थी । सभी अनगढ़ रूप में ही थी । जब कोई मूर्ति पूरी तरह तैयार हो जाती थी, तो अगली ही सुबह उसे बिकने के लिये अच्छी तरह तैयार करके बाजार भेज दिया जाता था ।
आँख खुलने के बाद बचपन से ही यही सिलसिला देखता आ रहा हूँ । बचपन मं कई बार इच्छा होती थी, कि पिता जिन मूर्तियों को तैयार करते हैं, कम से कम दो-एक दिन के लिये ही उस सजीव-सी दिखती संपूर्ण आदमकद मूर्ति के पास बैठकर उसे देखू, उससे अपने मन की बातें कहूँ किंतु ऐसा हो नहीं पाया । पिता को अपनी मूर्तियों में अंतिम रूप-रेखा देने का काम शायद रात के किसी प्रहर में सुहाता था, जब सब लोग सो जाते थे तो वे अपनी छैनी व हथौड़ी की हल्की-सी ठक्-ठक् के साथ अपनी अधूरी कृति को पूर्णता देते हुये उस कक्ष में ही अक्सर सोते मिलते थे, सुबह की पहली किरण के साथ ही वे हड़बड़ा कर उठते और उस अपनी महिनों के मेहनत से बनी किसी-किसी मूर्ति को तो बरसों लग जाते थे, को बिना किसी मोह आसक्ति के उचित मूल्य पर बिकने के लिये बाजार में रवाना कर देते थे ।
मूर्तियों से बात करने की अधूरी हसरतों के साथ मैं बड़ा हुआ । शायद इन्हीं अधूरी इच्छाओं ने मुझे मूर्तियाँ बनाने के लिये प्रेरित किया । और फिर एक दिन मैंने खुद को पिता के उसी बरसों पुराने कार्यशाला में खुद को उनसे मूर्तियाँ बनाने के जरूरी निर्देशों को ध्यान से सुनते हुये पाया । पता नहीं मूर्तियाँ बनाने में मेरी वाकई दिलचस्पी थी भी या नहीं यह तो मैं नहीं जानता था किंतु उन मूर्तियों से बात करने की हसरत अत्यंत तीव्रता से मेरे नन्हें-से मन की गहराईयों में बरसों से छुपी हुई थी । आज शायद उन्हीं अधूरी हसरतों को खुद के हाथों से मूर्ति बनाना सीखकर पूरा करना चाहता था ।
किंतु कहाँ ! मेरी वह हसरत भी अब तक अधूरी ही रह गई थी । मूर्तियों के चेहरे को सजीव रूप देता हुआ उसे अंतिम रूप-रेखा तक पहुँचाता हुआ अक्सर मैं इतना थक जाता था मैं उस अपनी ही बनाई हुई मूर्ति के सामने सो जाता । सुबह पिता आकर मुझे उठाते और मूर्ति की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुये उसे सूखे घास-फूस में मोटी रस्सियों से लपेटकर एक किराने रख देते थे और मैं अपनी अधूरी कामनाओं को पिता को बताये बगैर ही घर पर लौट आता था ।
अब तक शायद तीन या चार मूर्तियाँ बनाई होंगी मैंने । यह शायद चौथी या पाँचवीं मूर्ति होगी । ओह ! मैं भी कितना अजीब भुलक्कड़ हूँ । महिनों-बरसों की मेहनत से दिन-रात एक करके मूर्तियाँ बनाता हूँ आज तक कितनी मूर्तियाँ बनाई यह भी ठीक-ठीक याद नहीं । मुझे खुद के ही इस भुलक्कड़ स्वभाव पर हँसी आ गई ।
एक पानी पिलाती हुई स्त्री की थी । दूसरी मूर्ति सामने दर्पण में खुद को निहारती अपने बालों को दोनो हाथ पीछे ले जाकर ठीक करती हुई कमसिन बाला की थी । तीसरी मूर्ति .......... मैं याद करने की कोशिश कर रहा था । मैं भी कहाँ मूर्ति बनाते-बनाते मूर्तियों की गिनती करने बैठ गया । ये आँकड़ों का गणित मुझे कभी भी समझ नहीं आता । मैं वापस से छैनी और हथौड़े की बहुत ही हल्की-सी ठक्-ठक् के साथ अपनी मूर्ति को अंतिम प्रारूप देने के लिये अत्यंत सावधानी के साथ झुक गया । पिता अक्सर कहा करते थे कि मूर्ति को अंतिम रूप-रेखा देते वक्त बहुत ही सावधानी की जरूरत पड़ती है । तेजी या हड़बड़ी दिखाई तो लंबे समय तक की गई साधना को अनायास ही क्षति पहुँच सकती है, फिर लाख कोशिशें करते रहो, उस गड़बड़ को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है । बल्कि यूँ कहूँ कि उसे कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता । उनकी यह बात मैंने अपने मन में अच्छी तरह गाँठ बाँध कर रख ली थी । कभी मूर्ति जल्दी पूरी करने की उत्कंठा अंतिम समय में जागती भी थी, तो मैं अपने मन को बड़े ही धीरज और संयम से थाम लेता था । खुद को जरा भी विचलित नहीं होने देता था ।
अब बस मनचाहे रूप में मेरी मूर्ति अपना अंतिम रूप लेने ही वाली थी । बस उसकी आँखों में वह सजीव भाव नहीं थे, उन्हें जीवंत व साकार रूप देने की अपनी अंतिम कोशिशों में मैं तल्लीनता से लगा हुआ था ।
मेरी आँखें आज फिर हमेशा की तरह बोझिल होने लगी थी । अपनी आँखों को हथेलियों से मसलता आँखों को दो-चार बार झपकाता गर्दन को धीरे-से दायें-बायें झटकता मैं खुद को निद्रा की बोझिल अवस्था से जागरण की अवस्था में बार-बार लाने का प्रयास कर रहा था किंतु आँखें थी कि थकान दिन और रात के लगातार जागरण से बार-बार बोझिल हुई जा रही थी । मुझे मूर्ति बनाने से ज्यादा खुद को जगाये रखने के लिये मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही थी । मैं आज वाकई जागना चाहता था । अपने ही हाथों गढ़ी कृति से दिल खोलकर बातें करना चाहता था ।
ऐसा लग रहा था मानो मेरी यह मुरत एकांत साधना में लीन हो न जाने कितना समय हो गया था
बोझिल होती आँखों को जबरन खोले रखने की कोशिशें नाकाम होती देखकर वहाँ से उठ गया । अपनी दोनों हथेलियों से मैंने बार-बार अपने चेहरे व आँखों पर भरपूर छींटे दिये उसके बाद आस्तीन से अपना ठंड़ा चेहरा पोंछता हुआ जब मैं वापस अपनी जगह पर बैठा तो दंग रहा गया । अपने ही द्वारा तैयार की गई उस अद्भुत मूर्ति को देखकर पलक झपकाना ही भूल गया । अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस मूर्ति को पूरा करने में समय लगने वाला है किंतु यह तो मेरी बोझिल आँखों के साथ ही पूर्णता के अंतिम शिखर पर खड़ी मुस्कुराती नजरों से देख रही थी । अपने सौन्दर्य-शिल्प व अदा के साथ उसका रचयिता को देखना कितना रोमांचकारी लग रहा था । वह मेरी कृति थी जिसका रचयिता मैं था जिसका सृजनकार मैं था मेरे ही हाथों गढ़ी होने के बावजूद आज मुझसे स्वतंत्र पृथक वजूद के साथ मुझसे चंद कदमों का फासला बनाकर सम्मोहन की मुद्रा में मुझे देख रही थी । उसकी इस मुद्रा के साथ इस कमरे की हर चीज जैसे सजीव होकर बोल पड़ने को आतुर हो उठी हो । सामने टेबल पर छैने-हथौड़े के साथ-साथ कमरे में रखी कुछ आधी-अधूरी मूर्तियाँ और उन्हें लपेटने के काम आने वाला सूखा भूसा । यह सब उस छोटे-से दीपक की पीली रोशनी में साकार होकर मुझसे गुफ्तगू करने के लिये उत्सुक हो उठे हों । बरसों से देखा गया सपना आज जैसे पूरा होने वाला हो । छूकर उसकी जीवंतता को महसूस करने के लिये आगे बढ़ा ही था कि मुझे अपने कंधे पर मानवीय स्पर्श रूपी चेतना का भान हुआ । हृदय में एक कंपन-सा हुआ । इस सुनसान से कमरे में जिसमें मेरे सामने रखी मूर्ति के अलावा कुछ आधी-अधूरी और बेतरतीब-सी मूर्ति है वहाँ चेतना का यह मानवीय स्पर्श !
मैं पीछे मुड़ा । मेरी नजर अपने पिता के चेहरे पर पड़ी । वह एकटक विस्मित से खड़े मेरी बनाई मूरत को देख रहे थे । पिता को इतने मुग्ध भाव से किसी मूर्ति को निहारते हुये मैंने कभी देखा नहीं था । ऐसा लग रहा था, जैसे वो हाड़-मांस के जीवित इंसान नहीं बल्कि स्थिर मुद्रा में खड़े मूर्ति में ही तब्दील हो गये हों । एक ही दिशा में एकटक देखती आँखें । न चेहरे पर भावों का आता-जाता रंग न शरीर में कोई स्पंदन ऐसा लगा मानो यहाँ रखी आधी-अधूरी मूर्तियों के बीच दो बुत इस कक्ष में खड़े हैं, जिनमें से एक मूर्ति तो मैंने अभी-अभी बनाई थी और दूसरी मेरे पिता की थी जिसे सृष्टि के रचयिता ने बनाया था । उन दोनों के बीच सिर्फ़ मैं ही खड़ा था जिसकी धड़कनें अभी चल रही थी । साँसों के उठने गिरने का क्रम अभी तक चालू था । मुझे लगा उस कक्ष में यदि मैं और थोड़ी देर रूका तो मैं भी अपने पिता की तरह ही एक पाषाण मूरत में तब्दील हो जाऊँगा ।
और मैं वहाँ उस कक्ष से बाहर की तरफ भाग आया । मुझे पता नहीं मैं कितनी देर और कब तक भागता रहा । भागते-भागते जब मेरी साँस फूलने लगी और मैं पसीने से पूरा तरबतर हो गया तब एक चौराहे पर साँस लेने के लिये रूका ।
आज ऐसे मोड़ पर मैं खड़ा था जहाँ से दिशाऐं अलग-अलग राह की तरफ मुड़ रही थी, एक राह तो वह थी जहाँ से अभी-अभी मैं भागकर आया था, और दूसरी राह एथेन्स नगर के भीड़ भरे रास्तों से होकर गुजरती थी ।
वहाँ एक छोटा-सा सराय था । जिसके बाहर हल्की-सी रोशनी में कुछ लोग बैठे हुये बातें कर रहे थे ।
वह सराय मुझे जिंदगी और जीवंतता से भरपूर लगा । जिंदगी से जुड़ी हलचल थी । लोगों की आवाजाही थी । मैं भी धीरे-से जाकर वहाँ रखी एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया । अजनबी चेहरों ने मुझे थोड़े से आश्चर्य से देखा किंतु कोई प्रश्न नहीं किया । धीरे-धीरे मैं भी उनकी बातचीत में शुमार होता चला गया । मूर्तियों से बात करने की मेरी हसरत आज पूरी हो गई थी ।
पहले भी मैं इन लोगों के बीच रहा होऊँगा, किंतु आत्मलीन अपने ही दायरे में कैद अपने ही ख्यालों के घेरे में गुम मेरा ध्यान जिंदगी की इन चलती-फिरती धड़कनों की तरफ गया ही नहीं । पहली बार लगा कि महिनों तक मैं जिन मूर्तियों को तराशने की कोशिशों में जुटा रहा उनके चेहरे पर खूबसूरत भावों को उकेरने के प्रयास में दिन-रात मशक्कत करता रहा वह सारे भाव खूबसूरती के सारे रंग विधाता ने मेरे आस पास के अनेकानेक चेहरों पर स्वयं अपने हाथों से गढ़ तो दिया था ।
पत्थर की मूर्तियों में मैं भावनाऐं, आंतरिक सौन्दर्य ढूँढ़ रहा था जो मुझे मिल नहीं रहा था । मेरे सामने तीन चेहरे थे एक पिता का दूसरा मेरा अपना चेहरा जो मैं रोज आईने में देखा करता था और तीसरा भीतर बहती हुई आत्मिक सौन्दर्य की खूबसूरती जिसे मैं दुनिया के सामने खूबसूरती से तराश कर प्रस्तुत करना चाहता था
दूर कहीं शांत स्थल जंगलों के बीच सांय-सांय करते किसी निसर्ग शांति की कामना मुझे नहीं थी । अपने पिता से मूर्तियों को बनाने का शिक्षण लेते हुये युवाकाल का एक लंबा समय इन्हीं मूर्तियों के बीच छैने व हथौड़े की ठक्-ठक् के साथ इन्हीं को तराशते हुये खामोशी के साथ बिताया है ।
एक लंबी साँस लेकर मैंने खुद को ढ़ीला छोड़ दिया । जहाँ से मैं भागकर आया था वापस से उन्हीं बेजान मूर्ति और सांय-सांय करते सन्नाटे में लौटने को मेरा दिल नहीं था । मुझे तो एथेन्स नगरी की यह भीड़-भाड़, लोगों का शोर कोलाहल आवाजें तथा आते जाते कदमों की थिरकन व पदचाप आकृष्ट कर रहे थे ।
आखिरकार पत्थर की मूर्तियाँ हम बना रहे थे और मानवाकृति के रूप में इन चलती-फिरती मूर्तियों को ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ इनमें प्राण फूँके हैं । विधाता की रची चलती-फिरती मूर्तियों की भीड़ ही मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी
सौन्दर्य व खूबसूरती की तलाश में एथेन्स नगरी की इसी भीड़ में
मैं न जाने कब शुमार हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता ।
मुझे याद है मूर्तियों को लपेटने के काम आने वाली रस्सी की गांठ पिता बहुत ही सावधानी के साथ लगाते थे ताकि उन मूर्तियों को जब बाजार में बेचने के लिये रस्सियों को खोला जाये तो किसी भी तरह की परेशानी न हो । हर चीज बड़ी सुलझी हुई अनुशासित और तरतीबवार होती थी । वह इस शहर के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे इसीलिये संयम व धीरज उनका स्वभाव ही बन चुका था ।
एक बार धागे के बचे हुये छोटे-से टुकड़े के साथ खेलते-खेलते मैंने उसे धरती पर छोड़ दिया था और थोड़ी देर बाद उसी धागे के छोटे-से टुकड़े में ही उलझ कर गिर पड़ा था । पिता ने उस छोटे-से रस्सी के टुकड़े को अपनी हथेलियों में समेटकर एक किनारे रख और
पिता रस्सियों के उलझने व लोगों के फंसकर गिरने से पहले ही सावधान रहते थे रस्सियाँ सुलझी रहे ताकि मूर्तियों को रस्सियों से लपेटने में सहूलियत हो । ऐसी उलझी हुई गुत्थियों व घुमावदार मोड़ को सुलझाने में मजा आता था । उनकी गांठों को अपने दोनो हाथों से धीरे-धीरे खोलने में जिस सावधानी व संयम की जरूरत पड़ती थी वह पिता से नैसर्गिक स्वभाव के रूप में मेरे भीतर उपस्थित था । जब बरसों से पड़ी गांठ एक-एक करके खुलती जाती थी और तुड़ी-मुड़ी रस्सी धीमे-धीमे एकसार और सीधी-सरल होती जाती थी लोगों को दायरों से मुक्त करके जिंदगी की ओर ले जाने में तो मुझे अपार सुख व संतोष का अनुभव होता । ऐसा लगता जैसे मैंने निर्जीव मूर्ति में प्राण फूँक दिये हों । गढ़न की प्रक्रिया सतत् रूप से आज भी जारी है ।
आज एथेन्स की गलियों में भटकते हुये मेरी नजर काले कोट व काले पैंट पहने एक दुबले-पतले-लंबे से व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क के बीचोंबीच नाचता हुआ धीमे-धीमे आगे की ओर बढ़ रहा था जिसने धूप से बचने के लिये सिर पर एक काली टोपी भी पहन रखी थी ।
आस-पास चलने वाले लोग उसे अजीब-सी नजरों से घूर रहे थे वह दीन-दुनिया से बेखबर अपनी ही मस्ती में डूबा आनंदमग्न नाच रहा था । लय के साथ नृत्य-शैली के अंदाज में कभी एक पाँव उठाता, तो कभी दूसरा । नृत्य की तन्मयता में डूबे उसके एक पाँव से इतने में चप्पल निकल गई । उस निकलते हुये चप्पल को उसने हवा में ऊपर की तरफ उछालकर दो-तीन फिरकनी दे दी । वहा चप्पल इतने शानदार तरीके से हवा में घूमा रहा था कि वास्तव में नजारा देखने लायक था । मुझे ऐसा लगा मानो इस दुबले-पतले-लंबे से शख्स के भीतर कोई खिलाड़ी छुपा है जिसे दुनिया पागल समझकर अजीब-सी नजरों से देख रही है वास्तव में वह तो अपनी ही दुनिया में लीन आनंद व खुशी के क्षणों को ढूँढ़कर अपने हिसाब से जिंदगी को जीते हुये बिता रहा है ।
कई बार होता है कि जिसे हम पागल समझते हैं वह सबसे समझदार होता है बस उसमें एक कमी होती है कि वह समाज व शहर के नियमों के दायरों से सर्वथा मुक्त स्वयं के जीवन को अपने तौर-तरीकों से जीता है और अपने ऊपर किसी भी तरह के बंधन व दबाव को स्वीकार नहीं करता । भीड़ जिस तरह चलने के लिये चलती है वह उस तरह नहीं चलता । भीड़ जिस तरह से सोचती है वह उस तरह से नहीं सोचता । भीड़ जिस तरह से नियमों व परिपाटियों को अपने कंधे पर ढ़ोती है रस्म और रिवाजो को वह अपने कांधे पर ढ़ोने के लिये तैयार नहीं होता, इसी कारण से भीड़ उस शख्स को पागल करार दे देती है एक आम आदमी बनने व दिखने की चाह में व्यक्ति अपनी जितनी कुर्बानियाँ देता है वह उस पागल की नजर में क्या ज्यादा बड़ा पागलपन नहीं है । पर यह भी सच है कि जिंदगी को वास्तव में जीना हो तो पागलपन के साथ ही जिया जा सकता है ।
अल्लसुबह एथेन्स की गलियों में मैं आज अकेला ही भटक रहा था । ऐसा लग रहा था कि इस नगर के लोगों की नींद आज खुली ही नहीं है । मैं अकेला ही अपने आप से बातें करता हुआ चला जा रहा था । गली के दूसरे मोड़ तक पहुँचते-पहुँचते मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिससे मैं कुछ बातें कर सकूँ । अपने आप से भी कोई व्यक्ति आखिरकार कितनी बात कर सकता है सोचता हुआ मैं यूँ ही रास्ते के किनारे-किनारे बढ़ता चला जा रहा था ।
इस रास्ते पर अकेले चलते हुये न जाने क्यों किसी साथी की कामना मन में जागी थी । ऐसा लग रहा था मानो उम्र का एक लंबा पड़ाव मैंने अकेले ही बिना किसी हमराही के काट दिया हो आज अपने आप से अकेले में बातें करने की बजाय मुझे अपने सफर में एक राही की जरूरत लगने लगी थी जिससे अपने मन की बात खुलकर कर सकूँ । छोटी-छोटी-सी ही सही किंतु ऐसी बातें भी होती हैं जिनमे किसी की भागीदारी व साझीदारी की कामना मैं करने लगा था । उम्र के पचास साल के पड़ाव के किनारे खड़ा मैं द्वन्द्व का अकेला ही साक्ष्य व साक्षी रहा हूँ आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब बहुत हो गया ।
तभी मेरे बगल में खड़े पेड़ के तने से एक गिलहरी अपनी लंबी पूँछ हिलाती नीचे धरती पर कुछ उठाने के लिये उतरी उसके पीछे-पीछे दूसरी गिलहरी भी उतर आई । दोनो यहाँ-वहाँ फुदकते रहे फिर वापस पेड़ पर चढ़ गये ।
प्रकृति में हर प्राणी को एक साथी की जरूरत पड़ती ही है । प्रेम स्नेह आनंद व जीवन के खिलवाड़ का सुख बिना किसी साथी के भला कैसे लिया जा सकता है । कोई न कोई साथी तो हो जिसका हाथ थामकर जीवन के सुख-दुःख को महसूस कर सके ।
अपने आप से बातें करता हुआ मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था । तभी रास्ते के किनारे थोड़ी ही दूरी के फासले पर छोटे-से गड्ढ़ेनुमा खाई में हँस का जोड़ा पानी में अठखेलियाँ करता मिला । आसमान में दूर से अपनी यात्रा करके आये पक्षी का यह जोड़ा शायद अपनी प्यास बुझाने धरती पर उतर आया था । सुबह-सुबह तो इनकी उड़ान का समय होता है ठहरे हुये इस छोटे-से तालाब के ऊपर वे तरह-तरह के खिलवाड़ करते डुबकी लगाते जल-क्रीड़ा का दृश्य इतना खूबसूरत व मनोहर लग रहा था कि मेरे कदम अपने आप रूक गये ।
ठहरा हुआ पानी हँसों के किलोल व खिलवाड़ से बहती धारा में परिवर्तित हो गया । रूके हुये पानी में जल-तरंग बज उठा हो हँसों के किलोल ने आस-पास के संपूर्ण परिदृश्य को जीवंतता प्रदान कर दी थी । थोड़ी देर पहले यहाँ छाई सघन खामोशी व मेरे भीतर पसरे हुये एकांत चुप्पी को हँसों के कलरव ने हलचल में तब्दील कर दिया हो ।
उनके किलोल को देखकर मैंने अपने विवाह का निर्णय ले लिया था । उम्र के इस मोड़ पर ही सही मन में जब भाव जागे तभी सही । हालांकि मेरी उम्र सामाजिक परंपराओं व विवाह के वैधानिक उम्र की समाज में बरसों से चली आ रही परिपाटी के हिसाब से बड़ी थी फिर भी वैवाहिक जीवन के बँधन में बँध जाने की इच्छा करना सामाजिक दायरों से बाहर भी नहीं था जिसके लिये मैं स्चयं को मानसिक द्वन्द्व व अंतर्विरोधों के नये जाले में जबरन उलझने के लिये बाध्य करता । यह एक आम मानवीय अनुभूति थी जो स्वाभाविक व नैसर्गिक थी
तुम्हारे चेहरे पर छाये जिंदगी से भरे-पूरे भावों ने मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित किया था । ठहरी हुई खामोशी को तोड़ते हुये मैंने बातचीत की शुरूआत ठीक वहाँ से की जब हम पहली बार एक-दूसरे से मिले थे । उसके बाद तो बातों का सिलसिला बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया जैसे मंझधार में छोड़ी हुई कश्ती पानी के बहाव के साथ अपने-आप अपनी दिशा तय कर जाती है ठीक वैसे ही हमारी बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी । मेरा मस्त-फक्कड़ स्वभाव और तुम्हारी एक से बढ़कर एक फब्तियों पर हँसी के दौर से गुजरते तुम शरारती आँखों से मेरी तरफ देखती हुई अपने होंठों पर ऊँगली रखते हुये मुझे चुप रहने का इशारा करती । एक संपूर्ण चेहरा मैंने तुम्हें संपूर्णता के साथ स्वीकार कर लिया था ।
तुमने धीरे-से दस्तक देते हुये मेरे जीवन में प्रवेश किया । हम दोनो के लिये गृहस्थ-जीवन में पदार्पण का अनुभव थोड़ा अनोखा-सा था बदलाव समझौते व सामंजस्य से मेरा परिचय हो रहा था । तुम मेरे जीवन का अहम् हिस्सा बन चुकी थी ।
तुम्हारी आम-सी आदतें व सामान्य व्यवहार ऐसा लगा जैसे जीवन की धड़कनों का नया संगीत मैं तुम्हारे साथ-साथ सुन रहा हूँ ।
सृष्टि के रचयिता ने हमें इस तरह बनाया है कि हम खुद के चेहरे को नहीं देख पाते मेरे सामने जो चेहरा था वह तुम्हारा था ।
जीवनसाथी का संपूर्ण चेहरा संबल देता है ।
खूबसूरत और मुस्कुराती मूर्तियाँ तो मैं सालों से अपने परिवेश के भीतर और आस-पास देखता आ रहा हूँ किंतु बदलते मौसम के साथ संघर्षों से जूझता तपा हुआ चेहरा ही असली चेहरा होता है
तुम्हे देख कर मैं विस्मित हो उठता था जैनथपी अपनी सीधी-सरल और छोटी-सी गृहस्थी में बच्चों की परवरिश में तुम कितनी लीन हो । तुम्हारे दायरे उन्हीं के इर्द-गिर्द ही सिमटे हुये हैं । इस विस्तृत और विशाल जगत में तुमने अपने जीवन के साथ-साथ खुशियों को और दुःखों को भी कितने सीमित दायरों में बाँध लिया है । बगीचे से सब्जी टोकरी में भरकर लाते देख कलियों को खिलता देखकर चिड़िया की चहचहाहट सुनकर तो कभी बच्चों के साथ थोड़ा-सा वक्त बिताकर तुम कितना खुश हो जाती हो तुम्हे देख कर मैं विस्मित हो उठता था जैनथपी अपनी सीधी-सरल और छोटी-सी गृहस्थी में बच्चों की परवरिश में तुम कितनी लीन हो । तुम्हारे दायरे उन्हीं के इर्द-गिर्द ही सिमटे हुये हैं । इस विस्तृत और विशाल जगत में तुमने अपने जीवन के साथ-साथ खुशियों को और दुःखों को भी कितने सीमित दायरों में बाँध लिया है । बगीचे से सब्जी टोकरी में भरकर लाते देख कलियों को खिलता देखकर चिड़िया की चहचहाहट सुनकर तो कभी बच्चों के साथ थोड़ा-सा वक्त बिताकर तुम कितना खुश हो जाती हो मैं चाहकर भी तुम्हारी तरह नहीं बन सकता । विधाता ने जिन मूरत को अपने हाथों से गढ़ा है उनके हिस्से में सौगात भी अलग-अलग सौंपे हैं ।
स्वर्णिम धागे से बुना संसार खुली किताब सा बिखरा है । जिंदगी को अपने ढंग अपनी मर्जी से जिया जा सकता है पढ़ने के लिये पुस्तक में अनेक पन्ने हैं जरूरी तो नहीं हाथ में आते ही सबसे पहले पुस्तक के अंतिम पृष्ठ खोलकर उत्सुकता को हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त कर लिया जाये ।
प्रातःकाल कितनी खूबसूरती के साथ मेरे द्वार पर हर रोज़ दस्तक देता है । निसर्ग प्रकृति का सारा सौन्दर्य मेरे आस-पास बिखरा पड़ा था । किंतु मुझे जिस चीज से प्रेम था वह था मानव । मनुष्य ही मुझे सबसे प्रिय था । प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर मेरे आस-पास हर जगह मौजूद थी फिर भला मैं और किसी चीज के बारे में क्या विचार करता भौतिक ऐहिक लौकिक अलौकिक सांसारिक सभी वस्तुऐं मुझे प्राणवान खूबसूरत मानवाकृति के सामने बहुत छोटी लगती थी मेरे पिता की बनाई मूर्तियों से भी खूबसूरत थी यह मानवाकृति मूर्तियों को मानव के हाथ गढ़ते हैं किंतु मानव की रचना तो विधाता ने स्वयं अपने हाथों से की है । अंकुरण की कोमल-सी दस्तक के प्रस्फुटन को मैं रोक नहीं पाया । सृजन की प्रक्रिया में प्रकृति संघर्ष रूपी थोड़े रोड़े जरूर डाल ले किंतु बाधक कभी नहीं होती
अंतिम सच तक सत्य के चरम बिन्दु तक मैं वार्तालाप कर रहे व्यक्ति के साथ पहुँच जाना चाहता था जहाँ पाप-पुण्य सही-गलत परिपाटी-प्रथाओं व मान्यताओं से परे सिर्फ शुभ ही सत्य होता है और कुछ भी नहीं । जिंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं होता ।ईश्वर की बनाई जिंदगी हमेशा से खूबसूरत रही है ।
मेरा पाँव सड़क के किनारे पड़ी रस्सी के उलझे हुये फंदे से टकराया । सड़क पर पड़ी हुई मोटी-सी उलझी हुई रस्सी । मन में क्या आया कि झुकते हुये मैंने उसे अपने दोनों हाथों में उठाया एकाध गाँठ यहाँ-वहाँ बेवजह पड़ गई थी जिसे बड़ी ही आसानी के साथ आराम से खोलकर धीरे-से धरती पर वहीं छोड़कर मैं आगे बढ़ गया ।
मैं लौट रहा था
मैंने कदम बढ़ाये ही थे कि मेरी नजर सड़क कें बीचोंबीच पड़े उसी रस्सी के टुकड़े पर जाकर स्थिर हो गई जिसे सुलझाकर मैंने किनारे रख दिया था ताकि उससे कोई उलझकर गिर न जाये ।
मेरी सुलझी हुई रस्सी से कोई अनजाने में उलझकर गिर गया था जिससे वह वापस उलझ गई थी या किसी ने खेल-खेल में उसे फिर से उलझा दिया था । ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज तक जीवन की गाँठों को सुलझाता रहा हूँ अन्यथा तो इस प्रकृति की तरह मानव का जीवन भी सीधा-सादा और सरल है हम खुद ही उसमें इतनी उलझन भरी गाँठें लगा देते हैं कि जीवन-भर उसे सुलझाते रहने के सिवा और कोई काम बचा नहीं रह जाता
लोगों के मन में और दिलों में पड़ी हुई गाँठों को सुलझाने के लिये ही तो इन गलियों में भटकता रहा हूँ ।
चलते-चलते मैं रूक गया । यह मेरी पुरानी आदत थी । लोगों से वार्तालाप करते हुये चरम क्षणों में चलते-चलते अक्सर ही मैं रूक जाया करता था । मित्रगण मुझसे अक्सर कहते भी थे कि सुकरात चलते-चलते भी हम बातें कर सकते हैं किंतु बातचीत जब सार्थक पड़ाव पर पहुँच रही हो, तो उन क्षणों में मैं ठहर जाना ही पसंद करता था या फिर यूँ कहूँ कि अनजाने में मेरा शरीर ठहराव की प्रक्रिया को अख्तियार कर लेता था ।
मैंने बड़े आराम से रस्सी में पड़ गये उलझी हुई गाँठों को सुलझाया । सड़क के किनारे धीमे-से रखते हुये भविष्य के अनदेखे से पथ पर धीरे-धीरे कदम बढ़ाता चला गया
बाहर कुछ शोर था कुछ अजीब आवाजें भीतर आ रही थी । इस तरह के शोर की मुझे अपने घर में आदत नहीं थी । यूँ समाज व परिवेश में व्याप्त शोर से मैं सर्वपरिचित था और उनकी आदत-सी डाल ली थी । किंतु ये शोर मेरे शिष्य और एक अजनबी के बीच था ।
मैं उस समय ध्यान की अवस्था में लीन था । घर में इस वक्त हम दोनों के सिवा तीसरा कोई भी मौजूद नहीं था, और यह समय किसी आगंतुक के आने का नहीं था । फिर यह अजनबी आगंतुक इतने शोर-शराबे के साथ मेरे घर के भीतर मेरे शिष्य से क्यों उलझ पड़ा है । न जाने बाहर से आती हुई उन आवाजों में कैसी दृढ़ता और आकर्षण था कि ध्यान को बीच में विराम देते हुये मैं उठने के लिये स्वयं को तैयार करने लगा । अपने आसन को उठाकर तह करके रखते हुये चंद आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी । धूर्त मक्कार लालची दंभी महत्वाकांक्षी धृष्ट यह सारे शब्द वह व्यक्ति मुझे संबोधित करके कह रहा था पुरजोर विरोध करते शिष्य का उसी दृढ़ता से उभरता स्वर ।
आज तक मुझ पर यह आरोप किसी ने नहीं लगाया था । आसन को मोड़कर यथास्थान रखते हुये मेरे माथे पर त्यौरियाँ पड़ती चली गई थी आखिरकार यह अजनबी आगंतुक कौन है जो इस असमय आने की धृष्टता के साथ-साथ मेरे घर पर आकर अशिष्ट व्यवहार कर रहा है
मैं बाहर आया । गुस्से से तमतमाये भृकुटी चढ़ाये उस उग्र व्यक्तित्व के हाथ में ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें देखकर मैं समझ गया कि यह बड़ी-बड़ी पुस्तक अध्ययन के साथ मीमांसा में लगा कोई प्रकांड ज्योतिषाचार्य है ।
मेरे विनम्र अभिवादन को भी उसने उसी अशिष्टता के साथ ठुकरा दिया था और शिष्य की तरफ मुड़ते हुये अपनी कही बात के प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये मुझसे ही मुखातिब होकर कहा पूछ तो अपने गुरू से कि मैंने जो कहा वह झूठ था । इससे पहले कि शिष्य दुविधा और संशय की स्थिति में आता मैंने आगे बढ़कर बात संभाल ली थी
महान ज्योतिषीजी आपने जो कुछ कहा वह सत्य है किंतु एक सच और है जिसे आप नहीं जानते मैंने अपनी कमियों को विवेक से दबा दिया है । मेरा विवेक इन सब मानवीय अवगुणों से ऊपर है ।
लोग मेरी बातों से अक्सर यह भ्रम पाल लेते थे कि मैं प्रजातंत्र का विरोधी हूँ दरअसल मैं प्रजातंत्र का नहीं भीड़तंत्र का विरोधी था । भीड़ में विवेक कहाँ होता है । उसे कानून और राजनीति का भी सम्यक ज्ञान नहीं होता ।
मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि देश का शासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हो जो राजनीति के विशेषज्ञ हो। सचमुच यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश के शासन जैसे गंभीर विषय पर जहाँ इतने व्यक्तियों के सम्मान और सुरक्षा का प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारी मान लिया जाता है जबकि कुर्सी-मेज जैसी साधारण चीजों के निर्माण में हम उन वस्तुओं के विशेषज्ञों की राय लेना आवश्यक समझते हैं । यह तो कोई बात नहीं हुई कि राष्ट्रीय नीति निर्धारण के समय जब उचित अथवा अनुचित का प्रश्न उपस्थित हो तो जो भी उठकर बोलने लगे उसी को न्यायाधीश के समान उपयुक्त और योग्य मान लिया जाऐ ।
मेरा तो शुरू से ही यह मानना रहा है कि समीक्षा की कसौटी पर कसे बिना जीवन जीने योग्य नहीं होता । इतने दिनों तक जीवन के इस पक्ष की समीक्षा किये बिना कैसे रहा यह खुद मेरे लिये आश्चर्य का विषय था ।
अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करके कोई काम नहीं किया और ना अपने दर्शन और सिद्धांतों से कभी डिगा । बाकी तो जीवन की छोटी-मोटी समस्याऐं तो हर व्यक्ति के जीवन के साथ ही चलती हैं । उनके साथ कदमताल करते हुये जीवन गुजार दो तो संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति विधाता के द्वारा रची हुई सबसे सुंदर जगह लगती है ।
यहाँ प्रकृति पूर्णतः व्यस्थित है । प्रत्येक का अपना उद्देश्य है । मानव इस सृष्टि में सर्वोत्तम है । सृष्टि की सभी चीजें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, विभिन्न ऋतुओं का मानव के लिये ही सृजन हुआ है । विभिन्न पशु-पक्षी भी मानव को सुख देने के लिये ही बनाये गये हैं । स्वयं मानव शरीर की संरचना भी मानव के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर की गई है । यहाँ तक कि मानव का बौद्धिक वैभव, स्मृति, भाषा और सारे मनोभाव भी उसके प्रति सृजनहार का विशेष प्रेम दर्शाते हैं ।
और तो और मुझे तो ईश्वरीय आदेश में भी दृढ़ विश्वास है । हम सबके भीतर ईश्वरीय अंश के रूप में अंतरात्मा होती है जो वास्तव में हमें ईश्वरीय वाणी सुनाती है । बस उसी वाणी को अपने ही अंतर्मन में उठने वाली आवाज को ही तो मैं ‘देववाणी’ कहा करता था । यह तो हम सबके भीतर होती है ।
मैं सोच रहा था ईश्वर के बारे में जिसे पाने के लिये आदिकाल से ऋषियों और मुनियों ने न जाने कितने तप, उपवास और साधना किये हैं । उसकी उपस्थिति के एक हस्ताक्षर को पढ़ लेने की कोशिशों में अब तक मानव न जाने कितने प्रयास करता रहा है । इस खूबसूरत किंतु रहस्यमय जगत् को अपनी जादुई दुनिया से चित्रित करने वाले सृजनकार को कभी भी किसी ने अपनी खुली आँखों से आज तक नहीं देखा शायद इसीलिये इस विश्व का हर प्राणी अपनी कल्पना से उसके विविध रूप चित्रित कर अनेकानेक नामों से विभूषित करता आया है । तभी तो देश और काल के साथ-साथ देवताओं के नाम और स्वरूप परिवर्तित होते रहेते हैं । हम सभी उसे महसूस करते हैं, उनका आभास करते हैं किंतु उसे व्यक्त करने का सबका अंदाज अलग-अलग होता है ।
जैसे एक कुम्हार कच्ची माटी को अलग-अलग रूपों में ढ़ालता है, वैसे ही हम सभी उस दैवीय शक्ति को अपनी कल्पना के माध्यम से अलग-अलग साँचों में ढ़ालने की जीवन-भर कोशिशें करते रहते हैं । और कई बार तो हमें पूर्वजों द्वारा गढ़े गये स्वरूप ही इतने प्रभावी लगते हैं कि हम उन्हीं में अपनी आस्था के नन्हे-नन्हे मोती पिरोकर उसी खूबसूरत माला को और मजबूत बनाते चले जाते हैं ।
हो सकता है आने वाला समय मेरे आज कहे जाने वाले कथन को ही प्रतिमान बनाकर एक नई परिभाषा गढ़ दे, जो आने वाले समय का सच बन जाये ।
ऐसा लग रहा था मानों प्रश्नों की उलझी हुई गुत्थी से मुझे हमेशा-हमेशा के लिये मुक्ति मिल गई है ।
पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़कर मानव के पास कुछ भी बचा नहीं रह जाता । उस चोटी से आगे ऐसी कोई भी ऊँचाई बची नहीं रह जाती, जिसे वह अपने कदमों से नापने के लिये आगे बढ़ सके ।
उसके सामने कोई भी लक्ष्य, कोई भी गंतव्य, कोई भी मंजिल नहीं बचती है । वह शिखर ही उसके लिये ठहराव का सबब बन जाता है । सामने दिख रहे उस सबसे खूबसूरत स्वर्गीय नजारे को देख लेने के पश्चात् उसके पास संभलकर धीरे-धीरे पीछे लौट आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता । क्योंकि उसके बाद सिवाय शून्य के और कोई ऊँचाई नहीं बची रहती ।
ईश्वर को पा लेने या उसे जान लेने के पश्चात् मानव के मन में कोई कामना कोई लालसा या कोई इच्छा नहीं होगी उसे पा लेना रहस्य के अंतिम पड़ाव को पार कर लेने के समान ही होगा उसे पा लेने के बाद तो उसकी बनाई यह सारी दुनिया ही शून्य व अर्थहीन लगने लगेगी ।
इस जीवन के छोटे-छोटे सुख-दुःख, पीड़ा और माया में उलझा संसार ही तो जीवन को भरपूर तरीके से जी लेने का सबब है । इसी में रचे-बसे और उलझे हुये हम रोज अपनी जिंदगी को नये सिरे से जीते चले जाते हैं ।
कहते हैं व्यक्ति जैसे-जैसे तार्किक होता जाता है वैसे-वैसे कोमल भावनाओं के ऊपर यथार्थ हावी होता चला जाता है ठोस बौद्धिकता के नीचे कविता की कोमल भावनायें हृदय की अतल गहराई में कहीं सूखने लगती है ठोस धरातल वर खड़ा व्यक्ति जिंदगी को अपनी तार्किक कसौटी पर कसने लगता है ।
जीवन के प्रारंभ से लेकर सत्तर साल की उम्र तक मैं बौद्धिक और तार्किक नजरिये से दुनिया को और इसके रहस्यों को देखता आया हूँ । विवेक का दामन मैंने कभी नहीं छोड़ा । उम्र के इस पड़ाव पर बैठकर विश्राम के इन क्षणों में शांति के साथ बैठकर अपनी रचना के साथ उफनती लहर में डूब-उतरा रहा हूँ । ठीक है जीवन के जिस रस से मैं आज तक वंचित रहा उसका इस उम्र में ही सही रसास्वादन तो कर रहा हूँ ।
मैंने कारणों पर विचार नहीं किया । जिंदगी जिस रूप में जैसी भी स्थिति में मेरे सामने थी उसके साथ रूबरू होता गया कई गाँठें खुलती रही गुत्थियाँ सुलझती रही मैं समंदर पर समाधि की मुद्रा में शांति से आँखें बंद किये लहरों के बीच डूबता-उतराता रहा ।
एक पूरा जीवन जिया है मैंने । अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से चीजों को स्वीकारता रहा छोड़ता रहा । जीवन को संपूर्णता के साथ जिया है मैंने । इस शहर से कोई शिकायत नहीं है मुझे । यहाँ के लोगों से कोई शिकवा नहीं है । इन सबसे आज भी प्रेम है मुझे । मेरे मानसिक धरातल को अपने सर्वोच्च शिखर तक ले जाने की स्वतंत्रता व आजादी दी है इस शहर ने ।
क्षितिज पर चाँद ने अपनी कलाओं के साथ बसेरा बना लिया था । रात की कालिमा घिरने से पूर्व ही चँद्रमा आसमान में हमें यह बताने के लिए उपस्थित हो जाती है कि रात कितनी भी काली हो आशा की शुभ्र किरणे इस धरती की आशाओं को सुनहरे सपनों को कभी क्षीण नहीं होने देगी । अपनी कलाओं के उतार चढ़ाव के साथ वह धरतीवासियों को नई दुनिया सजाने के लिये बाध्य करता रहता है ।
यथार्थ कितना भी कड़वा हो, सच कितने ही जहर के प्याले के साथ खड़ा हो रात कितनी ही काली हो कल्पना व स्वप्न के सतरंगी इंद्रधनुषी सपने इस संसार में हमेशा जीवित रहने चाहिये । आसमान के अँधेरे फलक पर छाया चाँद कल्पनाओं को मिटने नहीं देता उस खूबसूरत से चाँद को देखकरमैं धीमे से मुस्कुरा दिया ।
स्वयं को विराम देते हुये मैंने एक नई यात्रा पर अपने कदम बढ़ा दिए ।
मुझे मालूम था कि मेरे मित्र मेरे विचारों को कभी मरने नहीं देंगे । और आत्मा की अमरता पर तो मुझे शुरू से विश्वास था । मुझे विश्वास था कि मैं इन्हीं के माध्यम से पुनर्जीवित हो उठूँगा । रक्तबीज-सा ही मैं उनके विचारों में एक नहीं अनेकों बार पुनः उग आऊँगा ।
मुझे विश्वास था कि एथेन्स की इस धरती पर जो नन्हे-नन्हे बीज मैंने आज बोए हैं वह कालांतर में एक सुंदर वृक्ष के रूप में धरती पर छा जायेगा । इस वृक्ष की छाया में आने वाले समय में अनेक लोगों को शीतल छाया मिलती रहेगी । सदियों का समय भी इसे सुखा नहीं पायेगा ।