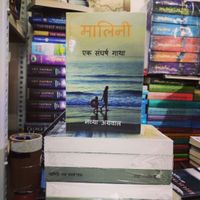संवाद और समझ की केमिस्ट्री
संवाद और समझ की केमिस्ट्री


अपनी समझने की शक्ति को निखारें। पारिवारिक सामाजिक या राजनैतिक जीवन में हमें परस्पर एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में यथार्थ समझ का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार दूसरों के विषय में हमें उनकी आंतरिकता की समझ उनसे संवाद करने के बाद ही होती है। निश्चित समय तक परस्पर संवाद के अनुभव के बिना हमें यूं ही किसी के भी बारे में अपना मंतव्य नहीं देना चाहिए। दूसरों के बारे में अपना मंतव्य देने से पहले आपको स्वयं को पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। आप पूरी तरह आश्वस्त तभी हो सकते हैं जब आप उनके साथ संवाद के एक निश्चित दौर से निश्चित समय तक गुजरे हों। अन्यथा नीम हकीम वाली बात हो सकती है।
संवाद दो तरह के हो सकते हैं। एक संवाद होता है निष्प्रयोजन। दूसरा संवाद प्रयोजन से होता है। निष्प्रयोजन संवाद में सब रोजमर्रा की साधारण बातें आती हैं। उसमें जरूरी और गैर जरूरी सब प्रकार का संवाद आता है। दूसरा संवाद वह होता है जिसका एक विषय और ध्येय होता है। वह तथ्यों पर आधारित और समूल रूप से व्यावहारिक होता है। संवाद से एक दूसरे की समझ बढ़ती है। यदि समझ (ज्ञान) की शक्ति हो तो संवाद में संकोच नहीं होता। समझ हो तो संवाद सौहार्दपूर्ण होता है। समझ हो तो संवाद को नकारने की बात नहीं होती। समझ हो तो समय का एक टुकड़ा संवाद के लिए निश्चित निसंदेह किया जा सकता है। संवाद नहीं तो अन समझी, अनुमान और शंकाएं बढ़ती हैं। फिर बहुत कुछ नकारात्मक होता है। जीवन के बहुत से स्तर ऐसे भी होते हैं जिनमें यदि सौहार्दपूर्ण संवाद नहीं होता तो जीवन नारकीय अनुभव कराने वाला भी बन सकता है। पारस्परिक निष्प्रयोजन संवाद को कम तो कर देना चाहिए पर पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहिए। वह संवाद भी कम मात्रा में अनिवार्य होता है। प्रयोजनार्थ जो संवाद आवश्यक होते हैं उनको चूकने ना दें। ऐसे संवाद को पूरे उदार हृदय से विवेक पूर्वक करें। यदि आप प्रयोजनार्थ संवाद को चूकेंगे और उसे नहीं करना चाहेंगे या स्थगित करते जाएंगे तो उसके प्रकंपन आपका पीछा करेंगे। लिहाजा बेचैनी दो तरफा होगी।
संसार में जितने भी दुराव या कलह कलेश की स्थितियां बनी हुई हैं और उन्हें सुलझाने में अच्छी खासी ऊर्जा और लम्बा समय लगता है, उनके मूल में केवल सौहार्दपूर्ण संवाद की ही कमी होती है। अहम अथवा अहंकार तो सब समस्याओं के मूल में कार्य करता ही है लेकिन उसके भी मूल में एक और तत्व काम कर रहा होता है। वह तत्व है अज्ञानता के द्वारा पनपी अनसमझी का। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है भय और आशंका का। यदि ज्ञान की स्थिति बढ़ जाए और भय कम हो जाए तो संवाद की कमी हो ही नहीं सकती। केवल इस एक कमी को दूर करने से ही संसार की आधे से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसलिए ही ज्ञान को समाधान कारक कहा गया है। "The Knowledge is problem solving. The Ignorance is problem creating.
यहां प्रश्न यह उठता है कि लोगों को ज्ञान होते हुए भी उनका ज्ञान समाधान कारक क्यों नहीं होता? इसके तीन मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। एक - व्यक्ति को यह ज्ञान तो होता है कि संवाद के द्वारा स्पष्टता हो सकती है। स्पष्टता होने से कठिनाई को ठीक तरह से जाना समझा जा सकता है। उसके बाद उसका उचित समाधान सम्भव हो सकता है। मान लीजिए यदि उचित समाधान नहीं भी सम्भव हो सकता है तो भी इतना तो अवश्य हो ही जाता है कि मन में किसी प्रकार का द्वंद या किसी प्रकार की ग्लानि कुंठा नहीं रहती। इतना हो जाना भी तो कम नहीं होता है। लेकिन ज्ञान हो जाने के बाद भी संवाद नहीं होता, उसके परोक्ष में भय शंका का तत्व कार्य कर रहा होता है। भय के मूल में तो अहंकार का अंश होता है। दूसरा - दो तरफा आह्वाहन नहीं होता। पारस्परिक संवाद की सहजता में एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि संवाद तभी अपनी सहजता से प्रकट होता है जब संवाद करने वालों की दो तरफा आवाहन की मनोस्थिति होती है। अन्यथा केवल एक तरफा आह्वाहन होने से संवाद सम्भव नहीं होता। तीसरा - मुझे सब पता है। मैं सब जानता/जानती हूं। यह सब जानने की जो भ्रान्ति होती है यह भी बहुत बड़ी रुकावट होती है। जबकि हमें इस मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति के अन्दर पूर्वाग्रहों का अंतर्विज्ञान काम कर रहा होता है। इसलिए उसके अंदर यह भ्रान्ति निर्मित हो जाती है कि मैं तो सब जानता हूं। जबकि पूर्वाग्रह तो होते भूतकाल (पास्ट) के और आपको जानना होता है मनुष्य की वर्तमान की परिस्थिति व मनोस्थिति को।
पारस्परिक संवाद के परिप्रेक्ष्य में यह भी जान लेना जरूरी है मनुष्य की अनुमान लगाने की और शंकाएं/भय पैदा करने की आदतें ज्यादा होती हैं। वह अपनी आदतों वश दूसरों के बारे में अपने मंतव्य देता है। आप स्वयं के बारे में कुछ भी सोच समझ लेने में स्वतंत्र हो। क्योंकि आप स्वयं ही स्वयं को सबसे ज्यादा जान समझ सकते हैं। हालाकि कई बार आप स्वयं ही स्वयं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हो, वह बात अलग है। लेकिन आप अपने स्वभाव गुणों के बारे में जितना बखूबी बता सकते हैं उतना दूसरों के बारे में नहीं। दूसरों के बारे में आप कोई निश्चित मंतव्य नहीं दे सकते। कुछ भी सोच समझ नहीं सकते हो। दूसरों के बारे में आपका सोचना समझना केवल एक अनुमान ही होता है। इसलिए दूसरों के बारे में कुछ भी सोचने, समझने और अपना ओपिनियन देने से पहले उनसे खुलकर संवाद करें। यदि कभी कुछ प्रयोजनार्थ परस्पर संवाद करना आवश्यक लगे तो बेशक निसंकोच दूसरों से संवाद करें। डरें नहीं।
जो है उसे स्पष्ट हो जाने देने में संकोच/भय कैसा? बल्कि स्पष्ट होने के बाद अन्तर मन में बैठे हुए संकोच या भय दूर होंगे। वस्तुस्थिति के स्पष्ट होने से, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने से, वस्तुस्थिति को स्पष्ट समझने से कोई तत्काल समाधान हो या ना हो, लेकिन जो भी उस परिस्थिति से संबंधित लोग होते हैं उनकी मानसिक बौद्धिक ऊहापोह (चिन्ता/व्यर्थ संकल्प) जरूर दूर हो जाती है। स्पष्टता का इतना असर भी क्या कम है? स्पष्टता से कठिनाइयों का हल जल्दी निकालता है जबकि अस्पष्टता से असमंजस और किंकर्तव्यवमूढ़ की अवस्था बनी रहती है। ध्यान रहे - कर्म, सम्बन्धों, स्व पुरुषार्थ आदि के किसी भी क्षेत्र में स्पष्टता (क्लैरिटी) को ही सब कुछ कहा गया है। क्योंकि स्पष्टता के बाद ही ततक्षण मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक ऊर्जाओं का प्रवाह उस ओर निमज्जित होना शुरू हो जाता है। 🙏👍🌹