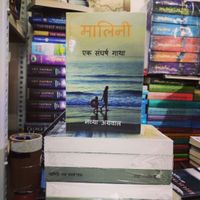अन्दर से बाहर की ओर
अन्दर से बाहर की ओर


"क्या नव संस्कारों की निर्मिती संभव है"
"चीजें अन्दर से बाहर की ओर प्रकट होती हैं"
यह सृष्टि का एक मौलिक मूल सिद्धांत है कि चीजें अन्दर से बाहर की ओर प्रकट होती हैं। अन्दर से बाहर प्रकट होकर वे एक ऐसा स्वरूप ले लेती हैं जिसमें एक ऐसी प्राकृतिक व्वस्वस्था बनती है जिससे पुनः अन्दर से बाहर प्रकट होने की चक्रवत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बीज अन्दर से बाहर प्रकट होकर वृक्ष बनता है। वृक्ष अनेक प्रक्रियाओं से गुजर कर पुनः बाहर प्रकट होकर बीज बन जाता है। इस प्रकार यह एक अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। अनादि और प्रक्रिया जो है उसे हम ऐसा समझ कर चलते हैं कि आंतरिकता से ही बाहरी स्वरूप प्रकट होता है। ठीक यही स्थिति आत्मा (चेतना) की भी होती है। हमारी आत्मा की आंतरिकता ही बाहरी रूप से भौतिक जगत में प्रकट होती है। इसे गहरे में आप मनोविज्ञान या और भी ज्यादा गहरे में अध्यात्म विज्ञान भी कह सकते हैं।
जैसे हमारे विचार, भाव या संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे व्यावहारिक जीवन से प्रकट होते हैं। संस्कार एक बड़ी ही अवचेतन अचेतन की आन्तरिक बात है। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही वे बाहर प्रकट होते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही बाहरी जगत में वाचा और कर्म व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं वे ही भाव प्रकट होते हैं विचार, बोल और कर्म के रूप में। हमारे आन्तरिक जगत में (आत्मा की आभा में) जो कुछ भी होता है वह बिना बोले, बिना कहे भी मूक अवस्था में भी प्रकंपन के रूप से बाहर प्रकट होता रहता है। हम अपना सारा आन्तरिक आण्विक संसार सदा साथ लिए चलते हैं।
इसे आप सिम्पल साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। "बर्तन में जो होता है वही बाहर छलकता है।" तात्पर्य है कि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। हमारे पास जो कुछ भी है जैसा भी कुछ है हम उसे ही दूसरों को चाहे अनचाहे, ऐच्छिक या अनैछिक रूप से दूसरों को दे सकते हैं या देते हैं। यदि हमारी आन्तरिक दशा शान्तचित्त की है तो हम दूसरों को स्वत: शान्ति के प्रकंपन देते हैं या अन्यान्य रूपों में हमारे व्यावहारिक रूप से शान्ति प्रकट होती है। हमारे अन्तर में यदि सुख है तो हम दूसरों को भी सुख ही देते हैं। यदि हमारे पास दुख है तो हम दूसरों को दुख ही देते हैं। यह सच है। यदि हमारी आन्तरिक दशा दुख की है तो हम चाहें या ना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे, प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से हम दूसरों को कम या ज्यादा दुख ही देते हैं। यानि कि सूक्ष्म स्तर पर कहें तो.. हम अपनी आन्तरिक स्थिति से निरन्तर देने या निरन्तर लेने की स्थिति में होते हैं। इसे अध्यात्म विज्ञान ने बहुत गहरे वैज्ञानिक तरीके से आण्विक स्तर पर इस तरह कहा है कि ("मैं तुम में हूं और तुम मुझमें हो, I am in you, you are in me"). इसी स्थिति के सूक्ष्म स्तर को यदि स्थूल स्तर के अनुसार कहें तो पदार्थ जगत के बारे में कहा जा सकता है। उसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भौतिक विषय वस्तु होती है, हम वही दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है वह दूसरों को नहीं दे सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी पात्रता/योग्यता/क्षमता के अनुसार ही बाहरी जगत में देता है या अपनी अपनी पात्रता/योग्यता/क्षमता के अनुसार ही बाहरी जगत में लेता है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ लेने देने का कार्य बड़े व्यवस्थित ढंग से एक स्व चालित मशीन की कार्यविधि की तरह चलता रहता है। हम इसे अपनी बुद्धि से स्पष्ट रूप से इसके आण्विक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, वह बात दूसरी है।
हमारी आंतरिकता को बाहरी जगत में प्रकट होने में समय, स्थान और परिस्थितयों का भी बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है। हमारी आंतरिकता यूं ही कभी भी कैसे भी प्रकट नहीं होती। जैसी जैसी परिस्थिति, या जैसा जैसा समय या जैसा जैसा स्थान का संयोग बनता है, ठीक उसी से मिलती जुलती आंतरिकता प्रकट होती है। यानि कि हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व का निर्मित होना या व्यावहारिक जगत में प्रकट होना; वह सब स्थान, परिस्थिति और समय पर निर्भर होता है। अध्यात्म के जगत के कुछ रहस्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनके प्रकट होने में समय स्थान और परिस्थिति की निर्भरता जरूरी नहीं होती हो। किन्तु भौतिक जगत में जिस विषय का संबंध मनोविज्ञान से है वह सब कुछ तो समय, स्थान और परिस्थिति पर ही निर्भर होता है। इसलिए भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के परवश रहता है। कर्मों के सिद्धांत की प्रक्रिया भी प्रकृति के मूलभूत अदृश्य नियमों के अन्तर्गत ही आता है। अर्थ यह हुआ कि मनुष्य प्रकृति के परवश होकर तो कार्य करता ही है लेकिन साथ साथ वह अतीत और भविष्य के कर्मों के भी अधीन होकर कार्य करता है। इसलिए ही तो अध्यात्म विज्ञान कर्म सिद्धांत से पार के नियति के विज्ञान को मानता है और नियति के निर्दोष होने की उन्मुक्त उदघोषणा करता है।
एक ओर तो अध्यात्म विज्ञान नियति को सर्वोपरि मानता है, वह सब कुछ की पुनरावृत्ति को मानता है। जो एक कल्प में जो गया, वह चक्रवत फिक्स्ड हो गया। अब उसकी ही पुनरावृत्ति करनी है। अब उससे अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर मनोविज्ञान का कहना है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा हम अपनी आंतरिकता का नव निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा बाहर के प्रकटीकरण की सूक्ष्म छवि (ब्लू प्रिंट) अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं ताकि जो कुछ भी प्रकट हो वह हमारी उच्चतम मनोदशा के अनुकूल, नैतिक, मूल्यनिष्ठ और सुखद हो। हो ना हो।