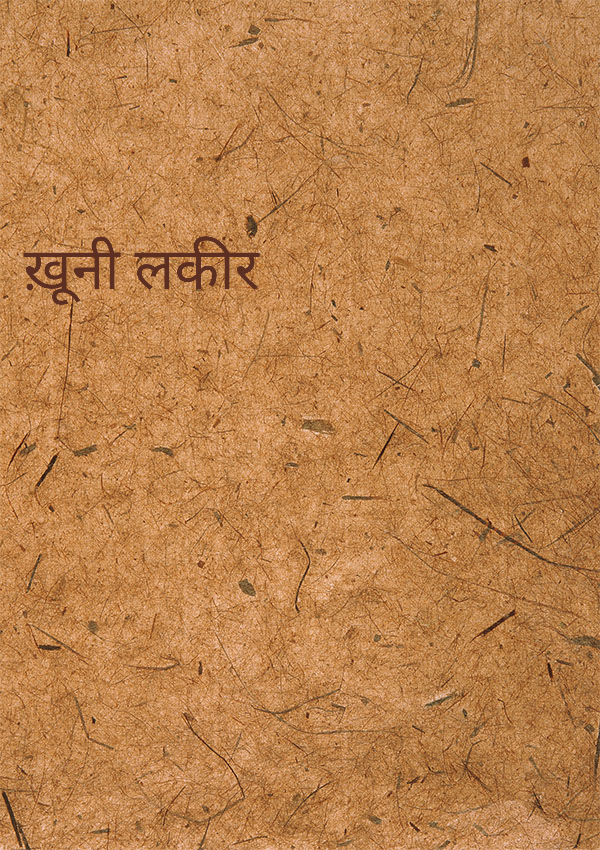ख़ूनी लकीर
ख़ूनी लकीर


इन्सानियत के दुश्मनों ने ये ठाना है,
भाई के हाथों भाई को मरवाना है।
कभी टूटता है मन्दिर तो कभी मस्जिद
गिरती है,
मक़सद तो बस इंसां को इंसां से
लड़वाना है।
याद है मुझे वो ख़ौफ़नाक मंज़र,
जब हर सिम्त मज़हबी अदावत का
था असर।
नफ़रत की आग में हज़ारों घर जल रहे थे,
बच्चे तलवारों के साए में पल रहे थे।
जो ख़ुदग़र्ज़ लोग थे इक़्तिदार में,
सब कुछ था उनके इख़्तियार में।
बस अपनी मर्ज़ी से लिख डाली तक़दीर,
हमारे दिलों पर खींच डाली एक ख़ूनी
लकीर।
मनहूस हवा चली, धर्म-ईमान सो गए,
रफ़ीक़ थे जो एक दूजे के, वोह रक़ीब
हो गए।
कुछ शैतान पैकर-ए-मौत बने घूम रहे थे,
इन्सानों को काट कर सुर्ख़ तलवारों को
चूम रहे थे।
बस यूँ ही बाँध के सामान कुछ इन्सान
घरों से निकल पड़े,
जान बचाने को एक अनजान मंज़िल
की ओर चल पड़े।
सोचा था कि कभी तो लौट के वापिस आएँगे,
यक़ीन न था कि उधर के होके रह जाएँगे।
शायद जहन्नुम से भी बढ़कर इब्रत्नाक
जहां था वो,
कैसे मान लूँ कि ईद और दीवाली का
हिन्दोस्तां था वो।
बरसात का पानी ज़मीं पे आके सुर्ख़ हो रहा था,
ऐसा लगा मानो आसमां ख़ून के आँसू रो रहा था।
लाशें ही लाशें हर तरफ़ बस लहू ही लहू,
आरज़ूएँ मर गईं थीं, बस जीने की थी जुस्तजू।
भूखे-प्यासे और रोते बिलखते बच्चे,
बीमार, तड़पते, मरते, बूढ़े माँ-बाप।
कुछ तो छूट गए थे हाथों से,
वो अब सम्भलेंगे अपने आप।
नाउम्मीदी का आलम ऐसा कि कुछ माँ-बाप ने,
अपने बच्चों को मौत के घाट उतार डाला।
इज़्ज़त न लुट जाए कहीं बेटियों की,
चुनांचे अपने हाथों से उन्हें मार डाला।
माओं की छातियाँ दरख़्तों पर लटक रहीं थीं,
उनकी सर कटी लाशें भी वहीं कहीं थीं।
किसी को प्यास ने मारा तो किसी को पानी में
मिले ज़हर ने,
किसी को तारीकी-ए-शब ने मारा तो किसी को
नूर-ए-सहर ने।
जानवरों से भी बद्तर हालत थी इंसा की,
क्योंकि जानवरों में लड़ाई नहीं थी
हिन्दू-मुसलमां की।
कुछ बह गए, कुछ ज़िन्दा रह गए,
कुछ मर गए, कुछ सरहद पार कर गए।
बहुत से यतीम हुए और बहुत से हुए बेऔलाद,
आज भी ख़ौफ़ज़दा कर देती है उस बेरहम
वक़्त की याद।
इतनी मुद्दत बाद भी वो अपने घर को याद
कर रोते हैं,
याद करके वो मंज़र जिस्म उनके
ज़र्द-ओ-सर्द होते हैं।
आज भी उनको ख़याल में क़त्ल-ओ-ग़ारत
होती दिखाई देती है,
ख़्वाब में आज भी उनको चीख़-ओ-पुकार
सुनाई देती है।
समझ न आए कि क्यों और कैसे जश्न मनाए
आज़ादी का,
वो आज़ादी ही बायस बनी थी हिन्दोस्तां की
बर्बादी का।
दिल रोता है जब सरसों के साग की
ख़ुशबू सरहद पार से आती है,
उधर से अपने ही नग्मों की आवाज़
आके दिल को तड़पाती है।
क्यों बन गई ये सरहद-ए-हिन्दोस्तान-ओ-पाकिस्तान,
जाने क्यों टुकड़े हुआ, क्यों बंट गया हिन्दोस्तान।
इस लकीर के सदक़े में लाखों सर हुए क़ुर्बान,
ज़ख़्मी हुआ ईमान और धर्म भी था लहू-लुहान।
हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान के झगड़े में,
नाहक़ ही मारे गए लाखों इन्सान।
ऐ अहल-ए-हिन्दोस्तां, ओ मेरे मोहसिन-ओ-मेहरबां!
पहले हिन्दोस्तानी हैं हम, बाद में हैं, हिन्दू, सिक्ख,
मुसलमां।
अब हमें इन्सानी ख़ून से लिखी तहरीर नहीं चाहिए,
हिन्दोस्तान की छाती पर एक और ख़ूनी लकीर
नहीं चाहिए।