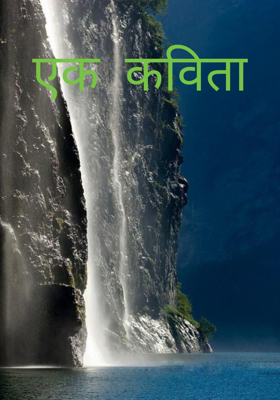दो रूहें
दो रूहें


कभी लगता है
जिस्म के भीतर,
दो रूहें बसी हैं संग-साथ।
एक बुझी हुई, राख सी ठंडी,
एक जलती है अब भी दीए की तरह।
पहली—
थक चुकी है, हार चुकी है,
ना कोई सपना, ना कोई आस।
पहाड़ों की ओर भाग जाना चाहती,
सबसे दूर, ख़ुद से भी उदास।
न कोई चेहरा उसे भाता,
न कोई रिश्तों का रंग।
बस मुक्ति की तलाश में भटकती,
मलंग, बिलकुल मलंग।
पर दूसरी—
अब भी धड़कती है उम्मीद में।
कहती है मुझसे—
“उठ यार!
अभी सांसों में आग बाकी है,
अभी जीवन में राग बाकी है।
भागना कायरों का काम है,
योद्धा हालातों से टकराते हैं।
पहाड़ तो हर किसी को बुलाते हैं,
मगर ज़मीन पर टिककर रहना,
यही असली वीर कहलाते हैं।
”
दो रूहें हैं मेरे अंदर,
एक बुझी हुई, एक उजली।
लड़ाई जारी है दोनों के बीच,
और शायद यही जंग है —
जो मुझे ज़िंदा रखती है।