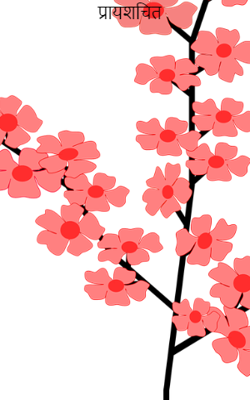पितृऋण
पितृऋण


'समय' अर्थात मैं, जाने कब से, शायद ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के भी पहले से, खानाबदोश की तरह एक युग से दूसरे युग तक स्वछन्द विचरता रहा हूँ । कितने ही ग्रह बने जहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई, उन्ही में से एक थी 'पृथ्वी' । इसी धरा पर अनगिनत वनस्पतियों व जीवधारियों का विकास हुआ । इन्ही जीवों में से एक जीव था 'मनुष्य' । वैसे तो मैं हर एक सजीव या निर्जीव सभी रचनाओं में अदृश्य तत्त्व की तरह विद्यमान हूँ लेकिन मनुष्य के प्रति मेरी विशेष अभिरुचि इसलिए है की उसने मेरे महत्त्व को समझकर मेरी ‘महत्ता’ को अपने ग्रंथों व शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया । मनुष्यों ने सर्वप्रथम खुद का विकास किया, फिर परस्परता व सापेक्षता के नियम का पालन करने के लिए समाज-व्यवहार बनाए । पुनः उसने मानव के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित धर्म, संस्कार का समाकलन किया । मैं, 'मनुष्य से मानव' व 'मानव से इंसान' बनने की श्रृंखला को, और फिर इंसानों के आदि व अंत को एक मूक दर्शक की तरह अपनी नंगी आँखों से देखता रहता हूँ । मैं देख रहा हूँ की विकास की दौड़ में वो अपने द्वारा व अपने लिए बनाये अनिवार्य कर्मो को कैसे भूलता जा रहा है तथापि उसके ऊपर चढ़ रहे ऋणों का हिसाब मुझे ही रखना पड़ता है । ये हर उस इंसान के लिए है जो विकास की राह में प्रतियोगी हैं, जिसे मै अपने समयकोष से निकाल कर एक छोटी सी घटना के रूप में तुम्हारे समक्ष परोस रहा हूँ ….
मुझे याद है जब नीरज का चयन झांसी के एक बड़े कॉलेज में हुआ था । प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर की वजह से उसे अच्छा कॉलेज मिला था । ये उसके लिए पहली बार था, जब वो किसी 'शहर' में पढ़ने के लिए जा रहा था । माँ ने थोड़ा-थोड़ा करके लगभग सबकुछ बाँध दिया था, आम का अचार, चबेना, 'सरताज' नमकीन, गुड़, सरसों का तेल, आटे का ठोकवा (मीठी कचौड़ी), ब्रश, साबुन, कंघी, चूरा, कच्चा चना, भुना हुआ चना, आदि । छोटी बहन 'रेखा' दौड़-दौड़ कर सामान लाये जा रही थी, और माँ झोले में भरे जा रहीं थीं । उन्हें अफ़सोस हो रहा था की निम्बू का अचार अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाया है । पिता 'रामसनेही' ने समझाया की वो बाकी सामान फिर कभी पहुंचा आएंगे, तब जाके उन्हें सांत्वना मिली, फिर भी जाकर एक बार शीशे की जार को हिला कर देखा, शायद कुछ अचार बन गए हों, माँ का दिल ही ऐसा है की जितना बाँध दो उतना कम ही है । रात भर की यात्रा के बाद सुबह रेलगाड़ी से उतर कर वे दोनों पैदल चलने लगे । नीरज के लिए सामान उठाना मुश्किल पड़ रहा था । " अरे ! चला जाएगा, कितना वजन है, ही"- ऐसा कहते हुए उसके पिता ने बीस-बाइस किलो का बोरा अपने कंधे व सिर के बीच टिका लिया । गर्मी अपनी चरम पे थी, सड़क चमक रही थी, ऐसा लग रहा था की कोलतार पिघल रही हो । कुत्ते भी किनारे कहीं पेड़ की छावं में , तो कहीं ट्रक के नीचे बैठे कर अपनी जीभ निकाले हांफ रहे थे । लगभग आधा मील पैदल चलने के बाद नीरज ने गौर किया की पिताजी का चेहरा काफी लाल हो गया है, पसीने की बूंदे कान के पीछे से निकलकर उनकी ठुड्डी से टपक रही थीं, और उसे भी काफी प्यास लग रही थी, सो नीरज ने थोड़ा रुक जाने को कहा । घर से दो लीटर की पानी की बोतल भर लाया था, लेकिन वो तो आज रेलगाड़ी से उतरते वक़्त ही ख़त्म हो गया था, आठ घंटे का सफर थोड़ा लम्बा था । वो और उसके पिता के बीच मित्रता का भाव अभी तक नहीं आया था, दोनों रिश्तों की अपनी-अपनी सीमाओं में बंधे थे । वो अपनी उम्र को कम समझता था इसलिए पिता की बातों को कभी काटता नहीं था, व पिता अपनी उम्र ज्यादा समझते थे इसलिए वो उसके ज्यादा करीब नहीं हो पाए थे । एक छोटी सी पान वाले की दूकान से उसने पंद्रह रूपए लीटर वाली पानी की बोतल खरीद ली । आदर दिखाते हुए पहले पिताजी को पीने के लिए कहा, पिता ने बोझा सिर से उतार कर नीचे रखते हुए, दोनों हाथों को पीछे कमर पे रख कर पीठ को ऐंठते हुए उसकी तरफ इशारा किया । वो गटागट करके पानी पीने लगा, प्यास ज्यादा लगी थी, आधी बोतल यूँ ख़तम हो गयी की पता नहीं चला । फिर पिताजी ने दो घूंट पीकर वापस उसे पकड़ा दिया । उन्होंने दो रूपए का पान खरीदा और चबाने लगे । केवल दो ही घूँट ! क्यों? ये उनका समझौता था अपनी जेब और अपनी प्यास के बीच में, ये उनका बलिदान था, खुद की प्यास का, अपने बच्चे की प्यास पर, छोटा सा ही सही । ये कोई नई बात नहीं थी । नीरज ने पहले तो कभी इसपे ध्यान भी नहीं दिया । ये सिलसिला तो कब से चलता आ रहा था । उसको लिम्का और फ्रूटी बहुत पसंद थे, वो जब भी पिता के साथ बाजार जाता, उसे ये सब दिला देते और अपने केवल पान चबाते रहते, उससे कहते की उन्हें पसंद नहीं, लेकिन नीरज उन्हें दूसरे की शादियों व बारातों में खूब जी भर के इन सब चीजों को पीते देखता । किसी के यहाँ द्वार करने जाते तो मिठाई से भरा पुरवा बचा कर घर लेते आते, सुबह की बासी रोटी अक्सर इन्ही के हिस्से में जाती, इनसे बच गयी तो माँ की थाली में । पके हुए आम के गूदे से नीरज का मन न भरता और ये गुठली चाट के संतोष कर लेते । भगोने के ऊपर के पके हुए चावल से नीरज का दोपहर का भोजन रख दिया जाता और नीचे के जले हुए चावलों से इन लोगों के दिन की शुरुवात होती । थाली में परोसी गयी लाइ-नमकीन (चबेना) में से उनकी मुट्ठी में लाइ ही ज्यादा आती, और नीरज की मुट्ठी में नमकीन के साथ मूंगफली भी , उनके आधे दूध के गिलास में नीरज को कभी भी मलाई नहीं दिखी, गर्मी में सिन्नी पंखे के सामने आगे नीरज सोता था, फिर माँ और फिर उसके पिताजी, ये लोग ऐसा क्यों करते थे ?.... खैर ।
नीरज को कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा मिल गया था, उसके पिता ने कमरे को व्यवस्थित करके नीरज को आस-पास का सारा बाजार, बैंक, ढाबा, जरूरत की सारी दुकाने, आदि दिखा दीं । हॉस्टल के वार्डन से भी व्यवहार बना लिया, फिर रात की गाडी पकड़ने के लिए निकलने लगे । नीरज को कुछ पैसे देते हुए समझाया की वो पैसे की चिंता न करे, समय-समय पे वो मनीआर्डर कर दिया करेंगे । अनजान शहर, ऊपर से माँ-बाप, घर-गाँव, यार-दोस्तों की यादें । पिता ने उसके चेहरे को देखा, उसके मन में उमड़ते भाव को चेहरे से पढ़कर, सांत्वना देने लगे-" हम भी आते रहेंगे, तुम भी एक-दो महीने में घर आते रहना, कितनी दूर है ही घर, पैसेंजर गाड़ी से रात को बैठो सुबह पहुँच जाओ, फ़ोन भी करते रहेंगे ।" उस रात न ही नीरज को नींद आयी, न ही रामसनेही को, माँ के लिए तो ये दूसरी रात थी । एक-एक कर ढेर सारी यादें नीरज के दिमाग में घूमने लगी थीं, सुबह-सुबह जल्दी उठ कर गाँव के पुराने पेड़ के गिरे हुए आम बीनने जाना, माँ का द्वार पे बैठ के रात की कढ़ाई और तवा माजना, पिताजी का दातुन चबाते हुए बुधनी (भैंस ) को चारा डालना, कुएं के ठन्डे पानी से नहाना, स्कूल में हिंदी के अध्यापक का पद्य-संकलन की एक-एक पंक्ति की व्याख्या करना, विशेष रूप से 'उधौ ! मोहे ब्रज बिसरत नाही' व 'काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी' जैसी पंक्तियों का, माँ के बनाये रोटी व अचार, स्कूल से मधुबन (दोस्त ) की साईकिल पर बैठ कर घर आना, मोती (कुत्ता) के पूंछ हिलाने पर उसको सहलाना ,छुपन-छुपाई व बीस-अमृत खेलना, दादी के साथ बाजार जाना, फ्रूटी पीना, शाम को दादा को चारो तरफ से घेर कर बैठना, उनका 'रघुपति राघव राजा राम' भजन सुनना, रात में पिताजी को दिखाने के लिए किताब खोल कर बैठ जाना, बिजली न रहने पर माँ का बेना ( हाथ का पंखा ) हिलाते हुए नींद आ जाना…, ये सब परसों की ही तो बातें हैं ,अब जाके दिमाग में गोल-गोल घूम रहीं थीं । नीरज को समझ नहीं आ रहा था की ये सपना है? या सोच? रात बीत रही है? या ठहर गयी है? वो गाँव में है? या कहीं और? लेकिन रामसनेही को पता था की वो गाडी में हैं, जब गाडी चलती तो सीट हिलती थी, हवाओं को चीरती हुई गाडी की आवाज खिड़की से आती रहती, जब ये स्टेशन पे रूकती तब भी 'चाय-चाय' व 'पान-मसाला-गुटका' की आवाज के साथ लोगों के कदमो की आवाजें भी आतीं । दूर गाँव में नीरज की माँ को भी कुछ आवाजें सुनाई देतीं जैसे, नीरज के खाना मांगने की, नीरज के झोला मांगने की, उसके सीढ़ी पे चढ़ने की, दोस्तों के साथ खेलने की, साईकिल चलाते समय गिर जाने की…, माँ घबरा कर उठ जाती । आस-पास देखती तो कोई नहीं है, सारा गाँव सन्न मार के सो रहा है, बोल रहे हैं तो केवल, पेड़ पर अपने बच्चों के पास बैठे उल्लू और खेत में अपने अण्डों के पास बैठी टिटिहरी । अगर हम संतोष के तराजू से तौले तो सबसे ज्यादा संतोष पिता के ही हिस्से में गया, बेटे से दूर होने का दुःख उन्हें भी था लेकिन इस बात की ख़ुशी ज्यादा थी की अब बेटे का भविष्य बन जाएगा । उससे कम संतोष, नीरज के हिस्से में आया क्योंकि उसे गाँव व उससे जुडी सभी चीजों से दूर होना पड़ा, सांत्वना बस इस बात की थी की वो पिता का नाम रौशन करेगा । लेकिन माँ का पलड़ा खाली था, किसी भी बात का कोई संतोष नहीं था क्योंकि ‘ममता’ बेटे को आँखों के सामने रखना चाहती है, उसकी भावना बेटे के भविष्य से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से जुडी होती है । ये रात थी, २ जून की । इस रात के बाद भी कई रातें आयीं । धीरे-धीरे कर के लोग अपने दुखों को भूलने लगे क्योंकि नयी बातें, पुरानी यादों के ऊपर अपनी परत जमाने लगीं । मेरा (समय) निरंतर बदलना ही मेरी प्रकृति है और यही मेरी वास्तविकता भी । लेकिन जिस वास्तविकता में तुम जी रहे हो, हो सकता है कल तुम्हे ये सब भ्रम लगे । शुरुआत में नीरज का मन नहीं लगता था, कभी-कभी तो उसका मन पिता के प्रति ही विद्रोही हो जाता, क्योंकि वो ही उसे गाँव से दूर शहर ले आये थे । लेकिन आगे चलकर नए दोस्तों की संगत ने पुराने दोस्तों को गाँव के कुएं के पास ही छोड़ दिया । गाँव के एक दूकान से पिताजी का कभी-कभी फोन आता, पीछे से माँ की आवाजें भी आती रहतीं, जिसमे वो सहेजतीं की पानी खूब पीते रहना, खाना में जो भी मिले खा लेना, आनाकानी न करना, पानी (बरसात) में भीगना मत, गीले कपडे मत पहनना, सिर पर तेल रख लिया करना, मफलर और टोपी (जाड़े में ) पहने रहना… आदि जबकि पिता पूछते की पढ़ाई कैसी चल रही है?, पैसा-वैसा चाहिए ? परीक्षा कब है? शुरू-शुरू में नीरज ने सोचा था की हर दो महीने में घर घूम आएगा, लेकिन फिर मन लगने लगा और पढ़ाई के चलते छह-छह महीने बीतने लगे । दिवाली पर घर आने की ख़ुशी थी, माँ ने लौकी के पौधे लगाए थे, उन्हें पता था की नीरज को लौकी का रायता बहुत पसंद है, बुधनी ने दूध देना बंद कर दिया था तो पड़ोस से दही लेकर माँ ने एक दिन पहले ही रायता बना कर रख दिया था । उसके आने से पहले मालपूआ भी तैयार था । छह महीने की ही बात थी, लेकिन ऐसा लगा की कोई वनवास काट के घर लौटा हो । इस बार जब नीरज ने पिता के पैरों को छुआ तो उनके आशीर्वाद में एक नया सा अभिमान झलक रहा था । गाँव से वो पहला था जो शहर केवल पढ़ाई के लिए गया था । वैसे तो लोग शहर जाते थे, लेकिन केवल काम ढूढ़ने । घर व दूकान को साफ़ करने में नीरज ने अपने पिता की मदद की, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा-थोड़ा समझने लगा था । पंद्रह साल पहले जब रामसनेही ने अपने दूकान की शुरुआत की तब थोड़े ही सामान थे, जैसे, ताम्बे के तार के एक-दो बण्डल, लकड़ी के चार-पांच स्विचबोर्ड, 'लक्ष्मी' व 'फिलिप्स' के बीस-तीस बल्ब व ट्यबलाइट, 'खेतान' व 'सिन्नी' के दो-चार पंखे, अमीटर, वोल्टमीटर, 'एवरेडी' व 'निप्पो' बैटरी की दो बण्डल, झालर के छोटे-छोटे बल्ब, ऊपर टंगे तार के कुछ बण्डल, पिलास, कुछ जले हुए मोटर, 'सीसम' लकड़ी का बनवाया हुआ एक मेज , एक ‘लंगड़ी’ कुर्सी जिसका एक पाँव नीचे से टूट गया था, उसके नीचे ईंट रख हुए थे, आदि । वो नीरज के दादा-दादी के अकेले बेटे थे, सो उन्होंने वहीँ गाँव में रहकर कुछ करना उचित समझा । उनकी मेहनत रंग लायी, आगे चलकर यही सब सामान चार-पांच गुने हो गए, उनके ग्राहक बढे और बाजार में लोग उन्हें उनके काम से जानने लगे । बेटे को शहर भेजा है पढ़ने के लिए, ये बात भी बहुत जल्द ही बाजार के लोगों में फैलने लगी । बाजार के लोगों से सम्बन्ध और भी अच्छे बनने लगे, वहीँ दूसरी तरफ गाँव के कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या-द्वेष की भावना घर करने लगी थी । 'रेखा' (छोटी बहन) की शादी में रामसनेही नीरज को बड़े गर्व से नए रिश्तेदारों से मिलवा रहे थे । बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है यह सुनकर लोग भी नीरज से मिलना चाहते थे । रेखा की शादी गाँव से छह मील दूर 'खमरिया' नाम के छोटे कस्बे में हुई थी । नीरज एक कुशाग्र बुद्धि का छात्र था, गाँव में वो सबसे तेज था, उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे लेकिन जब वो शहर में पढ़ रहा था, उसके अंदर 'कम नम्बर न आ जाएँ' ये डर बैठ गया क्योंकि वहां एक से बढ़कर एक धुरंधर थे । ये डर हर उस शख्श के अंदर मौजूद होता है जिसे सबसे आगे बढ़ने की चाह होती है, इसी के चलते कभी-कभी वो एकदम पीछे रह जाता है और फिर हतोत्साहित होकर गुमनाम हो जाता है । ऐसा ही कुछ नीरज के साथ भी हुआ, उसके नंबर अच्छे नहीं आये । उसमे एक ख़ास बात थी की वो अपने पिता से सब कुछ सच-सच बता देता था । ये बात भी उसने बताई, तो पिता ने उसे संभाला, उन्होंने सांत्वना दी की इस बार ना सही अगली बार फिर से मेहनत करना, ये सब तो चलता रहता है, वो मन दुखी न करे और माँ से बात कर ले । रामसनेही ने भी अपनी जिंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे थे, उन्हें अहसास था की ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती है, शहर की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है । नीरज को उनके अंदर एक 'दोस्त' दिखा, उसको थोड़ी ताकत सी मिली । अगली बार नीरज ने थोड़ी और मेहनत की तो परिणाम अच्छे निकले । भाग्य और कर्म से लड़ते हुए और दोनों को साथ लेकर नीरज ने अपने चार वर्ष की पढ़ाई पूरी की, हांलाकि उसकी डिग्री के अंक औसत ही आये । इन चार वर्षों में वो कितनी बार हतोत्साहित हुआ, लेकिन हर बार पिता ने एक नई आशा की किरण दिखाई । वो हमेशा से कहते की 'हमारे कर्म, हमारी कठनाइयों से बड़े हैं ।' रामसनेही का चरित्र कर्मप्रधान था, उन्हें भाग्य की परिभाषा जानने की जरूरत कभी नहीं पड़ी । जब भी नीरज घर जाता, दादी उससे अक्सर पूँछा करती थी कब नौकरी लगेगी? दादी के लिए जो भी शहर जाता, केवल कमाने ही जाता है । दादी को नहीं पता था की कोई पढ़ाई चार साल भी चल सकती है । दादा भी अपनी गंभीर मुस्कान से अपनी चेहरे की लकीरों को खींच देते । चार साल का अंतराल वैसे तो 'समय- कोष' के लिए नगण्य होता है लेकिन मनुष्य की जीवन-आयु के हिसाब से एक लम्बा वक़्त कह सकते हैं । इस अंतराल में नीरज को कई नए चेहरे दिखे, लेकिन दो पुराने चेहरे भूत से चलकर, वर्तमान की परतों में कहीं अदृश्य हो गए, पुनः वे कभी भविष्य में नहीं दिखे, उसके ‘दादा’ व ‘दादी’ । अब नीचे का कमरा खाली ही रहता है । जब कभी नीरज उस कमरे में जाता, एक सन्नाटा सा व्याप्त रहता । इंसान गुजर जाता है, रह जाती हैं तो अतीत की ओझल होती उसकी प्रतियां, कानो में विक्षोभ डालती उसकी कही हुई कुछ टूटी-फूटी बातें, और शांत कमरों में खाली पड़ी हुई उसके कपड़ों की खूंटी, दीवाल की खाली पड़ी आलमारी के एक कोने में सहूलियत से रखे उसके चश्मे, कोने में खड़ी हुई उसकी खटिया, किसी कोने में या दीवाल की नीचे वाली आलमारी में रखा उसका जंग लगा लोहे का बक्सा, और भी बहुत कुछ, ऐसा लगता है जैसे मेरी (समय) गति में विराम लग गया हो । लेकिन मुझे व जीवन दोनों को वरदान मिला हुआ है, निरंतर बढ़ते रहने का, किसी न किसी रूप में, और इसी कारण से उस शांत, एकांत कमरे में दीवाल-घडी की सूई की 'खट -खट' के साथ कुछ आवाजें निरंतर आती रहतीं, जैसे चूहों की कानाफूसी की, छिपकलियों के झगड़ों की, छछूंदर के दौड़ने की…।
पढ़ाई पूरी होने के बाद, नीरज काम की तलाश में अपने दोस्तों के साथ पुणे चला गया । पिता ने उसे एक फ़ोन खरीद के दिया था जिससे कभी-कभी वो घर के पास वाली दूकान के लैंडलाइन पे बात कर लेता, अनजान शहर है । वो और उसके तीन दोस्त एक किराए के कमरे में रहने लगे । उसके डिग्री के अंक कम थे, इसलिए नौकरी खोजने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी । उसके साथ आये दोस्तों की नौकरी कहीं न कहीं, कम या ज्यादा वेतन पर लग ही गयी । शुरुआत में उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उसके अंक कम थे, इससे उसके अंदर एक डर बैठने लगा । फिर इसी डर को लेकर जब बाद में वह साक्षात्कार के लिए गया तो हड़बड़ाहट में सटीक जवाब न दे पाया, और खाली हाथ में अपना बायोडाटा लेकर लौटना पड़ता । बरसात की दोपहर में, जबकि उसके सारे दोस्त अपने-अपने ऑफिस जाते, वो अकेला कमरे में बैठ कर खाली पड़े उनके बिस्तरों को निहारता । बरसात के तुरंत बाद की खामोशी को वो महसूस करता, पानी की बूंदे खिड़की की लकड़ी से कतार बनाकर सरकती हुईं टप से गिर जातीं, एक बूँद… 'टप', दूसरी बूँद… 'टप' । कमरे की उमस को वो अनुभव करता और मक्खियों की भनभनाहट सुनता । उसके दोस्त छुट्टी के दिन काफी खुश रहते, लेकिन उसके लिए क्या 'रविवार' और क्या 'सोमवार' । पिता को उसने सारी बातें बतायीं । रामसनेही ने उसे एक मित्र जैसा ही समझाया, उसे ढांढस बंधाया और फिर से एक बात कही 'हमारे कर्म, हमारी कठनाइयों से बड़े होते हैं ।' उसे अपने व रिश्तेदारों के कई उदाहरण भी दिए, जिससे नीरज को थोड़ी सांत्वना मिली । पैसा किसी न किसी के हाथों उसके पिता भिजवा देते । छह महीने लगे, कर्मों ने कठिनाईओं पर विजय पायी, जाड़ों की धूप के साथ उसकी किस्मत भी खिली । थोड़े कम वेतन पर उसे एक नौकरी मिल गयी । वो मन लगा कर काम करता क्योंकि उसके बीते हुए छह महीने बड़े गाढ़े थे । लोगों के लिए वो केवल छह महीने थे, लेकिन नीरज के लिए वो बीते …’ १८४ दिन’ थे । उसके कर्मो ने उसकी किस्मत को थोड़ा और तराशा, लगभग तीन महीने बाद ही उसे एक सरकारी नौकरी मिल गयी । उसके पिता बहुत खुश हुए, गाँव में सरकारी नौकरी का कुछ ख़ास ही रुतबा होता है, भले ही वो चपरासी की नौकरी हो या कलट्टर की । रामसनेही का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया, चेहरे पर एक अलग सा संतोष बना रहता, एक अलग सी मुस्कान बनी रहती, जिससे भी मिलते, बेटे की बात जरूर बीच में ले आते । उन्हें ऐसा लगता की उनकी वर्षों की मेहनत व इंतज़ार का फल, बेटे की नौकरी के रूप में उन्हें मिल रहा हो । आस-पास के लोगों की जलन पे मैंने (समय) जैसे घी छिड़क दिया हो । लेकिन अब वो इसकी चिंता नहीं करते थे । अबकी बार जब नीरज घर लौटा तो पिता के आशीर्वाद में उसने एक गर्व का अनुभव किया । नीरज ने अपनी पहली कमाई से पिता को एक फ़ोन खरीद कर दिया । अब सुगमता से बातें हो जाती थीं । वो चाहता था की पुराने गाँव के मित्र उससे पहले जैसा ही व्यवहार करें, लेकिन वो लोग नीरज से बात करने में हिचकिचाने लगे थे, उसे अब लोग 'शहरी-बाबू' कहते थे । वैसे तो उसे ये संज्ञा उसी समय दे दी गयी थी, जब वो पहली बार शहर पढ़ने गया था । लेकिन अब इस शब्द में ईर्ष्या का भी समावेश हो गया था । कुछ मित्र ऐसे भी थे जिन्हे संतोष था, और वो खुश थे की नीरज की जिंदगी संवर गयी । कॉलेज के तीसरे वर्ष में नीरज को किसी लड़की ‘प्रगति’ से प्यार हो गया था । धीरे-धीरे ये रिश्ता और भी मजबूत होता गया । वो इस रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में बदलना चाहते थे । मैं तो गवाह हूँ उन दोनों के पवित्र प्यार का जिसमे जरा भी खोट नहीं था । रचयिता ने पांच दृश्य तत्त्व मिटटी, आकाश, पवन, अग्नि व जल के अतिरिक्त कुछ अदृश्य तत्त्व भी बनाये जिनमे ममता, प्रेम व दया सर्वोपरि हैं । ये सभी तत्त्व, जीवधारियों को सामान रूप से परोस दिए गए हैं । हम जो भी कर्म करते हैं, इन दृश्य व अदृश्य तत्त्वों की मात्रा उन कर्मो में विद्यमान होती है, इसलिए ये प्रकृति के वरदान भी हैं । सभी जीव प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं, यही कारण है की वे इसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ये कार्य मौसम के अनुकूल ही निर्धारित किये गए थे । फिर धीरे-धीरे एक विशेष प्रकार के जीव 'मनुष्य' ने अपने-आप को विकसित करना शुरू किया, यद्यपि उसे ये प्रेरणा उसी प्रकृति से ही मिली, आगे चलकर उसने इसके विरोध में भी कार्य करने आरम्भ कर दिए । 'भेद' शब्द का रहस्य सर्वप्रथम मनुष्यों ने ही खोजा, हांलाकि ये पहले से ही व्याप्त था, जब से ‘सृष्टि’ का आरम्भ हुआ । फिर इस शब्द को नए तरीके से परिभाषित किया गया, और इसकी परिभाषा को मनुष्यों ने हर एक चीज पर लागू किया । इसी के फलस्वरूप धर्म, जाति, वर्ण, स्थान, रहन-सहन, जीवन-मरण, कर्म-विधान, पूजा-पाठ आदि जहाँ-कहीं भी वो कर सकता था, उसने प्रकृति के नियमो के विरोध में एक बार पुनः, 'भेद' के अंतर्गत सबको परिभाषित किया । आज इस समाज में फैली 'जाति' की भिन्नताएं इसी का परिणाम हैं । रामसनेही भी इसी समाज का एक हिस्सा थे, और इनके सुव्यस्थित समाज में जाति को लेकर असमानताएं व्याप्त थीं । लड़की समाज के हिसाब से नीच वर्ग की थी । इसी डर से नीरज ने अपने प्यार का जिक्र कभी नहीं किया । रेखा उन दोनों के प्रेम के बारे में जानती थी, लेकिन नीरज ने घर में बताने से यह कह कर मना कर दिया था की समय आने पर वो खुद ही बता देगा । लेकिन उसका अंतर्मन ये चाहता था की रेखा धीरे-धीरे करके ये बात माँ को इशारों में बताती रहे, जिससे एकाएक पहाड न टूटे, और माँ भी प्रगति को पसंद करने लगे । नौकरी लगने की वजह से, शादी के रिश्ते आने लगे थे । पहले तो नीरज बहाना बनाकर टालता रहा, फिर बाद में फ़ोन पर उसने अपनी माँ को सब-कुछ बता दिया । लड़की 'नीची' जाति की है, माँ-बाप दोनों ने ही नहीं माना । लेकिन धीरे-धीरे बेटे की ख़ुशी के लिए माँ मान गयी । पिता अभी भी बीच में पिस रहे थे, 'बेटे' की ख़ुशी व 'समाज' के भय के बीच । एक डर बैठा जा रहा था की आस-पड़ोस के लोग ऊँगली उठायंगे, बाजार के लोग क्या कहेंगे, फूफा, नाना, मौसा आदि रिश्तेदारों से कैसे नजरें मिलाएंगे । कई रिश्ते और कई रिश्तेदारों के सहयोग से एक सामाजिक व्यक्ति बचपन से जवानी, शादी-शुदा व फिर बुढ़ापा की ओर बढ़ता है, फलस्वरूप उसके लिए ये समाज और भावी रिश्तेदार एक अहम् भूमिका के रूप में उसके इर्द-गिर्द विद्यमान रहते हैं । कभी-कभी इन्ही लोगों के चलते उसे अपनी निजी खुशियों का गला घोटना भी पड़ सकता है । रामसनेही भी इन्ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे, वो अपनी निजी खुशियों को नजरअंदाज कर सकते थे लेकिन, अपने बेटे की ख़ुशी को कैसे ? उन्होंने नीरज को बहुत बार समझाने की कोशिश की, उस लड़की से भी फ़ोन पर बात की, लेकिन दोनों ने अपनी जिद पकड़ ली थी । उधर रामसनेही के जीजा ने साफ़ कह दिया था की अगर ये शादी हुई, तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे । अभी तक ये बात आस-पड़ोस तक नहीं पहुंची थी । उन्हें अपनी जग-हंसाई का भी भय था । कभी-कभी नीरज के अंदर अपने पिता के प्रति मूक विद्रोह भी फूट पड़ता, फ़ोन पर बात करते समय उसकी बातों में चिड़चिड़ाहट की झलक दिखती थी । मै (समय ) इस समाज से आस लगाए घूमता रहा , लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही रही । रामसनेही अक्सर अपने कुछ ख़ास मित्रों से इस दुविधा पर चर्चा किया करते । 'अगर', 'लेकिन', 'नहीं तो', 'क्यों', 'किन्तु-परन्तु' के अधीन रहकर 'समाज', 'रिश्ते', 'परिवार', 'मर्यादा' व 'खुशियों' का नाप-तौल करते-करते उनको एक साल बीत गए । 'हमारे कर्म, हमारी कठनाइयों से बड़े होते हैं ।' जो भी होगा उससे निपट लेंगे, 'इंसान' के लिए समाज बना है 'समाज' के लिए इंसान नहीं बना, लोगों ने समाज को गलत तरीके से परिभाषित किया है, ऐसी परकल्पनाओं व इसके परिणाम को समझते हुए उन्हें बेटे की ‘ख़ुशी’, अपने ‘डर’ से ज्यादा महत्त्वपूर्ण लगी । अंत में वो मान गए । लेकिन विधान का चक्र देखिये, प्रगति के घर वाले नहीं मान रहे थे । रामसनेही ने उन लोगों को बहुत समझाया, फ़ोन पे बात भी की, उनके घर जाकर उनसे निजी तौर से मिलना चाहा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया । प्रगति ने हर जतन किये उन्हें मनाने की, लेकिन अलग जाति में शादी के लिए वे राजी नहीं हुए । उसके पिता 'कुंजन' ने उसके सामने दो विकल्प रखे-वो नीरज को भूल जाए या अपने माता-पिता को । वो भी दुविधा में थी, एक तरफ भविष्य था तो दूसरी तरफ उसका अतीत । वैसे तो नीरज और प्रगति घर से भाग कर भी शादी कर सकते थे, लेकिन एक-दूसरे से वाद-विवाद करने के बाद प्रगति को ये अहसास हुआ की घर से दूर होकर शादी करना इतना भी आसान नहीं है-"पुराने रिश्तों का गला घोंट कर, क्या नए रिश्ते फूल-फल सकते हैं? माँ-बाप कितने भी गलत क्यों न हों, और हम कितने भी सही क्यों न हों, उनकी भावनाओं को ठेंस पहुंचाकर हम कितना और कबतक खुश रह पाएंगे? अपने बच्चे की वजह से आने वाली शर्मिंदगी का बोझ लेकर अकेले, माता-पिता किस-किस को जवाब देते फिरेंगे? इस समाज में रहने वाले परोपकारी लोग जिन्हे अपने घर की तकलीफों से ज्यादा चिंता पड़ोस की खुशियों से है, ऐसे लोग ऊँगली उठा-उठा कर रहना दूभर कर देंगे, और अगर ऐसे समय में कोई अपना, उनका साथ न दे तो फिर परिवार की परिभाषा ही क्या रह जायेगी? अपने वर्तमान को हँसते-हँसते बलिदान करने वाले माता-पिता को अपने स्वार्थी भविष्य के लिए रोता छोड़ देना क्या सही होगा? कभी अकेले में क्या मेरी आत्मा मुझसे सवाल नहीं करेगी? बाहरी दुनिया से तो मैं लड़ जाउंगी लेकिन, अपने अंदर की लड़ाई से कब तक लड़ूंगी?" ऐसे ही जाने कितने सवाल, बिना किसी जवाब के प्रश्नचिन्ह लगाते रहे । यह संघर्ष तो सदियों से चला आ रहा है, जब से समाज बना, केवल सन्दर्भ अलग होते हैं । हर समय किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी जगह पर यह अंतर्द्वंद चलता है । इसी के लिए कुछ लोग मर जाते हैं तो कुछ मार दिए जाते हैं । नीरज और प्रगति समझदार थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया । उन्होंने इस अध्याय को एक खूबसूरत शीर्षक देकर वहीँ समाप्त कर दिया । हांलाकि जिंदगी के ये पन्ने कभी-कभी स्मृति की हवाओं से अपने-आप ही पलट जाते और इन पन्नों पर लिखी प्रेम की अधूरी कहानी स्याही बनकर मस्तिष्क-पटल पर फ़ैल जाती । वो उस सुनहरे अतीत को याद कर थोड़ा हँस लेते और कभी-कभी थोड़ा…रो लेते । उस दौरान नीरज ने अपने पिता को 'उसकी' ख़ुशी के लिए खुद से, खुद के उसूलों से, पुराने रिश्तों से, समाज से और उन सभी से जो आड़े आ रहे थे, संघर्ष करते हुए देखा था, शायद इसी को 'पिता' कहते हैं ।
नीरज को छह महीने लगे, प्रगति की यादों को दिमाग के किसी एक कोने में संजो कर रखने में, उसकी बातों पे पूर्णविराम लगा कर उस, प्रसंग का पन्ना पलटने में । उसका मन भी अशांत रहा । आगे चलकर 'दिव्या' से उसका रिश्ता हो गया । नीरज ने पुराने फ्रेम में नई तस्वीरें लगाना ही उचित समझा, यद्यपि कभी-कभी वो यादें अचानक से उभर जातीं, लेकिन इसी को वक़्त का तगाजा समझ कर खुद को समझा लेता और 'प्रगति' के साथ गुजारे हुए वो पल खूबसूरत थे, लेकिन गुजरते हुए ये पल भी खूबसूरत हैं, ऐसा मानकर संतोष कर लेता । शादी से पहले दिव्या को उसने अपने अतीत के बारे में बताया था । वो भी एक समझदार लड़की थी और उन दोनों के त्याग व भावनाओं के मूल्य का आदर करती थी । उसने नीरज के पुराने घावों को कभी नहीं कुरेदा । नए रिश्ते की परत ने पुराने घावों को ढक दिया । नीरज की शादी में रामसनेही के साथ फूफा, चाचा, मौसा सभी ने हाथ उठा-उठा के नाचा । माँ के साथ चाची, मौसी व बुआ ने भी । सभी कुछ पूर्वनिर्धारित तरीके से निपट गया और मै भी अपनी पूर्वनिर्धारित चाल से दो गर्मी और आगे खिसक गया…।
रामसनेही ने दो कमरे का दूसरा मंजिल तैयार करवा लिया, अब नीरज के एक बेटा भी है,'अंशु' । पास-पड़ोस की जलन, जेठ की दूपहरी की तरह तप रही थी । लेकिन रामसनेही को क्या, उन्हें कौन सा हाथ सेंकना था । सरकारी नौकरी में नीरज का तबादला समय-समय पर होता रहा, कभी चंडीगढ़, कभी गुड़गावं । वो अपने परिवार को लेकर अलग-अलग जगहों पर किराए पे रहता रहा । परिवार? हाँ परिवार । पति, पत्नी व बच्चे का परिवार । परिवार की परिभाषा धीरे-धीरे कैसे बदल जाती है । माता-पिता का स्थान, नाती-पोते ले लेते हैं । यह संकल्पना एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी, दूसरी से तीसरी की ओर अग्रसर होती रहती है । ‘शब्द’ वही रहता है केवल समूह के व्यक्ति बदलते रहते हैं । जब भी नीरज व उसका परिवार गाँव से विदा होता, माँ भर-भर कर चीजें बांध देती जैसे, गुड़ के लड्डू, खांड, 'सरताज' नमकीन के पैकेट, रास्ते के लिए पूड़ी-सब्जी, लाइ, चूरा, देशी घी, सरसों का तेल, घर का चना, नीबू व आम का अचार,…। फिर भी उन्हें ये कमी लगी ही रहती की ये नहीं बाँध पायी, वो नहीं बाँध पायी । माँ अपने आंसू भी बाँध के रखती, जो की उनके चेहरे के हाव-भाव से साफ़ दिख जाता । जब वो सामान बांधती रहती तो केवल सामान के बारे में ही सोचती, लेकिन जब आखिरी गाँठ लगाती तो अचानक से बोल पड़ती-"देखो…! अब, कब आना होता है, विदेश जा रहे हो, यहीं कहीं नौकरी ढूंढ लो, छह महीने पे आते हो, हर महीना आया करो ।“ समझ में नहीं आता था की वो पूछती थी या, बताती थी । नीरज मुस्कुरा कर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं । माँ के लिए गाँव से बाहर जाना मतलब विदेश जाना, क्योंकि उनके लिए उनका गाँव ही एक देश था । माँ व पिताजी बस-स्टैंड तक छोड़ने आते, और जब तक बस उनकी आँखों से ओझल न हो जाती तब तक उसी सड़क की लम्बाई नापते रहते, शायद वो एक-दूसरे से नजरों की प्रतियोगिता करते की, पूरी तरह लुप्त होने से पहले किसको बेटे की बस दूर तक दिखी? रामसनेही हाथ-घडी देखते और बस ओझल होने में ‘कितना समय लगा’, ये याद कर लेते । जब दोनों लोगों के मत एक हो जाते, तब वो लौट जाते । हफ्ते में दो-तीन बार फ़ोन से बात हो जाती थी । पिता जब बात करते, माँ पीछे से सहेजती रहती की- "अंशु को स्वेटर पहनाये रखना (जाड़े में), लाल वाला टोपा कान तक ढका रहता है, पैर की तालू में सरसों के तेल से मालिश करना, नीरज को बोलो की मफलर बाँध के बाहर जाए, मसालेदार खाना कम खाना (गर्मी में), नीबू का शरबत पीये जाना, दूध दो बार गर्म करना नहीं तो फट जाएगा,…। कभी-कभी तो पिता अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाते और चिढ़कर माँ को फ़ोन दे देते । फिर माँ इन्ही सब निर्देशों को पुनः समझाती ।
विधाता ने मेरी आयु सीमा निर्धारित करते हुए मुझे 'ब्रह्माण्ड के अंत' तक विचरते रहने का वरदान दिया । लेकिन ये वरदान मेरे लिए एक 'अभिशाप' भी बन जाता है, जब मैं इस सृष्टि की सबसे बुद्धिमान रचना की 'आयु-क्षय' को देखता हूँ । इंसानों की आयु निश्चित होती है, 'खूबसूरत' बचपन से 'उर्जात्मक' जवानी तक चलते हुए और फिर 'कांपते' बुढ़ापे से ठिठुर कर चिर निद्रा में सोते हुए उन्हें बस… देखता रहता हूँ ।
नीरज के माता-पिता भी अब बूढ़े हो चले थे । वैसे तो, वो ये जानते थे की सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, और इसका वो गर्व भी करते थे लेकिन, एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब बाहर के रिश्ते-नाते, पास-पड़ोस के लोग, उनके यार-दोस्त सभी पराये लगने लगते हैं, केवल अपना खून ही 'अपना' लगता है, बुढ़ापा केवल उसी में अपनत्त्व को ढूंढता है, वो एक बड़े परिवार, बेटे-बहु, नाती-पोते, के साथ जीना चाहता है । उसके लिए बाहर की नौकरी छोटी लगने लगती है, फिर वो अन्य विकल्प भी ढूंढ़ने लगता है । माँ तो ऐसा पहले से ही चाहती थी, कभी-कभी तो कहती की वो जब मर-मरा जायँगी तब नीरज आएगा क्या? उसकी माँ ने दिव्या पर भी बल डाला की वो नीरज को समझाए । उन्हें उन लोगों की कमी खलती है । हो सके तो अंशु को ही गाँव में छोड़ दे । वो उसके बच्चे को पाल-पोस लेंगी, कम से कम अपने पोते में ही नीरज का बचपन देख लेंगी, वैसे भी दादी-दादा की जान उनके पोते-पोतियों में बसती है । लेकिन दिव्या 'अंशु' को लेकर बहुत संवेदनशील थी, उसका मानना था की बच्चे का पालन-पोषण माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता, आखिर माँ अपने खून को हमेशा अपनी आँखों के सामने ही रखना चाहती है, इसलिए वो इस बात से सहमत नहीं थी की अंशु, गाँव में रहे । रामसनेही में भी उम्र ढलते यही लक्षण दिखने लगे थे । जब भी फ़ोन करते बातों-बातों में कहते की “आ जाओ गाँव में वापस, यहीं दूकान खुलवा देंगे या किसी स्कूल मे अध्यापक की नौकरी कर लेना । खेती-बाड़ी में इतना होता है की साल भर खाने की कमी नहीं होगी ।“ नीरज भी सोचता था की, दस-पंद्रह साल और नौकरी कर ले, थोड़े पैसे कमा के बचा ले, फिर चलेंगे गाँव वापस । तनख्वाह का कुछ हिस्सा वो घर भेजता था, बाकी से शहर के खर्चे और बचत देखता, यद्यपि जो हिस्सा वो घर भेजता वो भी पिताजी संभाल कर बैंक में जमा कर देते, उसी के भविष्य के लिए । माता-पिता को 'कमाई' नहीं बल्कि 'कमानेवाला' चाहिए था । पिताजी की दूकान से ही उनके घर का खर्चा चल जाता । नीरज सोचता की अभी से गाँव जाकर क्या करेंगे, गाँव में रखा ही क्या है? सरकारी नौकरी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, कौन सी दूकान रख लेंगे, किराना की? या फिर कंप्यूटर की? आस-पास ढंग के कॉलेज तो छोडो, स्कूल भी नहीं, अध्यापक की नौकरी में कितना कमा लूंगा? खेती करके कितना ऊगा लूंगा? माना साल भर खाने की कमी नहीं होगी, लेकिन बस उतना ही पर्याप्त नहीं होगा, भविष्य में बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, उसके हॉस्टल की फीस, कॉलेज की फीस, उसकी शादी का खर्चा कहाँ से जुटा पाऊंगा? शहर की आबो-हवा अच्छी है, एक प्रतियोगिता है यहाँ, जिंदगी दौड़ती है, गाँव में जैसे सबकुछ रुक सा गया है, वहां जिंदगी सुस्त सी चलती रहती है । नीरज अंशु के भविष्य की भी चिंता करता था । वो सोचता था की बेटे की परवरिश गाँव की अपेक्षा शहर में अच्छी तरीके से होगी । यहाँ अच्छे व बड़े स्कूल हैं, अंग्रेजी माध्यम से अध्यापक पढ़ाते हैं, बड़े-बड़े पुस्तकालय हैं, अच्छे बच्चों की संगत मिलेगी तो प्रतियोगिता में मानसिक विकास होगा, ढेर सारे पार्क बने हुए हैं तो शारीरिक विकास भी होगा, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, नौकरी के लिए बड़ी-बड़ी कम्पनिया हैं, शिक्षित समाज में रहेंगे तो रहन-सहन के स्तर ऊँचे उठेंगे, आदि ऐसे बहुत से कोने थे जिसमे बेटे के भविष्य के लिए उसे शहर ही सही लगता था, और शायद रामसनेही को भी कहीं-न-कहीं यही ठीक लगता था । असल में नीरज के अंदर डर बैठ गया था, अपने भविष्य का डर । हम अपने वर्तमान से नहीं अपितु भविष्य को सोच कर डरते हैं । डर अपने पावँ जमाये तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है । गाँव के आदमी को शहर में रहने का डर है, शहर के आदमी को गाँव में रहने का डर है, पढाई में अच्छे अंक न लाने का डर है, उसके बाद नौकरी न मिलने का डर है, नौकरी मिल गयी तो फिर से छूट न जाए उसका डर है, नौकरी में ऊपर बैठे अधिकारियों का डर, प्रमोशन कैसे होगा उसका डर, फिर पनपते परिवार का डर, बच्चे के भविष्य का डर, आदि । असल में लोग पढ़-लिख कर जितना होनहार बनते हैं उतना ही डरपोक भी । पढ़ा-लिखा आदमी अपने ही शान में जीता है, वो अपना स्तर ही अलग समझता है, अपने दिमाग की बदौलत वो लोगों के कामो में भी अंतर देखने लगता है, ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है । नीरज की भी यही समस्या कभी-कभी गाँव में देखने को मिल जाती, जैसे, गोबर उठा के खेत में कैसे डालें? लोग हसेंगे, धान की फसल को सिर पे रख कर कैसे लाएं? लोग देखेंगे, हैंडपंप से पानी भरने रात को जाएंगे, लोग जानने न पाएं, आदि । पिताजी अकेले ही सब काम कर देते । चूँकि रेखा की ससुराल ज्यादा दूर नहीं थी, वो अपने बच्चों को लेकर आती-जाती रहती थी, जिससे दोनों लोगों का मन लगा रहता था । नीरज तो नहीं आया, हाँ लेकिन उसकी प्रकृति में थोड़ा बदलाव जरूर आया, जब दो साल बाद उसकी माँ अकस्मात् गुजर गयीं । यह बदलाव उसमे शमशान से लौटने के बाद से दिखाई पड़ने लगा था । इसे 'शमशान-वैराग' भी कह सकते हैं । ये कुछ दिन तक लोगों के दिमाग में घूमता है, और मन को वैरागी बना देता है, इस अवस्था में आदमी को हर उस नश्वर चीज, जैसे पैसा, जमीन, जायदाद, घर आदि से मोह छूट जाता है, सब कुछ पराया लगने लगता है, उसे केवल अंत ही अंत दिखाई देता है, पहले अपने परिजनों का, फिर हर उस जाने-पहचाने चेहरों का और अंत में खुद अपना । उसे ‘शरीर नश्वर है' की वास्तविकता समझ में आती है, इस अवस्था में न कोई शत्रु रह जाता है, न कोई मित्र, सब एक समान दिखने लगते हैं, कोई ऊंच-नीच नहीं , कोई जाती-धर्म नहीं । वैसे ये अवस्था केवल थोड़े ही समय तक रहती है, बाद में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है, फिर से वही ऊंच-नीच, जाती-धर्म, जमीन-जायदाद, अपने-पराये…।
पिताजी अब अकेले हो गए हैं उनकी बातों से अकेलेपन का सन्नाटा झलकता है, अब फ़ोन पर पीछे से माँ की आवाज नहीं आती, जाड़ा अभी भी वही है, गर्मी अभी भी वही है । पिताजी ही माँ की पुरानी कही हुई बातों को दोहरा देते । नीरज भी सोचता की पांच साल और नौकरी कर ले फिर वापस गाँव जाकर पिता के साथ रहेगा । कभी-कभी वो उनको अपने पास रहने के लिए बुलाता । एक-दो बार उन्होंने कोशिश की नीरज के साथ शहर जाकर रहने की, लेकिन वहां की आबो-हवा के अनुकूल नहीं हो पाए । वो सोचते जहाँ जीवन के ६२ साल बिता लिए, बाकी के कुछ साल भी वहीं बीते । अपने गाँव से एक अपनापन जुड़ा हुआ था, फिर वो गाँव की स्मृति में खो जाते । जहाँ उनका जन्म हुआ, पले-बड़े, दादी के लाड व दादा की फटकार से गुजरे, उन्हें आज भी अपना बचपन साइकिल की टायर के पीछे दौड़ता हुआ दिख जाता, उसी बचपन को बगल के पेड़ से आम चुराते हुए देखते, जेठ की दोपहर में कुएं के ठन्डे पानी की मिठास से उनकी आत्मा तर हो जाती, नहर में तैरते हुए जब थक जाते तो वहीँ किनारे बैठ के थकावट दूर करते, मैदान में कबड्डी खेलते हुए मिटटी से सन जाते, जब खेत की मेढ़ पर वो दौड़ते तो सरसों के फूलों का पीलापन उनके शरीर पर दिखता, जब उनकी भैंस अपनी रस्सी तोड़कर दूसरे के खेत में घुस जाती, और फिर खेत वाले लोग माँ से झगड़ा करने आते, माँ (नीरज की दादी ) खेत में रोटी और गुड़ ले आती, उनके पिता (नीरज के दादा ) दिनभर खेत में ही खटते थे । बरसात के दिनों में घर के दूआर से बहती पानी की एक पतली नाली से सरकते केंचुओं को उठाकर दोस्तों को डराते, वो मिटटी की भीनी-भीनी खुशबू, बारिश में प्लास्टिक की बोरी ओढ़कर स्कूल जाते, सूखे घोंघे को मुट्ठी में लेकर सिटी बजाते, पत्थरों की गोटी बनाकर खेलते…, कितनी ही यादें स्मृतियों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान थीं और माँ की आवाज, पिता की फटकार, कबड्डी का शोर, पम्पिंग-सेट की 'झर-झर', आटे की चक्की की 'पुक-पुक', सियार की ‘हूँहूँ’, पीपल की सूखी पत्तियों का 'पड़पड़ाना', भोर के मुर्गे की 'कुकड़ूं-कूं', भुट्टे की फसल से तोतों के पंखों का 'फटफटाना', कोयल के कटे आमों का पेड़ से 'भद्द' से गिरने की आवाज, अध्यापक के डंडे से पिटने की 'सट-सट', कुत्ते की 'भौं-भौं', चौथे पहर में चिड़ियों की 'चहचाहट', आदि कितनी ही ध्वनियाँ अभी भी कानो में कम्पन करतीं । वो शहर में पांच-छह दिन रुक कर गाँव वापस लौट आते ।
नीरज भी पिता के बुढ़ापे को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने कई बार कहा की वो अब दूकान बंद कर दें, उनकी आँखें भी कमजोर हो चुकी हैं । पिता के लिए दूकान ही एक मात्रा जरिया था, अपने बचे हुए दिनों को काटने का । वहीँ पे उनके बाजार के दोस्त आ जाते, फिर जहान-भर की बातें होती । कोई अपनी सुनाता, कोई दूसरों की सुनता । पहले तो रामसनेही ख़ुशी से फूले न समाते, क्योंकि बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, लेकिन उम्र ढलते उनकी बातों में वो ख़ुशी कहीं छिप सी गयी । लोग उनके दर्द को समझते, लेकिन कुरेदते नहीं । आस-पड़ोस के बच्चे वहीँ गाँव में रहकर कुछ न कुछ कर रहे थे, उन्हें देखकर ही संतोष कर लेते । यद्यपि कोई किराना की दूकान रखे हुए था, कोई देहाड़ी पे मजदूरी करता था, कोई चश्मे बनाता, तो कोई दूध ही बेच लेता, कोई टूशन से कमाता, तो कोई सफाईकर्मी था, कोई कपडे की दूकान पे बैठता तो कोई खाली ही बैठता । किसी न किसी तरीके से सभी के पेट पल रहे थे, और बच्चे भी बढ़ रहे थे । वो सभी गाँव में ही रहे, अपने 'पुराने' परिवार के साथ क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे ।
नीरज अपने परिवार के साथ जब-कभी गाँव आता, रेखा भी उन लोगों से मिलने आ जाती थी । तब रामसनेही को एक बड़े परिवार, बेटा-बहू, बेटी-दामाद, बच्चों के साथ समय गुजारने का मौका मिलता । लेकिन यह धूम-धाम केवल कुछ ही समय तक रहता, बाकी के सन्नाटे भरे दिन वो इन्हीं सजीव-स्मृतियों को बार-बार याद करते हुए बिताते थे । जब नीरज शहर जाने लगता पिता और बहन मिलकर उसका सामान सजाते क्योंकि अब, माँ नहीं थी । अब आम व निम्बू के अचार नहीं थे, फिर भी पिता से जो बन पड़ता बाजार से खरीद कर ला देते, कुछ चीजें उन्हें याद रहतीं कुछ बहन को । ऐसा लगता दोनों ‘माँ’ का अधूरा बचा काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हों । बस-स्टैंड पर जाकर पहले की ही भांति बस को ओझिल होने तक देखते, लेकिन अब कोई प्रतियोगिता नहीं होती और मत भी अब एक ही होता । धुंधलाती नजरों से बस जल्दी ही धूमिल हो जाती, वो हाथ-घडी की सुई टटोलते और वहां खड़े होकर ठीक उतना ही समय बिताते जितना, पहले बीतते थे । बुढ़ापे में पति-पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन अब तो पत्नी भी नहीं है इसीलिए रामसनेही के बूढ़े व एकाकीभरे दिन थोड़े ज्यादा ही गाढ़े ‘बीत रहे थे’ या गूढ़ शब्दों में कह लें तो, 'ठहर रहे थे' । तीसरे पैर का सहारा लेकर वो बत्तख की तरह चलते । नीरज के भेजे हुए पैसे को बैंक में जमा करने के लिए कांपते क़दमों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था, कभी-कभी तो वो लाइन में वहीँ जमीन पर बैठ जाते और खिसकते हुए आगे बढ़ते रहते । जब पौरुख जवाब देने लगा तो खेत अधिया पे उठवा दिया, खेत में जो कुछ उगता आधा उनको मिल जाता और आधा काम करने वाला ले जाता । जब तक पत्नी थी, चक्की पर गेहूँ पिसाने साथ में चली जाया करती लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होती, कभी गाँव के बच्चे टॉफी-बिस्कुट की लालच में उनके साथ चले जाते, तो कभी उनकी बेटी रेखा उनके साथ जाकर महीने भर का गेहूँ पिसवा लाती । जब नीरज गाँव आता तो उसे आटे के पीपे भरे ही मिलते क्योंकि रामसनेही पहले से ही ये काम कर लेते, वो सोचते की बेटा दो दिन के लिए आ रहा है, कहाँ गेहूँ के चक्कर में परेशान होगा । लाइट बिल जमा करने के लिए भी उन्हें जेठ की गर्मी में लू झेलनी पड़ती क्योंकि लाइन खुले आकाश के नीचे से शुरू होती । अब वो नीचे अपनी पत्नी के कमरे में ही रहते इसकी दो वजह थी, पत्नी की यादें, व अब उतनी ताकत नहीं थी की रोज एक-दो मंजिल चढ़ें-उतरें । खाना बनाने के लिए गोबर के 'उपलों' का उपयोग करते, इसकी भी दो वजह थी, पहली ये की गैस-सिलिंडर ऊपर वाली रसोई में रखा था, दूसरा, अगर गैस ख़त्म हो जाएगा तो कौन भराएगा? कभी-कभी बाटी-चोखा खाने का मन होता तो गाँव के बच्चों को बुला लेते । बच्चे भी रामसनेही को घेरा बना कर बैठते, उनके लिए तो ये त्यौहार जैसा ही लगता । फिर कहानी सुनाते हुए बैगन, आलू, भूंजते, आटे की लोई बनाकर सुलगती हुई उपलि पर रख देते, कुछ जल जाते तो कुछ कच्चे रह जाते । कोई बच्चा आधी बाटी खाता तो कोई दो । इसीतरह वो चूल्हे पर खिचड़ी भी बनाते । जब तक उनकी पत्नी जिन्दा रहीं, उपल तैयार कर देती थीं और मरने से पहले ढेर सारा बना कर गयीं थीं जो काफी दिनों तक चला भी । बाद में उपल बनाने के लिए रामसनेही गोबर को एक टीन पर पतला-पतला फैला देते, चार-पांच दिनों में जब ये सूख जाती तो इसे ही उपल की तरह उपयोग करते । हिम्मत जवाब देने लगी थी सो हर महीने मिटटी के तेल के लिए बाजार जाना भी बंद कर दिया था, कौन राशन-कार्ड लेकर एक-घंटे भीड़ में खड़ा रहे । गर्मी में धीरे-धीरे खटिया बाहर खिसकाते । कभी-कभी रात भर खांसने की आवाज आती रहती । खांसते हुए वो उठ कर बैठ जाते । मोती (कुत्ता) का बच्चा 'कल्लू' का छोटा बच्चा 'जग्गा' जो उनके खटिये के नीचे ही सोता था, कान खड़े कर पूंछ हिलाने लगता । वहीँ बगल में बलगम थूक कर लोटे से एक घूँट पानी पीते 'हे राम' कह कर फिर लेट जाते । बरसात के दिनों में जब छत पे पानी भर जाता तो कांपते पैरो से कैसे भी करके वो दूसरी मंजिल तक चढ़ते, झाड़ू से खींच-खींच कर छत को साफ़ कर दिया करते । अब उन्होंने दूकान जाना भी बहुत कम कर दिया था, उनके बाजार के मित्र वहीँ घर पे मिलने आ जाते थे । वैसे तो नीरज का फ़ोन हर दो-तीन दिन में आ जाता, लेकिन इसके अलावा जब कभी उन्हें बात करने का मन करता, किसी बच्चे को बुला कर नीरज के नंबर पे फ़ोन लगवा लेते, क्योंकि धुँधलातीं नजरों से नंबर खोजना मुश्किल जान पड़ता । कभी कुएं व कभी हैंडपंप पे नहाते, लेकिन दोनों ही जगहों में पानी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती । नीरज अक्सर उनको कहता की खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लें, लेकिन वो मना कर देते । रेखा महीने में दो बार आ जाती थी, बाकी कभी खिचड़ी, कभी बाटी-चोखा, कभी दाल-चावल खुद ही बना लेते । पास-पड़ोस के लोगों को उनपर तरस आता, ईर्ष्या छोड़ वे लोग ही उनकी मदद कर दिया करते । जब वो बीमार पड़ते उन्हें दवाएं दे देते, सर्दी में शाम को काढ़ा दे देते । बातों-बातों में वे लोग नीरज को कोसते लेकिन रामसनेही यह कह कर टाल देते की नीरज चार-पांच सालों में हमेशा के लिए यहीं रहने आ रहा है, थोड़े समय की ही बात है, वो नीरज की मजबूरियों को भी समझते थे और यह भी मानते थे की शहर में उन लोगों का विकास ज्यादा होगा । रामसनेही के पास ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बेटा शहर में अच्छा कमा-खा रहा है, जब वो गाँव वापस लौट के आएगा तो घर व खेत की देखभाल कर लेगा लेकिन कुछ इच्छाएं थीं जो मरीं जा रहीं थीं और इन्ही के चलते वो दिन-प्रतिदिन कमजोर हो रहे थे । वो ये भी मानते थे की अगर नीरज उनके बुढ़ापे के दिनों में साथ होता तो रोज के छोटे-छोटे काम आसानी से हो जाते, आस-पास के लोगों की दया का पात्र न बनना पड़ता,
चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदुमात्रं विशेषता। सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता॥
अर्थात, चिता और चिंता समान कही गयी हैं पर चिंता में एक बिंदु की विशेषता है, चिता तो मरे हुए को ही जलाती है पर चिंता जीवित व्यक्ति को ।
एक रात रामसनेही अपनी माँ के कमरे (नीचे वाले घर) के बाहर खाट बिछा के सो रहे थे । खाट की आधी टूटी हुई सुतलियाँ झूलते हुए जमीन को निहार रहीं थीं, मेढकों के टर्राने की आवाजें आ रही थी, झींगुर भी जगे हुए थे । मघा-नक्षत्र की बूंदे गिरी तो मिटटी अपनी सोंधी-सोंधी खुशबू उनके खाट के चारो ओर बिखेरने लगी । रामसनेही के जर्जर मन व बूढ़े शरीर ने बादलों की ठंडक ओढ़ ली, उनके प्राण-पखेरू अनंत आकाश में समय-यात्रा करने उड़ चले …। सुबह लोगों ने फ़ोन करके नीरज को यह खबर दी ।
मैं, उनके निस्तेज पड़े शरीर को, घडी की सुइयों के बीच अवाक बैठा देखता रहा । वो अगले चार साल बेटे का इंतज़ार नहीं कर पाए, लेकिन एक मैं हूँ जो, अपने वरदान और 'अभिशाप' स्वरूप तीस साल आगे खिसक गया…
मै तो समय हूँ, बोल नहीं सकता क्योंकि मै गूँगा हूँ, मै केवल देख सकता हूँ, तुम्हारे किये हुए कर्मो का लेखा-जोखा मै अपनी पीठ पर लादे खिसकता रहता हूँ, एक नियत चाल से । मेरा भूत भी निर्धारित था और मेरा वर्तमान भी निर्धारित है, लेकिन भविष्य के लिए मै तुम्हारी ओर एक आस से देखता रहता हूँ, तुम्हारे ऊपर चढ़ते हुए ऋण को मै नहीं उतार सकता क्योंकि मै अपंग भी हूँ, मुझे ऐसा वरदान नहीं मिला, नहीं तो मै नियति को ही बदल देता और अपनेआप को रामसनेही की मृत्यु से पहले ही पांच साल आगे खिसका देता,
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ।
अर्थात, पिता प्रसन्न हो तो सब देव प्रसन्न होते हैं ।
जब मेरी उत्पत्ति हुई, मुझे एक शाप मिला था, 'जड़त्व' का शाप । मैं स्थिर नहीं हूँ लेकिन मेरे कर्म में ‘जड़त्व’ है । मैं सब-कुछ देखते हुए, सब-कुछ समझ सकता हूँ लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कुछ कर नहीं सकता । रचयिता ने मेरे कर्मो को भी निर्धारित किया है इसलिए मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मैं किसी को फल नहीं दे सकता, केवल तुम्हारे किये हुए भूत के कर्मो को यादों, घटना या किसी न किसी रूप में वर्तमान में तुम्हारे सामने परोसता रहता हूँ ।
आपको याद होगा जब नीरज पहली बार 'झाँसी' गया था, वो २ जून था । आज भी २ जून है। दो जून की रोटी कमाना कितना मुश्किल है ये तो आपने सुना होगा लेकिन दो जून का संतोष पाने के लिए भी वर्षों बीत जाते हैं, ये अंदाज़ा आप नीरज को देख कर लगा सकते हैं । वो बैठा हुआ है अपनी बढ़ती उम्र या अप्रत्यक्ष रूप से 'घटती हुई उम्र' के बचे हुए भार को उठाये । बेटे 'अंशु' व बिटिया 'राधा' की शादी के जिम्मेदारियों से गुजर कर, बुढ़ापे की नसों को टटोलते हुए उसी लंगड़ी कुर्सी पर, जिसपे उसके पिता 'रामसनेही' अपनी दूकान में बैठा करते थे । बेटा 'अंशु' व बहू 'प्रिया', यूरोप (विदेश) में नौकरी कर रहे हैं, उनका अपना छोटा सा परिवार है । नीरज ने कई बार अंशु को अपने देश वापस बुलाया, यहाँ भी कमाई हो सकती है, लेकिन उसको विदेश की आबो-हवा ज्यादा अनुकूल लगी, हांलाकि उसने कोई वादा नहीं किया की वो वापस आएगा, लेकिन उसे भी नीरज के बुढ़ापे की ‘चिंता’ है…।
रामसनेही के देहांत के बाद नीरज कई बार गाँव वापस आया, अपनी वसीयत, घर, खेत व भैंसों को बेचकर हमेशा के लिए, इंदौर में बसने के लिए । इंदौर में उसका आखिरी तबादला हुआ था । लेकिन सही खरीदार न मिलने की वजह से उसने घर व खेत किराए पर उठवा दिए थे । साल में दो बार गाँव जाकर हाल-समाचार ले आता । वहीँ किसी दिन दादी के कमरे में, पिताजी के चश्मे वाले डिब्बे में एक चिट्ठी मिली थी । उसमे केवल एक ही वाक्य लिखा था- 'हमारे कर्म, हमारी कठनाइयों से बड़े होते हैं ।'
रामसनेही को पता था की नीरज बहुत जल्दी हत्तोत्साहित हो जाता है, वो अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरीके से समझते थे, इसीलिए वसीयत में वो चिट्ठी भी उसी के लिए छोड़ गए थे, ऐसा नीरज का मानना था । लेकिन मेरा मानना है की ये पंक्ति उन्होंने खुद के लिए लिखी थी, अपने-आप को सांत्वना देने के लिए, उस मजबूरीभरे, अकेलेपन में अपने कांपते हाथों से । नीरज के लिए तो वो कुछ साल ही थे, लेकिन रामसनेही के लिए अनगिनत दिन और एक-एक दिन में ठहरते आठ-आठ पहर थे …।
अंशु को फ़ोन पर नीरज समझाता- "यूरोप में ठण्ड होगी, जैकेट, टोपी व दस्ताना पहने रहना ।" और उसे देश वापस लौटने के लिए कहता जबकि नीरज का अंतर्मन यह भी जानता था की अंशु…नहीं आएगा । क्योंकि ऐसा ही उसने भी अपने पिता के साथ किया था । मै (समय) उसके भूत को वर्तमान बना कर उसे कुछ याद दिलाना चाहता हूँ । मनुष्य के ऊपर आने वाले तीन ऋणों की व्याख्या ग्रंथों में की गयी है- 'देव-ऋण', 'ऋषि-ऋण' व 'पितृ-ऋण' । कहीं-कहीं पर ब्रहमा के ऋण का उल्लेख भी मिलता है । पितृ ऋण कई तरह का होता है। कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, मां का, पत्नी का, आदि । नीरज के ऊपर भी यही ऋण है, 'पितृऋण' । वैसे तो उसने पितृपक्ष में कर्म-काण्ड, पूजा-पाठ करके सामाजिक रूप से अपने दोषों का निवारण कर लिया था लेकिन, जो दोष व ऋण मानसिक रूप से चढ़े हैं उसका निवारण उसका बेटा 'अंशु' ही करेगा । शास्त्रों में लिखा है की 'पुत्र-प्राप्ति' के बाद पितृऋण से मुक्ति मिल जाती है । नीरज के लिए ये व्याख्या एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि रामसनेही की भावनाओ की मूल्यता व उनके एकाकीपन की करुण व्यथा का अदृश्य व अप्रत्यक्ष ऋण जो नीरज के ऊपर चढ़ा है, जिसे नीरज व मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं देख सकता, उसे उतारने या फिर उसकी व्याख्या करने के लिए नीरज को ‘अंशु’ के रूप में संतान-प्राप्ति हुई थी । उस अहसास को उसे समझना जरूरी है, तभी वो मुक्त हो पायेगा । वो इस गूढ़ रहस्य को अब भली-भांति समझ भी रहा है, इसलिए वो इंदौर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वापस गाँव लौट आया है । उसने एक भैंस भी खरीद ली है, उसी की देख-रेख करता, अपने खेतों को पिता समझकर सेवा करता, बचपन के यार-दोस्तों के साथ बैठकर शाम की चौपाल, आदि में अपना मन लगाता है, पास-पड़ोस के बच्चों को 'रघुपति राघव राजा राम' सुनाता है । जब मन थोड़ा अशांत हो जाता है तो दादी वाले कमरे में जाकर रखी हुई पुरानी चीजों व बासी यादों से अपने मन को तर कर लेता । वैसे तो घर काफी बड़ा है, जिनमे ५-६ कमरे और एक बड़ा सा दालान है और कमरों में उसकी पत्नी के अलावा, १७-१८ दीवालें, ६-७ खिड़कियाँ, ५-६ दरवाजें व ४-५ रोशनदान ही रहते हैं। इन्ही से वो बातें करता है । आज भी वो यही कर रहा है । वो बैठा हुआ है अपने पिता की लंगड़ी कुर्सी पर जिसके कील अब ढीले हो चुके हैं, दादी के कमरे की चौखट के पास । बगल में उसके पिता की टूटी बद्धि वाली चप्पल पड़ी है, दीवाल की आलमारी में दादा के चश्मों के बगल में पिता का मोबाइल, उनका चश्मा, चश्मे के डिब्बे में वो चिट्ठी, उनकी सुई वाली घडी, खूँटी पर टंगा 'कपडे की चक्ति' लगा हुआ छाता, उनका दाढ़ी बनाने वाला सामान, दूकान के जंग लगे हुए सामानों का बण्डल, उनकी बूढी साइकिल, आदि सभी-कुछ संभाल कर रखे हुए हैं । दीवाल-घडी की सूई की 'खट -खट' के साथ चूहों की आवाजें आती रहती है, छिपकलियां एक दूसरे के पीछे दौड़ रहीं है, मक्खी भनभनाते हुए नीरज के कंधे पर बैठ जाती, बारिश होने के बाद की शान्ति है, बूंदे छज्जे से सरकती हुई ‘टप-टप’ गिर रहीं हैं, केंचुए मिटटी में रेखाए बनाते हुए प्रतियोगिता कर रहे हैं, नीम के पेड़ पर बगुले अपने बच्चों के साथ घोसले में बैठे हुए हैं, पेड़ के उल्लू अपने भीगे हुए पंखों को सुखाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, जग्गा (कुत्ता) अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, भीनी-भीनी खुशबू, ठंडक का अहसास करा रही है और नीरज का गुजरता बुढ़ापा….रामसनेही के गुजरे हुए एकाकीपन का ….
कालः पचति भूतानि कालः संहरते तथा ।
कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥