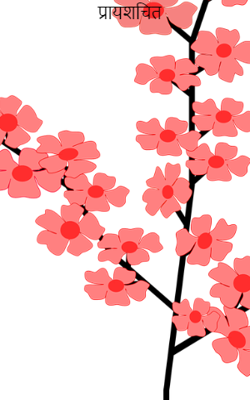जड़ें
जड़ें


‘रुक नहीं सकती नग़मा ? आज रुक जाओ। मुझे भी कुछ तुम्हारी तरफ़ का काम है। कल साथ चली चलूँगी। मेरा काम भी निबटवा देना......वही.....अंगूठियाँ बनवाने का।’
मैं अभी-अभी विदेश से पांच वर्ष बिताकर लौटी थी। पिछली कड़ियाँ मिलाने की कोशिश के तहत ही इस दिन नग़मा को सपरिवार घर बुलाया था। अभी तो बीते वक़्त की खाइयाँ भरी भी न थीं कि जाने का वक़्त हो गया था तभी तो रुकने का इसरार किया था। सुझाव सबको सूट कर गया और नग़मा रुक गयी।
नग़मा मेरी मित्र थी....ऐसी मित्रता, जिसे समय और परिस्थितियाँ खण्डहर नहीं बनातीं। एम.ए. से चली आ रही मित्रता की कड़ियाँ परत-दर-परत गाढ़ा व पक्की हो गयी थीं, इतनी पक्की कि वक़्त के अन्तराल व दूरियों जड़ें से भी बेअसर थीं। ऐसी दोस्तियाँ जंग न पकड़ पाती हैं। मिलें न मिलें, ज़ेहन के किसी कोने में दोस्त होने का सुरक्षा कवच थामे रहतीं। सालों बाद अचानक फ़ोन की बातचीत से ही दोनों एक-दूसरे से बँध जाते-
‘एक बेटी.....प्यारी...गुदगुदी....रुई के गाले-सी....की माँ बन गयी’....फिर फ़ोन पर ही-
‘बिटिया तीन बरस की हो गयी है....तेरी तरह बातूनी है।’
और.....
‘बेटे के जन्म’ की ख़बर भी ढेर-सी बधाइयों के साथ फ़ोन पर ही मिल गयी थी।
बस! यह थी कुछ फ़ोन पर की बातचीत। मानों फ़ोन न हुआ, आकाशवाणी समाचार हो गया। फिर एक दिन अचानक नग़मा की बिटिया ‘सबा’ के विवाह का कार्ड मिला, तब मुलाकात हुई।
‘हाय! नग़मा! कितनी मुटा गयी है....हूँ....लगती है एक भारी-भरकम सास....’ विवाह के रस्मों-रिवाजों तथा मेहमानों की देखभाल में फंस नग़मा ‘आओ’। बैठो....कैसी हो....खाना खाया....दूल्हा कैसा है....अच्छा! ये हैं साहिल और सना....इतने बड़े हो गये। जानते हो मुझे ? मैं तुम्हारी ख़ाला हूँ.....पर ये क्या जानें ?’
वे ख़ुद ही से बात करते-करते जैसे किसी और मेहमान की अग़वानी करने चली गयी। फिर मिली तो बेटे के निकाह के मौके पर और सामान्य बातचीत के बाद,
‘अब बनी असली सास! दामाद तो अपने घर में रहता है, हर रोज़ की टकराहट ही नहीं.....पर बच्चू! अब बहू आई है। रोज़-रोज़ का साथ-टकराव और झांय-झांय के पूरे मौके सारे खिड़कियाँ, झरोखों, कोनों-कुचीलों के साथ खुले पड़े होंगे।’
‘देखते हैं....कन्धे झटका दिये थे उसने।
वक़्त बीता......पता ही न चला। बच्चे जब छोटे होते हैं तब वक़्त का पता ही कहाँ चलता है। समय धावक गति से निकल गया। न नग़मा को पता चला न मुझे। वह तो दादी-नानी बनकर निश्चिन्त भाव से अपने घुटनों की जकड़न, ब्लड प्रेशर की मारा-मारी, पति के स्वास्थ्य की अनेक चिन्ताओं में डूबतह-उतरा रही थी और मैं.........बच्चों को विदेशों में मिली बड़ी-बड़ी नौकरियों की मजबूरी से विदेश भेजकर अपने अकेलेपन को झेल रही थी। बच्चों के होने का मनोविज्ञान भी अजीब है। होते हैं-तो उनकी बढ़ती मांगों, आलोचनाओं गड़बड़ झालों, कभी काम न करने का तनाव, कभी काम न होने की स्थिति पर झंुझलाती रहती, पर न होने पर घर काटने को दौड़ता। उनकी मांग ही न होती, तो रसोईघर सूना पड़ा रहता। घर ज्यों का त्यों पड़ा रहता। न बिखरना, न संभालना, न सब्ज़ी लाने की भाग-दौड़, न बनाने का ताम-झाम। धूल-मिट्टी तलक घर में घुसने का साहस न करती। विदेश से आकर तो यह अकेलापन और सालने लगा था, तभी नग़मा को मयपरिवार बुलाया और फिर रोक लिया था।
प्रोग्राम के अनुसार अगले दिन नाश्ता वगैरह निपटा कर निकल पड़े।
‘कहाँ जाने का है ?
‘मालीवाड़ा’
‘ये कौन-सा बाड़ा है। क्या यहाँ कभी माली रहते थे ?’
‘ये तो नहीं पता। पर इतना ज़रूर पता है कि इन दो-चार फीट की गलियों में अब तो कोई बाग़-बाग़ीचा नहीं बन सकता, जो माली की ज़रूरत महसूस हो। पहले चाहें रहा हो कभी।’
नग़मा ने ऐसे कहा जैसे इतिहास की विशेषज्ञ हों।
अचानक पुरानी दिल्ली का दौरा किया जाये वाला भाव ज़ोर मारने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही ‘दिल्ली-एक शहर’ नामक किताब ‘पुस्तक मेले’ में देखी थी। आज उसे ख़रीद कर पढ़ने का मन हुआ। दिल्ली की गलियों की यात्रा कितनी दिलचस्प होगी, सोचकर एक अजीब-सी ख़ुशी मिली। यह सोचकर दुख भी हुआ कि अब न तो पैरों में दम है, न ही शरीर में ख़म। चलना कैसे होगा, पता नहीं दिल्ली की ये गलियाँ मेरी नज़र में उतर पायेंगी-का प्रश्न बड़ा होकर सामने था। मन में कुछ निराशा थी, पर कुछ आशा भी जागी क्योंकि प्रोग्रामा मालीवाड़े का ही था।
थोड़ा-सा रुक कर नग़मा बोली-
‘अब तुम किस-किस के बारे में जानने का इसरार करोगी और मैं किसके बारे में बता पाऊँगी। यहाँ तो हर गली में एक कूूचा और कूचे में एक कटरा है। गली-कूचा शब्द शायद बना ही ऐसे है। सोच भी सकता है कोई कि एक-एक कटरे में हज़ारों दुकानें हैं और उनमें करोड़ों का माल भरा पड़ा है.......साड़ियाँ, गरम कपड़े, टेरीकाट, गोटाज़री, ख़मख़ाब, ज़रदोज़ी, साज-सज्जा के सामान, मसाले तरहं-तरहं के....एक अजब कसीदाकारी-सी...यह पुरानी दिल्ली की गलियाँ-कूचे नहीं हैं सिर्फ़......ये तो एक इतिहास, भूगोल, एक अजायबघर हैं। ये तो कदमों के नक़्श हैं....हर नक़्श की एक कहानी है...एक गाथा......बहुत लम्बी-चैड़ी-गहरी।’
नग़मा ऐसे बोल रही थी मानों वह गाइड हो, जो दिल्ली की पुरानी इमारतों को पूरे कथा-साहित्य के साथ दिखा रहा हो। ‘अब देखिये मेम साहब! ये हैं मुग़ल कसीदाकारी का नमूना। दूर से देखो तो कढ़ाई लगे, पास आओ तो क़ुरान की आयतें.....इधर आइये, ये देखिये लाल क़िला....वो दिल्ली-दरवाज़े पर लगे दो हाथी देख रहे हैं। पहले यहाँ दो राजपूत बहादुरों की मूर्तियाँ थीं-जयमल और फ़त्ताह, जो दो हाथियों पर सवार थे, जिन्हें औरंगज़ेब ने तोड़ दिया था। बाद में ये केवल हाथी बनाये गये और ये है नौबत ख़ाना। यहाँ शाही बैण्ड बजा करता था। इतवार, सूरज का दिन और शनिवार (राजा के जन्मदिन)....आदि जाने कितने क़िस्से।
नग़मा ने भी एक अद् द गाईड का फ़र्ज़ निभाया था।
नई सड़क के बाहर स्कूटर वाले ने छोड़ दिया था। अन्दर तक, ले जाने की न जगह थी, न इजाज़त। वहाँ की आठ-दस फुट चैड़ी सड़क तथा सैंकड़ों की तादाद में लोग, फिर सामान ढोते झल्ली वाले, रिक्शे, ठेले, रेड़ियाँ जाने क्या-क्या ? कन्धे से कन्धा भिड़ाते चलने की भी जगह नहीं। मज़ा ये कि तब भी आने-जाने की प्रक्रिया चल रही थी। एक-दूसरे के हाथ से हाथ ही नहीं टकराते बल्कि रिक्शों व ठेलों के पहिये भी आपस में टकराते रहते....फंसते....चालक बड़बड़ाते....निकलते जाते। सफ़र जारी रहता। कनखजूरे-सी रेंगती सड़क की सैंकड़ों टांगें न दीखतीं। उसी पर हमें जाना था। उम्र का तकाज़ा, जोड़ों के दर्द से मजबूर......हमने रिक्शा ले लिया। नई सड़क के भीतर धंसता रिक्शा मानों किसी खाई में या फिर सुरंग में घुसता-सा लगा। सामने थी....एक जद्दोजहद तथा भिड़न्त भरी सड़क।
लड़ते-लड़ते टकराते-सहमते और एक-दूसरे को थामते-थामते हमें मालीवाड़े के मुहाने तक पहुंचने का अजनबियत-भरा सफ़र तय करना था, जो अपने अजनबीपन के कारण मजे़दार भी हो चला था। मुझे तो इन सड़कों का अनुभव नाममात्र को ही था। बाहरी चांदनी चैक की चकाचैंध की दर्शक होने के साथ-साथ दरीबे की सोने के ज़ेबरों से लदफंद दुकानों से छुटपुट ख़रीदारी, फिर परांैठों वाली गली की दुकान से कभी-कभार लज़्ज़त और लिज्जत भरे पराठों की चसक-ठसक तथा ख़ुरचन, रबड़ी और मलाई वाला दही.....बस इतनी भर ही मेरी समूल जानकारी थी। अब पहली वाली घबराहट का स्थान उत्सुकता ने ले लिया था। विदेशों के सूने से लगते बाज़ारों में शाही अन्दाज़ की ख़रीदारी के मुक़ाबले में दिल्ली के दिल की लदी-फंदी नाड़ियों जैसी गलियों में का सफ़र अब मजे़दार हो चला था।
नग़मा पर इस सब लड़न्त-भिड़न्त का विशेष प्रभाव होता ही क्यों ? वह तो इस सबसे अजनबी न थी। विवाह से पूर्व यहीं रही थी। इन्हीं में बड़ी हुई थी। उसके जे़हन के भीतरी हिस्से में इन सब स्थानों के नक़्शे थे। बचपन की कच्ची नई-नई गीली सिमेंट पर पड़े नक़्श थे, मिटाये मिटते कैसे ? मैं दिल्ली के नये तबके में रही-पली-बढ़ी थी इसीलिए अन्जान, अजनबीपन की दहशत आँखों में भरे रिक्शे से गिर-गिर पड़ने की स्थिति को झेलती-बचाती उजबक की तरहं रिक्शे में बैठी थी। ख़ुद को संभालूं कि रंग-बिरंगे बाज़ार में बिखरे रंगों से आँखें सेकूँ, भीड़ को देखूँ कि बचूँ.....बहुत-सी चैहद्दियों में खड़ी थी-तभी नग़मा बोल उठी। आवाज़ की खनखनाहट तथा आँखों में खोयापन-सा था मानों कई वर्ष पीछे चली गयी हो। ‘पता है-साहिल के लिए हल्वेवाली गली से हल्वा मंगाया जाता था....बड़ा ताम-झाम होता था। हम दोनों (पति-पत्नी) घर से निकलते......युद्ध-स्तर की तैयारी के साथ.......लाल क़िले तक का सफ़र तो फिर भी आसान रहता......बाद में तो घोड़े की चाल कछुए की हो जाती। फिर हल्वे वाली गली तक पहुंचते-पहुंचते तो घिसटन ही बन जाती। मूँग की दाल का हल्वा बंधवाया जाता। ये कोई आसान न होता। ढेर-सा असली घी.......इतना कि चू-चू कर ज़मीन पर गिरने को मजबूर.......ज़रा-सा चसकदार मीठा.......‘ऐसा बाँध देना भाई कि घी कपड़ों में न लिस जाये’.........बार-बार इसरार किया जाता......फिर भी ......।’ थोड़ा-सा सांस लिया नग़मा ने। सांस थी या कि आह, कह पाना मुश्किल।
‘जानती हो, अख़बारों की तह की तह.....उनमें से रिसकर भी घी कपड़ों तक पहुंच ही जाता......कितनी साड़ियाँ ख़राब हुई होंगी......।’
नग़मा के चेहरे पर एक अजब तनाव था......कुछ कालिमा भरी उदासी भी थी। उसने बताया तो नहीं था....पर क्या सभी बातें बताने से जानी जाती हैं। बोले बिना भी तो समझ ली जाती हैं और कुछ तो बहुुत कह-सुनने के बावजूद भी पल्ले न पड़तीं.....साहिल.....उसका दामाद.....पुत्री का पति.....पता नहीं पुत्री के पति क्या कभी अपने नहीं हो पाते हैं। मेीे तो दोनों बेटे हैं, तब भी मुझे पता है। सदा से ये भाव मेरे मन को सालता रहा है। कैसे कोई व्यक्ति दामाद बन अपनी पत्नी के घर के लोगों का अनादर कर सकता है ? क्या सचमुच बेटी विवाह के बाद परायी हो जाती है....हो जानी चाहिए।....शायद नग़मा के मन का कोई ज़ख़्मी हिस्सा था, जो टीस रहा था।
मालीवाड़ा आ गया। रिक्शावाला एक गली के मुहाने पर रुक गया। सिर ही सिर....गिरते-पड़ते, भिड़ते लोगों का हुजूम.......उसी में रिक्शा का रुक पड़ना......चलती सड़क के लिए कोई छोटी-मोटी चट्टान-सी अड़चन न होती। मानों पहाड़ ने गति को रोक दिया हो। इन्सानी फ़ितरत भी अजब है....मौका परस्त......वक़्त के हिसाब से ढल जीने की आदत के तहत मैं भी उसी तरहं कोहनी को हथियार-सा इस्तेमाल करती रिक्शे से उतरी। मन में अपने लिए जगह बनाये जा सकने का भाव था। सामने की गली के मुहाने तक टूटी पटरी थी....जिस पर सीधी-उल्टी दोनों दिशाओं में लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी में टकरा जाने से रुक-रुक पड़ते थे। ख़ुद को इस स्थिति से बचाती तो शायद यह चार-पांच फीट का रास्ता भी तय न कर पाती। इन्हीं में से टकराती, टूटी पटरी से गिर पड़ने की स्थिति से बचती-बचाती, नग़मा के पीछे-पीछे चली। एक धक्का लगा, मैं और नग़मा गली में पहुंच गये।
छः फुटी गली के दोनों ओर दुकानों की चकाचैंध थी। पहली चार दुकानों पर साड़ियाँ टंगी थीं। एक सैकण्ड को निगाह उन पर टिकी। नग़मा ने हाथ पकड़ कर घसीटा.....
‘यहाँ ऐसे चलीं, तो यहीं शाम हो जायेगी....एक बज गया है। तीन बजे नहीं कि गलियाँ नज़र भी न आयेंगी। अभी तो चलना मुश्किल है, फिर रुक पाना भी न हो पायेगा।’
भागती-दौड़ती-घिसटती मैं नग़मा के पीछे-पीछे चल दी। लिथड़ती चप्पल, घिसटती नग़मा का भारी-भरकम शरीर, पीछे-पीछे बढ़ती चली जाती भीड़ की कल्पना से डरती-सहमती मैं थी। अचानक नग़मा किसी दरवाज़े में घुस पड़ी......मैं भी पीछे-पीछे घुसी। पर वह तो एक और गली थी। अ बवह छः फुट की गली चार फीट हो आई थी। मकानों की ऊँचाइयों के कारण भी और ऊपरी मंज़िलों में लिन्टन डाल कर दोनों ओर से एक-एक फुट बढ़ाकर गली की ऊपर की चैड़ाई दो फीघ्ट कर दी गयी थी। सिर उठाकर ऊपर देखा तो लगा कि कुछ गिर पड़ेगा, चक्कर-सा आ गया। गली में रोशनी की इतनी कमी थी कि नग़मा दीख नहीं पड़ रही थी। साथ की दीवार थामकर मैं आगे बढ़ रही थी।
नग़मा के मन के भीतर इन गलियों के सारे नक़्श बने थे। वो तो शायद आँख मूँद कर भी चल सकती थी। यही कारण था कि उसकी गठिया वाली चाल का भी मुक़ाबिला मैं न कर पा रही थी। गली करीब दस-बारह मीटर लम्बी थी। ख़त्म हुई तो एक खण्डहरनुमा दरवाज़े के पास खड़ी नग़मा बेचैन, मेरा इन्तज़ार करती दीख पड़ी। एक टूटे-हिलते पत्थर पर पैर टिकाकर नग़मा दरवाजे़ को ठेलती भीतर की ड्योड़ी में धंस गयी। ‘कौन जाये ग़ालिब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर’..........क्या इन्हीं गलियों का ज़िक्ऱ था उसमें। एक मोटी नस से छोटी-बारीक होती नसों में जैसे ख़ून बहकर शरीर को ताक़त देता है, क्या ऐसी हैं ये गलियाँ। आठ-दस फीट से छः फीट, फिर चार फीट तक होती ये गलियाँ क्या दिल्ली के दिल में ख़ून का दौरा करती नसें हैं ? शायद यही होगा ? कौन नसों के छोटे या बड़े होने का प्रश्नचिन्ह लगाता है....लगा सकता है ?.....बस हैं, तो हैं।
दरवाज़े के भीतर घुसी तो रोशनी बिल्कुल नदारद। नग़मा ने हाथ पकड़ कर सीढ़ियाँ दिखायीं। ऊपर से झांकती हल्की-झीनी-सी रोशनी अब दीखी तो सीढ़ियाँ भी साफ़ हुईं.....बारह-बारह इंच ऊँची.......। कहाँ गया हमारा सारा वास्तु विज्ञान, जिसके अन्तर्गत चढ़ने में पैर आसानी से मुड़ पायें और घुटने के जोड़ पर ज़ोर न पड़े, सिखाया जाता है। पूरा पैर ऊपर रखकर, सारा वज़न घुटने पर डाल, पूरा शरीर उठा कर दूसरा पैर सीढ़ी पर रखने में पूरा एक्रोबेटिक करना पड़ा तब कहीं जाकर पहली छः और थो़ड़ा मुड़कर बनी चार सीढ़ियाँ पार करनी पड़ीं। सीढ़ी के ख़त्म होते ही बांयी ओर दो फुट चैड़ी एक गलियारी थी।
‘क्या गणित है ?’......मुझे हँसी आ गयी। ‘दस फुट से शुरु होकर ये गलियाँ धीरे-धीरे कम होती दो फुट पर पहुंच गयी।
अब तक तो मुझे अपने दिल्ली-ज्ञान के झूठा होने का अहसास हो गया था। रिंग रोड पर अस्सी की गति से मारुति कार चलाने वाली मैं और दिल्ली की सभी काॅलोनियों का ज्ञान भ्रम साबित हो उठा था। मैं आसमान से पाताल में गिर पड़ी थी। इस दो फुट की गलियारी से ज़रा आगे बढ़े तो एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा भी चार या साढ़े चार फीट ऊँचा होगा। उसमें सिर झुका कर ही अन्दर घुसा जा सकता था। वहाँ पहुंचे तो लगा कि शायद मंज़िल पर पहुंच गये हैं।
‘क्या यहीं हीरों की जड़ाई होती है ?’ मेरे कथन में प्रश्न से अधिक आश्चर्य था।
‘हीरे-पत्थर सभी को बराबर महत्व देने वाले ज़हीन लोग हैं यहाँ तो। पत्थर भी जड़ दे ंतो हीरा लगे फिर हीरा तो हीरा ही है।’
दरवाज़ा फिर ऊँचाई पर था। नीचे कोई पत्थर भी नहीं रखा था। रखा भी कहाँ जाता ? दो फुट चैड़ी गलियारी थी। उसमें दोनों पांव रखकर कदम बढ़ा लिये जा सकें तो बहुत। फिर से उठा-पटक करती हम दोनों दरवाजे़ के भीतर समा गयीं।
भीतर तो और भी हैरतअंगेज़ नज़ारा था। एक अंधेरी चार गुणा चार की कोठरी थी। तीन-चार लोग अपने-अपने पास ट्यूब लाइट वाले लैम्प लगाये हीरे-जवाहरात की जड़ाई में डूबे थे। अजब दास्तान है ज़िन्दगी भी। इतनी नफ़ासत से हीरों का काम करने वालों की ज़िन्दगी अंधेरों से भरी थी, और उसे पहनने वाले....उनका अंधेरे कोने-कुचीलों से क्या वास्ता ?
सीधे हाथ की तरफ़ दो मूढ़े रखे थे। शायद हम जैसे लोगों के लिए ही थे। उसी के आगे ज़रा-सी नीचे फिर एक छः गुणा आठ का कमरा-सा दीखा। वहीं एक कोने में टेलिफून भी था। चटाई बिछी थी। उसी पर चार बच्चे, यही कोई 9 या 12 तक की उम्र के होंगे, अपने सामने वैसे ट्यूब वाले लैम्प रखे मोतियों की मालाएं पिराने में मशग़ूल थे। हम भीतर धंस गये, मूढ़ों पर बैठ गये। किसी ने आँख उठाकर भी नहीं देखा। अनदेखे-अन्जान से हम दोनों मूढ़ों पर हाँफ़ते से बैठ गये।
उम्र कोई पैंतीस-चालीस या हो सकता है इससे भी कम की हो, आँख उठाकर (अपने आतशी शीशे वाली आँख को बन्द किए-किए) देखा तो नग़मा बोलीं,
‘कहिये दादा, कैसे मिज़ाज हैं ?’
‘दया है उसकी....’ दादानुमा उस व्यक्ति ने ऊपर की ओर हाथ उठा दिये।
‘जी.....दादा.....वो तो है ही। अल्लाह तो सबको देखता है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सब उसी की मेहर है.....दादा। ये मेरी छोटी बहन है। कुछ काम करवाना चाहती है।’ नग़मा ने मेरा तार्रुफ़ करवाया।
‘ओवश्य....ओवश्य......दीजिये’ दादा कहलाये जाने वाला व्यक्ति बंगाली है, यह स्पष्ट था।
मैंने हीरे की टूटी हुई अंगूठी उनकी ओर बढ़ायी। टूटी अंगूठी से डिज़ायन समझाया। नाप दिया।
तब तक नग़मा मोती पिरोते बाल परिवार की ओर मुख़ातिब होकर उनका हाल-चाल पूछने लगी। मेरा ध्यान उन बच्चों की वजह से अपनी अंगूठी में नहीं लग पा रहा था। ये ज़रा-ज़रा-से बच्चे, जिनकी आवाज़ भी अभी नहीं फटी थी, जिनके चेहरे पर मूंछों-दाढ़ी की रेखायें भी नहीं फूटी थीं, इतने बारीक-नफ़ीस काम में जुटे अपनी आँखें फोड़ डाल रहे थे। हम पहुंचे ही एक बजे के बाद थे। तब तक बहुत-सी पिरो दी गयी मालाओं के ढेर लग चुके थे। सोने के टिकड़ों में धागे बाँधे जा रहे थे। मोती और सोने की टिकड़ियाँ मिलाकर चन्द्रहार बनाये जा रहे थे।
दादा अपने काम में माहिर थे। जल्द ही सब कुछ समझा, हीरे गिने, नोट किया, हिसाब लगाया, नाम लिखा, पुड़िया बनायी, नाप का नम्बर, पैसों का अन्दाज़ सभी लिखकर मुझे एक काग़ज़ थमाया और फिर काम में जुट गये इतने क़ीमती समय को बर्बाद करने की गुंजाइश की कहाँ थी ?
तभी सिर पर पग्गड़ बाँधे एक और आदमी दाखि़ल होता दिखाई दिया। उसने अपनी चमरौंधा कोने उतारा और भीतर धंसने लगा तो नग़मा चहक उठी,
‘आदाब ताऊ, कैसे मिज़ाज हैं ?’
‘अहा! नग़मा बेट्टी। थारी दुआ हैगी। कैस्से हैं सब ? बेरा है तैन्ने। तेरा भाई....वाई जो पिछली बार्यो मिल्या था, विदेस चल्या गया....वाई...कै कैवें....अमरीका।’
‘अच्छा....क्यों ताऊ ?’
‘अरे! याही...मोती-सोन्ने का काम करन की कोसिस कर रह्या था। कोई जान-पहचान वाल्ला था। ओस ने ही बुल्ला लिय्या’।
‘अच्छा...आपको कैसे लग रहा है ताऊ।’
‘के बताऊँ बेट्टी। इब्ब, इन बच्यां ने तो जान्ना ही पड़ेगा। अपना तो गुजारा हो गय्या उस गुचकुलिये में....इहों ही मर्र जावेंगे। वा तो खुल्ली हव्वा में साँस लै लें।’
मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी और उन बच्चों की स्थिति को देखकर अन्दर ही अन्दर सुलग भी रही थी। तभी नग़मा बोली,
‘ताऊ! ये मेरी छोटी बहन है। अदब पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में।’
‘बहुत अच्छा है। बेट्टियाँ पढ़-लिख लैं, तो अच्छा लागै है। इब तो ज़माना बदल गया हैगा।’
और ‘ताऊ’ एक सीढ़ी नीचे उतरे और उस छोटे-से कमरे में जाकर बैठ गये। भाषा से ‘हरियाणा के है’ लग उठा था। अब उनके साथ-साथ ध्यान कमरे के और कोनों की ओर भी गया। कमरे के साथ जुड़ा एक खम्बा बाहर की ओर निकला दीखा। वैसा ही एक खम्बा दूसरी ओर भी था। ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि यह खम्बा वास्तव में ऊपर की मंज़िल की चूल थी जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी होगी। वक़्त बीतते न बीतते यह चूल खण्डहर बनती इमारत के साथ टूट गयी थी। मुझे हैरानी भी हुई और डर भी पैदा हुआ। बिना चूल के इस कमरे में बैठे लोगों का हश्र सोचकर रीढ़ की हड्डी में एक सुरसुरी-सी हुई।
‘जा....सूरज की रोशनी समेट ला, आँक्खों मंे....नज़र साफ़ हो जावैगीं।’
बैठते-बैठते ये बात मोती पिरोते उस सफे़द कमीज़ वाले लड़के से कही गयी थी और मैं सोच रही थी-
‘देखें क्या गुज़रे हैं क़तरे पे, गुहर (मोती) होने तक’, जिसने ये बात कही थी, वो मियां जी क़िस्म के व्यक्ति थे। खुले पैयचों का पाजामा, ऊपर मटमैली-सी लम्बी कमीज़, सिर पर टोपी, मुँह में पान दबाये, कब उस कमरे में दाखि़ल हो गये थे, देख ही न पाई थी। शायद क़तरे के ख़ाक़ हो जाने में डूबी थी। उन मियां जी ने भीतर आते ही उस बच्चे को आँख मिचमिचाते देख लिया था, शायद तभी बोले थे। बैठते-बैठते उनकी निगाह हम पर पड़ी-
‘अरे बाजी, आदाब, कैसे मिज़ाज हैं ?’
‘शुक्र है अल्लाह का....आप कैसे हैं मियां जी ?’
नग़मा ने पूछा था
‘जी! बस, सब दुरुस्त है। उसका रहमो-करम रहना चाहिए।’
मैं उस छः गुणा आठ के कमरे में छः जनों को काम में मशग़ूल देखकर भौंचक थी तभी नग़मा ने पूछा,
‘ये बच्चे नये दीख रहे हैं ?’
‘हाँ! बाजी! सभी अपने ही रिश्ते से हैं। गली-गली मारै-मारै फिरै थें मरदुए। मदरसे भी तो न जावै थे। रिश्ते में कोई भतीजा, कोई भांजा हैगा....पहले घर में ही कराऊँ था....पर टिकते न था....ज़रा-सा इधर-उधर हुए तो ये जा....वो जा.....स्सा.......।’
मियां जी कनखियों से मेरी ओर देखकर चुप हो गये।
‘पर ये सब तो बहुत छोटे हैं.....कम उम्र हैं ना’ मुझसे कहे बिना न रहा गया।
‘हैं तो बहन। पर क्या करैं। ससुरे न पढ़ैं, न काम करैं। अब बैठाके तो कोई शंहशाह भी न खिला सकै। ये जो सलीम हैगा.....बाहर गया अभी.....सात बहनें हैं। बाप यहीं किसी दुकान पे बैठे हैगा.....अब क्या कमायलै....क्या खालै-क्या खिला लै........फिर सारा-सारा दिन आवारागर्दी करै थैं..........यहीं बिठा लिया।’ मियां जी के चेहरे पर सचमुच दुख झलक आया था।
प्र.....इनकी आँखें.....इतना बारीक-नफ़ीस काम, फिर घण्टों लगातार......’
मेरे जे़हन में ढेर-से प्रश्न थे। पूछूँ कैसे का सवाल भी अहम था।
मियां जी थोड़ा चुपा आये थे फिर बोले, ‘बाजी! आप तो पढ़ी-लिखी हो। कानून जानो हो। पर पेट का कानून उसकी किताबों से अलग हैगा। नाली के कीड़े-मकोड़े-मच्छर देखे हैं बाजी....उन्हें निकालकर साफ़-सुथरे कमरे में छोड़ दो......मरे.....कोने कुचीले ढूंढ ही लेवैं।....फिर आंखें फूटे या दीदे निकले....पेट तो नहीं निकाल सकते ना।’......
बोलते-बोलते मियां जी, पता नहीं लगातार बोलने के कारण या फिर दुख की बहुतायत के कारण हाँफ़ने लगे थे। थोड़ा रुक कर फिर बोले-
‘पर बाजी! ठीक तो कहती है आप भी। मैं दिखाऊँगा इन्हें आँखों के डाॅगदर को, कोई दवा-दारू तो होनी ’ही चाहिए....हैं तो अपने ही बच्चे।
मेरा मन भर आया। थोड़े-से सुकून के भाव से मैंने कहा-
‘यहाँ रोशनी भी बहुत कम है.....काम बहुत बारीक है.....सूरज की एक किरण भी नहीं.......दिन में भी अंधेरा......’
हाँ....बहन.....सब सही है तभी तो बल्व नहीं ये ट्यूब लैम्प मुहैया करवाये हैंगे। ये सभी मेरे सगे हैं। इन्हें दर्द होता है तो मेरा भी मन दुखता है....मुझे देख रही हैं। अभी से चालीस साल की उम्र.........और इतना मोटा चश्मा। आँखों के ख़राब हो जाने का दर्द क्या होता, मैं जानूं हूँ।’
मियां जी दोहरे दर्द से तड़प-सा गये । नग़मा ने मरहम पट्टी करते हुए कहा-
‘माफ़ कीजिये मियां जी। ये मेरी छोटी बहन यूनिवर्सिटी में अदब पढ़ाती है, इसलिए इतनी बहस-मुबाहिसा कर रही है।’
मैं न तो उनके ज़ख़्म कुरेदना चाहती थी, न ही उनकी दुखती रग पर हाथ रखना चाह रही थी। किताबी व अख़बारी पढ़ाई के अनुसार यही जानती थी कि बाल मज़दूरी गुनाह है....इतना बड़ा गुनाह कि करवाने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए।........अभी पिछले दिनों ही दिवाली पर पटाखें न चलाये जाने का अभियान किया गया था, स्कूल के बच्चों ने अनेक तरीकों से ये बात लोगों तक पहुंचाई थी। कारण था कि पटाखों की सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले ये खेलने-खाने की उम्र के बच्चे कैसे आग के गोलों पर बैठे ज़िन्दगी बिताते हैं। शायद ज़िन्दगी ही उन्हें छोटी-सी उम्र में निगलनी आ जाती है। जाने कितनी ख़बरें........कितने लेख.....कितने दूरदर्शन के प्रोग्राम देखे थे........सभी ने आज दम तोड़ दिया। समस्या का क़ानूनी हल कुछ भी हो, यथार्थ तो कुछ और ही था और फिर कितना कड़वा था.....़क़ानून सिर्फ़ एक मीठा मुलम्मा था। शुगर कोटिंग मात्र, एक थ्योरी जो किताबों के लिये थी। पटाख़ों के ढेर पर बैठे कार्बन फाँकते, या फिर मोतियों के ढेर पर बैठे आँखें फोड़ते इन बच्चों की स्थिति के सच में तो कोई फर्क़ न था।
पता नहीं इन्हें कोई रोशनी की जगह क्यों नहीं मुहैया करवाई जा सकती ? क्यों कोई इन्हें खुली हवा, धूप नहीं दे सकता ?
‘मियां जी! माफ़ कीजियेगा। अब तो शहर इतने फैलते जा रहे हैं। आप लोग अभी भी अंधेरे गलियारों से क्यों जुड़े हैं ?’
‘चाहता तो मैं भी हूँ कि यहाँ से कट जाऊँ। बहुत बार चाहता रहा हूँ। इसके लिए बहुत बार, बहुत तरीकों से कोशिश भी की है। पर....इन गलियारों में कितनी सुरक्षा का अहसास होता है.....आपने आस-पास की काॅलोनियों और फ़ार्म हाऊसज़ की ख़बरें तो पढ़ी ही होंगी.....रोज़ का अख़बार इसी से भरा रहता है।’
मेरी आँखों के सामने पिछले दिनों के अख़बार की ख़बरें घूम गयीं। पहले कभी तीसरे पन्ने की ये ख़बरें अब पहले पन्ने की हो गयी हैं। आज हम किस दहशत और असुरक्षा के बीच जीने लगे हैं। इस स्थिति को ढेर-से विशेषणों को लगाकर क्या व्याख्यायित किया जा सकता है ? मियां जी ने ही मुझे चुप देखकर कहा-
‘हमारा काम ही ऐसा है बाजी। इतने क़ीमती जे़वर, हमारे यहाँ पड़े रहते हैंगे। कुठ हो-हवा जाये तो खुद का बेचकर भी चुका सकना नामुमकिन। हमेशा एक डर, एक भार-सा रहता है सीने पर। सिर पर जैसे तलवार लटकी हो। यहीं इन गली-गलियारों-कोठरियों में जहाँ सूरज की किरण भी घुस न पाये, वहाँ पर भी ये काम करने के ढेर से जोखिम हैं, कहीं बाहर कैसे जायें ?’
दो बनजे वाले थे। उन बच्चों के द्वारा पिरोयी मालाएं मन को लुभा तो रही थीं, पर मन का कोई कोना टीस भी रहा था। नग़मा और मैं आदाब, नमस्कार करती नीचे उतर आईं थीं। सड़क, वास्तव में, अ बनज़र न आ रही थी। कुछ खाने और चाय पी लेने के भाव से नग़मा पराठेवाली गली की ओर चल दी। ग़ालिब की इस दिल्ली को देखने की अजब उत्सुकता मन में जाग उठी थी। पूछने पर नग़मा ने ही बताया-
‘ये गली, सीधा चलते जाओ तो किनारी बाज़ार से होती हुई दरीबा पहुंच जाती है। दांयी ओर ढेर से कटरे हैं। बांयी ओर पराठे वाली गली, शाॅलवाली गली और भी जाने कितनी गलियाँ हैं....ढेर-सी हवेलियाँ हैं।’
सामने दीख पड़ती एक हवेली की ओर इशारा करते हुए नग़मा ने बताया-
‘जानती हो, ये हवेली नहीं एक मुहल्ला है। हर हवेली एक पूरा हिन्दुस्तान है जो जाति, धर्म, वर्ग किसी भेद-भाव को नहीं जानता। अजीब बात है....जाति व धर्म के कारण होने वाले दंगों से अख़बार भरे रहते हैं पर यहाँ इन हवेलियों में बसते सैंकड़ों परिवारों के बच्चों को खेलता देखकर ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन किसके बच्चे हैं। मानों एक जुड़ा परिवार हो जिसमें आलू, प्याज़, नमक, चीनी तो नदी के पानी से इधर से उधर जाते रहते हैं-एम सील लगाकर जुड़े हों मानों-त्यौहार सभी साँझे हो जैसे। उधर जामा मस्जिद पर रोज़ों के आस-पास बिकती शीरमाली रोटियाँ बननी शुरु हुईं, इधर शाम का खाना बन्द। बच्चे तो पराठे वाली गली पहुंचे, रबड़ी खाई और फिर खेलने निकल गये।’
पराठेवाली गली तक पहुंचते-पहुंचते मैंने शिमला की मटर, सेंजने के फूल, काला चाट मसाला, काली गाजरें, ताज़ा इमरती, मेरठ की रेवड़ी-गजक और फिर ताज़ा-तरीन खुरचन और गाजर का हल्वा, जाने क्या-क्या पैक करवा लिया था। इत्तफ़ाकन झोला नग़मा के पर्स में निकल आया था। हैरानी इस बात पर थी, चाय की दुकानें थीं तो पर एक भी ऐसी नहीं कि बैठकर पी पाते।
तभी नग़मा के सुझाव को मानते हुए कढ़ा-गुलाबी-मलाई डला दूध पीने का निश्चय हुआ। दूध पिया, गला तर हो गया।
यही ज़रा-सा सफ़र लम्बाई-चैड़ाई, गहराई में था तो कुछ मीटर का, पर गुणात्मक इतना कि असलियत की हज़ारों परतें मेरे सामने खोल गया था।
दूध पीकर आगे आये तो बैठ गये, उन्नीसवीं शती से चली आती परांठेवाले की दुकान पर, जिनके परौंठों की चर्चा विदेशों में भी है। पड़दादा से पड़पोते तक तो ख़ासियत विरासत में मिली है। उस दिन इन परांठों को खाने की इच्छा तो पूरी हुई ही, सीखने का मौका भी मिल गया। पापड़ तेल में तला, चूरा बना था और लोई में परत लगाकर भर दिया। पापड़ का पराठा पापड़ जैसा कड़क व करारा.........परत वाला परांठा। लोई को रोटी के आकार का बेल लिया सालेह टुकड़ों में काटा और घी की परत देेकर एक-दूसरे पर इकट्ठा कर बेलकर सेंक दिया......खोलो तो एक-एक परत अलग। ‘हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले’ किस-किस ख़्वाहिश को पूरा करती ? वक़्त ही कहाँ था ? किनारी बाज़ार के गोटे किनारी से लदे-फंदे बाज़ार में घुसती या फिर दरीबे के जे़वरात के शो की सजावट देखती या फिर कटरा अशर्फ़ी, शालों वाल कटरा.....जाने कहाँ-कहाँ ?
पिछले दिनों ही विदेश से लौटी थी। वहाँ तीन वर्ष बिताये थे। जीवन के सुख, घरों का वैभव, रहने-सहने के ठाट-बाट, कामकाजी मशीनें, चैड़ी साफ़-सुथरी गन्दगी रहित सड़कें, कहीं धूल-धक्कड़ का नाम नहीं यानी कुल मिलाकर एक सुखद, साफ़, प्रदूषण रहित जीवन। यह अधिक सुखद, माधुर्य और मिठास के कड़ुवेपन का अहसास होता रहता था। इन गलियों-गलियारों में पता नहीं क्या था, जो जोड़ रहा था, शायद अपना होने का अहसास था। हवाई जहाज़ की यात्रा करते हुए जिस परायेपन को महसूसा था, जो विदेशी ज़मीन पर मिला था, यहाँ अब समाप्त था। मानों, मिट्टी-ग़ारे के नीचे दबी मेरी जड़ें थीं, जो मुझे वक़्त-बेवक़्त ताक़त देती थीं, धमनियों में ख़ून बनती थीं, जिनसे मैं ज़िन्दा थी....वे ही यहाँ मिल गयी थीं।
लौटने का वक़्त हो चला था। चार बज चुके थे। वे चार-छः फुटी गलियाँ अब लोगों का हुजूम बन गयीं थीं। दिल्ली के दिल में ख़ून का दौरा अपनी पूरी गति पर था। एक अजब-सी शान्ति से पहले की भाग-दौड़ थी यह। इन गलियों के भीतर धंसना भी आसान न था, पर उनसे बाहर निकलना तो और भी मुश्किल हो उठा था। फिर बाहर निकलकर.....थ्री व्हीलर पकड़ना....जाने कितनी मुश्किलें थीं......पर इतनी कठिनाइयों में भी मज़ा आने लगा था। ये कठिन सफ़र जानलेवा नहीं लग रहा था। विदेशों में अचानक अनेक मिली आसानियाँ भी नागवार गुज़र रही थीं.........बोरियत की हद तक। और...अब भीड़ के ताने-बाने में फंसी मैं बिल्कुल बोर नहीं थी। शायद यही मेरी असलियत थी।
ये सफ़र दिल्ली के दिल का नहीं था, चैक की चाँदनी भरी सड़कों की चमक का नहीं था। मालीवाड़े से लेकर किनारी बाज़ार तक के गली कूचों का नहीं था। ये कोई देहयात्रा नहीं थी, ये तो मेरे.......मेरे भीतर का सफ़र था। इसमें तो मैं, मेरी रुह धड़क रही थी, जिसे मैं जानती तक न थी। आखि़र दिल के धड़कने का अहसास कहाँ होता है, वो तो ज़िन्दा रहने की शर्त भर है।