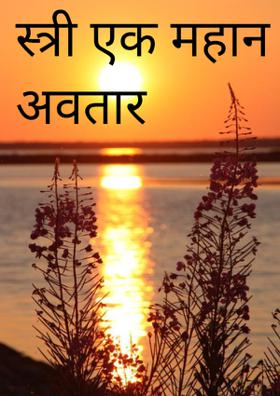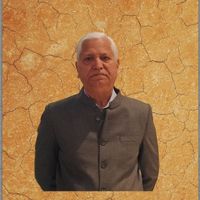नेह के दाने
नेह के दाने


देहरी पर फुदकती चिड़िया
चुगती नेह के दाने।
उतरती, कभी आँगन में।
कभी चौबारे पर।
और कभी
जा बैठती छत की मुंडेर पर।
बेचैन-सी, ढूँढ़ती है
शिशुओं की चुहल।
पायलों की रूनझुन।
चूड़ियों की खनक।
बर्त्तनों की छन-छन।
आँगन की वो बैठकी।
बड़ों का छलकता प्यार।
दादी की प्रेमपगी मनुहार।
दादा जी का डाँट भरा दुलार।
और
घर के कोने-कोने से नि:सृत
प्रेम की भीनी-भीनी-सी फुहार।
परंतु , अफसोस
अब गूँजती है, सिर्फ
बूढ़ी दादी की खाँसी की आवाज़।
घर के वीरान सन्नाटे में।
कहाँ सुनाई देती है अब दालान में
भैंस-गायों के रम्भाने की आवाज ?
और, पक्षियों के संग-संग -
अपने घरौंदों की ओर लौटते हुए
थके कदमों की आहट भी ?
नहीं होता अब तो
ढलती शाम के धुंधलके में
घरों से निकले धुएँ के बादलों का
ऊपर आसमान में, आपस में मिलना भी।
खो गयी है
पड़ोसी के चूल्हे की आग माँगने की परंपरा भी।
और साथ ही, बंद हो गया है
जमुनिया बुआ का घर-आँगन घूम-घूम
नित नयी कहानियाँ बाँचने का सिलसिला भी।
जाने कैसे टूट गया
सुबह-शाम कुएँ पर पानी भरने के बहाने
दुल्हनों-माँ-बहनों के
आपस में सुख-दु:ख बाँटने का चिरंतन क्रम भी।
आगे बढ़ने की होड़ में
न जाने कहाँ पीछे छूट गयी
परिवारों की परंपरा।
संस्कारों की सीख।
स्नेह की शीतल छाँव।
नीम तले की चौपाल।
मुखियाजी की ग्राम-कचहरी।
फागुन की रंग-मंडली।
दशहरे की नौटंकी।
और
ग्रामीण एका ?
क्यों नहीं जलाते हम
मिट्टी की नेह से पके दीये
मन का अंधेरा मिटाने को भी ?
क्या इन सबको निगल लिया है
गगनचुंबी इमारतों में पनपती
मॉलों में पलती
लिफ्टों में चढ़ती
सैंट्रो में विचरती
हाइवे पर दौड़ती
बस, "स्व" में डूबी
इस भौतिकवादी, पश्चिमोन्मुख
अत्याधुनिक संस्कृति ने ?
यह क्षरण है
या रूपांतरण
एक संस्कृति का ?
सोचती है चिड़िया
विह्वल-विचलित-विगलित।
नेह के दाने तलाशती।
उदास फुदकती।
इस देहरी से उस देहरी।
इस मुंडेर से उस मुंडेर।