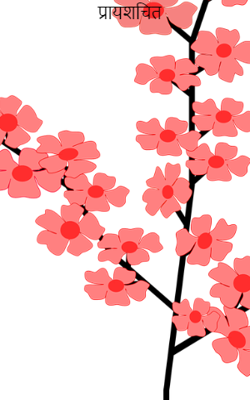स्त्रियों का कोई घर नहीं होता
स्त्रियों का कोई घर नहीं होता


बचपन में जिस आंगन की मिट्टी में नहाकर इठलाती है वो अबोध बालिका
उसे कहाँ पता होता है कि यह आंगन,जो बसता है उसके देह के हर अंश में, वह उसका नहीं है
हंसीठिठोली में हो या हो गुस्से में, उसे याद दिलाता है हर शख्स की वह पराया धन है
समय के साथ बदलती भावनाओं को अपनाते हुए वो मान भी लेती है कि ब्याहने पर मिलेगी उसे उसकी जमीन, उसका वो आंगन
वो आंगन जिसमें उसे कोई पराया नहीं कहेगा, जिसे छोड़कर जाने का भय उसके मन में नहीँ रहेगा
हजारों सपने बुनकर, अपने अपनों को छोड़कर रोते बिलखते पहुंच जाती है उस आंगन जिसे,उसके लिए तय किया गया है
मन ही मनमें एक आस है एक विश्वास है, जो मिला है वो सिर्फ और अपना है
लेकिन होता है फिर एक छल
जिस आंगन में भेजा गया था ये कहकर कि वो तुम्हारा है वो भी किसी और का घर समझाया जाता है।
हर बातों पर हर शख्स भी फिर वही कहानी दुहराता है और बताता है उस कि वो पराए घर से आई है यह घर उसका कहाँ
वो जो टूटे हुए खुद को जरा सी मरहम पट्टी से जोड़ ही रही होती, उसे फिर तो तोड़ कर बिखेर देते हैं उसके ही अपने
दूसरों की तीमारदारी में लगी स्त्रियाँ ढंढूती रह जाती हैं उम्र भर अपने हिस्से की जमीन और छोटा सा आसमां
कहने को दो घरों की रौनकें होती हैं लेकिन स्त्रियों का कोई घर नहीं होता।