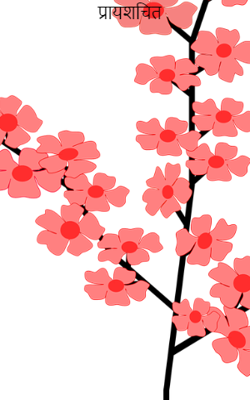पीतल से कुंदन
पीतल से कुंदन


झलती, छलती, खेलती, खुलती, मदमस्त ब्यास नदी में, मैं पीतल की छोटी सी बटोही, सखी के हाथ से छूटी और बह गयी। छलता, छलछलाता, धूप का दर्पण, छम से कूदा और बोला- ऐ री सखी तू तो गयी।
अनुभूतियों की परतें खोलती लहरें, मन को मेरे टटोलती लहरें, नये क्षितिज की संभावनाओं को संग लिये, चुलबुली, बेदाग़, पाक, बेबाक और बेतुकी लहरें, मुझमें समां गयीं, बहाकर अपनों से दूर किसी और दुनिया में ले गईं।
वो घोर बिलास और आनंद की अनुभूति भर ली अपने अंदर मैंने, नदी के पत्थरों पर लटक-मटक, पटक-भटक, खटक-झटक, टूटती चोटें सहती बहते आगे मैं बढ़ चली। आनन्द, उत्साह, वियोग, बिछोह सब झेलती आगे-आगे मैं चल पड़ी, खिलती, खिलखिलाती, फूल, पत्ते, टहनी, फल साथ बरसाती चंचल पवन मुझसे होकर गुज़री तो इक सिहरन सी मचल पड़ी।
इक गाँव किनारे देखा मैंने स्त्री-पुरुष, प्रेमी-प्रेयसी, वो मानव भावनायें, संभावनाएं, परंपराएं और मर्यादायें, कुछ देर वहाँ ठहरा पानी, सोचा थोड़ा विश्राम कर लूँ, शायद किनारा मिल जाये तो कुछ क्षण मैं आराम कर लूँ, पर सत्य असत्य से परे, भाग्य दुर्भाग्य संग लिये, मैं इक बार फिर से बह गयी। अँधेरे उजाले सब झेलते हुए, अकेले आगे मैं बढ़ती गयी, कई साथ ही चले मेरे, वो संस्कृतियाँ और विकृतियाँ, उस नदी में सदियों से बहतीं बहतीं, मेरी संगी साथी बन साथ बहीं मेरे संग-संग खेलते हुऐ।
नदी चली अब सागर में समाने, अपने संग संग मुझे लिये, गागर में सागर भरने लगा, नयी लहर और नयी सम्भावनाओ की अनुभूती लिये, मुझमें नये जज़्बे भरने लगा। सब सहती, अपनाती, ठोकरें खाती मैं सागर में बस समां गयी, ऐ री सखी, इन थपेड़ों से मैं पीतल से कुंदन बन गयी।।