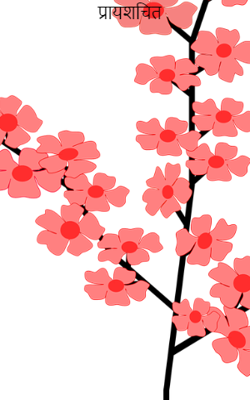नया सूरज
नया सूरज


‘नहीं, अब और नहीं सहेगी वह। बस। बहुत हो चुका। किसी की नहीं सुनेगी, किसी कीमत पर नहीं सुनेगी। सुनेगी तो केवल अपने मन की। करेगी तो अपने मन की।’ सब्जी काटते हुए माधुरी अपने पर ही मानो झुंझला उठी थी।
बचपन से माधुरी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों में ‘विचित्र प्राणी’ और ‘विद्रोही आत्मा’ के रूप में प्रसिद्द थी। एक आग सी सुलगती रहती थी उसके अन्दर जिसकी ज्वालाएँ अब किसी भी कीमत पर शांत होने को तैयार न थीं। उन ज्वालाओं ने भी मानों विद्रोह का बिगुल बजा दिया हो, जिन्हें अब तक वह शालीनता, संस्कारों और मर्यादाओं के छींटे डाल-डाल कर बुझाती रही थी। पर, बूंदों से कभी दावानल शांत हुआ है कोई, जो अब होता।
‘छुन्न ।’ कढ़ाही के तेज़ गर्म तेल में जैसे ही उसने सब्जियों के टुकड़े डाले, भाप और धुंएँ के बादलों के साथ माधुरी ने अपने निर्णय पर भी मानों मुहर लगा दी थी। वह जितनी तेज़ी से कढ़ाही में कलछुल चलाने लगी और उतनी ही तेज़ी से उसका मन मुड़कर पीछे की ओर दौड़ने लगा।मन के पीछे माधुरी भी दौड़ पड़ी।
बचपन से सौम्य, सरल स्वाभाव, कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा की धनी माधुरी की शिराओं में रक्त नहीं संस्कारों, नैतिकता और आज्ञाकारिता के विटामिन्स और मिनरल्स प्रवाहित होते थे। जो देखता, उसके शालीन सौन्दर्य पर रीझ उठता था। सुन्दर तो थी ही वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह। किन्तु, विशिष्ट विटामिन्स और मिनरल्स के साथ उसके रक्त में कुछ ऐसे कीटाणु भी रेंगते थे जो सुप्तावस्था में रहते हुए जब-तब उभर आते, बीच-बीच में विद्रोह की अग्नि भड़काते और संस्कारों की एंटीबायोटिक खाकर चुप रह जाते किन्तु मर कभी न पाते थे। समाज की, परिवार की झूठी मान्यताओं और थोथी परम्पराओं को न चाहते हुए भी मानते रहने की अपनी विवशता को वह आज तक समझ न पाई।
कुकर में दाल के साथ हल्दी और नमक डालते हुए जैसे ही उस पर ढक्कन लगाया, वह ‘चट्ट’ की आवाज़ के साथ बंद हुआ और उधर दूसरे चट्ट’ की आवाज़ के साथ उसकी यादों पर लगा ढक्कन भी खुल गया।
उसके माता-पिता ने भाईयों और बहनों के बीच शिक्षा और संस्कारों को लेकर कोई भी कभी भी भेद-भाव किया हो, ऐसा उसे याद नहीं पड़ता। बस।एक ही बात उसको हमेशा सालती रही और वह थी पिता जी का माँ के प्रति उपेक्षित व अपमानजनक व्यवहार। उस पर भी माँ का दोनों बहनों को सदा सब कुछ सहन करने की शिक्षा देना। उसे बहुत बुरा लगता था जब जब माँ पिता के तानों और व अपमान को चुप होकर सहना और कुछ न कहना अपना कर्तव्य समझतीं और ऐसा करना पिता का पुरुषोचित अधिकार। आखिर क्यों करतीं हैं माँ ऐसा? क्यों सहन करतीं हैं ? क्यों कुछ नहीं बोलतीं? अगर वह उनकी जगह होती तो हरगिज़ यों चुप न रहती। बिस्तर पर नींद का बहाना कर चुप होकर जब भी उसने जब भी पिता की गुस्से भरी लाल लाल ऑंखें और माँ का उतरा चेहरा अपनी बंद मिची आँखों से देखा, उसने यही निश्चित किया कि वह माँ जैसा नहीं सहेगी। हरगिज़ हरगिज़ नहीं!
समय बीतता गया, वह बढ़ती गयी, पढ़ती गयी, परिस्थितियाँ बदलीं और बदले मौसम भी।
खाना लगभग तैयार हो चुका था। माधुरी ने उड़ती हुई एक निगाह घड़ी पर डाली। बच्चों के आने में थोड़ी देर थी। सो चाय का प्याला लिए वह बालकनी में आ बैठी। चाय के घूँट भीतर समाते गए और यादों की परतें एक-एक कर उघड़ती रहीं।
पढ़ी-लिखी स्वतंत्र विचारों वाली, आत्मविश्वास से लबालब हर प्रतियोगिता को जीतने वाली माधुरी विवाह के बाद जैसे अपनी माँ का ही जीवन दोहराने लगी। भीतर उठते विद्रोह का तूफ़ान संभालती और बाहर से शालीनता और मर्यादा की विवशता से उस तूफान को भीतर ही दबाये रखने का भरसक प्रयास करती रहती। पिता के दूसरे रूप में पति उसके सामने खड़े मिलते। ‘नहीं! वह माँ जैसी हरगिज़ न बनेगी ! कभी नहीं!’ उसने एक बार फिर स्वयं को कहा। चाय का अंतिम घूँट माधुरी ने हलक में उड़ेला और उठ खड़ी हुई। चेहरा तना हुआ किन्तु स्वाभाविक शांत मुद्रा थी।
माधुरी ने राहुल और रोहिणी को अपने तरीके से पाला। अपने संस्कार दिए। ससुराल व् मायकेवालों की इच्छा के विरुद्ध। जब भी राहुल ने पुरुषोचित संस्कारों के वशीभूत होकर छोटी बहन रोहिणी को सताने कि चेष्टा की, भले ही बचपने में या मज़ाक में, तब तब उसने राहुल को आड़े हाथों लिए। लड़की होने के नाते उसने रोहिणी को चुप रह कर पीड़ा सहना नहीं सिखाया और न राहुल को लड़का होने के नाते अधिकारों का दुरूपयोग ही करने दिया था। दफ़्तर में रात-दिन उलझे पति को इतना समय ही कहाँ था जो बच्चों को देखते। पर हाँ, इतनी व्यस्तता में भी पुरुषोचित अधिकारों का प्रयोग करना कभी न भूलते थे।
बच्चों के पालन-पोषण करते हुए घर गृहस्थी के कामों में उलझी माधुरी को अहसास ही न हुआ कि समय कितनी तेज़ी से पंख लगा कर उड़ता रहा। कब बच्चे बड़े हो गए और अब तो रोहिणी के विवाह की वह शुभ बेला भी आ गयी जिसका उसे कब से इंतज़ार था।
कल रोहिणी का विवाह है। घर रिश्तेदारों व मित्रों से भरा पड़ा था। बच्चों की उछल-कूद, एक ओर ढोलक की थाप तो दूसरी ओर स्पीकर पर नए ज़माने के फ़िल्मी गानों का शोर; फिर भी माधुरी मन से उठते उस शोर को दबा नहीं पा रही थी जिसे आज तक वह अनसुना करती रही थी। लड़कियों की हथेलियों पर सज रही थी मेहँदी और उधर माधुरी के मन में जगमगाती नयी छवि कुछ नए रंग ही भरने की तैयारी में थी। एक नया केनवस उसने अब अपने मन में जमा लिया था।
वह शुभ घड़ी आखिर आ ही गयी जिसका सभी को इंतज़ार था। माधुरी का घर आज रंगीन बल्बों और झालरों से जगमगा रहा था। बेला, गुलाब और गेंदें के फूलों की खुशबुओं से सारा माहौल सराबोर था। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर तेज़ थी। रोहणी ने नाश्ता करते हुए किसी को भी उपवास न करने की सलाह जो दे दी थी।
“बिना उपवास के कन्यादान कैसे होगा और क्यों?” किसी ने तेज़ आवाज़ में पूछा तो रोहणी ने आखिरी कौर मुँह में डाल, सर को हल्का सा झटका दिया और बर्तनों को समेट कर रसोई में रखने के लिए चली गयी। इस ‘क्यों’ का जवाब अभी उसे देना था।
संध्या के समय वर और वधु ने वकील, मजिस्ट्रेट व गवाहों के समक्ष रजिस्टर में हस्ताक्षर किये। सभी की बधाइयाँ स्वीकार करते हुए उनके चेहरे बिजली के प्रकाश में और भी अधिक जगमगा उठे।
जीवन भर परम्पराओं और रूढ़ियों को कोसती हुई भी उन्हें स्वीकारने वाली माधुरी आज ईश्वर से शक्ति देने की बार-बार प्रार्थना किये जा रही थी। रिश्तेदारों व पति से आज न जाने वह कितनी बार उलझ चुकी थी। कई बार उसे लगा कि एक बार फिर वह टूट जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। पर नहीं! अब नहीं! अपने नए सूरज का उजाला देखे बिना वह टूटेगी नहीं।
मंडप में अग्नि के सम्मुख यज्ञ वेदी के निकट बैठे हुए रोहिणी व अनुज वैदिक रीतियाँ संपन्न कर रहे थे। आँचल गाँठ के पश्चात पंडित जी ने कन्यादान की रस्म शुरू करने का ऐलान किया। अपनी सारी शक्तियाँ बटोर कर माधुरी लगभग चीख़ सी पड़ी थी
“नहीं, नहीं होगा कन्यादान! कोई नहीं करेगा मेरी बेटी का दान !”
सभी आश्चर्य मिश्रित क्रोध और तिरिस्कार भाव से माधुरी की ओर देखने लगे।
“मैं ऐसी किसी परंपरा, किसी रस्मों रिवाज़ को नहीं मानूँगी जिसके कारण एक स्त्री सदियों से झुकती, सहती और प्रताड़ित होती आई है।”
बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये माधुरी ने सन्नाटे को चीरते हुए दोबारा कहना शुरू किया -
“फेरे होंगे, सातों वचन भी पढ़े जायेंगे और सुने भी जायेंगे पर कन्यादान। हरगिज़ नहीं। शब्दों पर जोर देते हुए उसने आगे कहा।
“वह कपड़े-लत्ते, रुपये-पैसों के समान अपनी बेटी का दान हरगिज़ नहीं करेगी। नहीं चाहिए वह मोक्ष जो बेटी को पराया करके ही मिले। ऐसे स्वर्ग का वह क्या करेगी जो कोख जाई को नरक में धकेल कर मिलेगा।”
“पर विवाह की रस्म कन्यादान को रस्म को पूरा किये बिना संपन्न नहीं होगी।” पंडित जी ने निर्णायक घोषणा की। पति ने भी आँखे तरेरीं।
“माफ़ कीजियेगा पंडित जी! विवाह तो हो चुका है। वह देखिए, रजिस्टर में दर्ज है। आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।” शालीन स्वर में माधुरी ने उस रजिस्टर की ओर इशारा किया जो वकीलों के हाथ में था। बरसों के दावानल को अहिस्ता से बहा देना चाहती थी वह।
“हाँ, हाँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे परंपरा को बदलने वाले। राहुल की शादी में देखेंगे तेरी ये चोंचलेबाजी।” बनारस वाली चाची सास नें हाथ नाचते हुए कहा।
“ज़रूर देखिएगा चाचीजी! मैं दान में मिली कन्या को अपनी कुललक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करुँगी। माधुरी के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास के भाव साफ़ नज़र आने लगे।
“चाहे जो भी हो जाये। नरक मिले या स्वर्ग। मोक्ष मिलेगा या नहीं। किसने देखा है। इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। किन्तु मैं अपनी बेटी का दान नहीं करुँगी। यह तय है।”
रोहिणी और अनुज के साथ राहुल भी माँ के गले लग गया। अपने निर्णय पर बच्चों का सहारा पाकर माधुरी गदगद हो उठी। मेहमानों की भीड़ में उपस्थित लड़कियों की नज़रें अपनी अपनी माओं की तरफ उठ गयीं शायद वे पूछना चाहती थीं कि क्या हम दान देने की वस्तु हैं आपके लिए?
माधुरी के भीतर का दावानल बांध तोड़ कर आँखों से प्रवाहित हो चला। अपने बच्चों को सीने से चिपकाये वह न जाने कितनी देर तक मन की शीतलता अनुभव करती रही। बहुत खुश और संतुष्ट थी आज वह कि आखिर कुछ हद तक थोथी परम्पराओं के मकड़जाल को काट सकी। अभी तो और कितने ही मकड़जालों को काटना बाकी है।
अपने रचे नए सूरज के उजाले में अपने तन-मन को भिगोती रही थी माधुरी।