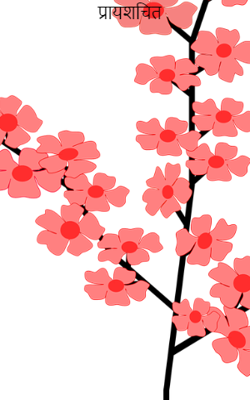मृग मरीचिका
मृग मरीचिका


शतरंज की बिछी हुई बिसात पर सबको मोहरा बना कर खेलती हुई प्रकृति कितनी निष्ठुर हो उठी होगी जब उसने मानव मन के अंदर 'प्यास' के अंकुर रोपे होंगे कि अपनी स्थिति से सदैव असंतुष्ट, थोड़ा सा और प्राप्त कर लेने की आतुरता में, किसी न किसी मृग मरीचिका के पीछे भागते रहने को अभिशप्त हम, जिस चीज को प्राप्त कर चुके होते हैं, उसके आस्वादन तक का वक्त नहीं होता है हमारे पास !
बचपन की न जाने कौन सी नासमझ, अंजान राह पर मेरी भी इस जिजीविषा से मुलाकात हो गई थी। एक थे हमारे देवेन्द्र भैया, जिंदगी भर जिनकी तरफ पूरी आँख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकी थी मैं ! सचमुच उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा जरूर था कि लोग अक्सर उनके सामने पड़ने से कतराते थे। वो ऊँचा गठीला शरीर, चौड़ी मूछें, घनी भँवों के बीच पड़े बल और आत्मविश्वास से दीप्त बेहद कठोर दृष्टि ! हम लोग तो खैर उस समय बच्चे थे, अच्छे अच्छे लोग उनके रोब-दाब के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। गुस्सा तो उनकी नाक पर कुछ ऐसे बैठा रहता कि आस-पास के सभी लोग मानों उनको शांत रखने के यत्न में ही व्यस्त रहते।
उनसे बेहिसाब डरने के बावजूद हमारे मन में उनके कार्य कलापों और उनकी उपलब्धियों के लिये एक अदम्य आकर्षण भी था। मैं अपने सभी भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और देवेन्द्र भैया के घर में ताक झाँक करनी हो या मौका मिलने पर चुपके से तलाशी ही लेनी हो, सबसे आगे मैं ही होती थी। वैसे तो हम लोगों का घर एक ही था पर बीचों बीच से दो हिस्सों में बाँट दिया गया था। हमारी तरफ वाले हिस्से में थी पर्याप्त अव्यवस्था और हम सात बहन भाइयों की अनवरत किच-पिच ! गृहस्थी का बोझ ढोते-ढोते पिताजी के कंधे झुक रहे थे और कनपटियों से सफेदी झाँकने लगी थी। उधर साल दर साल प्रसव के बोझ से टूटा, थका और बीमार शरीर लिये चुपचाप गृहस्थी के काम करते करते जाने कब माँ का सौन्दर्य भी अपनी लुनाई खो बैठा था। इसके विपरीत देवेन्द्र भैया की तरफ का हिस्सा किसी राजमहल की तरह सजा रहता।
उनके बड़े से बेडरूम में चमचमाता हुआ काला आबनूसी पलंग था जिस पर हाथी दाँत की कारीगरी देखते ही बनती थी... उसके मोटे मोटे गद्दे पर अनुसुइया भाभी अक्सर नख से शिख तक सजी धजी बैठी रहती थीं। रसोईघर जो उनकी तरफ जाते ही किचन में तब्दील हो जाता था, से तो जैसे भाभी को कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि महीने में कितने किलो अनाज की खपत है और कौन सी चीज किस भाव में आती है। उस जमाने में आयातित फ्रिज़ और पंखे से सजे धजे किचन को रमिया और चम्पा, दो नौकरानियाँ ही सँभालती थीं। गोश्त या अँग्रेजी खाना बनाने के लिए आता था वो भिंची भिंची आँखों वाला मुसलमान बावर्ची...! बड़ा सा गोल डाइनिंग टेबल, जिसके बीच का हिस्सा हाथ लगाते ही घूम जाता था, वर्दी में सजे-धजे वेटरों के जिम्मे था। रोज ही अलग-अलग डिजाइन की विदेशी क्राॅकरी अँग्रेजी ढंग से सजाई जाती, खुशबूदार फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता बीच में सजाया जाता, रिकार्ड प्लेयर पर अंग्रेजी संगीत का रिकॉर्ड लगता, घंटों मेहनत कर के सलाद की प्लेट सजाई जाती और बड़ी-बड़ी गड्ढेदार प्लेटों में सूप परोसा जाता तब देवेन्द्र भइया और भाभी का लंच और डिनर होता। हमेशा ही ढेर सारे मेहमान साथ होते जिसमें ज्यादा संख्या में अँग्रेज साहब और मेम होती थीं।
हमें समझ ही नहीं आता था कि इतने-इतने लोगों से देवेन्द्र भैया को आखिर काम क्या होता है। बहुत ध्यान देने पर उन लोगों की बातें अगर हमें सुनाई पड़ भी जाती तो भी वह अंग्रेजी गिटर-पिटर किसी को समझ नहीं आती पर उन नशे में धुत, रिकार्ड प्लेयर की धुन पर नाचते-गाते लोगों को देखने का कौतूहल ही अलग था। इस समय देवेन्द्र भैया का स्वरूप बदल जाता था। चुटकुले, ठहाके... भाभी का हाथ थाम उनके कदम से कदम मिला कर नाचते-गाते देवेन्द्र भैया कभी कभी पार्टनर भी बदल लेते थे। भूरे बाल और नीली आँखों वाली कोई मेम उनके काफी करीब आ जाती और लजाती शर्माती गुलाबी-गुलाबी भाभी किसी साहब का हाथ थाम कर थिरकने लगतीं। उन लोगों की बैठक उनके घर की सबसे खूबसूरत जगह थी।
दीवारों पर भुस भरे हुए चीते और बारहसिंगे सजाए गए थे और एक तरफ भैया का एक आदम कद तैल चित्र था, बंदूक लिये हुए! पूरी जमीन ईरानी कालीन से ढँकी थी... मोटे मोटे गद्दों वाला सोफ़ा सेट, छत से लटकता मधुर आवाज वाला झाड़फनूस जो रोशनी पड़ते ही पूरे कमरे को रंगों से नहला देता था .... आदम कद शीशे, साइड टेबल पर सजी चाँदी की सुराहियाँ और पूरे घर को चाँदी की तरह चमकाते रहने के लिए हर समय मुस्तैद, वर्दी में चुस्त दुरुस्त नौकर चाकर !
घर के नीचे के हिस्से में स्थित अस्तबल में स्वस्थ और खूबसूरत घोड़ों की मालिश करते साईंस, चाँदी मढ़ी हुई घोड़ागाड़ी जिसके चाबुक की मूढ़ सोने की थी। इस सारी चमक-दमक में लगातार बढ़ोतरी ही होती जाती थी कि न देखी न सुनी... ऐसी-ऐसी चमत्कारी चीज़ें, हम आँखें फैला कर देखते रहते थे... शहर में सबसे पहले भैया के यहाँ ही अँग्रेजी फिटन आई थी। काली, चमचमाती, बिना घोड़े के चलने वाली गाड़ी जिसको एक गोल पहिया घुमा घुमा कर चलाया जाता था। पीछे की सीट पर भैया जब अकड़ कर बैठते तो राह चलते लोगों के सिर अपने आप ही झुक जाते।
चोरी छिपे भैया का वैभव निहारते हुए, आश्चर्य से आँखे फैलाते हम, बंद आँखों में उन्हीं चीज़ों का सपना पालते, बड़े होते जा रहे थे। देवेन्द्र भैया मेरे ताऊ जी के बेटे थे। ताऊ जी ने अपने जीवन काल में पर्याप्त संपत्ति अर्जित कर के अपने इकलौते बेटे को विरासत में दी थी। इसके अतिरिक्त देवेन्द्र भैया स्वयं अँग्रेजी हुकूमत में एक बड़े अफसर थे। हजारों लोगों को उनसे काम पड़ता रहता था जिसके लिए वे लोग देवेन्द्र भैया को अपने सर पर उठाकर रखते थे। ऐसी-वैसी हैसियत का कोई आदमी उनके सामने पड़ने की हिम्मत तक नहीं करता था कि ज़रा-ज़रा-सी बात पर चाबुक उठा लेना मामूली बात थी। जाने कितने लोग ड्योढ़ी पर केवल सलाम बजाने आते... कभी-कभी तो लगता कि सवेरे का सूरज भी अपनी पहली किरण का अर्ध्य उन्हीं के यहाँ फेंकता होगा।
फिर सबकुछ बड़ी तेजी से परिवर्तित होने लगा। अँग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, भारी राजनीतिक उथल-पुथल और श्राप जैसे सीमा विभाजन के बाद एक स्वतंत्र देश आकार लेने लगा। सत्ता के दुश्मन जिन्हें पहले बागी और अस्पृश्य समझा जाता था अब क्रान्तिकारी के नाम से सम्मानित होने लगे और अँग्रेजी सत्ता के ओहदेदारों के लिये लोगों के मन में छिपी हुई घृणा स्पष्ट रूप से सामने आ गई। देवेन्द्र भैया पर इन बदलती परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना ही था अतः एक दिन अपना घर किसी अजनबी के हाथ बेचकर उन्होंने अनुसुइया भाभी के साथ शहर छोड़ दिया !
बहुत कुछ बदल गया था, नहीं बदला तो बस मेरी आँखों में पलता वह स्वप्न... बड़ा सा आबनूसी पलंग, सखी सहेलियों से घिरी, वैभव के पालने पर झूलती, साहबों और मेम साहबों के साथ लंच और डिनर लेती हुई मैं.... दरवाजे पर बँधे हुए घोड़े हाथी और सलाम करता हुआ एक पूरा शहर !
मुझे याद आते हैं वो पल जब आँचल का एक सिरा अरूण के साथ बाँध कर मैं अग्नि के गिर्द फेरे ले रही थी। कितनी खुश थी, कि कमसिन उम्र में भी मुझे इस सत्य का पूरा भान था कि अरूण का पद और वेतन देवेन्द्र भैया से भी बढ़ चढ़ कर है। उन पलों में मुझे लगता था जैसे एक साम्राज्ञी सी किस्मत लेकर आई हूँ मैं, कि जो भी चाहा मुझे मिल गया। अरूण किसी सपनों के शहजादे की तरह ऊँचे और बलिष्ठ थे, गोरे रंग पर फबती घनी काली भँवें, भावप्रवण आँखें, चौड़ी मूँछों में छिपी सदाबहार स्मित उन्हें बेहद खूबसूरत करार देती थी और उनकी आँखों की गहराई में से झाँकती एक शालीन प्रबुद्धता ऊँगली पकड़ कर उन्हें साधारण की पाँत से बाहर ला, विशिष्ट साबित कर देती थी।
तो क्या मुझे भी अनुसुइया भाभी की तरह जीवन के सारे सुख परोसे हुए मिल जाएँगें ? फिर जब वास्तविकतासे सामना हुआ तो सपनों को मन की किसी बंद कोठरी में दफ़न कर देना पड़ा था। बड़े से संयुक्त परिवार में अरूण का बड़ा वेतन किसी बड़े सम्मान का अधिकार था न विशेष अधिकार का ! बाकी सभी पुरुष सदस्यों की तरह अरूण भी निःसंकोच परिवार के मुखिया, अपने बड़े पापाजी को पूरा वेतन पकड़ा कर निश्चिंत हो जाते।
यूँ कमी हमें किसी चीज की नहीं थी... त्योहारों पर कीमती गहने-कपड़े भी बनते ही रहते थे, पर अनुसुइया भाभी की तरह सज-धज कर, पलंग पर बैठ, हुक्म चलाने का सुयोग कभी नहीं आया। यहाँ न कोई ड्योढ़ी पर सलाम बजाकर अपनी एक झलक दिखा देने को उतावला ही रहता था, न मेवों और मौसमी फलों की डलिया ही उतरती थी। सवेरा होते ही रसोईघर में जो सामूहिक लंगर शुरू होता वह देर रात तक चलता रहता। ढेर सारे सदस्यों वाला घर, नौकर-चाकर, आए-गए लोग... काम तो मानों निपटता ही नहीं था। रसोई की खिट-खिट, हर निर्णय में परतंत्रता, अपने से कम पढ़ी जिठानी और गरीब घर की देवरानी को बराबर का दर्जा देने की मजबूरी... न एक टेबल पर अरूण के साथ बैठकर खाना खाना संभव न उनके किसी मित्र के सामने जाने का रिवाज़... यूँ तत्कालीन स्त्रियों की तुलना में हम काफी सुखी थे कि हमलोग नाते-रिश्तेदारी के अतिरिक्त घूमने भी ले जाए जाते थे और कभी कभी घूँघट में सिमटी हम औरतों की मंडली, बड़ी बूढियों के संरक्षण में सिनेमा, सर्कस और रामलीला भी जाती रहती थी।
सही शब्दों में कहूँ तो सबकुछ होते हुए भी उस स्वामित्व का अभाव था जो अनुसुइया भाभी को अनायास ही मिला हुआ था। उनके ठाठ-बाठ याद आते ही मुझे अपना सबकुछ तुच्छ लगने लगता। एक असंतोष मन में सदैव मुखर रहता कि चाह कर भी मैं अपनी आकांक्षाओं और हकीकत के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रही थी और परोक्ष-अपरोक्ष इसका असर मेरे रिश्तों और दाम्पत्य पर पड़ता ही होगा। यह सब शायद यूँ ही चलता रहता यदि उन दिनों मैं अपनी चचेरी नन्द के घर एक शादी के उत्सव में न जाती जहाँ एकाएक अनुसुइया भाभी से भेंट हो गई।
वैसे उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल काम था... कहाँ वो रूप यौवन और प्रसाधनों से जगमगाती महमहाती काया और कहाँ ये मोटी पुरानी साड़ी में लिपटा जीर्ण, आभूषण रहित शरीर... न हाथों में कड़े, न माथे पर बिंदिया ! एक बार तो जी धक् से रह गया... कहीं देवेन्द्र भैया को तो कुछ नहीं हो गया ? पर तभी उनकी माँग पर नजर पड़ी तो सिंदूर की एक महीन रेखा किसी सांत्वना भरी हथेली की तरह मन को सहला गई। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हुआ, कैसे पहचान न सकी इन्हें ? कहीं से कोई साम्य तो हो... पर है न... आँखें वही हैं, यहाँ तक कि उनमें भरे हुए भाव तक वही हैं। व्यथा वेदना की इस छाया, इस दर्द को तो मैंने तब भी इन आँखों में पलते देखा है, भले अपनी कम उम्र के कारण समझ न पाई हूँ।
पता चला देवेन्द्र भैया अब किसी दूसरी औरत के साथ रहते हैं और अनुसुइया भाभी को उन्होंने घर से निकाल दिया है। जी धक् से रह गया ! जिस औरत को नख से शिख तक सोने से मढ़ कर, कीमती चीज़ की तरह सँभाले रखा था, एक काम तक नहीं करने दिया कि उनके हाथ पैर गंदे न हो जाएँ, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर मायके में, निर्दयी भाई भाभियों के बीच कैसे फेंक सकते हैं ? ऐसा भी होता है क्या ? पत्थर की शिला बनी अनुसुइया भाभी को पिघलाना आसान नहीं था। फिर पता चला कि उन्हें पहचानने में मैंने भूल की थी कि उन आँखों में भी अब परिवर्तन आ चुका था। हर चाह और भाव से बेज़ार, किसी अंतिम पल का इन्तज़ार करती उन आँखों मे जो धा, वो दर्द नहीं, विरक्ति कहलाएगा... संसार से विरक्ति, संबंधों से, और स्वयं से भी! "आपके भैया की पत्नी तो मैं कभी बनी ही नहीं।
मेरी हैसियत तो केवल आपके ताउजी की बहू की थी।" न जाने क्या बताने जा रही थीं वो... हतप्रभ थी मैं ! "आपके भैया तो मेरे उस घर में जाने के पहले से ही शादीशुदा थे। अग्नि के गिर्द फेरे लिये बिना ही उनका एक अलग परिवार था, बच्चे थे, खुशियाँ थीं। आपके ताउजी ने उसे स्वीकार नहीं किया था, इस बात का बदला लेने के लिए आपके भैया ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ये भी हो सकता है कि मुझे देखते ही उन्हें अपनी हार याद आती हो, क्रोध आता हो, जो कितने ही निरीह नौकर-चाकरों पर उतरता। बाद के दिनों में जब उनका सामाजिक दायरा बढ़ा तो मुझे उनकी बैठक में सजी हुई भुस भरी जानवरों की खालों की तरह, एक लुभावनी सामग्री का सम्मान मिल गया जिसके पास अपना कुछ नहीं होता... वह जिसके अधिकार क्षेत्र में होती है, उसकी सम्पत्ति कहलाती है। किसी निर्जीव वस्तु की तरह झाड़-पोंछ कर मैं आपके भैया की बगल में बिठा दी जाती थी। मुझसे ज्यादा जरूरी तो किचन में काम करने वाली नौकरानियाँ थीं उस घर में !"
"क्या कह रही हैं भाभी आप ?" मैं उत्तेजना से चीख ही पड़ी थी... "तो क्या भैया कहीं और जाकर रहते थे ? इतने वर्षों तक साथ रहकर भी हमें ये मालूम ही नहीं ?"
जाने क्यूँ ऐसा लग रहा था कि केवल भैया को बदनाम करने के लिए ही तो वे यह सब नहीं कह रहीं ?
"आप लोग बच्चे थे, नहीं पता होगा, वरना पूरे शहर को पता थी ये बात ! और यह कोई नई या असंभव बात तो थी नहीं, हर साधन संपन्न व्यक्ति यही करता है।" उस समय के संदर्भ में सचमुच ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि ज्यादा से ज्यादा औरतों से जुड़ना शान की बात मानी जाती थी और चाहे न चाहे ब्याहताएँ अक्सर इन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा ही लेती थीं। सामाजिक स्तर पर पत्नी का ओहदा होना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है... फिर पत्नी को घर से निकाल देने का क्या औचित्य ? "अंग्रेज गए, तो आपके भैया की नौकरी और रोब-दबदबा के साथ हर महीने की मोटी तनख्वाह भी चली गई। उनकी वफादारी, जिसकी रोटी वो खाते थे, अब अपराध कहलाने लगी। न जूते की नोंक पर रहने वाले कीड़े-मकोड़े जैसे लोगों के हाथ अपनी पगड़ी पर बर्दाश्त किया जा सकता है है और न ही सीमित हैसियत के साथ उसी शहर में रहना संभव था। तब अगर एक नये अन्जाने परिवेश में, किसी नये परिचय के साथ जा रहे हों तो अनचाही और निपूती पत्नी की क्या जरूरत ? वह क्यों नहीं जिसे कच्ची उम्र से, स्वयं से बढ़कर चाहा था ?"
एक मोटी बूँद के नीचे दब, उन आँखों की विरक्ति धुँधला उठी। दर्द कुछ इतना तीखा हो उठा था कि मेरा सर्वांग सिहर उठा... यही है वह स्त्री, जिससे जीवन भर मैं ईर्ष्या करती रही हूँ ? जिसके जैसा जीवन पाने के लिये जीवन भर शिव अर्चना की है, भूख सह कर व्रत रखे हैं ? मेरी भीगती पलकों से आँसू के साथ कुछ और भी दरक कर बह रहा था, जिसे भाभी से छुपाने के लिये मैंने आँचल में पोंछकर मुट्ठी में दबा लिया।