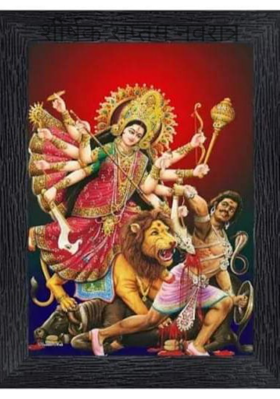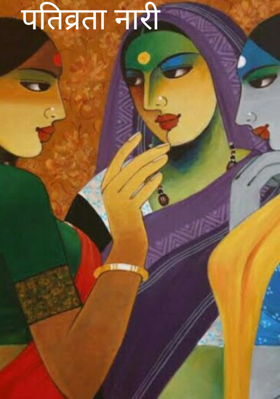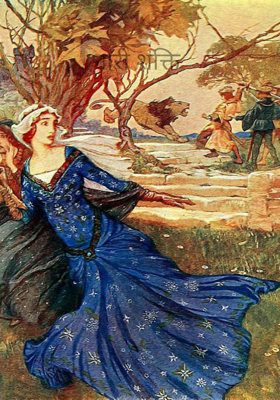व्यथित विजेता
व्यथित विजेता


दो शब्द:
क्या एक विजेता कभी व्यथित हो सकता है? इतिहास के जानकार कदाचित सम्राट अशोक और उनके कलिंग-विजय का प्रकरण उद्धृत करेंगे। सत्य ही, वह शांतिप्रिय सम्राट कलिंग युद्ध में जीत के पश्चात व्यथित थे, वह जीत जिसने अनेक पुरा युद्धों की ही भाँति एक बार पुनः वसुधा को उसी की संततितयों के शोणित में स्नान कराया था। किन्तु उस व्यथा का मूल कारण क्या था? इतिहास साक्षी है उस व्यथा का तार सम्राट अशोक की राज्य विस्तार की प्रवृत्ति और कभी तृप्त न हो सकने वाली तृष्णा से जुड़ा था। किन्तु अगर वह युद्ध स्वयं के अधिकारों का हनन एवं किसी भी प्रकार की संधि - और विवेक - को अस्वीकार करने वाले किसी क्रूर शासक के विरुद्ध किया गया होता?
इस प्रश्न का उत्तर जानने - और उसपर विवेचन करने - के लिए हमें इतिहास में कुछ और पीछे जाने की आवश्यकता है। द्वापर में शांतिप्रिय राजा युधिष्ठिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध - और उससे हुए भारत के अनगिनत सुतों के पतन - से विजयी होने के पश्चात भी उतने ही व्यथित थे जितना सम्राट अशोक कलिंग-विजय के पश्चात। किन्तु उनकी व्यथा मात्र एक संत-मनुज के निर्मल हृदय की आकुल पुकार थी। वह पुकार जो एक भावुक संत को तो तड़पा सकती है किन्तु जिसका आवेग शस्त्र और शास्त्र के अद्वितीय संगम - पितामह भीष्म अथवा भगवान कृष्ण - के समक्ष मंद पड़ जाता है। अर्थात जब युद्ध स्वयं के न्यायसंगत अधिकारों के रक्षण के लिए किया गया हो, तब अव्यवहारिक अथवा संत-हृदय-मनुष्य के अतिरिक्त किसी को उस युद्ध में हुई भीषण हानि के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानना भारी भूल होगी। तो क्या ऐसे युद्ध में कोई विजेता किसी भी कारणवश व्यथित हो सकता है?---
“व्यथित विजेता” कोई कथा-काव्य नहीं है। यद्यपि इसमें उद्धृत कुरुक्षेत्र-युद्ध के प्रसंग वास्तविक हैं, किन्तु मेरी इस काल्पनिक कृति जैसा प्रकरण महाभारत में कहीं नहीं आया है। मैं जो बात पाठक-गणों के समक्ष रखना चाहता था, वह बात निश्चित ही महाभारत के प्रसंगों को उद्धृत किये बिना भी कही जा सकती थी; किन्तु महाभारत जैसी पृष्ठभूमि और उसमें वर्णित सभी पात्रों के चरित्र के माध्यम से अपनी बात कहना मेरे लिए सर्वथा आसान बन गया। उदाहरणार्थ, वीर अर्जुन - इस कृति का केंद्रबिंदु - के विषय में लिखते हुए महाकवि श्री मैथिलि शरण गुप्त जी ने “जयद्रथ-वध” में लिखा है:
“खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य को यों कर रहे,
निश्चिन्त, निर्भय, सामने ही मोद नद में तर रहे।
है धन्य अर्जुन के चरित को, धन्य उसका धर्म है;
क्या और हो सकता अहो! इससे अधिक सत्कर्म है!
वाचक विलोको तो जरा, है दृश्य क्या मार्मिक अहो?
देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शील यों धार्मिक कहो?
कुछ देखकर ही मत रहो, सोचो विचारो चित्त में,
बस, तत्व है अमरत्व का वर-वृत्तरूपी वित्त में;
यह देख लो निज धर्म का सम्मान ऐसा चाहिए,
सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए।
सहृदय जिसे सुनकर दृवित हों चरित वैसा चाहिए,
अति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए!”
अर्थात अर्जुन के प्रिय पुत्र अभिमन्यु का हंता - सिंधुनरेश जयद्रथ - अर्जुन के ही क्षात्र-धर्म और युद्ध-मर्यादा की शीतल छाया में अभय होकर स्वयं अर्जुन का ही उपहास जैसा दुस्साहस कर सकने की स्थिति में था। कैसी अद्भुत निष्ठा, निज धर्म के प्रति!
और अंत में, यद्यपि किसी भी कृति के सभी सर्ग किसी माला में सावधानीपूर्वक पिरोए गए भिन्न-भिन्न पुष्पों की भाँति होते हैं, तथापि इस कविता का तृतीय सर्ग बाकी कविता से पृथक करके भी पढ़ा व समझा जा सकता है। किन्तु ऐसे में, वहाँ उपयुक्त शब्द “समर” को उसके शाब्दिक अर्थ से नहीं, अपितु मानव-जीवन के किसी चुनौतीपूर्ण प्रसंग की तरह समझा जाना चाहिए। और “समर की कीच / समर की कालिमा” आदि का अर्थ उस प्रसंग में मानव द्वारा अपनाए गए अशुभ साधन या साधनों से है। ये अशुभ साधन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं: (१) जो उपरोक्त प्रसंग में इतने सामान्य हो चुके हैं की समाज ने उनको ऐसे प्रसंग का अभिन्न अंग मान लिया है या (२) जिनको मनुष्य बाह्य जगत की दृष्टि से ओझल रखने में सफल हो जाता है। किन्तु क्या निज-धर्म पर अटूट आस्था रखने वाले मनुष्य की आत्मा उसके द्वारा उपयुक्त इन अशुभ साधनों को उतनी ही आसानी और तत्परता से स्वीकार कर लेती है जितनी उसकी विजय-कामना?
व्यथित विजेता
(१)
अहो! क्या दृग-लुभावन दृश्य है यह
नहीं हर वीर को जीवन में उसके प्राप्य है यह
कुरुक्षेत्र में जय का गान गाकर
समूचे राष्ट्र को अपना बनाकर
हृदय में जीत का उत्साह लेकर
समस्त संसार को सौगात देकर
चले हैं पाण्डुपुत्र अब राज-भवन में
स्वर्णिम स्वप्न सजाए पुलकित नयन में
निष्कंटक सदा अब राह होगी
सभी को धर्म की अब चाह होगी
न फिर लाक्षा-भवन निर्माण होगा
वधू-जन का सदा सम्मान होगा
किया अपमान कितना कौरवों ने
दिया वनवास हमको कौरवों ने
अतीत अपना अत्यंत दुःखद है
कथा का अंत सचमुच ही सुखद है
सभा के मध्य में जयकार गूँजी
लगा गाण्डीव की टंकार गूँजी
सभी जन स्तब्ध से हो देखते थे
धनुर्धर श्रेष्ठ की जय बोलते थे
दिया दर्शन जिसे था खुद हरि ने
बहायी ज्ञान-गीता मध्य अरि के
उचित ही उस सभा का तूर्य था वह
उदित होता हुआ सा सूर्य था वह
प्रखर कान्ति चमकती थी नयन में
सभी जन गान करते थे भवन में
“मही का श्रेष्ठ योद्धा है धनञ्जय
दिया भगवान ने भी था समन्वय
समर में शत्रुओं का नाश करके
स्वयं के धर्म का सम्मान करके
मही पर व्याप्त है अब पार्थ-गर्जन
हुआ है धर्म का पुनः आज सर्जन”
स्वयं की इस प्रशंसा को श्रवण कर
भगीरथ कार्य कर बोला, प्रभु की वह शरण धर
“प्रभो! मेरे सभी हों कर्म बस तुमको समर्पित
करूँ हर कर्म जीवन में, तुम्हीं से होके प्रेरित
दिया था तुमने मुझको ज्ञान गीता को सुनाकर
समर के मध्य में, निस्तेज मन में प्राण भरकर
दिखाया पथ, मुझे उस मार्ग पर चलना सिखाया
बिना मोहित हुए परिणाम से, कर्म करना सिखाया
मिलेगी जीत अथवा हार, इसको सोचना क्या?
जो नौका जा रही मझधार में, उसे रोकना क्या?
विजय का मार्ग है भगवान! तुमसे ही प्रकाशित,
मुझे साधन तुम्ही ने है बनाया, जीत के हित”
सभा में फिर सभी का करके वंदन
श्री चरण में सर झुकाए पाण्डु-नन्दन
स्वयं के ज्येष्ठ भ्राता को नमन कर
किया अभिषेक उनका सजल नयन धर
सभा में यूँ विजय का गान गाकर
उपस्थित सब जनों से मान पाकर
घरों को लौट आए पाण्डु-नन्दन
प्रमुदित थी वहाँ जनता-जनार्दन
(२)
शयन-कक्ष में अकेला है धनञ्जय
मगर क्यों हो रहा उसको है संशय?
स्वयं से पार्थ वार्ता कर रहा है
निराशा से मगर क्यों भर रहा है?
विजय श्री कर चुकी है वरण जिसका
रिपु जीवित नहीं है एक उसका
भला क्यों वह विकल-सा हो रहा है?
विषम किस वेदना में रो रहा है?
(अर्जुनोवाच)
कहूँ कैसे धनुर्धर श्रेष्ठ हूँ मैं?
कला-रण में सभी से ज्येष्ठ हूँ मैं?
कहीं जो धर्म-सम्मत युद्ध होता
महाभारत समर से शुद्ध होता
विजय श्री क्या वरण करती हमारा
नहीं लेते अगर छल का सहारा
शरों की सेज़ क्या निर्माण होती?
पितामह की भुजा निष्प्राण होती?
नहीं लेते सहारा जो कपट का
शिखण्डी के अनोखे भाग्य-तप का
बनाकर ढाल उसको मैं लड़ा था
समर में तब विजय-झंडा गड़ा था
नहीं जो भाग्य उसका साथ देता
कभी क्या निहत होता परशु-जेता?
समर वह शूर-वीरों का नहीं था
बना मैं छली-कपटी योद्धा मही का
कभी क्या शपथ मेरी पूर्ण होती?
नहीं माया की गर तब साँझ होती
अगर मैं शकटव्यूह को भेद पाता
भला क्या सूर्य पर तब ग्रहण छाता?
हरी किञ्चित नहीं माया रचाते
मेरा बल-शौर्य ही मुझको जिताते
मगर सञ्चित पराक्रम रह गया कम
नहीं नर ग्रहण करता सूर्य का तम
[प्रभो! वह तिमिर को रौशन बनाता
अमावस में रवि कृत्रिम उगाता]
प्रभो! कान्ति क्या मेरी तम नहीं है?
तिमिर की कालिमा से कम नहीं है
सदा वह जीत का सम्मान करती
नहीं निज साधनों का ध्यान करती
कभी क्या कर्ण को मैं पा भी पाता
कवच-कुण्डल कहीं वो संग लाता
इसी से इंद्र ने तब छल किया था
स्वयं के पुत्र को कुछ बल दिया था
जगत है जानता था कर्ण दानी
कवच-कुण्डल सुशोभित महा वरदानी
अजय था वीर वह कुण्डल-कवच में
मगर हारा जनक से, वह प्रपंच में
प्रभो! कितना पतन मैंने कराया
पिता को चोर-भिक्षुक था बनाया
गए तो विप्र के थे वेश में वे
मगर लौटे हृदय में क्लेश ले वे
नहीं एकघ्नी से क्या भीत थे हम
मगर आकुल थे फिर भी जीत को हम
नहीं बस भीम-सुत उस दिन मरा था
सदा को शीश मेरा भी झुका था
स्वयं की मृत्यु से भयभीत होकर,
बिना करे युद्ध ही निज-जीत खोकर
घटोत्कच को बनाया ग्रास हमने छल-कपट का
प्रभो! साक्षी रहेगा वह हमारे कर्ण-भय का
हँसी नटनागर की उस दिन की,
कभी भूल क्या पाऊँगा
विजय-कामना के हित माधव,
कितनों की बलि चढ़ाऊँगा
“पार्थ की हार, कर्ण की जय”
प्रभु की मुस्कान बताती थी
मुझको मेरा ही परम-शत्रु,
केशव की हँसी बनाती थी
हुआ हत कर्ण संगर में यथा रथ-हीन होकर
मरा था वीर वह उस दिन धनु-शर-जीत खोकर
प्रभो! वह दृश्य आँखों से मगर हटता नहीं है
समर में हारकर भी कर्ण अब हँसता कहीं है
मगर रोता अभी तक है प्रभो! अंतर हमारा
समर में क्षात्र-मूल्यों से किया हमने किनारा
बना मैं कर्ण-जेता युद्ध-नियमों को जलाकर
विजय का ताज पहना पुण्य-कर्मों को गलाकर
मगर यह ताज कण्टक-का प्रभो! अब लग रहा है
विजयी में भाव जेता का नहीं क्यों, जग रहा है?
(३)
विजय श्री क्यों नहीं उल्लास भरती?
विजेता के हृदय को व्यथित करती?
विजय का क्या चरित इतना मलिन है
इसी के हेतु नर करता क्या रण है?
समर में निखिल निज को झोंक देता
नहीं वह धर्म की भी रोक लेता
विजय के हित पतन अपना कराता
विजय को खोजता पाताल जाता
मगर जब जय-कमल का पुष्प खिलता
समर की कीच के वह मध्य मिलता
मगर आकुल हुआ नर कब सँभलता
समर की कीच में भी पाँव धरता
उसे निज वैरी जब दिखते वहाँ पर
मनुज का धर्म फिर जाए कहाँ पर?
प्रभो! पर नेतृ-नायक क्या नहीं वो?
समर की कालिमा छूता नहीं जो
सदा है शुभ्र जो निज साधनों से
नहीं डिगता भयंकर आतपों से
ज़हर की कीच में जब पाँव धरता
स्वयं के तत्व को नित स्मरण करता
नहीं निज कोष विष का खोलता है
हलाहल में नहीं विष घोलता है
हलाहल क्या कभी निर्माण होता?
नहीं जो धर्म गहरी नींद सोता?
स्वयं का कोष विष का खोलते सब
मगर इतिहास को हैं बोलते सब
“हलाहल के सृजन का दोष उसका
खुला पहले गरल का कोष जिसका
प्रथम विष कोष वैरी का खुला था
समर में विष उसी दिन से घुला था
किया मैंने जो कुछ भी, धर्म ही था
काल-देश के अनुरूप, सत्कर्म वही था”
प्रभो! यह सांत्वना झूठी नहीं क्या?
मनुज की साधना रूठी नहीं क्या?
मुखौटा धर्म का पहने मनुज ने
किए हैं कर्म कितने ही दनुज से
मगर आरोप औरों पर लगाकर
धर्म के तत्व को पंगु बनाकर
स्वयं का तो पतन नर है कराता
कलुष वातावरण जग में बनाता
(४)
(अर्जुनोवाच)
प्रभो! निज पाप थे कितने भयंकर
विषम विष वेदना से क्षुब्ध अंतर,
मुझे अब तक प्रताड़ित कर रहे हैं
मेरे गौरव को प्रति-पल दलित वह कर रहे हैं
कभी क्या त्राण इससे पाऊँगा मैं
पतन के गर्त में या जाऊँगा मैं?
मिलेगी क्या मुझे शांति कहीं पर
प्रभो! है फैलती कान्ति मही पर
मगर यह कान्ति अब तड़पा रही है
मेरा अंतर मलिन-सा कर रही है
नहीं मिलता कहीं भी चैन मुझको
मेरे आँसूं, नहीं देखे जगत इनको
प्रभो! यह आत्मा कितना मुझे धिक्कारती है
‘धनुर्धर-श्रेष्ठ’ को कर्कश-ध्वनी सी मानती है
प्रभो! इस भाँति निज से मैं भला, कब तक लड़ूँगा
सदा क्या आत्म-ग्लानि की अनल सहता रहूँगा
प्रभो! अंतर सदा को हो चुका कलुषित हमारा
मगर दिखता नहीं, मुझको कहीं, कोई सहारा।