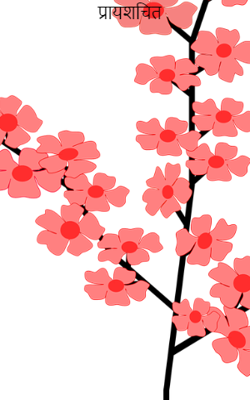हिरामन दादा
हिरामन दादा


" ए ! साहेब हम अकेले रहते हैं। सब बेटा-पतोहू अलग हो गए हैं। फुलबसिया भी तो हमसे वादा करके पहिलहीं छोड़ गई, नहीं तो बहुत साहस मिलता बूढ़ारी में ..."
बैंक मैनेजर साहब जो 30-32 बरस से ज्यादा के नहीं थे रेमण्ड के कपड़े से बने नीले और सफेद चेक शर्ट में खिल रहे थे और इस मैनेजर की कुर्सी पर 6 साल से विराजमान थे। ये गाँव उन्हें ज्यादा भाता नहीं था, गाँव से 20 किलोमीटर दूर पास ही के टाउन में रहते थे। रोज अपने लाल चर-चकिया से अप-डाउन करते थे राजापुर गाँव में।
हिरामन की दुहराती हुई बातों से खीज कर बोले :
"दादा ! अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा लीजिए नहीं तो आपके वृद्धा पेंशन आने में और देरी होगी और आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ये आप तीसरी बार यहाँ मेरे केबिन में आए हैं, अब आप जाइए मेरा लंचटाइम हो गया है।"
ददा अपने बाँस की एकदम चिकनी लाठी लेकर अपने बस्ती की ओर चल पड़े ।
यह बस्ती हर एक गाँव में हुआ करती है जहाँ केवल चर्मकार जाति के बहुजन बसा करते हैं। सरकार इन्हें आरक्षण की बैसाखी पकड़ाने की बहुत कोशिश की पर उनमें-से कुछ ही सरकारी दफ्तरों तक पहुँच पाए। इनके पिछड़ेपन को बरकरार रखने में समाज के जिम्मेदार वर्ग के साथ सरकारी स्कूलों का भी घाल-मेल रहा। बस्ती में 20 कच्चे घर हैं लाल -पथरीली मिट्टी से बने हुए, जिनपर या तो गोबर का लेप लगा होता था या पीली मिट्टी का जो गाँव से 2 किलोमीटर दूर बबूल के जंगल के करीब से लाया जाता था। और बस तीन पक्के घर जिनके बेटों ने सफाई कर्मी की सरकारी नौकरी पा ली थी 2002 के रिक्रूटमेंट में।
हिरामन ददा की अभी उम्र ज्यादा नहीं हुई थी। वो 53-54 के करीब के थे।
गाँव के बाबू साहब की इनपर इतनी कृपा दृष्टि बनी रही कि 16-17 की उम्र में दिन-भर खटने के बाद वेतन की जगह दोपहर में चार सूखी रोटी और आकड़-पत्थर से भरपूर पनछोछर रहर की दाल और साथ में पोषण रहित हड्डियों का ढांचा मिला था।
ये तो अच्छा हुआ कि फुलबसिया दादी से इनका लग्न हो गया नहीं तो वहाँ दिहाड़ी मजूरी कर-कर अब तक दूसरा जन्म ले चुके होते।
फुलबसिया दादी का चेहरा गेंहुआ और गोल था। आँखों में कोई जादू था जिससे ददा एकदम काबू में रहते थे।
फुलबसिया दादी ददा की बस पत्नी भर नहीं थी अच्छी दोस्त भी थीं। ये दोनों सुबह होते ही काम के लिए निकल पड़ते। उन दिनों गाँव में अस्पताल , डाकघर और बैंक के निर्माण कार्य एक के बाद एक हुए थे। शाम को लौटते वक्त दोनों बाज़ार से साक-सब्जी ले आते और मिलकर खाना पकाते। उन दिनों दादा के चेहरे पर वैसी ही चमक आ गई थी जैसे कोई नवजात अपनी माँ के दूध से पोषित हो रहा हो, ददा को रोटियाँ नहीं बनाने आती थी तो दादी ने ही सिखाया था।
दादी कहती थी, " दुनिया बहुत ज़ालिम है मेरे जाने के बाद आपको पतोहुएँ कितने दिन तक बनाकर खिलाएगा! " ददा और दादी ये तोता-मैना की जोड़ी बस 28 बरस ही चली सकी थी। दादा तो फुल रुमानियत में हमेशा से उनके साथ थे पर दादी बीच में सफ़र छोड़ चली गई।
दादी को किसी अनजान बीमारी ने जकड़ लिया था और हाँ उन दिनों सरकारी अस्पताल में उतनी फसिलिटी भी कहाँ थी ! वो जब दुनिया छोड़ गई तो ददा लोगों के सामने तो खुद को संभाल लेते थे पर अकेले में उनके आँसू रुकते ना थे।
बच्चे बड़े हो गए थे दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पंख निकल आए थे। तीनो सपूतों की शादी हो गई थी। छोटे बेटे सुगाराम ने तो खुद के पसन्द से ही पास के गाँव में शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही सबों ने अपने अलग-अलग घर बना लिए थे।
ददा दिन में कहीं- न - कहीं काम कर लेते और जो मिलता उससे कुछ राशन और पान-पत्ती ले आते थे पर फिर भी कई सालों बाद भी हिरामन ददा का मन तो अपनी उसी हीर फुलबसिया में लगा रहता था। कभी- कभी दादी की कोई बात याद करते-करते मन ही मन मुस्का देते और उनकी आँखें ये सोचकर नम हो जातीं , "उन्होंने एक सच्चे साथी को खो दिया है ।"
ददा ज़्यादा पढ़-लिख नहीं पाए थे। पर रुपए-पैसे का हिसाब-किताब रख सकते थे। वो अक्षर पहचानना और टेढ़े-मेढ़े ढंग से सिग्नेचर करना भी जानते थे। ये सब सरकारी स्कूल माटसाब गुप्ता जी की मेहनत का नतीजा था कि ददा तीसरी तक पास हो सके थे।
उनका इस उम्र में कोई सच्चा साथी बचा भी था तो वो उनका वृद्धा पेंशन। और कुछ मेहनत अब भी कर सकते हैं। पर आठ घण्टे वाली मजदूरी अब उनके बस की ना थी।
"मेरा आधार कार्ड तो बन ही नहीं पाया था"
ये बात ध्यान में जब-जब आए ददा घबरा जाते। पिछली गर्मी में इन्हें लू लग गई थी फिर भी ये शिविर में गए थे जो सरकारी स्कूल के हॉल में लगी थी। पर कुछ टाइपिंग गड़बड़ी के कारण इनका आधार कार्ड नहीं बन पाया था। उन्हें ये भी पता चला की सरकारी आवास का पैसा भी इनके ही एकाउंट में आएगा तो ददा और भी चिंतित हुए।
बहुत कोशिश के बाद इन्हें कोई तोड़ नहीं मिल पाया आधार कार्ड का।
तब एक दिन सहसा किसी के मुँह से सुना ,
"दखिन टोले से 6 किलोमीटर दूर किष्नापुरी गाँव में आधार कार्ड का शिविर लगा है। "
इन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन वो किष्नापुरी जाएंगे। सुबह 8 बजे नहा-धोकर तैयार हो गए और खड़ंजा रास्ता पकड़कर चल पड़े।
जून का तपता महीना था, 9 बजे ही धूप तीखी हो गई। दो किलोमीटर दूर पहुँचने पर इनका गला सूखने लगा, कमर और जोड़ों में दर्द उठने लगा। उन्हें आजकल कुछ कमजोरी भी थी। आस-पास कोई घर भी नहीं था ना ही कोई बैठने का स्थान कि थोड़ा रुक कर सुस्ताया जा सके। कुछ दूर चलते ही उनकी सांस फूलने लगी।
उन्हें ऐसा लगा उनका अंतिम क्षण निकट आ गया हो और वो गश खाकर गिर पड़े। कुछ ही पल में अपनी माँ का दुलार से हीरा बाबू कहना उन्हें याद आ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी माँ अभी उन्हें गोद में लिए हुए है और बालों के बीच कंघी कर रही है। बेटे-पोते-पोतियों के चेहरे बार बार उसके सामने घूम रहे थे।
उनकी फुलबसिया के ललाट की वो लाल बिंदी जिसमें वो गिरे जा रहे हों उन्हें ऐसा लग रहा था। फुलबसिया दादी जवानी के दिनों में जैसे मुस्काती थी एक बार उनकी ओर मुसकाई और ददा भी उनकी ओर देखकर आख़िरी बार मुस्काए और उसी अनन्त लाल बिंदी में सिमटते चले गए।
गाँव में इनके बेटों को ख़बर मिली। तीनों ने मिलकर अच्छे से दाह-संस्कार किया। बिरादरी में भोज हुआ। जिनको जीतेजी अपने बेटों से प्रेम ना मिला मरने के बाद उनके बेटों ने कुछ दिनों तक उनकी कमी महसूस की।
उनके बैंक का पासबुक बिना आधारकार्ड के लिंक हुए वैसे ही सुना रहा जैसे काशी के तट पर गँगा के शीतल धारा में अपनी सफ़ेद सुनी सूती साड़ी को धोती एक विधवा की मांग।