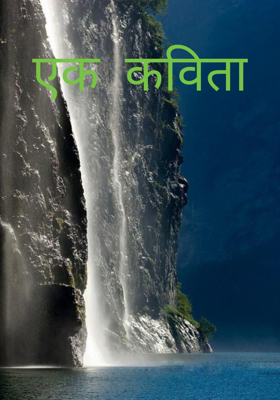मैं और मेरी ज़बान
मैं और मेरी ज़बान


मैं माहिर-ए-ज़बान तो कभी न था
तुम क्यों मुझ से नाराज़ हुए जाते हो
मैं खुद से कहाँ खुश रहता हूँ
तुम क्यों शर्म से बेआवाज़ हुए जाते हो
क्या करूँ मैं इस न शुक्री जुबां का
जो न हो कहना वो कह ही जाती है
कभी बुलंद आवाजों में खो जाती है
कभी ख़ामोशी में बुलुंद हो जाती है
कभी सोचता हूँ जो चुप हो गया तो
कौन मुझसे हाल-ऐ-ज़िन्दगी पूछेगा
जो कह दूँगा मैं बात दिल की तो
है किसमे हिम्मत जो हालात से जूझेगा
कम्बख्त,
मैं और मेरी ज़बान
मुझे और मेरी ज़बान को साथ ही रहने दो
तुम न घबराओ, मेरा ये काम तो रहने दो
ये चुप भी रहती है और फिर भी कह जाती है
मेरी बर्दाश्त से जुड़ी है, उसी हिसाब से चल जाती है
मैं माहिर-ए-ज़बान तो कभी न था
तुम क्यों मुझ से नाराज़ हुए जाते हो