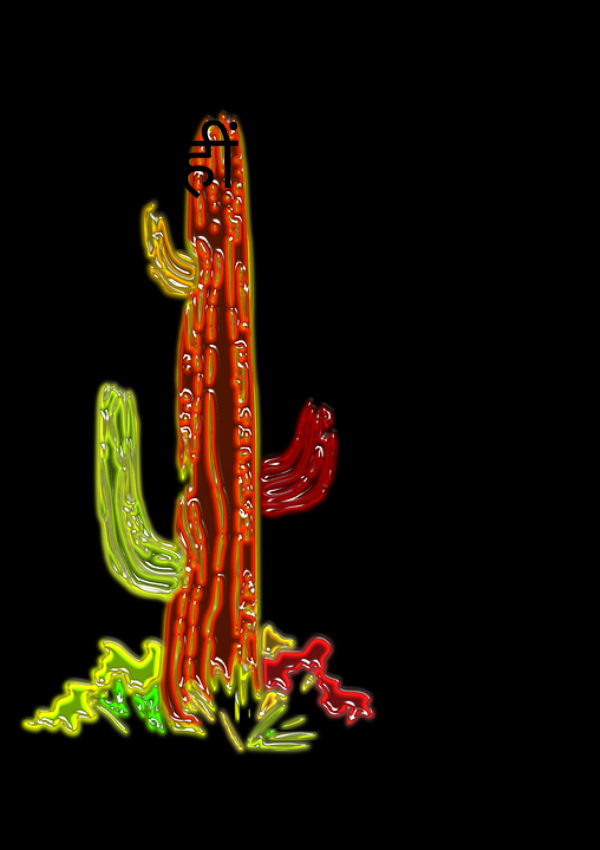■ ज़िंदगी कोई खेल नहीं ■
■ ज़िंदगी कोई खेल नहीं ■

1 min

244
काश! वो दिन फिर लौट आए कहीं से,
जब ज़िंदगी बताशा हुआ करती थी।
टूटे खिलौने, गुड़िया और ऑफिस से,
लौटे पिताजी से आशा हुआ करती थी।
जब सपने में घूम आया करते थे चाँद तक,
कंधों पर पापा की सवारी हुआ करती थी।
बचपन में खाये इमली की डलियों से,
खट्टी- मीठी सी महक अब भी आती है ।
आम के झुरमुट बुलाते हैं अपने पास,
कसैली निम्बोली भी शान से मुस्काती है।
बड़े होने पर जाना कि ज़िंदगी का,
बताशे से होता कोई मेल नहीं।
अब कवायद तेज है जंग जीतने की,
और ये ज़िंदगी यहां कोई खेल नहीं।