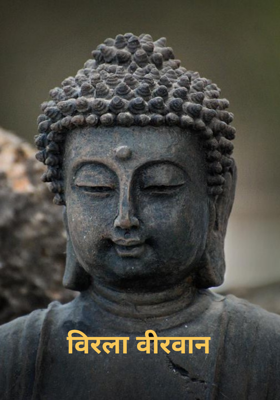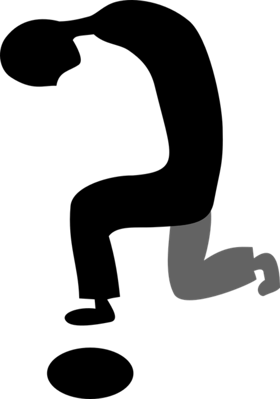कमबख़्त रोज़ आइना देखते हैं
कमबख़्त रोज़ आइना देखते हैं


कमबख़्त रोज़ आइना देखते हैं,
जो अक्सर झूठ के लिहाफ़ में सच रखते हैं,
वो कमबख़्त भी रोज़ आइना देखते हैं।
ज़मीर ज़िंदा होता है उनका भी,
सही और ग़लत का फ़र्क़ वो भी समझते हैं।
हर बार आइने में उनका ज़मीर उठ खड़ा होता है,
मगर कमबख़्त, इच्छाओं के बोझ तले —
उसे दबाकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं।
फिर बड़े सुकून से, झूठ के लिहाफ़ में
सच को परोसते हैं,
मगर कमबख़्त रोज़ आइना देखते हैं...
जो अक्सर झूठ के लिहाफ़ में सच रखते हैं,
वो कमबख़्त भी रोज़ आइना देखते हैं।
ये बेहया —
हर गाँव, कस्बे, शहर और उनके गली-मोहल्लों में मिलते हैं,
हर संस्था-संस्थान में मिलते हैं,
थाना-कचहरी में तो इनकी बहुतायत है।
ये हर जगह बसते हैं,
हर जगह मिलते हैं,
ये सर्वव्यापी हो गए हैं।
ये पहले झूठ के मीठे लिहाफ़ में
सच को लपेटते हैं,
फिर उसे छद्म भावों की तस्तरी में परोसते हैं।
लिहाफ़ और तस्तरी का चयन —
व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति के अनुरूप
चतुराई से करते हैं।
कमबख़्त जब-जब आइना देखते हैं,
ज़मीर इनका चीख़ उठता है —
मगर ज़मीर की चीख़ को ये अनसुना कर देते हैं,
उसे ही गुनहगार बता देते हैं!
क्योंकि —
इनकी इच्छाओं की अदालत में
इच्छाएँ ही वकील और इच्छाएँ ही जज हैं।
बेग़ैरत क्या जाने ज़मीर की सीरत को,
इसीलिए आइने में मुखौटा देखते हैं,
कमबख़्त रोज़ आइना देखते हैं...
जो अक्सर झूठ के लिहाफ़ में सच रखते हैं,
वो कमबख़्त भी रोज़ आइना देखते हैं।
-हेमंत "हेमू"