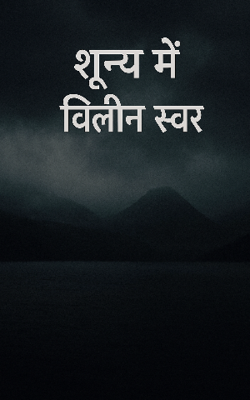अछूत सा मैं
अछूत सा मैं


बैठा था बस चुपचाप, बिन कहे या कुछ आस लगाए,
पास जो बैठा था कभी, आज क्यों दूरियाँ बढ़ाए?
वो रिक्शे की सीट नहीं थी, थी बस एक परख गहन,
नज़रों से कहा उसने—अब नहीं बचा कोई अपनापन।
न छुआ मैंने, न कुछ माँगा, न कोई शब्द उचारा,
सामान्य क्षण भी न माँगा, बस मौन में मन को सँवारा।
न पास गया, न लाँघी रेखा, बस अपनी मर्यादा साधी,
फिर भी मौन ने सुनाया न्याय — दोष तेरा था, तू ही अपराधी।
उसके मौन से नहीं, पर नज़रों से लहूलुहान हो गया,
जो सामने बैठ गया, बस वही रहा—दूर, पर देखता हुआ।
क्या इतना गिर गया हूँ उसकी नज़रों में?
या उसने कभी देखा ही नहीं मुझे अपनी आँखों से?