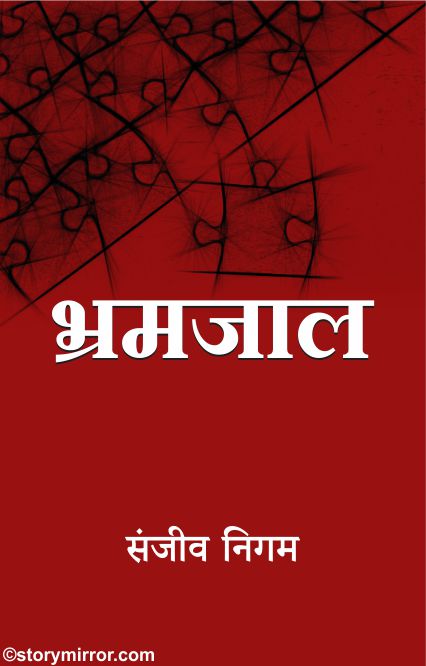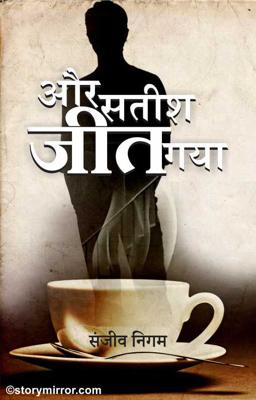भ्रमजाल
भ्रमजाल


इस शहर में मेरा घर यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण अक्सर वहाँ से गुज़रना होता था। उस वक़्त बरबस निगाहें वहाँ तिराहे पर एक ओर बिछी खाट पसरे उस थुलथुल से आदमी की तरफ उठ जाती थीं। मैला सा भगवा चोला पहने हुए उस व्यक्ति की कुछ अजीब सी शख्सियत थी। चेहरे पर छितरी हुई सी दाढ़ी मूंछें व सिर के ऊपर एक छोटी सी जूड़ी में बँधे हुए बाल, एकबारगी किसी भीख माँगने वाले सड़कछाप साधु जैसे व्यक्तित्व का आभास देते थे। किन्तु तभी नज़र उसके आस पास सड़क पर अपनी गृहस्थी का डेरा जमाए दो स्त्रियों व तीन चार बच्चों पर जाती थी जिससे सड़क के उस कोने में लटके टाट के पर्दे के साये तले एक संसार का आभास होता था।
एक बात का मुझे हमेशा ताज्जुब होता था कि मैं जब भी वहाँ से गुज़रता था उस बेडौल काया को यूँ ही खाट पर पड़े हुए देखता था। मैंने उसे कभी ठीक प्रकार से बैठा हुआ या खड़े होकर चलता हुआ नहीं देखा था। शायद मैं उसके इस अजीब से व्यक्तित्व की ओर बार बार ध्यान न देता यदि मुझे उसकी सूरत एक ऐसी सूरत से मिलती न दिखाई देती जो मेरे मन में अपना एक चोर स्थान बनाए बैठी थी। इसलिए वहाँ से गुज़रते हुए मेरी नज़र खुद ब खुद उसकी तरफ चली जाती थी और उसके चेहरे को यूं खँगालने लगती थी जैसे कोई बुज़ुर्ग अपने बचपन की एलबम में से कुछ भूले बिसरे चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा हो।
मैं अच्छी तरह से जानता था कि यह मात्र मेरा भ्रम है क्योंकि जिसकी मुझे तलाश थी वह आदमी जैसी दिखती ज़रूर थी पर थी वह एक औरत। मुझे तलाश थी अपनी सल्लो दद्दा की। हालाँकि उन्हें गायब हुए एक लम्बा अर्सा हो गया था। वे पुरानी दिल्ली के हमारे मौहल्ले का अपना घर छोड़ कर एक दिन न जाने कहाँ चली गई थीं, किसी को कुछ पता नहीं था। अतः दिल्ली से इतनी दूर इस शहर में अब उन्हें पाने की बात बेमानी है और फिर यदि वे सामने आ गईं तो क्या मैं उन्हें पहचान पाऊँगा? वैसे भी मैं तो उन्हें लगभग भुला ही बैठा था, न जाने क्यों वह आदमी मेरी आंखों के सामने आता था और सल्लो दद्दा के निराकार अस्तित्व को मेरे मस्तिष्क में पुनः साकार कर देता था।
सल्लो दद्दा हमारी ताईजी की लड़की थीं। उनकी अम्मा हमारी सगी ताईजी न होकर मौहल्ले के रिश्ते से ताईजी थीं। तब पुरानी दिल्ली में 'अंकल-आंटी' वाले कृत्रिम सम्बन्ध बनाने का रिवाज़ नहीं था। पास पड़ोस के लोगों में भी एक खानदान की तरह सम्बन्धों का स्पष्ट जुड़ाव हुआ करता था। इसी लिहाज़ से मैं सल्लो दद्दा के माता पिता को 'ताईजी-ताऊजी' कहा करता था। सल्लो दद्दा के पिता एक कपड़े के सेठ के यहाँ मुनीम थे तथा छोटी मोटी दलाली भी करते थे। हमारी अम्मा बताती थीं कि सल्लो दद्दा के होने से पहले ताईजी के एक के बाद एक तीन बच्चे जचगी में ही गुज़र गए थे। सल्लो दद्दा के पैदा होने से पहले ताईजी ने बहुत मन्नतें मानी थीं। पता नहीं उन मन्नतों का सर था या सल्लो दद्दा के कर्मों का पर सल्लो दद्दा जी गईं थीं। ताऊजी-ताईजी के सम्पूर्ण लाड़ प्यार का एकमात्र केंद्र थीं हमारी दद्दा। ताईजी ने शुरू से ही उन्हें लड़का बना कर रखा था। वे उन्हें लड़कों जैसे कपड़े पहनाती थीं और उनसे लड़कों की तरह ही बातें करती थीं। और तो और ताऊजी ने किसी तरह से जुगत बिठा कर उन्हें लड़कों के प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में भर्ती करवा दिया था। उस स्कूल में लड़कों की संगत ने सल्लो दद्दा के 'मैं आऊँगा - मैं जाऊँगा' आदि को बिल्कुल पक्का कर दिया था। सल्लो दद्दा खुद को पूरी तरह से लड़का ही मानती थीं।
में उनसे तीन साल छोटा था। मुझे उनकी सबसे पुरानी याद वह है जब मेरे द्वारा भूल से उन्हें दीदी कह दिए जाने पर उन्होंने एक झन्नाटेदार झापड़ मेरे गाल पर रसीद करते हुए कहा था, "कमबख्त लड़के और लड़की को भी नहीं पहचान सकता। मैं तेरा दद्दा हूँ, दद्दा, समझा।" उस दिन मैं उस बात को ऐसा समझा कि आज तक नहीं भुला पाया हूँ।
पूरे दिन धमाचौकड़ी मचाने वाली दद्दा मौहल्ले के सभी हमउम्र व छोटे बच्चों की मुखिया थीं। उनके सारे खेल व करतब लड़कों वाले होते थे। रोज़ शाम को वे गली में लड़कों के साथ क्रिकेट, पिट्ठू, गिल्ली डंडा या सोटम साटी खेलती हुई मिलती थीं। प्राइमरी के पश्चात वे सहशिक्षा वाले हमारे पब्लिक स्कूल में आ गई थीं किन्तु यहाँ भी उनका ग्रुप लड़कों के साथ ही रहता था।
लड़कियों से तो जैसे उन्हें एलर्जी सी थी। वे कभी उनके चिए चुरा लेती थीं तो कभी खेलने के गिट्टे छिपा देती थीं। स्कूल में बाकी सभी लड़कियाँ स्कर्ट पहना करती थीं केवल दद्दा लड़कों की तरह नेकर पहन कर जाती थीं।
लड़ाई में भी दद्दा बहुत तेज़ थीं। बात बात में उनका हाथ चल जाता था। मौहल्ले के कई लड़के उनके हाथ से पिटते रहते थे। किन्तु जब हमारे मौहल्ले के किसी लड़के का पड़ोस के किसी मौहल्ले के लड़के से झगड़ा हो जाता था तो दद्दा यहाँ के लड़कों की टोली लेकर वहाँ लड़ने जा पहुँचती थीं। एक बार में पतंग वाले के यहाँ से पतंग लेकर आ रहा था तो दूसरे मौहल्ले के एक लड़के ने मेरी पतंग छीन ली थी। मैं रोता हुआ घर लौट रहा था कि रास्ते में दद्दा मिल गईं। उन्होंने मुझे रोक कर पूछा, "क्यों रे, क्यों रो रहा है? "मैंने बताया, "मैं पतंग लेके आ रहा था, उसने छीन ली। "दद्दा ने पूछा, "किसने?" मैंने कहा, "दुलारे ने।" दद्दा बोलीं, "वो मुर्गों की गली वाला लौंडा। अच्छा यानि चीटियों के पर निकल आए हैं।" फिर ज़ोर से मुझसे कहा, "चुप हो साले। क्या लौंडियों की तरह से टसुए बहा रहा है। मैंने भी उस साले हरामी को पीट कर तेरी पतंग न निकलवाई तो मेरा नाम सल्लो नहीं।"
फिर वे मुझे साथ लेकर दुलारे के घर पहुंच गईं। वे सीधे उसकी छत पर गईं। जाते ही उन्होंने दुलारे के कस कर दो तीन हाथ जमाए और वहाँ रखी सारी पतंगे उठा कर मुझसे बोलीं, "चल बिट्टू, भाग यहाँ से।" और इससे पहले कि दुलारे की आवाज़ सुन कर कोई आता, दद्दा मेरा हाथ पकड़ कर भागते हुए अपने मौहल्ले में आ गईं। इन चक्करबाजियों में कभी कभी दद्दा खुद भी पिट जाती थीं। उन्हें यदि कभी कोई ज़रा सी भी चोट लग जाती थी तो ताईजी पूरा मौहल्ला सिर पर उठा लेती थीं।
कुछ दिनों बाद दद्दा में हमें एक परिवर्तन सा लगने लगा था। वह हर महीने में तीन चार दिनों के लिए बीमार हो जाती थीं। उन्हें खेलने के लिए बुलाने उनके घर जाते थे तो ताईजी हमें बाहर से ही भगा देती थीं। जब दद्दा ठीक हो जाती थीं तो फिर पहले की तरह उछल कूद में लग जाती थीं। पढ़ने में दद्दा का मन शुरू से न था, अपनी इस बीमारी के कारण एक बार स्कूल में उन्हें अपने सहपाठियों की हँसी का सामना करना पड़ा था। बस उस दिन दद्दा स्कूल छोड़ कर जो भागीं तो फिर कभी स्कूल वापस नहीं लौटीं।
धीरे धीरे उम्र के कुछ उभार दद्दा पर भी दिखने लगे थे पर दद्दा ने जैसे उन्हें अपनी ओर से पूरी तरह से नकार रखा था। वे तो ठीक किसी दादा की तरह अकड़ कर चलती थीं। वही अपने हमउम्र लड़कों की तरह से पैंट शॉर्ट पहनना, लेटेस्ट स्टाइल के बाल कटवाना व कभी कभी छिप कर सिगरेट पीना। उनसे छोटे मेरे जैसे लड़कों पर तो उनका रौब पूरी तरह से ग़ालिब था। उन दिनों हमारे की जवां लड़कियों और बहुओं को बाज़ार या सिनेमा ले जाने की ज़िम्मेदारी दद्दा खूब निभाती थीं। किसी पड़ोसन भाभी ने उन्हें 'लालाजी ज़रा सुनना' कह कर बुलाया नहीं कि सल्लो दद्दा दौड़ पड़ीं अपनी साईकल उठा कर अपनी भाभी का हुकुम बजा लाने को।
लड़कपन तक तो सल्लो दद्दा के लड़केपने को सबने खूब चला लिया पर आते हुए परिवर्तनों की छाप सल्लो दद्दा या उनके माता पिता को न दिखाई देती हो, दूसरों को तो साफ दिखाई देती थी। मौहल्ले के अन्य लोगों की आँखों में अब उनका यूँ लड़का बना रहना खटकने लगा था। उन्होंने अपने लड़कों को दद्दा के साथ से दूर कर दिया था। बेचारी दद्दा को यह समझ नहीं आता था कि कल के उनके ये दोस्त आज उन्हें अकेला छोड़ कर कैसे घूमें चले जाते हैं। अकेले में उनसे बात करने में क्यों कतराने लगे हैं? दद्दा तो अब उसी तरह से रात को रामावतार के चबूतरे पर गप्प-गोष्ठी के लिए आकर बैठ जाती थीं पर उनके होते हुए वहाँ अब कोई दूसरा नहीं आता था। तब अकेले बैठे बोर होती दद्दा राह चलते जानकारों को रोक कर कुछ बातें कर अपना समय गुज़ार देती थीं। ऐसे ही एक दिन रात को दद्दा को मैं आता हुआ मिल गया। दद्दा ने मुझे रोक कर पूछा, "क्यों रे बिट्टू, आजकल तुम लोग यहाँ गप्पें मारने के लिए क्यों नहीं आते हो?” मैंने अचकचा कर कहा, "दद्दा वो बात ये है कि आजकल सब पर पढ़ाई का बड़ा बोझ है। टाईम ही नहीं मिलता है। "दद्दा ने दूसरी तरफ मुँह करके कहा, "सही कहता है यार, अपन ने तो किताबों को बहुत पहले ही आग लगा दी थी। अब तुम पढ़े लिखें के मुँह क्या लगें?" उसके बाद से दद्दा ने वहाँ बैठना बंद कर दिया था।
धीरे धीरे उनके जीवन में खालीपन का घेरा बढ़ता जा रहा था। हमेशा साथियों से घिरी रहने वाली दद्दा इस अकेलेपन से तालमेल नहीं बैठा पा रही थीं। उनकी चुप्पी बढ़ने लगी थी। हम सब जीवन में अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हो गए थे। ऐसे में किसे यह सोचने की फुर्सत थी कि कोई एक है जो किसी छत पर अकेले पतंग उड़ाते हुए हम लोगों के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। अपना समय काटने के लिए दद्दा अब कई बार मौहल्ले के छोटे बच्चों को साईकल चलाना या पतंग उड़ाना सिखाती रहती थीं।
कुछ समय बाद मौहल्ले में शादियों का दौर शुरू हुआ। एक एक करके दद्दा के साथ के सभी लड़के लड़कियाँ ब्याहते गए। ताऊजी ताईजी भी जैसे वास्तविकता का उजाला चेहरे पर पड़ने पर हड़बड़ा कर जागे। पर तब तक दद्दा का खुद को लड़का समझने का भ्रम अपने आप में एक सच्चाई बन चुका था। हालत ये थी कि किसी लड़के से शादी की बात सोचना भी उनके लिए असम्भव था और किसी लड़की से उनकी शादी हो नहीं सकती थी।
शुरू की कुछ शादियों में दद्दा ने भाग लिया था पर थोड़े समय के बाद शादी तो क्या किसी भी सामाजिक समारोह में जाना बंद कर दिया था। लोग ताऊजी-ताईजी को ताने देते थे कि 'जवान लड़की को घर पर बैठा रखा है, भला लड़का समझने से भी कोई लड़का बन सकता है?’ ताईजी ताऊजी दद्दा पर हर तरह से दवाब डालते थे पर दद्दा हर बार यही कह देती थीं, सभी लड़के शादी थोड़े ही करते हैं। मैं भी कुँवारा रहूँगा।
इसी तरह से दिन बीतते गए और दद्दा के अकेलेपन की उम्र बढ़ती गई। अब उनके कटे बालों में काफी सफेदी झलक आई थी। उनसे छोटे हम लोग भी ब्याह शादी करके अपनी अपनी दुनिया में रम गए थे। दद्दा का अस्तित्व हम लोगों के लिए लगभग समाप्त सा ही हो गया था।
एक दिन अचानक ताईजी गुज़र गईं। उस दिन दद्दा खूब रोई थीं। मैंने पहली बार दद्दा को रोते हुए देखा था। उन्हें समझाते हुए मैंने कहा था, "सब्र करो दद्दा, तुम तो बहुत हौसले वाले हो।" दद्दा ने आँसू भरी आँखों से मुझे देखा और मेरे कंधे पर सिर टिका दिया था। उनका रोना तब भी नहीं रुका था। शायद उस दिन शरीर के सन्दूक में सबसे नीचे छिपा कर रखी गई भावनाओं की कुछ रेज़गारी दद्दा के हाथ से टकरा गई थी।
ताऊजी और दद्दा, घर में दो प्राणी ही रह गए थे। दोनों का अपना अपना अकेलापन था। शायद इसी अकेलेपन से डर कर वे दोनों अब आपस में खूब झगड़ा किया करते थे। बाहर तक उनके झगड़े की आवाज़ें खूब सुनाई देती थीं। छोटे छोटे घरेलू काम तक उन दोनों को लड़ने का अवसर देते रहते थे। पुराना मौहल्ला था इसलिए लोग लिहाज़ में ये सब बर्दाश्त करते रहते थे। उनके घर से सभी लोगों ने अपनी दूरियां बढ़ा ली थीं। कोई रिश्तेदार वगैरह भी आता न दिखता था। अब उनके घर तो में भी न जाता था किन्तु दद्दा कभी बाहर मिल जाती थीं तो कुछ बातें ज़रूर हो जाती थीं।
फिर एक दिन ताऊजी भी चल बसे। ताईजी के मरने पर बिलख बिलख कर रोने वाली दद्दा इस बार एकदम शांत थीं, हालाँकि वहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक ही चिंता थी कि, 'अब अकेले उनका जीवन कैसे कटेगा?’ ताऊजी का सारा क्रियाकर्म एक लड़के की तरह से खुद दद्दा ने किया था। आवश्यक रस्में पूरी होने के बाद 'दद्दा' का प्रश्न सामने आया। रिश्तेदारों के अनमनेपन व दद्दा की उनके साथ जाने की अनिच्छा ने उनका वहीं रहना तय कर दिया था।
दद्दा अपनी अधेड़ावस्था चौखट तक ही पहुंची थीं। सामने काफी ज़िन्दगी पड़ी थी। उनकी घर सम्पत्ति का हिसाब देखा गया तो पाया गया कि ताऊजी वह एक छोटा सा मकान और कुछ हज़ार रुपये ही छोड़ कर गए हैं। यह निर्णय लिया गया कि मौहल्ले के प्रत्येक घर से बारी बारी दद्दा को सुबह शाम खाना पहुँचा करेगा।
ग़र्मी के उस माहौल में बैठे समाजियों ने तब लम्बे लम्बे हुंकारे भरे थे, पर कुछ ही दिनों में असलियत सामने आने लगी थी। एक रात मैंने दद्दा को अपने चबूतरे पर बैठा पाया तो पूछा, "क्यों दद्दा, आज इधर कैसे?" दद्दा ने जल्दी से कहा, "बहुत भूख लग रही है। सुबह से कोई खाना ही नहीं लाया। बहू से कह कर खाना खिलवा दे न यार।" बचपन से स्वाभिमानी दद्दा के याचना भरे स्वर ने मुझे भीतर तक झिंझोड़ दिया था। दद्दा को उस दिन खिलवाते हुए मैं स्वयं अजीब से ख्यालों में डूबा हुआ था।
उसके बाद जब तक में वहाँ रहा था नियम से दोनों वक़्त का खाना दद्दा के घर पहुँचा आया करता था। फिर मेरा ट्रांसफर दिल्ली से आगरा हो गया था। जिस दिन मैं वहाँ से चला था दादा बहुत मुस्काई थीं, खूब दुआएँ दी थीं उन्होंने और कहा था, "मेरी चिंता न करना। मैं खुद अपनी देखभाल कर लूँगा। तू अपना और बच्चों का ख्याल रखना।" मुझे दद्दा की वास्तव में बहुत चिंता थी, पर मन में कहीं यह ख्याल भी था कि जैसे मैंने दद्दा का ध्यान रखा है वैसे ही मेरे पीछे कोई दूसरा दद्दा का ख्याल रख लेगा। लेकिन दो तीन महीने बाद ही जब में किसी काम से वहाँ वापस आया तो पता चला कि किसी दूसरे ने दद्दा का ख्याल न रखा था और वे एक दिन बिना किसी से कुछ कहे उस मौहल्ले को छोड़ कर न जाने कहाँ चली गई थीं। उनके मकान पर उनके एक दूर के रिश्तेदार ने कब्ज़ा कर लिया था।
छह सात साल आगरा में रहने के बाद, कुछ साल पहले मेरा ट्रांसफर इस शहर में हुआ था और अब दादा की शक्ल से मिलते जुलते उस आदमी को देख कर अक्सर दद्दा की याद हो आती थी। फिर एक दिन स्थानीय अखबार में बहुत चौंकाने वाली खबर पढ़ी, बिल्कुल अविश्वसनीय सी। उसमें लिखा था कि यूनिवर्सिटी के तिराहे पर जो आदमी दो औरतों व बच्चों के साथ डेरा जमाए हुए है वह कोई आदमी नहीं है बल्कि औरत है जोकि शारीरिक परिवर्तनों के कारण आदमी जैसी देखने लगी है। उसके साथ रहती औरतें व बच्चे उसके अपने नहीं हैं, बल्कि वह तो अपनों द्वारा तिरस्कृत लोगो का एक छोटा समाज है जोकि सभी तत्व मौजूद होने के कारण खुद ब खुद एक गृहस्थी बन गया था। उस पुरुषनुमा औरत की हैसियत उस परिवार में एक पुरुष की ही थी।
यह समाचार पढ़ते ही मेरे सामने दद्दा की छवि कौंध गई। अरे, हो न हो, ये कहीं दद्दा ही तो नहीं? और मैं 'पा लिया, पा लिया' की उत्तेजना से भर कर झपट कर घर से निकल पड़ा उस तिराहे की ओर।
वहाँ पहुंच कर कुछ दूर रुक कर मैंने उस आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे को गहराई से परखा और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये तो वाकई दद्दा ही हैं। में खुशी से भर कर उनकी ओर बढ़ना ही चाहता था कि अचानक एक प्रश्न मेरे मन में उभरा, 'मैं इतनी बार यहाँ से गुज़रा हूँ। दद्दा ने मुझे कई बार देखा होगा। और पहचान भी लिया होगा। फिर उन्होंने मुझे कभी आवाज़ क्यों नहीं दी? ..... .. क्या इसलिए कि मैं उनके उस अतीत का हिस्सा का हिस्सा हूँ, जिसे वह कभी न लौटने वाली दूरी पर छोड़ आई हैं।'
इस विचार ने उनकी तरफ बढ़ते मेरे कदमों को घर की ओर मोड़ दिया था। घर लौटते वक़्त मुझे यह सोच कर संतोष था कि इस रूप परिवर्तन ने दद्दा के भ्रमजाल में पूर्णता के एहसास का जो रंग भरा है उसे फीका करने का दोष कम से कम मेरे सिर पर नहीं है।